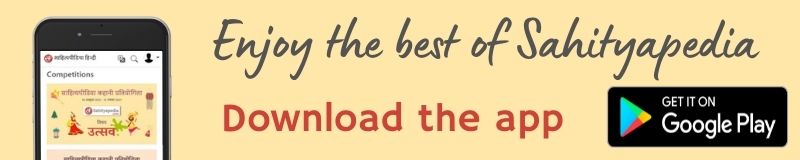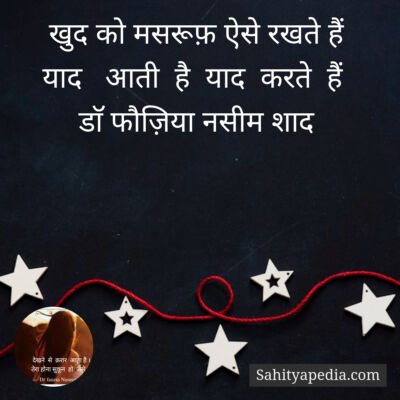भारत की न्यायपालिका; न्याय का मंदिर या भ्रष्टाचार का गढ़?: अभिलेश श्रीभारती

साथियों,
आप मेरे इस आलेख के शीर्षक को देखकर पूछेंगे कि यह कैसा बेतुका शीर्षक है?
लेकिन रुकिए?
आपका सवाल लाजमी है?
क्योंकि हम यह भी जानते हैं की अभी कुछ ही देर में आपका निर्णय बदलने वाला है क्योंकि हम आपको जिन विषय से अवगत कराने जा रहे हैं वह एक महत्वपूर्ण विषय है।
साथियों,
हमने हमेशा से कहा है कि हम एक ऐसे महान भारतवर्ष के नागरिक हैं जहां लोकतंत्र और गणतंत्र के शासन प्रणाली देश की महत्वपूर्ण भूमिका को निर्देशित करती है।
लेकिन अफसोस के साथ मुझे लिखना पड़ रहा है कि हमारे देश की कुछ राजनीतिक पार्टियों के नेता और कुछ लोग हमारे देश के लोकतांत्रिक और गणतांत्रिक ढांचा को दिमक की तरह दिन प्रतिदिन खोखला करते जा रहे हैं।
अब देखिए ना,
भारत में लोकतंत्र की तीन प्रमुख शाखाएँ हैं—विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। विधायिका कानून बनाती है, कार्यपालिका उसे लागू करती है, और न्यायपालिका न्याय सुनिश्चित करती है। परंतु जब न्यायपालिका पर ही सवाल खड़े होने लगें, जब न्याय का मंदिर ही भ्रष्टाचार का अड्डा बन जाए, तो लोकतंत्र के भविष्य पर गंभीर संकट मंडराने लगता है।
इसलिए
आज भारत की न्यायपालिका पर सवाल उठ रहे हैं, और ये सवाल केवल आक्रोश से उपजे नहीं हैं, बल्कि सच्चाई पर आधारित हैं। सबसे बड़ा प्रश्न यह है कि क्या भारतीय न्यायपालिका संविधान से ऊपर है? क्या न्यायाधीशों को कानून से परे रखा गया है? अगर प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति और राज्यपाल के पास भी सीमित अधिकार हैं, तो फिर न्यायाधीशों को इतनी असीमित शक्तियाँ क्यों दी गई हैं कि वे कानून के शिकंजे से बच निकलें?
भारतीय न्यायपालिका में जजों को इतनी विशेष सुरक्षा प्राप्त है कि न तो केंद्र सरकार और न ही राज्य सरकार उन्हें निलंबित कर सकती है। पुलिस, सीबीआई या प्रवर्तन निदेशालय (ED) को भी किसी जज के घर जाने से पहले चीफ जस्टिस की अनुमति लेनी पड़ती है। इसका अर्थ यह है कि यदि कोई न्यायाधीश भ्रष्टाचार में लिप्त पाया जाता है, तो भी उसके खिलाफ कार्रवाई करना लगभग असंभव हो जाता है।
ऐसा ही एक मामला हाल ही में जस्टिस वर्मा का सामने आया, जब उनके घर में आग लगी और फायर विभाग के एक कर्मी ने उसका वीडियो बना लिया। यह वीडियो सामने आते ही सच्चाई उजागर हो गई कि उनके घर में बेहिसाब नकदी भरी पड़ी थी। लेकिन इसके बावजूद सुप्रीम कोर्ट और दिल्ली हाईकोर्ट ने मामले को तुरंत “अफवाह” करार दे दिया और न्यायाधीश को क्लीन चिट दे दी। सवाल यह उठता है कि अगर एक आम नागरिक पर भ्रष्टाचार का आरोप लगता है, तो जांच एजेंसियाँ तुरंत सक्रिय हो जाती हैं, मगर जब एक न्यायाधीश पर आरोप लगता है, तो उसे तुरंत बचाने की कवायद क्यों शुरू हो जाती है?
जस्टिस वर्मा के कुछ पुराने फैसले उठाकर देखें तो यह साफ हो जाता है कि न्यायपालिका के कुछ हिस्से पूरी तरह से राजनीतिक प्रभाव में काम कर रहे हैं। उन्होंने झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के खिलाफ सीबीआई जांच पर रोक लगा दी थी। इसी तरह, दिल्ली दंगों में शामिल 11 आरोपियों को पर्याप्त सबूत होने के बावजूद रिहा कर दिया, जबकि निचली अदालत ने उन्हें उम्रकैद की सजा सुनाई थी। क्या यह फैसले स्वतः लिए गए थे, या फिर इनके पीछे कोई राजनीतिक या आर्थिक सौदेबाजी थी?
एक स्वस्थ लोकतंत्र में न्यायपालिका का स्वतंत्र होना अनिवार्य है, लेकिन स्वतंत्रता का अर्थ यह नहीं कि वह जनता के प्रति जवाबदेह न हो। जब विधायिका और कार्यपालिका की गतिविधियों पर जनता और मीडिया की नजर रहती है, तो न्यायपालिका इससे अछूती क्यों रहे? अगर जज भी भ्रष्टाचार में लिप्त होते हैं, तो उनके खिलाफ कार्रवाई के लिए कोई स्पष्ट प्रक्रिया क्यों नहीं है?
आज न्यायपालिका में सुधार की आवश्यकता है। हमें ऐसे तंत्र की जरूरत है जो न्यायपालिका को पूर्ण रूप से स्वतंत्र रखते हुए भी उसे जनता के प्रति जवाबदेह बनाए। जजों की नियुक्ति से लेकर उनके आचरण तक की निगरानी की एक प्रभावी व्यवस्था होनी चाहिए। यह भी आवश्यक है कि यदि किसी न्यायाधीश पर भ्रष्टाचार का आरोप लगता है, तो उसकी निष्पक्ष जांच हो और यदि दोष सिद्ध होता है, तो उसे भी वही सजा मिले जो एक आम नागरिक को दी जाती है।
अगर न्यायपालिका भ्रष्टाचार से मुक्त नहीं होगी, तो न्याय की उम्मीद कैसे की जा सकती है? जो व्यवस्था न्याय देने के लिए बनाई गई थी, अगर वही भ्रष्टाचार और राजनीतिक स्वार्थों का अड्डा बन जाए, तो यह समाज के लिए घातक सिद्ध होगा। भारत की न्याय व्यवस्था को पारदर्शी और जवाबदेह बनाना आज समय की सबसे बड़ी मांग है, ताकि न्याय केवल अमीरों और ताकतवर लोगों की बपौती न बनकर हर नागरिक के लिए समान रूप से उपलब्ध हो।
नोट: यह लेखक के अपने निजी विचार है।
✍️लेखक ✍️
Abhilesh sribharti अभिलेश श्रीभारती
सामाजिक शोधकर्ता, विश्लेषक, लेखक