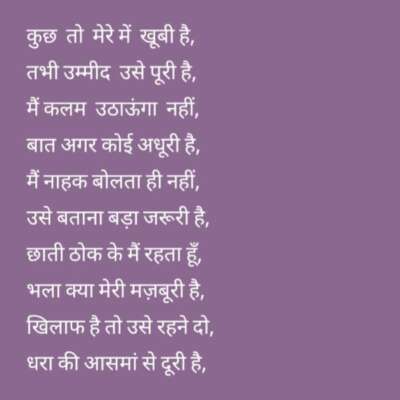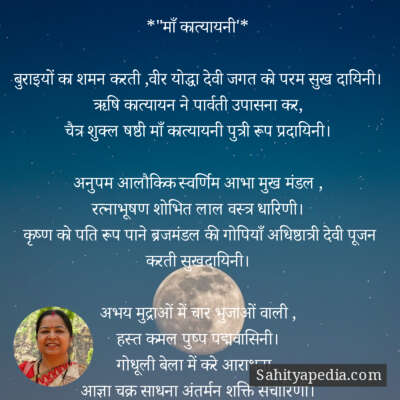■अतीत का आईना■

#एक_धरोहर-
■ जो हो चुकी है ध्वस्त।
● अतीत बना एक सदी का स्वर्णिम अध्याय।
【प्रणय प्रभात】
सबसे पहले नीचे दिए गए चित्र को देखिए। आज मलबे के ढेर में बदली यह जगह, जो सामान्य भू-खंड सी दिख रही है, उतना साधारण नहीं है। इसके साथ मेरे जैसे न जाने कितने लोगों की यादें जुड़ी थीं, जो अब दिल-दिमाग़ तक ही रह जानी हैं। या यूं समझिए, रह गई हैं। आज उजाड़ सी दिखने वाली यह जगह कल एक आलीशान भवन का रूप धारण कर लेगी। लगभग डेढ़ दशक तक सुनसान रहे हमारे इस क्षेत्र में कुछ महीनों बाद नगर के एक प्रतिष्ठित परिवार का आगमन हो जाएगा। वीरानगी के साए से लिपटे एक शांत व पुराने क्षेत्र का क्लान्त सा हो चुका यह उपक्षेत्र पुनः आबाद हो जाएगा। लेकिन वो अलौकिक रौनक कभी नहीं लौटेगी, जो यहां की अमिट पहचान रही। उस दौर में, जब साधन-संसाधनों के व्यापक अभावों पर आत्मीयता व आनंद के भाव हावी थे।
एक तिराहे की तीन दिशाओं में डामर की जर्जर सड़कें, पुराने लेकिन खुले-खुले घरों की क़तारें। सड़कों पर बारह महीने खेल-कूद में लगे बच्चों के दल, यत्र-तत्र आवारा जानवर व मवेशी। बरसाती दिनों में किचकिचाती सड़कों से उठती गोबर की गंध और हर पर्व-उत्सव को लेकर पूर्व तैयारी व भागीदारी का उत्साह इस उपक्षेत्र को औरों से अलग बनाता था। यहीं मना करता था एक महोत्सव। जिसमें सब खिंचे चले आते थे। भादों के भीगे हुए महीने में गाजे-बाजे व धूम-धड़ाके से धारने वाले भगवान मंगलमूर्ति अपने साथ लोक-रंगों का एक इंद्रधनुष लाते थे और तमाम सारी खुशियां देकर चले जाते थे। अगले साल फिर से आने की आस दिला कर।
उक्त पंक्तियों को आप इस संस्मरणात्मक आलेख का एक सुखद व सकात्मक पक्ष मान सकते हैं। जहां तक मेरा वैयक्तिक आभास है, वो अत्यंत दुःखद व नकारात्मक है। जो आज के लेखन का मुख्य केंद्र है। केंद्र में है एक भवन, एक परम्परा, एक उत्सव और उससे जुड़ा एक स्वर्णिम सा अतीत। जिस पर आंशिक के बाद अब पूर्ण-ग्रहण लग चुका है। लेख को आद्योपांत पठन के बाद ही कुछ या बहुत कुछ समझ पाएंगे आप। कुछ को बुरा लग सकता है। बुरा लगना स्वाभाविक भी है। जिस से मेरी सहमति-असहमति का कोई सरोकार नहीं। सबकी अच्छी-बुरी प्रतिक्रियाएं सहज, सहर्ष शिरोधार्य।
आज बिना नाम वाला एक विस्तृत आलेख पहली बार लिख रहा हूँ, तथापि संकल्पित हूँ उन परिवारों के बारे में पृथक से लिखने के लिए, जिन्होंने एक आयोजन के पौधे को रोपा, सींचा व छतनार वृक्ष बना दिया। विशेष रूप से मुजुमदार परिवार के अग्रणी, जिन्हें शासकीय व पारिवारिक व्यस्तताओं के बाद भी मैने हर मोर्चे पर जूझते अपनी आंखों से देखा। वो भी दो-चार साल नहीं, बल्कि आधी सदी तक। फर्श-दरी बिछाने व बिछवाने से लेकर उठाने व उठवाने तक। अतिथियों के सत्कार से लेकर श्रोताओं तक के लिए जलपान आदि की व्यवस्था पारिवारिक सहयोग से करते हुए। एकमेव अग्रपुरुष के रूप में। जो मेरे पिता के समकक्ष सहकर्मी होने के कारण ही नहीं, प्रेरक व प्रोत्साहक होने की वजह से भी परम् श्रद्धेय व पितृवत रहे हैं।
स्पष्ट कर दूं कि आलेखन का उद्देश्य न किसी को महिमा-मंडित करने का है, न किसी की भावना को आहत करने का। मन्तव्य मात्र अपने आंतरिक उद्वेग को शांत करना व साझा दायित्वों पर छोटा सा प्रश्न-चिह्न खड़ा करना भर है। वो भी सामाजिक राजनीति के आदी गिने-चुने विघ्न-संतोषियों की सोच पर, जो एक पौधे का रोपण कर पाने की सामर्थ्य न होने के बाद भी एक हरे-भरे विटप को धराशाई करने जैसा अक्षम्य अपराध करते हैं। वो भी मात्र चार दिन की महत्ता या गुरुता अर्जित करने की मंशा से। जिसका खामियाज़ा एक परिवार नहीं, बिरादरी भोगती है। जुड़ाव रखने वाले भी।
वस्तुतः प्रकरण एक भद्र परिवार के स्वामित्व वाली सम्पत्ति और उससे जुड़ी सार्वजनिक लोक-भावनाओं का है। उस विरासत का है, जो कुछ गौरवपूर्ण सदियों की “अचल” साक्षी रही, किंतु “अटल” नहीं रह पाई। वो साढ़े आठ से नौ दशक तक एक समृद्ध समाज की गरिमामयी सांस्कृतिक विरासत की पोषक रही एक सामन्तकालीन इमारत थी। जिसका प्रथम तल प्रतिवर्ष एक पखवाड़े के लिए सामाजिक धरोहर बन जाता था। एक 11 दिवसीय विशेष महोत्सव के कारण। जिसकी प्रसिद्धि सार्वजनिक रूप से श्री गणेशोत्सव के रूप में थी। एक पारंपरिक व धार्मिक पर्व को सामाजिक व सांस्कृतिक महोत्सव बनाने में मुख्य भूमिका उक्त भवन-स्वामी और परिवार की रही। जिसे हर स्तर पर समर्थन व सहयोग समाज के एक-एक परिवार के प्रत्येक सदस्य का मिला। जिसने एक सामान्य परिपाटी को महान परम्परा बना दिया।
आज मेरा मन अनगिनत नामों के उल्लेख का है, पर मैं ऐसा चाह कर भी नहीं कर पा रहा हूँ। कारण है अनेक नाम छूटने का अंदेशा। जो उन महानुभावों व उनके परिजनों का अपमान होगा, जिन्होंने तन-मन-धन से एक परम्परा को परम् वैभव देने में पूर्ण मनोयोग से यथासामर्थ्य योगदान दिया। दक्षिण भारतीय मान्यताओं तथा मातृ-सत्तात्मक विधानों वाले “महाराष्ट्र समाज” के सभी तत्कालीन परिवारों को आज अंतर्मन से नमन्। उन पितृ व पितामह-तुल्य विभूतियों, मातृशक्तियों का भावात्मक स्मरण, जिन्होंने सतत 11 दिवस तक विशेष भूमिका का निर्वाह स्वप्रेरित भावना के साथ स्वस्फूर्त रह कर वर्षों तक किया। स्नेह-भाव उस बाल व किशोर पीढ़ी के लिए भी, जो आज समकालीन होने के कारण मेरे समकक्ष हैं। इनमें तमाम विविध वजहों से देश के अन्यान्य नगरों के वासी हो चुके हैं। कुछ अब भी स्थानीय निवासी हैं और तीसरी पीढ़ी के रूप में अपने-अपने परिवारों के मुखिया बन चुके हैं। सभी बहिन-बेटियों को जीवन के 15वें संस्कार (विवाह) का पालन करते हुए अपनी जन्मभूमि एक न एक दिन छोड़नी ही थी, जो बरसों पहले छोड़ चुकी हैं। समाज के रीति-रिवाजों के अनुसार उपनाम के साथ-साथ मूल नाम तक बदलते हुए। जिन्हें सोशल मीडिया के विशाल प्लेटफॉर्म पर तलाश पाना भूसे के ढेर से सुई तलाशने जैसा है। कामना कर सकता हूँ कि जो जहां हैं, गणपति बप्पा के आशीर्वाद से चिर-आनंदित रहें। दावे के साथ भरोसा दिला सकता हूँ कि तीन पीढ़ियों के एक-एक सदस्य का मूल नाम हृदय की वीथिका में है और तत्कालीन चेहरा, स्वभाव और गुण मानस-पटल पर आज भी अंकित हैं। वजह बस इतनी सी, कि न मैं बदलते वक्त के साथ बदलने वालों में हूँ, न भूलने-भुलाने वालों में। होता तो यह वृत्तांत न लिख रहा होता। सारे काम-धाम छोड़ कर।
आगे कुछ लिखने से पहले विशेष साधुवाद उन्हें देना चाहता हूँ, जो शासकीय सेवक के रूप में एक छोटे-बड़े अंतराल तक उक्त समाज के सम्मानित क्षेत्रीय सदस्य व मेरी नगरी के गणमान्य नागरिक रहे। अपनी सामाजिक भागीदारी के बूते मूल निवासी न होकर भी अग्रगण्य रहे परिवारों को पुनश्च: धन्यवाद। धन्यवाद इसलिए भी, कि वे इस नगरी की मिट्टी से जुड़े रिश्तों व लगावों को आज भी जीवंत बनाए हुए हैं। इसके विपरीत धिक्कारना भी चाहता हूँ, कुछ लोगों को। जो पीढ़ी-दर-पीढ़ी इसी नगरी के वासी होकर भी यहां की देन के प्रति कृतज्ञ नहीं रह पाए। किसी न किसी नगर से जुड़ी पहचान को उपनाम में सम्मिलित करने वाले एक महान समाज के चंद लोग अन्यत्र जा कर क्या बसे, अजनबी से हो गए सदा के लिए। सम्वेदनहीनता के साथ सब कुछ भुला कर। कुछ की आंखें पद-प्रतिष्ठा व नगरीय चमक-दमक ने धुंधली कर डाली, तो कुछ की स्मृतियों को अगली पीढ़ी की सफलता ने दर्प की गर्त में धकेल दिया। विडम्बना की बात यह है कि उनके नाम के साथ अब “श्योपुर” का उल्लेख सोशल मीडिया तक पर नहीं है। सोच उनकी अपनी। जिसके बारे में अधिक कुछ लिखना भी शब्द, समय व श्रम व्यर्थ करना ही है। पुनः लौटता हूँ मूल विषय के केंद्र से जुड़ी उस इमारत पर। जो काल के कपाल पर कम से कम दो-तीन सदी अडिग रहने के बाद गत एक सप्ताह में ध्वस्त हो चुकी है। वो भी उन दिनों में, जब उसे रंग-रोगन कर सजाया-संवारा जाता था। विशेष प्रयोजन के लिए।
आज देश-दुनिया में दुःख-हर्ता, सुखकर्ता श्री गणेश जी के जन्मोत्सव की धूम है और 11 दिवस तक चलने वाले गणेशोत्सव का श्रीगणेश गत दिवस हो भी चुका है। मैं आपको डेढ़ दशक पूर्व तक की उस गौरव-गाथा से अवगत कराना चाहता हूँ, जो नव-निर्माण के लिए ढहाई जा चुकी एक इमारत के कण-कण में सुगंध बन कर रची-बसी रही। वो भी 10-20 नहीं बल्कि पूरे 80-90 साल तक। जिसके एक बड़े कालखंड का साक्षी मैं स्वयं रहा हूँ। वर्ष 1974 में कस्बे के सबसे शांत व समन्वित क्षेत्र “पंडित पाड़ा” का स्थायी निवासी बनते समय मैं मात्र 06 वर्ष का था। तब से लेकर अधेड़ावस्था के आरंभिक चरण तक मैं उस उत्सव का अंग रहा, जो “मुजुमदार साहब का बाड़ा” कहलाने वाले उक्त भवन को एक सिद्ध-स्थल बनाने वाला रहा। कला, संस्कृति व साहित्य के इस बहुरंगीय उत्सव में मेरी सहभागिता एक रसिक श्रोता से लेकर संचालक व संयोजक रचनाकार तक के रूप में रही। जिसके बदले मान-सम्मान व पहचान से अधिक प्राप्ति प्रेरणा व प्रोत्साहन की हुई।
मुझे कृतज्ञता के साथ यह लिखने में कोई संकोच नहीं, कि मुझ में कला व संस्कृति के प्रति असीम अनुराग का अंकुरण व पल्लवन इसी भवन से हुआ। कभी बारिश की फुहारों तो कभी बिजली की चमक के बीच एक से बढ़ कर एक पारंगत कलाकारों को रात-रात भर सुनने के बाद। वो भी बेहद क़रीब से, एक आत्मीय व पारिवारिक से परिवेश में। कलाकारों व श्रोताओं के बीच सान्निध्य व सामीप्य का श्रेय इस उत्सव परिसर के सीमित आकार को भी दे सकता हूँ। जो बहुत बड़ा न होते हुए भी कभी किसी को छोटा नहीं लगा। जो हमेशा समरसता व सामाजिकता का भाव उत्पन्न करता रहा। दर्ज़न भर संकरी सीढ़ियों से ऊपर पहुंचने के बाद बाएं हाथ पर तीन कलात्मक स्तंभों वाला दालान और उसके सामने उल्टे व्ही आकार के टीन-शेड से कवर्ड एक चौरस प्रांगण। शेड से लटके दो अदद पंखे। तीन ओर द्वार और एक छज्जे वाला परिसर। खुला-खुला सा, हवा और रोशनी से भरपूर। जिसके एक तिहाई हिस्से में कलाकारों के लिए बिछायत होती थीं। गद्दों पर सफेद चादर के साथ। सत्कार के प्रतीक एक या दो गाव-तकिए (लोड) लगाते हुए। शेष भाग व बरामदे से लेकर पिछले हिस्से व मध्य के छज्जे तक श्रोताओं का आधिपत्य होता था। एक दौर ऐसा भी था, जब सुर व ताल की जुगलबंदी और गायकी के दीवाने नीचे सड़क किनारे घरों के दरवाज़ों पर डटे दिखाई देते थे। मुश्किल से आधा-पौन सैकड़ा लोगों की क्षमता वाले उक्त परिसर में अक़्सर दो से ढाई-तीन गुना तक श्रोता दिखाई देते थे। वो भी बीच में फुट भर का गलियारा छोड़ने के बाद। आपस में घुसे हुए से। इनमें चंबल कॉलोनी व रेलवे स्टेशन तक के परिवार शामिल होते थे। जो साइकल से या पैदल यहां तक आते थे। आवागमन के दूसरे साधन न होने के बाद भी।
अतिथि-सत्कार की परम्परा के साथ आरम्भ होने वाले अधिकांश कार्यक्रम रात के दूसरे-तीसरे पहर तक चलते थे। तो कुछ ब्रह्म-मुहूर्त से भोर की वेला तक। सुगम से लेकर शास्त्रीय व अर्द्ध-शास्त्रीय संगीत की सभाओं में कई कलाकारों को प्रत्यक्ष सुनने का सुअवसर यहीं मिला। इनमें विविध विधाओं व छोटे-बड़े घरानों के निपुण कलाकार होते थे। जिनमें कुछ कालांतर में प्रसिद्धि के शीर्ष तक भी पहुंचे। कई अब कीर्ति-शेष हो चुके हैं। कुछ अब भी सुर व ताल की साधना में निमग्न हैं। स्थानीय कलाकरों के लिए भी यह दरबार एक वरदान जैसा रहा। जिन्हें सुधि श्रोताओं का पूरा साथ मिलता रहा।
सांस्कृतिक संध्या, कवि सम्मेलन, आत्म-दिन, एकल-पाठ व प्रस्तुति, अथर्वशीर्ष पाठ, अंताक्षरी, भजन सहित समाज की महिलाओं व बच्चों के लिए कला-कौशल व क्रीड़ा पर आधारित रोचक स्पर्द्धाएं इस उत्सव का ख़ास हिस्सा होती थीं। कभी-कभी बाल मेले भी भीड़ जुटाते थे। बारामदे से सटे छोटी रेल के डिब्बे जैसे एक लंबे कमरे के मध्य एक अस्थायी मंदिर बनाया जाता था। जिसमें विधि-विधान से विराजित श्री(बप्पा)जी, अपनी ओर मुंह किए प्रस्तोताओं व पीठ किए श्रोताओं पर समान भाव से आशीष की वृष्टि करते थे। श्रीजी की प्रतिमा के पार्श्व में थीं वो झरोखेनुमा नक़्क़ाशीदार खिड़कियां, जो भवन के वाह्य-भाग को दक्षिण-भारतीय शैली के भवन का स्वरूप देती थीं। यह वैशिष्ट्य इस समाज के कई परिवारों के निवासों के बीच इसी भवन को प्राप्त था। जो दुर्योगवश इस भवन के साथ ही क्षेत्र से भी छिन गया। इस भवन के बिक जाने के बाद, सदा-सदा के लिए।
भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी को श्री जी के आगमन से लेकर चतुर्दशी को विदाई तक चलने वाले उत्सव का समापन रात्रि वेला में पारितोषिक वितरण के साथ होता था। जबकि अगले दिन महाप्रसाद में समूचा समाज उमड़ पड़ता था। इसके अलावा उत्सव में किसी न किसी रूप में भागीदार स्थानीय कलाकार, जनप्रतिनिधि, गणमान्य नागरिक, मोहल्ले के सभ्रांत परिवार भी आमंत्रित किए जाते थे। जो इसे अपना सम्मान व सौभाग्य मानते थे। उत्सव की आमंत्रण पत्रिका पीले या गुलाबी काग़ज़ पर मराठी में ही छपती थी। जिसे उत्सव के पहले दिन चल-समारोह के दौरान बांटा जाता था। वो भी बिना किसी भेद-भाव के। ऐसा आज तक कोई और समाज अपनी “कूप-मण्डूकता” के चलते आज तक नहीं कर पाया। आयोजन के स्वर्ण-वर्ष तक पत्रिका घर-घर भी पहुंचाई जाती रहीं। समाज व मोहल्ले के परिवारों के लिए।
उत्सव के स्वर्ण (50वें) तथा हीरक (75वें) जयंती वर्ष का मैं एक जागृत व जीवंत साक्षी हूँ, जिसने बीते 45 वर्षों में तमाम बदलावों के साथ बड़े-बड़े उतार-चढ़ाव देखे। सच कहूँ तो मैं इस आयोजन के उत्कर्ष और विकर्ष का भी गवाह हूँ। मैं एक समय तक इस उत्सव के वैभव से हर्षित भी रहा और बाद में सतत पराभव से विचलित व आहत भी। इस महोत्सव के 100वें वर्ष की भव्यता को लेकर जो स्वप्न संजोए थे, वे 9वें दशक से पहले ही भंग हो गए। दूसरी पीढ़ी के तमाम पुरोधाओं के प्रस्थान या प्रयाण के बाद तीसरी पीढ़ी में उपजे आंतरिक राग-द्वेष ने एक विरासत की जड़ में दीमक लगाने का काम किया। परिणामस्वरूप प्लेटिनम (100वें) वर्ष से एक दशक पहले ही उत्सव खाना-पूर्ति बन कर रह गया। जो अब अपनी अधोगति का मूक साक्षी स्वयं है। सम्पन्नता के बाद भी सहकार व समर्पण की कमी ने आज उत्सव को मन मसोस कर की जाने वाली रस्म-अदायगी बना दिया है। जिसमें रस या गंध जैसा कुछ नहीं बचा। वो भी उस सियासी दौर में, जब छोटे-छोटे समाज भी अपने वैभव के प्रदर्शन को लेकर जागरूक हो चुके हैं। मेरे अपने समाज को छोड़ कर।
मेरा मानना है कि इस एक समृद्ध परंपरा के पराभव का यह दौर आयोजन-स्थल को बदले जाने के बाद और तीव्र हुआ। उत्सव को डेढ़ दशक पहले “मुजुमदार साहब के बाड़े” से किला रोड स्थित श्री जयेश्वर महादेव मंदिर परिसर में ले जाया गया। स्थानापन्न उत्सव दो-चार साल तक अपने अस्तित्व को बनाए रखने का संघर्ष करता दिखाई देने के बाद आत्मसमर्पण करता दिखाई देने लगा। जो अब लोप के मुहाने पर है। जिसमें अन्य समाज तो दूर आयोजक समाज के शेष परिवारों का जुड़ाव भी नहीं के बराबर ही बचा है। मैं इसे स्थान-परिवर्तन से रूष्ट श्री जी के कोप का परिणाम कहूँ तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। इस सच के कई ज्वलंत व दुःखद प्रमाण भी बीते दो दशक में सामने आए, जो हतप्रभ करने वाले रहे। उनका स्मरण भी पीड़ा का आभास कराता है। जो संतप्त हुए, उनके प्रति आत्मीय सम्वेदनाएँ कल भी थीं, आज भी हैं, आगे भी रहेंगी। जिन्हें भगवान विनायक की कृपा से अपार सुख व वैभव प्राप्त हुआ, उनके लिए हृदय से हर्षित हूँ। उन्हें ऐसी उपलब्धियों को अपने पूर्वजों के सुकृत्यों का सुफल मानना चाहिए। जिन पर बाबा गणपति कृपावान बने रहे। जीवन के साथ भी, जीवन के बाद भी। कुछ को ऐसे सुफल अपने सुकर्मों से भी मिले, जो अब उनसे ही विमुख हो चुके हैं।
उत्सव के उत्थान से पतन के बीच के बदलावों पर प्रकाश डाले बिना बात पूरी नहीं होगी। इसलिए प्रयास करता हूँ, अतीत के पृष्ठों को संक्षेप में समेटने का। इसे आप कल व आज के बीच की तुलना भी समझ सकते हैं और क्रमबद्ध विवेचन भी। स्मरण में है कि पिछली तीन पीढ़ियों में से पहली पीढ़ी के युग में बप्पा जी का आगमन और विसर्जन सकल समाज की एकता व प्रतिबद्धता का प्रेरक प्रमाण होता था। दोनों चल-समारोहों में महिला-पुरुष व बच्चे सब सम्मिलित होते थे। वो भी अपने पारंपरिक परिधानों में सज-धज कर। जो मराठी भाषा में सामूहिक संकीर्तन करते दिखाई देते थे। कालांतर में यह दृश्य दुर्लभ होते चले गए। आज की स्थिति लिखने योग्य नहीं। महिलाओं व बच्चों ने चल-समारोहों से समयानुसार दूरी बना ली है। कारण जो भी रहे हों। व्यस्तता को कारण नहीं माना जा सकता, क्योंकि आज से ज़्यादा काम पूर्वज पीढ़ी के पास थे। खेती-किसानी व लोकसेवा भी। सामाजिक व्यवहार व सरोकार के अलावा।
भली-भांति स्मरण है कि पहली पीढ़ी के नेतृत्व काल में श्री जी के दरबार में अखंड संकीर्तन का विधान था। जिसे महिला-पुरुष अलग पारियों में जारी रखते थे। कार्यक्रमों के दौरान भी एक-दो सदस्य मन्द ध्वनि में झांझ-मंजीरा बजाते रहते थे। जो उनके सामाजिक अनुशासन, धार्मिक समर्पण व दृढ़ इच्छा-शक्ति का परिचायक था। जिसमें दूसरी पीढ़ी भी बरसों तक प्रतिबद्धता के साथ भागीदार बनती रही। आज इस समर्पण के एकांश की भी कल्पना बेमानी है। उस दौर की महाप्रसादी में महाराष्ट्रीयन व्यंजनों का समावेश होता था, जो अब घरों की रसोई तक सिमट चुके हैं। सांध्य-आरती के बाद प्रसाद-रूप में नित्य वितरित होने वाले मोदक अब यदा-कदा ही बंटते होंगे शायद। नारियल व राजगिरी के बूरे वाले प्रसाद का वितरण तो अब भी हो रहा होगा। विसर्जन के उपरांत वितरित होने वाले चने की पिसी हुई कच्ची व तीखी दाल के अनूठे प्रसाद की तरह।
भक्तों की संख्या व उत्साह के समानांतर श्री जी के विग्रह का आकार भी घटता जा रहा है। विमान वही है, मगर उसके साथ आने-जाने वालों की संख्या बमुश्किल दहाई का आंकड़ा पार कर पाती है। चतुर्थी से चतुर्दशी के बीच लगता है कि समाज के परिवारों की संख्या अत्यंत न्यून हो गई है। यह धारणा उत्सव की पूर्णता के उपलक्ष्य में आयोजित सहभोज के अवसर पर उमड़ने वाली परिवारों की भीड़ को देख कर स्वतः मिथ्या साबित हो जाती है। यह सोच कर राहत का आभास कर सकते हैं कि आमूलचूल बदलाव के बाद भी कुछ तो है, जो नहीं बदला। एक दिन ही सही, समाज के सारे परिवार एकजुट तो होते हैं कम से कम। आंगन की जगह गमले में सही, परम्परा की जड़ बची हुई तो है।
एक स्वाध्यायी सामाजिक व सनातनी जीव के रूप में मेरी मान्यता है कि निर्माण और विध्वंस परस्पर विरोधी नहीं बल्कि एक-दूसरे के पूरक व पर्याय हैं। जो निर्मित होता है, उसका विध्वंस तय है। जिसका विध्वंस हुआ है, उसका नवनिर्माण भी। बावजूद इसके एक सत्य यह भी है कि धरोहरों का संरक्षण किसी एक व्यकि या परिवार नहीं, समुदाय की ज़िम्मेदारी होती है। समुदाय सम्पन्न हो तो यह ज़िम्मेदारी द्विगुणित हो जाती है। जो सामंती व जागीरी रसूख के मामले में समृद्ध उक्त समाज के संदर्भ में कतई अप्रभावी नहीं मानी जा सकती। अच्छा होता यदि उक्त भवन समाज या उसका ही कोई समर्थ (जिनकी कमी नहीं) प्रतिनिधि ले लेता। जो भवन में आंतरिक सुविधा व सज्जा रुचि-अनुरूप कराते हुए, इसके मूल-स्वरूप (ढांचे) को चिर-स्थायी रख पाने की दिशा में एक “भागीरथी” व “भामाशाही” पहल साबित होता। वो भी बिना किसी आर्थिक घाटे के। ऐसा होता तो वर्ष में एक बार श्री जी के श्रीचरण उस मोहल्ले में आते रहते, जिसका नामकरण ही इस समाज के परिवारों की अधिकता के कारण हुआ था। तमाम साल पहले किसी ज़माने में। हालांकि आज ऐतिहासिक शोध मेरा विषय नहीं, तथापि बताना मुनासिब होगा कि मुग़ल-कालीन उक्त भवन कम से कम 500 वर्ष से अधिक पुराना था। भवन की सुदृढ़ता की जानकारी मुझसे अधिक उन श्रमिकों को होगी, जिनका दम एक-एक पाषाण-खण्ड को निकालते हुए दस-दस बार फूला।
स्मरण करा दूं कि उक्त आयोजन के स्थान परिवर्तन के बाद श्री जी के विमान को नए परिसर तक ले जाए जाने से पूर्व पुराने स्थल तक लायी जाता रहा। कुछ साल बाद इसे भी बंद कर दिया गया। सम्भवतः इस उत्सव के अरसे तक सूत्रधार रहे उक्त भवन के मालिक के अन्यत्र चले जाने के कारण। यहां से स्थायी विदाई के बाद भवन-स्वामी के पास शायद कोई चारा नहीं था, भवन के विक्रय के अलावा। वैसे भी समय व परिस्थितियों में बदलाव के बाद पुरखों की विरासत सहेज कर रख पाना सम्बद्ध परिवार के लिए संभव नहीं था। ऐसे में एक सूने मकान से अधिक इसमें भौतिक दृष्टि से कुछ था भी नहीं। परिवार के बिना कोई घर न उपयोगी रहता है, न सहेज कर रखने योग्य। ऐसे में आज के अर्थ-युग में भवन की बिक्री को भी अनुचित नहीं ठहराया जा सकता। विदित है कि बिना विवशता के कोई भी अपने आशियाने से दूर होना नहीं चाहता। ऐसे में चाहे-अनचाहे बस वो होता है, जो हालात चाहते हैं। वैसे भी आवश्यक नहीं कि हर व्यक्ति व समाज के लिए धरोहर का अपना कोई मोल हो। ऐसी धारणा के बीच आज व्यक्तिगत क्षोभ की शांति के लिए बस इतना सा सोच लेना अधिक उचित होगा कि ऐसा होना भी बप्पा मोरया की इच्छा पर निर्भर रहा होगा। इतना सब लिखने का उद्देश्य मात्र एक उत्सवी इतिहास व उसके केंद्र को स्मरणीय बनाना भर है। वो भी केवल इसलिए कि एक दीर्घ अवधि तक हमारी पहचान अपने आदमी (आपला माणूस) के तौर पर रही। यह और बात है कि इस उत्सव के समापन के बाद हम अजनबी (अनोळखी) तब भी हो जाया करते थे, आज भी हैं। बहरहाल, जैसी प्रभु-इच्छा। इसे भी एक सुखद पक्ष मानता हूँ कि उक्त भवन का स्वामित्व अब मेरे ही एक सहपाठी व शुभचिंतक के पास आ गया है। जिनका वास्ता नगर के एक प्रतिष्ठित व समाजसेवी परिवार से है। अच्छी बात यह भी है कि वे अब तक 16 क़दम की दूरी पर निवासरत थे। नूतन गृह-प्रवेश के बाद 8 क़दम की दूरी पर रहने वाले पड़ौसी बन जाएंगे।
तमाम खट्टे-मीठे व कड़वे अनुभव और भी हैं, जो आगे कभी प्रसंगवश चर्चा का विषय बनेंगे। आज खेद बस इस बात का है कि धराशाई होने से पहले घर से मात्र आठ पग की दूरी पर स्थित उक्त धरोहर के चित्र तक नहीं जुटा सका। औरों से मिले भरोसे के कारण। जो इस धरोहर के साथ ही हमेशा के लिए ध्वस्त हो गया। यह सीख देकर, कि औरों पर भरोसा करना बहुत कुछ गंवाना है। वो भी उस दौर में, जब अपनी परछाई तक भरोसे के लायक़ न बची हो। बस,,,,,आज इसके सिवाय और कुछ नहीं। भूल-चुक क्षमा करें। शेष-अशेष।।
-सम्पादक-
●न्यूज़&व्यूज़●
(मध्य-प्रदेश)
👌👌👌👌👌👌👌👌👌👌👌