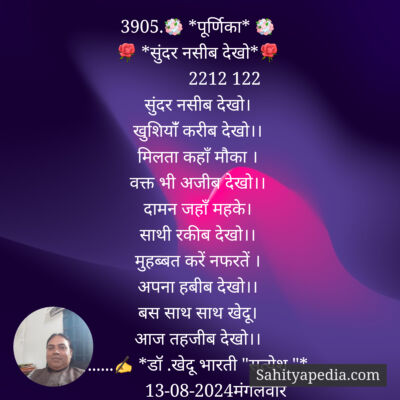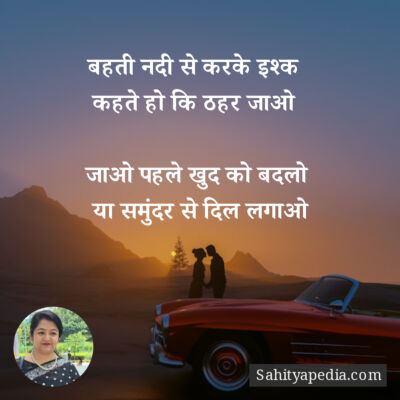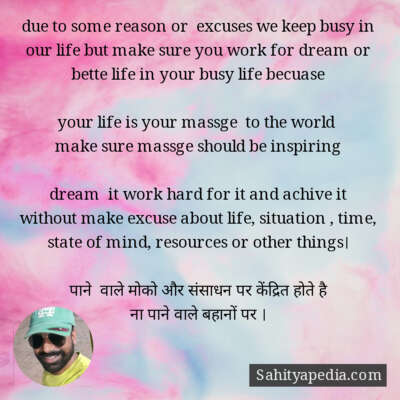गीता आत्मतत्त्व सार ( क्रमशः)
प्राक्कथन
भगवद्गीता समस्त वैदिक ज्ञान का नवनीत है।
——————————————————
ओउम श्री परमात्मने नम: श्री गुरूवाये नम:
ऊँ अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानञ्जनशलाकया ।
चक्षुरुमिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः ।।
मैं घोर अज्ञानान्धकार में उत्पन्न हुआ था और मेरे गुरु ने अपने ज्ञानरूपी प्रकाश से मेरी आँखें खोल दी । मैं उन्हें सादर नमस्कार करता हूँ ।
भगवद्गीता का मर्म भगवद्गीता में ही व्याप्त है।
जैसे औषधि का सेवन लिखे हुए निर्देशानुसार या चिकित्सक के आदेशानुसार करना होता है।भगवद्गीता को इसके वक्ता द्वारा दिये गये निर्देशानुसार ही ग्रहण या स्वीकार करना चाहिए।
भगवद्गीता ऐसा ग्रन्थ है जो भगवद्भक्त ( ज्ञानी,योगी,भक्त)के निमित्त है। निस्संदेह प्रत्येक व्यक्ति का भाववान से प्रत्यक्ष सम्बन्ध होता है और यह सम्बन्ध भक्ति की पूर्णता से ही जागृत होता है। प्रत्येक जीव का भगवान से शाश्वत सम्बन्ध होता है।
परम् पुरुषोत्तम भगवान परम् ब्रह्म है,परम् धाम परमेश्वर का निवास स्थान है,जो पवित्र,शुद्ध और भौतिक कल्मष से अरंजित
है।
पुरुषम-परम् भोक्ता,शाश्वतं – आदि सनातन, दिव्यम-दिव्य,आदि देवम-भगवान,अजम-अजन्मा,विभुम-महानतम जिसके समान कोई नहीं है।
जबतक भगवद्गीता का पाठ कोई विनीत भाव से नहीं करता है,तबतक उसे समझपाना अत्यंत कठिन है,क्योंकि यह एक महान रहस्य है ।
ईश्वर का अर्थ है नियन्ता और जीवों का अर्थ है नियन्त्रित , कम से कम बद्ध जीवन में तो नियन्त्रित है ही।
भगवद्गीता की विषयवस्तु ईश्वर और जीव से सम्बंधित है।
समय- इसमें प्रकृति,काल( समस्त ब्रह्मांड की कालावधि या प्रकृति का प्राकट्य तथा कर्म की भी व्यवस्था है।
जीव( मनुष्य) गुण में परम्-नियन्ता के ही समान है।
दुर्भाग्यवश संसारी झगड़ालू व्यक्तियों ने अपनी आसुरी लालसाओं को अग्रसर करके तथा लोगों को जीवन के सिद्धांतों को ठीक से न समझने देने में भगवद्गीता से लाभ उठाया है ।
मोहवश मनुष्य विभिन्न प्रकारों से अपनी इन्द्रीयतृप्ति करके सुखी बनना चाहता है,किन्तु इससे वह कभी भी सुखी नहीं हो सकता ।अपनी भौतिक इन्द्रियों को तुष्ट करने की बजाय उसे भगवान की इन्द्रियों को तुष्ट करने का प्रयास करना चाहिए। यही जीवन की सर्वोच्च सिद्धि है।
अभिज्ञ व्यक्ति स्वतोचालितयान की आभियांत्रिक कुशलता से परिचित होता है । वह सदैव जानता है कि इस यंत्र के पीछे एक व्यक्ति,एक चालक होता है। इसी प्रकार परमेश्वर वह चालक जिसके निर्देशन में प्रत्येक व्यक्ति कर्म कर रहा है , उसे केवल उसके संकेतों को समझने की आवश्यकता है।
जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में हम अपने कर्म के फल का सुख भोगते हैं या उसका कष्ट उठाते हैं।
जगत की अभिव्यक्ति को मिथ्या नहीं माना जाता,इसे वास्तविक,किन्तु क्षण-भंगुर माना जाता है ।प्रकृति शाश्वत है , मिथ्या नहीं है। परमेश्वर की भिन्ना-शक्ति है ।जीव भी परमेश्वर की शक्ति है। जीव का भगवान से नित्य सम्बन्ध है । भगवान जीव प्रकृति तथा काल ये सब परस्पर सम्बद्ध है और सभी शाश्वत है।
कर्म शाश्वत नहीं है, कर्म के फल अत्यंत पुरातन हो सकते हैं।
हम अनादिकाल से अपने शुभ-अशुभ कर्मफलों को भोग रहे हैं और साथ ही हम अपने कर्मों के फल को बदल भी सकते हैं और यह परिवर्तन हमारे ज्ञान पर निर्भर करता है।
हम यह नहीं जानते कि किस प्रकार के कार्य करने से
————————————————————
हम कर्म के फल से मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं ।
——————————————————-
जीव कभी भी परम् चेतन नहीं हो सकता है । वह चेतन तो है लेकिन
————————————————————-
पूर्ण या परम् चेतन नहीं।
—————————–
क्षेत्र-क्षेत्रज्ञ:- जीव अपने शरीर के प्रति सचेत रहता है। भगवान समस्त जीवों के शरीरों के प्रति सचेत रहते हैं। परमात्मा प्रत्येक जीव के हृदय में ईश्वर या नियन्ता के रूप में वास कर रहे हैं और जैसा चाहते हैं वैसा करने के लिए निर्देशित करते रहते हैं। जीव भूल जाता है कि उसे क्या करना है। एक विधि से कर्म करने का संकल्प करता है,लेकिन फिर वह अपने पाप-पुण्य में फंस जाता है ।
जीव के कार्यकलाप तभी बदल सकते हैं जब जीव
———- ———————- ——————–
सतोगुण में स्थित हो और यह समझे कि उसे कौनसे
————————- — ——————————-
कर्म करने चाहिए। यदि वह ऐसा करता है तो उसके
————————————————–
विगत (पूर्ववत ) कर्मों के सारे फल बदल जाते हैं।
———- ——————————————
अतः कर्म शाश्वत नहीं है ।
——————————
चेतना पदार्थ के संयोग से उत्पन्न नहीं होती ऐसा सोचना भ्रांतिमूलक है।भौतिक कल्मष-ग्रस्त चेतना से युक्त हुए बिना कोई दिव्य जगत के विषय में कुछ नहीं कह सकता।अतः भगवान भौतिक दृष्टि से कलुषित ( दूषित) नहीं है ।
भगवान का अंश होने के कारण हममें चेतना पहले से ही रहती है,लेकिन हममें निकृष्ट गुणों द्वारा प्रभावित होने की प्रवृत्ति पाई जाती है किन्तु भगवान परमेश्वर होने के कारण प्रभावित नहीं होते । परमेश्वर तथा क्षुद्र जीवों में यही अंतर है ।
वास्तव में परमेश्वर स्रष्टा और भोक्ता दोनों है और परमेश्वर का अंश होने के कारण जीव न तो स्रष्टा है और न ही भोक्ता है,वह मात्र सहयोगी है। वह सृजित तथा भुक्त है। जैसे हाथ पांव,आंखे आदि शरीर के अंग है,लेकिन ये वास्तविक भोक्ता नहीं है ,भोक्ता तो उदर है । यदि शरीर को स्वस्थ रखना है तो शरीर के सारे अंगों को उदरपूर्ति में सहयोग देना होगा ।( उदर ही प्रधान कारक है जो शरीर रूपी संगठन का पोषण करता है )
सृजन तथा भोग के बिंदु के केंद्र में परमेश्वर है और सारे जीव उनके सहयोगी है ।स्वामी तुष्ट है तो दास भी तुष्ट रहता है ।
भगवान को सच्चिदानन्द विग्रह कहा जाता है, परमात्मा सत् – चित (शाश्वत ज्ञान) की आनंदात्मक अनुभूति है ।
यह दृश्य जगत जिसमें हम रह रहे हैं वह स्वयं भी पूर्ण है क्योंकि जिन चौबीस तत्वों से यह नश्वर ब्रह्माण्ड निर्मित है,वे सांख्य दर्शन के अनुसार इस ब्रह्मांड के पालन तथा धारण के लिए अपेक्षित साधनों से पूर्णतया समन्वित है। इसमें न तो कोई विजातीय तत्त्व है न ही किसी वस्तु की आवश्यकता है।
क्षुद्र जीवों के लिए यह सुविधा प्राप्त है कि पूर्ण की प्रतीति करें। सभी प्रकार की अपूर्णताओं का अनुभव पूर्ण विषयक ज्ञान की अपूर्णता के कारण है।
ग्यारहवें अध्याय में भगवान को प्रपितामह के रूप में सम्बोधित किया गया है और वे तो इन पितामह के भी स्रष्टा है। किसी को किसी भी वस्तु का (अपने आप) को स्वामी नहीं मानना चाहिए,उसे केवल उन्हीं वस्तुओं को अपनी माननी चाहिए जो उसके पोषण के लिए भगवान ने अलग कर दी है ।
मनुष्यों को मनुष्य जीवन की महत्ता समझकर सामान्य पशुओं की भांति व्यवहार नहीं करना चाहिए। मनुष्य को अपने जीवन के उद्देश्य को समझना चाहिए और इसका निर्देश वैदिक गर्न्थो में दिया गया है,जिसका सार भगवद्गीता में मिलता है।
सनातन – धर्म जीव का शाश्वत अंग है। ब्रह्माण्ड के समस्त जीवों का धर्म है। धर्म का अर्थ है जो पदार्थ विशेष में निरन्तर रहता है। अग्नि के साथ ऊष्मा-प्रकाश सदैव रहते हैं, इनके बिना अग्नि शब्द का कोई अर्थ नहीं होता।
जीव चिर-सहचर है शाश्वत गुण – नित्य धर्म है।
जीव का स्वरूप या स्वाभाविक स्थिति भगवान की सेवा करना है।कोई भी जीव अन्य जीव की सेवा करने से मुक्त नही है। सेवा जीव की चिर सहचरी है और सेवा करना जीव का शाश्वत (सनातन)धर्म है।
सभी परिस्थितियों में धार्मिक विश्वास में परिवर्तन होने से अन्यों जीवों की सेवा करने का शाश्वत धर्म ( वृत्ति )प्रभावित नहीं होता । किसी विशेष विश्वास को अंगीकार करना अपने सनातन धर्म को अंगीकार करना नहीं है ।सेवा करना सनातन धर्म है।
स्वतंत्र रूप से सुखी बन पाना सम्भव नहीं है, जिस प्रकार शरीर का कोई भी भाग उदर से सहयोग किये बिना सुखी नहीं रह सकता ।
परमेश्वर की दिव्य प्रेमाभक्ति किये बिना जीव सुखी नहीं हो सकता।
भगवद्गीता में ( १५.६)भगवान के परमधाम का वर्णन इस प्रकार हुआ है :-
न तद्भासयते सूर्यो न शशांको न पावक:।
यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम ।।
यत् =जिस परमपद को
गत्वा =प्राप्त होकर (मनुष्य)
न,निवर्तन्ते=लौटकर संसार में नहीं आते,
तत्=उस (स्वयं प्रकाश परमपद को )
न=न
सूर्य: =सूर्य
भासयते=प्रकाशित कर सकता है
न =न
शशांक: = चन्द्रमा ( और )
न = न
पावकः =अग्नि ही;
तत् = वही
मम = मेरा
परमम् = परमधाम है ।
भगवद्गीता में ( ८.२१)भगवान के परमधाम का वर्णन इस प्रकार हुआ है :-
अव्यक्तोअक्षर इत्युक्तस्तमाहु: परमां गतिम् ।
यं प्राप्य न निवर्तन्ते तद्धाम परमम् मम ।।२१।।
अव्यक्त: = अव्यक्त