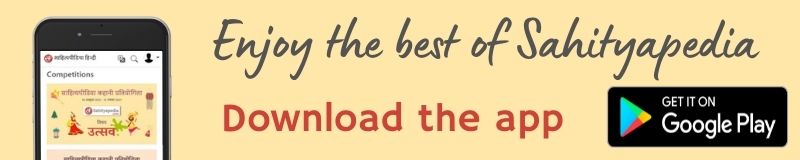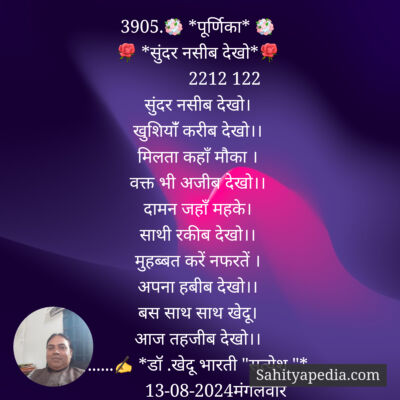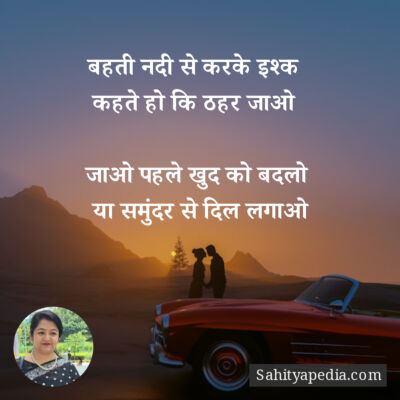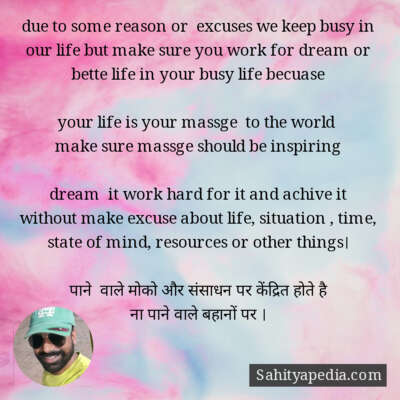इक्कीसवीं सदी की कविता में रस +रमेशराज

हिन्दी कविता के नवें दशक का यदि परम्परागत तरीके से रसात्मक विवेचन करें तो कई ऐसी अड़चनों का सामना करना पड़ सकता है कि जिनके रहते रस की परम्परागत कसौटी या तो असफल सिद्ध होगी या परख के नाम पर जो परिणाम मिलेंगे, वह वर्तमान कविता का सही और सारगर्भित रसात्मक आकलन नहीं माने जा सकते। अतः जरूरी यह है कि आदि रसाचार्य भरतमुनि के रसनिष्पत्ति सम्बन्धी सूत्र-‘विभावानुभाव व्यभिचारे संयोगाद रस निष्पत्तिः’ में अन्तर्निहित भावसत्ता का वैचारिक विवेचन किया जाये और यह समझा जाये कि भाव का उद्बोधन किस ज्ञान या बुद्धि अवस्था में होता है। रस को गूंगे का गुड़ बनाकर परोसने से जो गूंगे नहीं है, उनके प्रति तो अन्याय होगा ही।
वर्तमान कविता पर अक्सर यह आरोप लगाये जाते हैं कि यह कविता विचार प्रधान होने के कारण भावविहीन है | इसमें किसी प्रकार का रस.परिपाक सम्भव नहीं। यह तर्क ऐसे रसमीमांसकों का है, जो रस की अपूर्णता में ही पूर्णता का भ्रम पाले हुए हैं और भाव तथा रस की रट लगाये हुए हैं। उनके मन को यह मूल प्रश्न कभी उद्वेलित नहीं करता कि यह भाव किसके द्वारा और किस प्रकार निर्मित होकर रस.अवस्था तक पहुंचता है। रसों की तालिका में किसी नये रस की बढ़ोत्तरी भी नहीं करना चाहते हैं। जबकि आदि आचार्य मुनि ने जो रसतालिका प्रस्तुत की उसमें बाद में चलकर अनेक रस जोड़े गये। ऐसा इस कारण है कि आज के कथित रसमर्मज्ञ रस के प्रति चिंतक कम, व्यावसायिक ज्यादा हैं। उन्हें इधर.उधर से सामग्री इकट्ठा कर पुस्तक छपवाने और पैसा कमाने में रूचि अधिक है। मौलिक चिन्तन के प्रति उनका रूझान न बराबर है।
बहरहाल यह तो निश्चित है कि चाहे कविता का परम्परागत स्वरूप रहा हो या कविता का बदला हुआ वर्तमान स्वरूप, सबके भीतर रस की धारा झरने की तरह फूटकर, कल.कल नाद करती हुई नदी बनकर बहती है और हर एक सुधी पाठक के मन को आर्द्र करती है। परम्परागत कविता के रसात्मक आकलन के लिये तो हमारे पास एक बंधी-बंधाई कसौटी है, लेकिन वर्तमान कविता के रसात्मकबोध का हमारे पास कोई मापक नहीं। इसका सीधा.सीधा कारण यह है कि वर्तमान कविता में सामान्यतः उन रसों की निष्पत्ति नहीं होती, जो हमारे पूर्ववर्ती रसाचार्यों द्वारा गिनाये गये हैं। और हम नये रसों की खोज करने में आजतक सामर्थ्यवान नहीं हो पाये हैं। इसलिये अपनी खीज मिटाने के लिये हम तपाक से एक जुमला उछाल देते हैं कि-वर्तमान कविता तो विचार प्रधान कविता है | इसमें भावोद्बोधन का मधुर प्लावन कहां ? वर्तमान कविता को विचार प्रधान कविता सिद्ध करने वालों की महान रसात्मक बुद्धि को पता ही नहीं कि भाव विचार की ऊर्जा होते हैं।
विचार के बिना भाव का निर्माण किसी प्रकार न पहले सम्भव था और न अब है। यदि परशुराम की ज्ञानेन्द्रियों को यह विचार न उद्वेलित करता कि राम ने शिव का धनुष तोड़ दिया है, तो कैसा क्रोध और किस पर क्रोध। यदि रावण को यह विचार न मंथता कि लक्ष्मण और राम ने उसकी बहिन सूपनखा को अपमानित किया है, तो क्रोध के चरमोत्कर्ष के कैसे होते रावण में दर्शन। यदि राम के मन को यह विचार न स्पर्श न करता कि उनके अनुज को मेघनाद ने मूर्छित कर दिया है और यदि समय रहते चिकित्सा न हुई तो लक्ष्मण का प्राणांत हो सकता है, तो कैसा विलाप, कैसा शोक।
अस्तु! विचार के बिना किसी भी प्रकार के भाव का निर्माण सम्भव नहीं। यदि भावोद्बोधन नहीं तो कैसी रसनिष्पत्ति और कैसा रस ? जब रस का मूल आधार विचार ही है तो हम आज की कविता को मात्र वैचारिक कहकर रस के मूल प्रश्न से किनारा कर ही नहीं सकते। इसलिये जरूरी है कि यदि वर्तमान कविता पूर्ववर्ती रसाचायों द्वारा गिनाये गये रसों के आधार पर परखी नहीं जा सकती तो कुछ नये रसों को खोज की जानी चाहिए। वैसे भी यह कोई अप्रत्याशित और अरसात्मक कदम नहीं होगा | क्योंकि आचार्य भरतमुनि द्वारा गिनाये रसों में भी शांतरस, भक्तिरस जैसे कई रसों की बाद में जोड़ा गया है।
बात चूंकि नवें दशक की कविता के संदर्भ में चल रही है तो मैं यह निवेदन कर दूं कि नवें दशक की कविता की चर्चित विधा ‘तेवरी’ में मैंने अपनी पुस्तक ‘तेवरी में रससमस्या और समधान’ में दो नये रस विरोधरस और विद्रोहरस की खोज की है जिनके स्थायी भाव क्रमशः ‘आक्रोश’ और ‘असंतोष’ बताये हैं। वर्तमान कविता जिन वैचारिक प्रक्रियाओं से होकर गुजर रही हैए ‘तेवरी’ भी उसी वैचारिक प्रक्रिया का एक अभिन्न अंग है। अतः यह कहना अप्रासंगिक न होगा कि तेवरी में जिन रसों का उद्बोधन होता है, वही रस वर्तमान कविता में भी उद्बोधित होते हैं।
कविता में विरोध और विद्रोह रस की निष्पत्ति किस प्रकार और कैसे होती है, इसे समझाने के लिये ‘नवें दशक’ की कुछ कविताओं के उदाहरण प्रस्तुत हैं-
1. विरोध रस-इस रस का मुख्य आलम्बन वर्तमान व्यवस्था या उसके वह अत्याचारी शोषक और आतातायी पात्र हैं, जो शोषित और पीडि़त पात्रों को अपना शिकार बनाते हैं। आलम्बन के रूप में वर्तमान व्यवस्था या उसके पात्रों के धर्म अर्थात् आचरण को देखकर या अनुभव कर दुखी शोषित त्रस्त पात्र जब अपने मन में लगातार त्रासदियों को झेलते हुए यह विचार लाने लगते हैं कि वर्तमान व्यवस्था बड़ी ही बेरहम, अलोकतांत्रिक और गरीबों का खून चूसने वाली व्यवस्था है, तो यह विचार अपनी ऊर्जस्व अवस्था में अपने चरमोत्कर्ष पर ‘आक्रोश’ को जन्म देता है। विभिन्न प्रकार की वैचारिक प्रक्रियाओं से गुजरकर बना यह स्थायी भाव ही ‘विरोध’ को रस की परिपक्व अवस्था तक ले जाता है-
‘उत्तर प्रदेश की हरिजन कन्या हो
या महाभारत की द्रौपदी
दोनों में से किसी का अपमान देखने वाला
चाहे वह भीष्म पितामह हो
या गुरु द्रोणाचार्य या चरणसिंह
मेरे लिये धृतराष्ट्र ही हैं।‘
‘विरोध’ शीर्षक से साहित्यिक पत्रिका ‘काव्या’ के अप्रैल.जून.90 [सं- हस्तीमल हस्ती] में प्रकाशित श्री विश्वनाथ की उक्त कविता का यदि हम रसात्मक विवेचन करें तो इस कविता में उत्तर प्रदेश की हरिजन कन्या या महाभारत में हुए द्रौपदी के अपमान को सुनकर, देखकर या अनुभव कर आश्रय रूपी कवि का मन मात्र ऐसे धृतराष्ट्रों के प्रति ही आक्रोश से सिक्त नहीं होता जो आंखों से अंधे हैं। उसके मन में ऐसी वैचारिक ऊर्जा सघन होती है जो भीष्म पितामह से लेकर गुरु द्रोणाचार्य, यहां तक कि किसान नेता चरणसिंह के प्रति भी ‘आक्रोश’ को जन्म देती है। कारण-कवि के मन में यह विचार कहीं न कहीं ऊर्जस्व अवस्था में है कि धृतराष्ट्र की तरह ही सब के सब नारी अपमान के प्रति आंखें मूदे रहे हैं। ‘नारी अपमान को अनदेखा करने का यह विचार’ कवि को जिस आक्रोश से सिक्त कर रहा है, यह आक्रोश ही विरोधरस का वह परिपाक है, जिसकी रसात्मकता आत्मीयकरण की स्थिति में सुधी पाठकों को आक्रोश से सिक्त कर धृतराष्ट्रों के विरोध की और ले जायेगी।
2. विद्रोह रस- विरोधरस का मूल आलम्बन भी व्यवस्था और उसके वह पात्र होते हैं जो शोषित दलित पात्रों की अपेक्षाओं पर खरे नहीं उतरते। उनकी सुविधाओं पर ध्यान नहीं देते। परिणामतः मेहनतकश, दलित, शोषित वर्ग में ‘असंतोष’ के ज्वालामुखी सुलगने लगते हैं। ‘असंतोष’, ‘विद्रोह रस’ का स्थायी भाव है। इसके संचारी भावों में दुख, अशांति, क्षोभ, आक्रोश, खिन्नता, उदासी आदि माने जा सकते हैं। इस रस के मुख्य अनुभाव-अवज्ञा, ललकार, चुनौती, फटकार आदि हैं-
तुहमतें मेरे न सर पर दीजिए
झुक न पायेगा कलम कर दीजिए।
सत्य के प्रति और भी होंगे मुखर
आप कितने भी हमें डर दीजिए।
वर्ष 1988 में प्रकाशित दर्शन बेजार के तेवरी संग्रह-दे श खंडित हो न जाए’ की उपरोक्त ‘तेवरी’ का यदि रसात्मक विवेचन करें तो सत्य और ईमानदारी की राह पर चलने वाले एक सच्चे इन्सान की यह व्यवस्था उसे इस मार्ग को डिगाने के लिये मात्र डराती-धमकाती ही नहीं, उसका खात्मा भी कर देने चाहती है। ऐसी स्थिति में वह ऐसी घिनौनी व्यवस्था से कोई समझौता कर संतोष या चैन के साथ चुप नहीं बैठ जाता, बल्कि संघर्ष करता है, उसे ललकारता है। कुल मिलाकर उसके मन में व्यवस्थापकों के प्रति ऐसा ‘असंतोष’ जन्म लेता है, जो खुलकर ‘विद्रोह’ में फूट पड़ता है। भले ही उसका सर कलम हो जाये लेकिन वह कह उठता है कि ‘सत्य के प्रति ऐसे हालातों में मुखरता और बढ़ेगी’। व्यवस्थापकों के प्रति ‘असंतोष’ से जन्य यह अवज्ञा और चुनौती से भरी स्थिति ‘विद्रोह’ का ही रस परिपाक है।
नवें दशक की कविता को समझने के लिये आवश्यक है कि हम निम्न तथ्यों को भी समझने का प्रयास करें कि भाव विचार से जन्य ऊर्जा ही होते हैं। यदि कवि के मन में यह विचार न आया होता कि ‘उत्तर प्रदेश में हरिजन कन्या के साथ अत्याचार हुआ है और महाभारत काल में द्रौपदी का अपमान’ तो उसके मन में आक्रोश का निर्माण किसी प्रकार सम्भव न था। दूसरी तरफ वह निर्णय न लेता कि ‘नारी अपमान को अनदेखा करने वाले भी अंधे घृतराष्ट्र से कम अपराधी नहीं होते’। तभी तो वह भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य या राजनेता चरणसिंह को धृतराष्ट्र की श्रेणी में रखता है। उपरोक्त विवेचन से यह भी स्पष्ट हो जाता है कि रस की निष्पत्ति आलम्बन से नहीं, आलम्बन के धर्म से होती है। यदि द्रोणाचार्य, भीष्म पितामह या चरण सिंह ने नारी अपमान के प्रति अपना विरोध प्रकट किया होता या धृतराष्ट्र के नारी अपमान न होने दिया होता तो कवि के मन में आक्रोश की जगह इन्हीं पात्रों के प्रति श्रद्धा जाग उठती।
काव्य का सम्बन्ध जब दर्शक पाठक या श्रोता से जुड़ता है तो यह कोई आवश्यक नहीं कि उसमें उसी प्रकार के रस की निष्पत्ति हो जो काव्य के पात्रों में या काव्य में अन्तर्निहित है। इसके लिये जरूरी है कि पाठक, दर्शक, श्रोता का आत्म भी ठीक उसी प्रकार का हो जो कवि की आत्माभिव्यक्ति से मेल खाता है। इसी कारण मैं काव्य में साधारणीकरण नहीं, आत्मीयकरण की सार्थकता को ज्यादा सारगर्भित मानता हूं। यह आत्मीयकरण के कारण ही है कि तुलसी के काव्य के प्रति सारी सहृदयता को उड़लने वाले आचार्य रामचन्द्र शुक्ल, आचार्य केशव के प्रति इतने हृदयहीन क्यों हो जाते हैं कि उन्हें काव्य का प्रेत कह डालते हैं। जबकि डॉ. विजयपाल सिंह में केशव के प्रति कथित सहृदयता का तत्त्व साफ-साफ झलकता है।
इसलिये नवें दशक की कविता को रसाभास का शिकार बनाने से पूर्व इसमें अन्तर्निहित इन दो नये रसों के साथ-साथ हमें साधारणीकरण के मापकों को त्यागकर ‘आत्मीयकरण’ का नया मापक लेना ही पड़ेगा, तभी नवें दशक की कविता का रसात्मक आकलन हो सकता है।
————————————————————————
+रमेशराज, 15/109, ईसानगर, अलीगढ़-202001