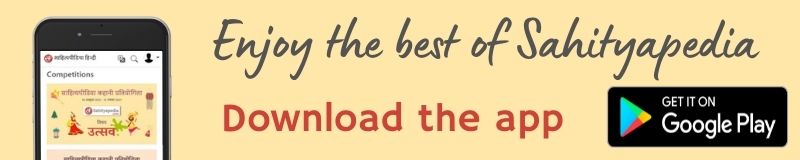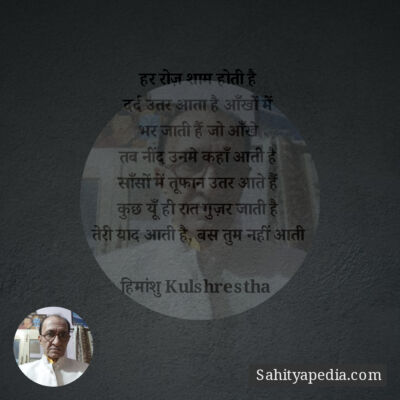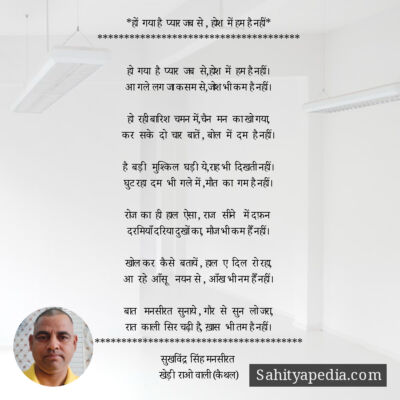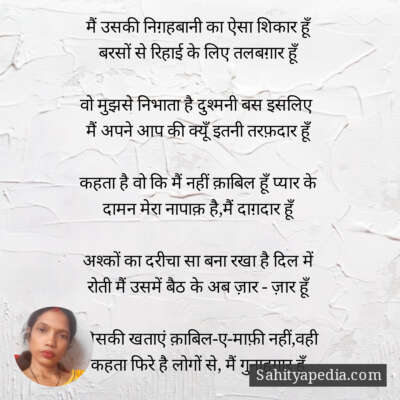आलेख
नवगीत-बोलचाल की भाषा
समय अपने साथ अनेक परिवर्तनों की जलवायु को समेटते हुए एक लंबी यात्रा पर निकला है. यह नहीं पता कि समय की मंजिल कहाँ है और वह कहाँ तक चलकर अपने गंतव्य तक पहुँचकर या बिना पहुँचे ही अपनी यात्रा समाप्त करेगा. वह चला जा रहा है और चल रहा है, चलता रहेगा. समय की यात्रा की कोई सीमा नहीं है. समय जिस दिन रुक जाएगा, एक प्रलय का अवतार होगा. प्रलय यानि कि समय का रुकना. समय का रुकना ही प्रलय है. समय न कोई व्यक्ति है और न जीव. यह ग्रहों द्वारा निर्धारित गति की एक लय है. हवा और पानी जीवन की आवश्यक आवश्यकतायें हैं. यदि जीवन है तो उसे भी कुछ जीने का सहारा अवश्य चाहिए, हवा, पानी और भोजन के अतिरिक्त. वह बहुत महत्वपूर्ण चीज है आनंद और चित्त का विकास. आनंद और चित्त का विकास उसे मिलेगा कहाँ से, पृथ्वी पर उपलब्ध वस्तुओं हरियाली, पेड़-पौधे, नदी, पर्वत, झरने आदि से. अधिक न कहकर सीधे पहुँचते हैं, साहित्य से. साहित्य यानि कि सहित का भाव और सहित यानि कि संग, समेत और भाव यानि कि मन में उत्पन्न होने वाली प्रवृत्ति आदि. गीत, लय, धुन, संगीत आदि जितनी भी चीजें साहित्य के लिए चाहिए, सब प्रकृति ने पहले से ही उपलब्ध कराए हुए हैं. ब्रह्मांड में जितनी भी चीजें दृष्टिगोचर होती हैं, सब में एक गीत, लय, धुन और संगीत छिपा हुआ है. यहाँ बात हम केवल गीत की करेंगे. कहा जाता है जो गेय है वह गीत है, यह बात कुछ सीमा तक सही लगती है, दोहा गेय है गीत है और अन्य छंद भी गीत हैं जो गेय हैं, मोटे तौर पर यह माना जा सकता है. दोहा, कुंडलिया, माहिया, कवित्त, चौपाई, सोरठा आदि एक छंद विधान और मात्रा विधान से बँधे हुए हैं, इसलिए वे उक्त नाम से पुकारे जाते हैं किन्तु गेय होकर भी उन्हें गीत कहना तर्क सम्मत नहीं है क्योंकि उनकी तरह और ठीक उसी प्रकार गीत और नवगीत भी कुछ साहित्यिक नियमों से बँधे हैं और इसलिए गीत और नवगीत एक अलग विधा के रूप में साहित्य में जाने जाते हैं. नवगीत गीत का छोटा भाई है.
गीत और नवगीत के उद्भव के विषय में साहित्य की कई कड़ियों को एक साथ जोड़ना आवश्यक होगा और इससे सबका एकमत होना सम्भव भी है और नहीं भी. समय बदलता है और समय के साथ जो कुछ भी दृश्य या अदृश्य है, उसमें भी कुछ न कुछ दिन-प्रतिदिन परिवर्तन हुआ है, होता रहा है और होता आया है और होता रहेगा. गीत में नवता सदैव समयानुसार आती रही है और यह एक अनवरत प्रक्रिया है. गेय कविता का जन्म मेरी समझ से बहुत पहले ही हुआ है, कह सकते हैं, मानवता के जन्म से ही, क्योंकि जब एक बच्चा धरती से अपना प्रथम अनजान परिचय प्राप्त करता है, तो वह अपने को असुरक्षित सा अनुभव कर डर की पीड़ा से प्रभावित होकर रोता है और यह ‘रोना’ भारतीय साहित्य में गीत माना गया है. गीत का उद्भव कब हुआ, इस पर साहित्यकारों की राय एक नहीं है. गीत का प्रारम्भिक स्वरूप लोकगीत ही रहा है, जैसे कि जाँत चलाते समय ‘जाँतसार’, शादी-विवाह के समय ‘सहाना’, खेत की सोहनी आदि के समय औरतों का गीत ‘झूमर’, भेंड़-बकरी, गाय-भैंस चराते समय चरवाहों और खेत की ओर पगडण्डी पर जाते, कंधे पर डंडा और माथ पर पगड़ी बाँधे किसान को गाते हुए देखा जाना, यह प्रमाणित करता है. बाद में समय और ऋतु के अनुसार गीतों के नाम पड़े. जैसे कि शादी के समय गाये जाने वाले गीत ‘शादी-गीत’ या ‘सहाना’ के नाम से जाने जाते हैं. होली के समय गाये जाने वाले गीत ‘होरी’ या ‘फगुआ’ कहे जाने लगे. चैत आने पर ‘चैता-चैती’ कहे गये. सुबह के गीत ‘प्रभाती’ या ‘आसावरी’ और शाम के ‘सँझवाती’ और थोड़ी रात बीतने पर गाये जाने वाले गीत ‘निर्गुण’ कहे जाने लगे. इस अवधि में गीत लिखे नहीं जाते थे, कंठस्थ किये जाते थे. गीत जब लिखित रूप में आये तो ‘पद’ कहे जाने लगे और उनके कहने और गाने की एक शैली थी. जोइंदु, सरहपा, बाबा गोरखनाथ, विद्यापति, बिहारी, तुलसी, सूर, कबीर, मीरा, गिरधर आदि ने सबदी, पद, साखी, दोहे, चौपाई, भजन, निर्गुण, चैता, चैती, सवैया, कुंडलिया आदि रूपों में गीत रचे, जिसका साक्ष्य भक्तिकाल और रीतिकाल के पास सुरक्षित है. कुछ आधुनिक कवि भी अभी तक इनका प्रयोग धड़ल्ले से कर रहे हैं किन्तु बाद में गीत को एक नया स्वरूप मिला जिनमें ‘मुखड़ा’ या ‘स्थायी’ या ‘टेक’ से प्रारम्भकर कुछ ‘अंतरे’ गीत में जोड़े जाने लगे. अंतरों की संख्या निर्धारित नहीं थी. छायावाद के कवियों ने भी इस प्रकृति के गीत लिखे. किन्तु प्रगतिवाद और प्रयोगवाद से जुड़े कवियों ने कविता की शैली ही बदल दी और पाश्चात्य साहित्य से प्रभावित होकर अतुकांत कविता की ओर हिंदी साहित्य को मोड़ दिया. गेय कविता को नकारना प्रारम्भ कर दिया, अपना वर्चस्व स्थापित करने के लिए. ये वो लोग थे जो वाह्य विचारधारा से प्रभावित थे और अच्छे-अच्छे सरकारी और सत्ता के पदों पर आसीन रहे या सत्ता के अधिक करीब थे. यह दावे के साथ कहा जा सकता है कि ये वे लोग थे जिनको साहित्य से कुछ लेना-देना नहीं था, गीत लिख नहीं सकते थे तो सेवानिवृति के बाद करते क्या ? गीत और साहित्य में बौद्धिकता का अभाव मानकर छंद की स्वच्छन्दता के आधार पर गीत को मृतक घोषित करने की चाल चलने लगे, यह कहकर कि ‘ गीत मर रहा है.’ गीत कभी न मरा न मर सकता है. गीत की पंक्तियों को याद रखने वाले हजारों मिल जायेंगे जबकि नई कविता करने वालों को अपनी स्वयं की नई कविता भी नहीं याद रहती. इनका उदाहरण भी मुहावरे के रूप में अधिक प्रयोग नहीं होता. गीतकारों ने इसकी काट निकाली और नई भाषा, नई शैली, नये छंदों, नये प्रतीकों और नये बिम्बों में गीत के ‘स्थायी’ और ‘अंतरों’ में परिवर्तनकर आधुनिक यथार्थ का अमृत घोलकर और अलंकार का पग छोटा कर गीत को ‘नवगीत’ के साँचे में ढालना प्रारम्भ किया और गीत को ‘नवगीत’ कहा. गीत को नवगीत तक लाने में और नवगीत की नींव पर ईंट रखकर नारियल फोड़नेवालों में महाप्राण निराला, डा. भारतेंदु मिश्र, दिनेश सिंह, माखनलाल चतुर्वेदी, देवेन्द्र कुमार, नागार्जुन, अज्ञेय, गुलाब सिंह, कन्हैयालाल नन्दन, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, प्रेम शर्मा, राजेन्द्र प्रसाद सिंह, धर्मवीर भारती, केदार नाथ सिंह, ठाकुर प्रसाद सिंह, वीरेन्द्र मिश्र, उमाकांत मालवीय, नईम, पंडित कन्हैयालाल ‘मत्त’, डा. शम्भू नाथ सिंह आदि का योगदान सराहनीय रहा है किन्तु इनमें से कुछ लोग नवगीत के ढाँचे में न ढल पाने या महत्वाकांक्षी होकर ‘नई कविता’ की ओर मुड़े और नवगीत विधा से अलग हो गये.
गीत क्या है
गीत की पहली पंक्ति को ‘स्थायी’ कहा जाता है और ये दो या चार पंक्तियों का होता है और इसमें ‘वर्ण’ या ‘मात्रा’ का बंधन होता है, जहाँ वर्ण का बंधन होता है उसे ‘वर्णिक’ और जहाँ मात्रा का बंधन होता है उसे ‘मात्रिक’ कहते हैं. स्थायी के नीचे की पंक्तियों को ‘अंतरा’ कहा जाता है. कह सकते हैं कि गीत दो हिस्सों में विभक्त होता है-
१.स्थायी
२.अंतरा
‘स्थायी’ को ‘मुखड़ा’ या ‘टेक’ या ‘मथेला’ भी कहा जाता है और इसे गाते समय प्रत्येक अंतरे के बाद दोहराया जाता है और इसको दोहराने से ‘स्थायी’ और ‘अंतरों’ में ‘निरन्तरता’ बनी रहती है.
गीत में दो या दो से अधिक अंतरे हो सकते हैं. गीत में अंतरों का बंधन नहीं होता.
गीत के अंतरे एक दूसरे से भाव-सम्पदा में जुड़े होते हैं.
गीत के अंतरों की अंतिम पंक्तियों का ऐसा तारतम्य और सामंजस्य मिलाया जाता है कि वह स्थायी के अंतिम शब्दों से या कुछ शब्द समूह से अक्षर और उच्चारण में समानता रखतीं हों ताकि गीत में लयता की एकरूपता का आभास और एक स्वर लहरी हो, समानता हो.
गीत में विषय और रस का बंधन होता है.
गीत प्राय: प्रेम, प्रकृति, श्रृंगार, दर्शन,भक्ति आदि पर ही लिखे जाते हैं.
गीत में संक्षिप्तता, मार्मिकता एवं सामयिकता का प्रायः अभाव होता है.
गीत में ‘देशज’ शब्दों का प्रयोग वर्जित है.
गीत की भाषा विस्तार लिए हुए होती है और अंतरों पर कोई प्रतिबन्ध नहीं होता है.
गीत में गीतकार अपनी आपबीती भावनाओं एवं अनुभूतियों का प्रयोग और वर्णन बेधड़क करता है.
गीत में ‘छन्दमुक्तता’ मान्य नहीं है.
गीत में ‘अलंकार’ का प्रयोग होता है और ‘अलंकार’ का अधिक प्रयोग क्षम्य है. अलंकार से गीत के रस के रसायन का रसायनशास्त्र उसे और आकर्षक बना देता है और गीत कर्णप्रिय और प्रभावशाली हो जाता है.
गीत के ‘स्थायी’ और ‘अंतरों’ का ‘छ्न्दविधान’, ‘मात्रा’, ‘लय’ और लय की गति एक समान होती है.
गीत का मूलतत्व ‘कथ्य’ है. इस कथ्य के अनुरूप ही ‘बिम्ब’ और ‘प्रतीक’ का चुनाव किया जाता है.
गीत में ‘कल्पना’ को पूर्ण सम्मान मिलता है और कहा तो यह तक जाता है कि कल्पना गीत के हृदय की अंदर-बाहर जाने वाली हवा है या गीत के स्वास्थ्य का अनुलोम-विलोम है.
गीत शिल्प प्रधान होता है.
गीत में कथ्य के विस्तार के लिए प्रचुर मात्रा में बिम्बों, प्रतीकों, उपमाओं आदि के प्रयोग पर कोई प्रतिबन्ध नहीं है. यह गीतकार की इच्छा पर है कि वह उसे कितना अधिक विस्तार देने की क्षमता रखता है और गीत को कितना लम्बा खींच सकता है. वैसे ५ या ६ अंतरों का गीत अच्छा माना गया है और इससे अधिक है तो उबाऊ.
गीत समानता का संकेतक होता है
गीत का उद्देश्य ‘सत्यं-शिवं-सुन्दरम’ की स्थापना करना है.
गीत एक असीमित समय का महाविस्तार है.
गीत पारम्परिकता से गुथा होता है.
गीत एक ही भावभूमि पर चलता है जो शब्दों, अलंकारों, उपमाओं और समस्त काव्य-सम्पदाओं को अपनी ओर आकर्षित करता है और गीत के संसार का निर्माण करता है.
गीत में कविता की तरह तीन तत्वों भाव, कल्पना और बुद्धि का होना अनिवार्य है. जिस गीत में इन तत्वों का समावेश हो जाता है, वह एक कालजयी गीत हो जाता है.
गीत भावाभिव्यक्ति का एक शाब्दिक और भाषिक रूप है.
गीत में संकेतन का बोध होता है यानि कि गीत कुछ संकेत करता है है और उपदेशात्मक होता है.
नवगीत क्या है
गीत की तरह नवगीत भी दो हिस्सों में बँटा है.
१.’स्थायी’ या ‘मुखड़ा’ या ‘मथेला’ या ‘टेक’
२.’अंतरा’
नवगीत के ‘स्थायी’ की पंक्तियों में ‘वर्ण’ या ‘मात्रा’ का कोई बंधन नहीं होता, किन्तु इस बात का ध्यान रखना आवश्यक होता है कि ‘स्थायी’ की या तो पहली पंक्ति या अंतिम पंक्ति के समान उत्तरदायित्व की पंक्ति ‘अंतरे’ के अंत में अवश्य हो और यह गेयता के लिए आवश्यक है. ‘स्थायी’ को दोहराने से कथन में निरन्तरता का सामंजस्य प्रभावशाली बनता है.
नवगीत में ‘अंतरा’ प्राय: दो या तीन ही होते हैं किन्तु चार से अधिक ‘अंतरे’ की मान्यता नहीं है.
नवगीत में विषय, रस और भाव का कोई बंधन नहीं होता.
नवगीत में संक्षिप्तता, मार्मिकता, सहजता, सरलता, बेधक शक्ति का समन्वय एवं सामयिकता का होना नितांत आवश्यक है.
नवगीत में ‘देशज’ प्रचलित क्षेत्रीय बोली के शब्दों का प्रयोग मान्य है और इसके प्रयोग से कथन में एक नयापन और हराभरापन आ जाता है.
नवगीत में नवगीतकार आम आदमी, मेहनत और मजदूरी वर्ग या सरल भाषा में कहें तो सार्वजनिक सामाजिक अवयवों की पीड़ा को अभिव्यक्त करता है.
नवगीत में नये-नये प्रयोग की प्रधानता दी गई है और लीक से हटकर कुछ कहने और लिखने के प्रयास को बढ़ावा दिया जाता है. किसी नये छंद का गठन नवगीत की एक विशेषता मानी जाती है.
नवगीत की भाषा सांकेतिक होती है और कम शब्द में अधिक बात कहने की क्षमता और सामर्थ्य होता है. नवगीत की भाषा आम बोलचाल की भाषा होती है.
नवगीत में ‘छन्दमुक्तता’ क्षम्य है किन्तु ‘छन्दहीनता’ नहीं, गेयता भंग नहीं होनी चाहिए.
नवगीत में ‘अलंकार’ का प्रयोग मान्य तो है किन्तु वह कथ्य की सहज अभिव्यक्ति में किसी तरह से बाधक नहीं होना चाहिए.
नवगीत में भाषा, शिल्प, प्रतीक, शैली, रूपक, बिम्ब, कहन, कल्पना, मुहावरा, यथार्थ आदि कथ्य के सामाजिक सरोकार में एक बड़े मजबूत सहायक के रूप में खड़े होते हैं.
नवगीत नवगीत होता है और अपनी गेयता के कारण ही वह गीत हो सकता है, किसी अन्य कारण या अर्थ में नहीं.
नवगीत ‘कथ्य’ प्रधान होता है.
नवगीत में ‘कथ्य’ का समुद्र रूप एक बूँद में समाहित होता है.
नवगीत में ‘कथ्य’ की अभिव्यक्ति का विस्तार नहीं होता. अभिव्यक्ति की व्याख्या के समय विस्तार तक पहुँचा जा सकता है.
नवगीत तात्कालिक है और उसमे सनातनता और पारम्परिकता का कोई स्थान नहीं है.
नवगीत का उद्देश्य समाज के बाधक कारको को और उत्पन्न स्थितियों की पहचानकर उन्हें समाज को बताना, इंगित करना और उचित समाधान की ओर मोड़ना है.
नवगीत काल की सापेक्षता है.
नवगीत में स्पष्टता का प्रभाव है. जो भी कहा जाए स्पष्ट हो. आम आदमी उसे आसानी से समझ सके और भाषा का प्रयोग आम आदमी की समझ की हो. कभी शब्द का अर्थ समझने के लिए किसी शब्दकोश का सहारा न लेना पड़े.
नवगीत में ‘छान्दस स्वतन्त्रता’ है.
नवगीत का कार्य समाज में छिपी किसी बुराई और असंगति के अनछुए सामाजिक छुईमुईपन की अनुभूति को समाज के समक्ष लाना है.
नवगीत न मांसल सौन्दर्य की कविता है और न संयोग-वियोग की स्मृतियाँ.
नवगीत मानवता के प्रथम पुरुष के जीवन की उठा-पटक, उत्पीड़न, गरीबी, साधनहीनता के संघर्ष और व्यथा-कथा की अभिव्यक्ति है.
नवगीत हृदय-प्रधान, छन्दबद्ध, प्रेम, संघर्ष और समस्याओं के उचित समाधान का काव्य है.
नवगीत की यह विशेषता है कि यह छन्दबद्ध होकर भी किसी वाद की लक्ष्मणरेखा के घेरे के अंदर नहीं, घेरे की अंतिम लकीर से भी कुछ दूर है.
अंत में अपने साहित्यिक गुरु स्व. डा. कमल सिंह (अलीगढ़) को न याद करना एक अपराध होगा. कुछ मित्र गुरु परंपरा में विश्वास नहीं रखते किन्तु मेरी गुरु में अटूट आस्था है. इस पुस्तक की भूमिका लिखने में लखनऊ के डा. मधुकर अष्ठाना जी का सहयोग सिर माथे और इस पुस्तक का नाम ‘भौचक शब्द अचंभित भाषा’ रखने के लिए उनका आभार व्यक्त करता हूँ. गाजियाबाद के डा. योगेन्द्र दत्त शर्मा जी का अनवरत् आभार कि अपने बहुमूल्य समय में से कुछ समय निकालकर इस पुस्तक की दूसरी भूमिका लिखकर प्रोत्साहन दिया. आवरण के अंत : पृष्ठ की निचोड़ भूमिका लिखकर फिरोजाबाद के डा. रामसनेही लाल शर्मा यायावर जी ने जो स्नेह अल्प समय में दिया उनका किन शब्दों में आभार व्यक्त करूँ,शब्द कम हैं. दूरभाष पर चलने वाले साहित्यिक व्हाट्सअप समूह, फेसबुक और पत्रिकाओं के संपादक मित्रों का भी आभार कि प्रत्येक रचना पर अपना स्नेह मेरी झोली में सहर्ष रखते गये. घर के सामने पार्क में खड़ी पानी की टंकी और मुख्य घर के सामने मेरी रक्षा करने वाले वे चार अशोक के पेड़ों को प्रणाम कि आपकी ओर जब भी देखा एक प्रेरणा दिए और गीत जन्मे. पड़ोसी सभी मित्रो को नमस्कार.
धन्यवाद.
दिनांक १५.०४.२०१८ शिवानन्द सिंह ‘सहयोगी’
‘शिवाभा’ ए-२३३
गंगानगर
मेरठ-२५०००१ (उ.प्र.)
दूरभाष- ०९४१२२१२२५५
अणु पता : shivanandsahayogi@gmail.com