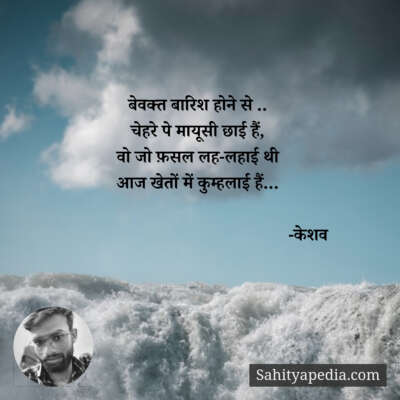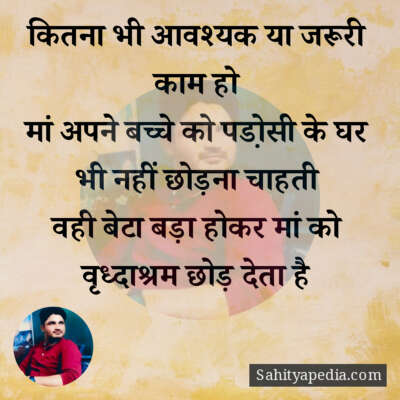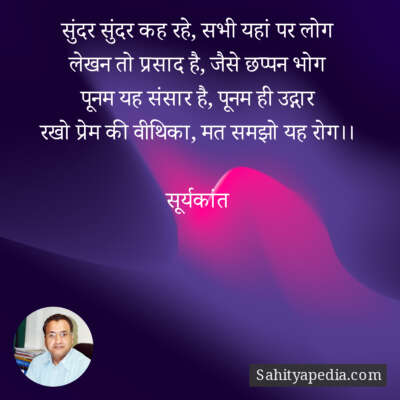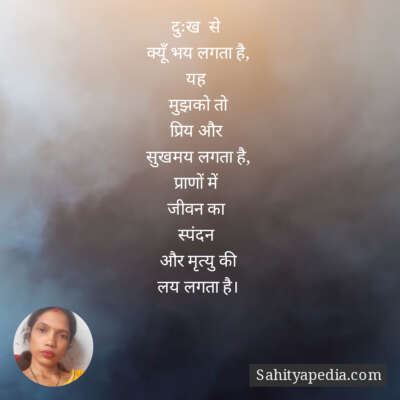‘मेरी आत्मकथा-किशोर साहू’ हिंदी सिनेमा के शुरुआती दौर की झांकी
पहली बार इस फिल्मी सितारे के नाम से मेरा परिचय 2011 में लोकमत समाचार, नागपुर के कार्यालय में संपादन कार्य के दौरान हुआ. सहकर्मियों के बीच नागपुर शहर से जुड़ी फिल्मी शख्सियतों की चर्चा चल रही थी. चर्चाओं के दौरान सोनू सूद, राजकुमार हिरानी के नाम आए, ये तो मेरे सुने हुए नाम थे, लेकिन ‘किशोर साहू’ मेरे लिए नया नाम था. नागपुर से जुड़ी शख्सियत होने के कारण उस वक्त लगाव-सा बन गया लेकिन बाद में मेरी मनोस्मृति से यह नाम ओझल हो गया. इसके बाद काफी लंबे अंतराल के बाद वर्ष 2017 में इस नाम से पुन: रू-ब-रूहुआ जब लोकमत समाचार के रविवारीय परिशिष्ट ‘लोकरंग’ में इनके बारे में संक्षिप्त जानकारी पढ़ी. इसके बाद ही ‘मेरी आत्मकथा किशोर साहू’ नामक किताब मेरे हाथ लगी जो मेरे कलिग पत्रकार हेमधर शर्मा जी से मिली. यह किताब राजकमल प्रकाशन ने सन 2017 में प्रकाशित की है. पृष्ठ संख्या 418 रुपए जबकि मूल्य 399 रुपए है. पुस्तक अमेजॉन में उपलब्ध है.
किताब इतनी शानदार लगी जो इतनी धाराप्रवाह और रोचक ढंग से लिखी गई थी कि तमाम व्यस्तताओं के बावजूद उसे पढ़ ही डाला. बीच में आपके प्रवाह को रोकने के लिए क्षमा याचना कर मैं यहां यह उल्लेख करना जरूरी समझता हूं कि मैं कोई किताब किसी से लेकर बहुत ही कम, अगर वह सहज दुकान में या आॅनलाइन उपलब्ध हो सकती है तो प्राय: खरीद कर ही पढ़ता हूं. कोई नवोदित रचनाकार अगर अपनी प्रकाशित कृति सौजन्य के तौर पर भेंट भी देता है तो मैं उन्हें उनकी उस किताब की मूल्य-निधि अवश्य ही देता हूं. खैर, तो इस आत्मकथा को पढ़ने में मुझे आठ-दस दिन का वक्त लगा. उसे पढ़कर मुझे इस तरह का अहसास हो रहा था कि मैंने स्वयं ही फिल्मी दुनिया के उस वक्त को साहू जी के साथ जी रहा होऊं. किताब इतनी रुचिकर लगी कि एक बार नहीं, तीन-तीन बार पढ़ी. अद्भुत लगा कि एक बहुआयामी व्यक्तित्व जो एक साथ अभिनेता, पटकथा लेखक, साहित्यकार, फिल्म निर्माता, निर्देशक सबकुछ था. यह शख्सियत विदर्भ की धरती पर ही पली-बढ़ी, शिक्षा हासिल की और कला-गुण सीखे और कम उम्र में ही मायानगरी में शून्य से ही अपना संसार रच लिया. आत्मकथा पढ़कर बॉलीवुड के ग्रे-लाइट पक्ष को करीब से जानने का मौका मिला. यह जानकर दुख भी हुआ कि इतनी बड़ी शख्सियत जो हमारे विदर्भ खासकर नागपुर शहर में पली-बढ़ी लेकिन उन्हें यहां कला, शिक्षा और पत्रकारिता से जुड़े ज्यादातर लोग नहीं जानते – आम जनता की कौन कहे. मुझे लगता है नागपुर के उस मॉरिस कॉलेज का मौजूदा शिक्षण स्टाफ भी नहीं, जहां इस महान शख्सियत ने शिक्षा हासिल की, जहां के वार्षिकोत्सव में शामिल होकर अभिनय व अन्य कलागुण सीखा. ‘लोकमत समाचार’ द्वारा हर वर्ष प्रकाशित होनेवाले दिवाली विशेषांक में जब मुझे अपना लेख देने का सुअवसर मिला तो मुझे लगा कि इस शख्सियत की जीवन-झांकी से पाठकों को अवगत कराया जाए लेकिन दुर्योगवश यहां भी स्थानाभाव के कारण यह आलेख प्रकाशित नहीं हो सका. यूं तो पाठकों को पूरी किताब पढ़नी ही होगी किंतु मेरी कोशिश होगी कि समीक्षा के तौर पर किताब के कुछ स्पृहणीय प्रसंगों को मैं उनके ही शब्दों में रखता चलूं.
किताब को पढ़कर यह प्रतीत हुआ हमारे विदर्भ-पुत्र किशोर साहू सिर्फ इसलिए अहम नहीं हैं कि वे इस क्षेत्र के पले-बढ़े अभिनेता हैं. इससे भी बड़ी बात ये है कि वे एकसाथ अभिनेता, कथाकार, उपन्यासकार, निर्माता और निर्देशक भी रहे – मुंबई की उस फिल्मी दुनिया में – जहां भाषा चाहे हिंदी, उर्दू हो या अंग्रेजी हो, किसी एक्टर-एक्ट्रेस को स्क्रिप्ट या डायलॉग रोमन लिपि में लिखकर दे दिए जाते हैं, वह भी उनसे ठीक से पढ़े नहीं जाते. साहित्य और किताबों की तो बात ही अलग है. अपना जीवन हिंदी से चमकाते हैं लेकिन इंटरव्यू अंग्रेजी में देते हैं. ये सारे नाम चमक रहे हैं – पुराने भी नए भी – लेकिन कितनी त्रासदपूर्ण बात है कि विदर्भ का यह सितारा जिसकी 2015 में जन्मशताब्दी थी लेकिन न तो उन्हें बॉलीवुड ने याद किया, न ही मीडिया ने, न ही हम विदर्भवासियों ने. आज यह किसको मालूम है 22 अक्तूबर 1915 को दुर्ग (छत्तीसगढ़) में जन्मे किंतु अधिकांशत: विदर्भ में पले-बढ़े किशोर साहू ने 1937-80 के दौरान लगभग 25 फिल्मों में अधिकतर बतौर हीरो अभिनय किया, 20 फिल्में डायरेक्ट की, 8 फिल्में लिखी, 4 उपन्यास, तीन नाटक और अनेक कहानियां भी लिखीं जो उनके जीवनकाल में ही अनेक पत्र-पत्रिकाओं के साथ ही पुस्तकाकार भी प्रकाशित हुर्इं. उन्होंने आज से 60 साल पहले विश्वप्रसिद्ध नाटककार शेक्सपियर के सर्वाधिक विख्यात और कठिन नाटक ‘हेमलेट’ पर इसी शीर्षक से फिल्म बनाने व उसमें स्वयं नायक का किरदार निभाने की आत्महंता कोशिश की थी. उनकी प्रतिभा में फिल्म- निर्माण, निर्देशन, अभिनय और साहित्य-सृजन के इस अद्वितीय संगम को देखकर ही उन्हें उनके सहयोगी-साथियों ने ‘आचार्य’ की अनौपचारिक लोक-उपाधि दी थी.
इस किताब में एक अहम बात यह निकलकर आई कि आत्मकथा का प्रकाशन किशोर साहूजी 1974 में ही कराना चाहते थे – इस बात का पता हिंदी के प्रख्यात उपन्यासकार राजेंद्र यादव जी के इस वक्तव्य से पता चलता है – ‘आत्मकथा के प्रकाशन के सिलसिले में किशोर साहू ने मुझे बंबई बुलाया. स्टेशन पर मुझे लेने आए थे किशोर के पिता कन्हैया लाल साहू, मैं ठहरा कमलेश्वर के यहां था. शाम को किशोर के यहां खाने पर उस परिवार से मेरी भेंट हुई. अगले दिन किशोर मुझे अपने वर्सोवा वाले फ्लैट पर ले गए जहां वे अपना पुराना बंगला छोड़कर शिफ्ट कर रहे थे. यहां हमने दिनभर आत्मकथा प्रकाशन पर बात की. वे इस आत्मकथा को दुनिया भर की तस्वीरों के साथ खूबसूरत ढंग से छपाना चाहते थे. लागत देखते हुए हम लोगों की स्थिति उस ढंग से छापने की नहीं थी. उन्होंने शायद कुछ हिस्सा बंटाने की भी पेशकश की थी. मगर वह इतनी कम थी कि अभिनंदन-ग्रंथ की तरह छापना हम लोगों के सामर्थ्य के बाहर की थी. आखिर बात नहीं बनी और मुझे दिल्ली वापस आना पड़ा.’’
यहां यह विशेष उल्लेख करना चाहूंगा कि किशोर साहू 14 मार्च 1931 को रिलीज हुई पहली सवाक फिल्म किशोर-वय (टीनएज) के लड़के की हैसियत से पर्दे के सामने देखकर ही सिनेमा के दीवाने हुए थे. इसके मात्र छह साल बाद खुद फिल्मों का इतिहास बनाने और उसमें अमर होने के लिए बाइस साल की उम्र में नागपुर जैसी मशहूर यूनिवर्सिटी और मॉरिस कॉलेज जैसी प्रतिष्ठित शिक्षण संस्थान का यह ग्रेजुएट नौजवान लाखों दर्शक का चेहता एक्टर-डायरेक्टर बन गया था.
बचपन से ही कलाभिरुचि
इस किताब में उन्होंने अपनी तेज स्मृति का दावा करते हुए लिखा है- ‘जब मैं छोटा था, यानी दो-ढाई वर्ष का तबसे मुझे याद है मैं सुंदर वस्तुओं को बटोरा करता था. जब चार साल का हुआ, न जाने कहां से मेरे पास देवदार की लकड़ी का बना संदूक आ गया, जिस पर रंदा नहीं था, न ही वार्निश. उसी बक्से में सुंदर-सुंदर वस्तुओं को संजोया करता और अवकाश के अवसर पर उस बक्से को खोलकर, उसमें निहित अपनी संपदा को बाहर निकाल, उसका निरीक्षण किया करता था. अपने उस अमूल्य संकलन के निरीक्षण में मुझे जो आनंद, समाधान, जो तृप्ति मिलती थी, वह अकथनीय है.
उन खूबसूरत चीजों में केवल खिलौने ही नहीं थे- खिलौने तो कम ही थे, खिलौने तो हर किसी बच्चे के पास होते हैं और वे मुझे सदा ही पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध रहे हैं – उनमें असाधारण, अनोखी अद्भुत चीजें थीं जैसे फानूस का रंगीन लोलक, बया पक्षी का घोंसला, भुट्टे की सुनहरी मुलायम बालियां (जो बाद में सूखकर काली हो गई थीं), स्त्रियों के बालों में लगानेवाला गटापार्चा का जापानी क्लिप, मेले में खरीदी हुई सीटी, डिबिया, काठ की बनी तिकोनी गुड़िया (जिसकी बड़ी-बड़ी आंख विलक्षण थी) कांच की रंग-बिरंगी गोलियां, मरी हुई तितलियां, किताब के बीच दबाकर सुखाए हुए जंगली फूल, नदी पर पाई गई सीपें, शंख, घोंघे, चिकने रंगीन पत्थर, जेब घड़ी की टूटी हुई चैन, छाते का हाथी दांत का हैंडल….’’ इस तरह यह बहुत लंबी सूची है जो आत्मकथा में दी हुई है. आगे वे लिखते हैं – ‘‘मैट्रिक पास करते समय जब अन्य छात्र अपने स्वच्छंद और भावी स्वप्नों को जीवंत करने में अग्रसर पाते थे, मैं अपने अतीत में संजोई हुई उन विलक्षण वस्तुओं के मोह में फंसा तथा बचपन की स्मृतियों के जाल में जकड़ा हुआ था.’’ यही पवृत्ति उनके कैरियर में लाभदायक साबित हुई. कै
बचपन में ही पहला क्रश
किताब में लिखा एक रोमानी प्रसंग उनके व्यक्तित्व के महत्पवूर्ण आयाम को हमारे सामने रखता है जिसने उनके अंदर एक कलाकर की बुनियाद रखी. आत्मकथा में वे लिखते हैं – ‘‘गोंदिया में हमारा घर रेलवे स्टेशन के बिल्कुल करीब था. रात-दिन इंजन की सीटी, भक-भक की आवाजें और डब्बों के शंटिंग की गड़बड़ाहट सुनाई पड़ती. दो क्रिस्तान युवतियां फ्लोरा और रोजी (ये नाम कल्पित हैं) हमारे घर कभी-कभी आया करती थीं. दोनों बहनें थीं. रोजी छोटी थी, लगभग 18 वर्षीया और वह फ्राक पहनती थी. एक बार किसी के साथ मैं उनके घर भी गया था. वहां एक युवक भी आया था जो धोती पहना था. मैं आधा घंटा शायद रहा हूंगा मगर इतनी देर में मेरी – छह वर्ष के बालक की – आंखों ने ताड़ लिया था कि रोजी और उस युवक में परस्पर कोई गुप्त संबंध है, जो मुझे अच्छा लगा और इस संबंध में मेरे बाल-हृदय में जिज्ञासा जागृत हुई थी – रोजी मुझे अच्छी लगती थी, सुंदर लगती थी. उसके समक्ष मेरे हृदय की धड़कनें बढ़ जाती थीं.’’ उनकी इस आत्मकथा में गोंदिया-भंडारा से उनके साथ जुड़े अनेकानेक दिलचस्प, मनोवैज्ञानिक, ज्ञानवर्धक प्रसंग और उस काल की उपयोगी-तथ्यपूर्ण जानकारी मिलती है जो उनकी पूरी आत्मकथा पढ़कर ही जानी जा सकती है.
शिक्षा प्रणाली पर उनके खयान
शिक्षा प्रणाली पर उनके सहज विचार उनके ही शब्दों में ‘‘गोंदिया में हम दोनों भाइयों को जी (पिता जी को सिर्फ ‘जी’ संबोधित करते थे) ने एक मास्टर रख दिया – चार रुपए मासिक वेतन पर. उसने मुझे प्रवेशिका पढ़ाई, पहली और दूसरी कक्षा की पुस्तकें भी पढ़ाई. ‘खिलौना’ नामक पुस्तक भी मैंने पढ़ी थी. उन दिनों दो-एक और भी पुस्तकें हुआ करती थीं. उदाहरणार्थ हिंदी की समस्त बारह खड़ी कविता में पिरोई गई थी. अ- अज बकरा कहलाता है. आ- आम चूसकर खाता है आदि. बड़ी बहन छोटे भाई को पढ़ना सिखा रही है. उसका रेखाचित्र भी बना हुआ है, जो मुझे अब भी याद है. कितनी सुंदर थी वह पुस्तक – ‘खिलौना’ और कितनी बढ़िया थीं उसमें छपी रचनाएं. छोटे बच्चों को पढ़ाई जानेवाली आज की शुष्क और ऊटपटांग पुस्तकें देखता हूं तो शिक्षा विभाग के महापुरुषों पर मुझे बहुत गुस्सा आता है.’’
फिल्मों से पहला परिचय
चलते-फिरते बाइसकोप (साइलेंट ट्रेवलिंग सिनेमा) कभी-कभी शहर में आया करता. आठ-दस चित्र मैंने देखे. ‘टाइपिस्ट गर्ल’ और ‘अनार कली’ – ये दो फिल्में मुझे विशेष जंचीं. नायिका मिस सुलोचना थीं. मेरे दिल में उतर गई थीं. मैं ही क्या सारा जमाना उन दिनों सुलोचना पर मरता था. पत्रिकाओं में उससे संबंधित कितने ही लेख, समालोचनाएं पढ़कर मैंने जानकारी हासिल की हुई थी. सुलोचना का असली नाम रूबी मायर्स था. कुंआरी थीं. सब अभिनेत्रियों से अधिक रूपवती थीं. सबसे अधिक वेतन पाती थीं- सुना था 5000 रु. महीना और सबसे अच्छा अभिनय करती थीं.’’ ‘‘उन दिनों मैं नहीं जानता था कि सात-आठ साल के अंदर ही मैं उस परम सुंदरी सुलोचना को साक्षात हाड़-मांस में देखूंगा. मैं नहीं जानता था कि मैं एक समय उस शिखर पर पहुंचूंगा और वही सुलोचना मुझसे मिलने, मेरे चित्रों में काम मांगने के लिए उतावली और बावली रहेगी.’’ यह प्रसंग बड़ा ही मार्मिक है. पुस्तक में ही पढ़ें तो बेहतर होगा.
नागपुर शहर से पहला परिचय
‘‘उन्हीं दिनों ‘आर्य सुबोध’ नाटक कंपनी नागपुर आया करती थी. भंडारा से नागपुर केवल 40 मील दूर है. यह कंपनी तरह-तरह के नाटक प्रस्तुत करती थी. उस नाटक कंपनी के मुख्य नायक बी.ए. बेंजामिन थे. यहूदी थे. उनकी मातृभाषा मराठी थी लेकिन हिंदी, उर्दू बहुत अच्छी बोलते थे. मां और हम बच्चों को लेकर जी (पिताजी) अक्सर नागपुर जाते और हमें नाटक दिखाते. पिताजी की बेंजामिन से दोस्ती हो गई थी. ‘हेमलेट’ मैंने कई-कई बार देखा. बेंजामिन हेमलेट के चरित्र में बस कमाल ही करते थे. कई दिनों तक नाटक के विभिन्न दृश्य मेरी आंखों के सामने झूला करते. मन ही मन मैंने ठान लिया था कि मैं भी अभिनेता बनूंगा. नागपुर के ‘व्यंकटेश थियेटर’ में एक दिन बड़ा होकर ‘हेमलेट’ की भूमिका करूंगा. एक दिन नागपुर में बेंजामिन ने हमारे परिवार को चाय के लिए अपने निवास स्थान पर आमंत्रित किया. उस दिन मैंने पहली बार बैंजामिन – अपने प्रिय हेमलेट – को रूबरू घरेलू यानी हमारे जैसे कपड़े पहने देखा.
मॉरिस कॉलेज में दाखिला
‘… भाई की मौत का दुख था. बड़ी मुश्किल से परीक्षा में बैठ पाया. पढ़ाई में मन नहीं लगता था. भाई की याद दिन-रात बेजार करती थी. लेकिन नतीजा जब निकला तो सेकेंड डिवीजन में मैट्रिक पास हो गया. उन दिनों नागपुर का मॉरिस कॉलेज श्रेष्ठ समझा जाता था. मैं मॉरिस कॉलेज में दाखिल हो गया. मैं अपने नागपुर की न्यू कॉलोनी में चाचा के पास पास रहने लगा.
नागपुर बहुत बड़ा शहर है. मॉरिस कॉलेज बहुत अच्छा कॉलेज था. योग्य प्राध्यापक थे. कॉलेज में 300 लड़के और 52 लड़कियां. सहशिक्षा का चलन उन दिनों नया-नया हुआ था. शहर के अन्य कॉलेज में लड़कियां गिनी-चुनी थीं. इसलिए मॉरिस कॉलेज में रौनक थी. तब स्कूलों में सहशिक्षा नहीं होती थी. इसलिए हम लड़कों ने जब लड़कियों को, और तरह-तरह की इतनी सारी लड़कियों को अपने पास देखा तो अजीब-सा लगा यानी अच्छा लगा. मगर लड़कियों का कॉमन रूम अलग था. क्लास में भी वे सब सामने की बैंचों में बैठती थीं. क्लास के बाहर निकलकर टोली बनाकर अहाते में घूमा-फिरा करतीं. लड़के दूर-दूर से उन पर आंखें सेंकते. उनसे मिलने-बोलने के लिए तरसते थे. पर हिम्मन न पड़ती और दिल मसोसकर रह जाते.
पहला वर्ष ‘फर्स्ट ईयर फूल’ बनने में तरह-तरह की बेवकूफियों में, फैशन और स्टाइल करने की कोशिशों और कॉलेज की लड़कियों की चकाचौंध में गुजर जाता है. मेरे साथ भी यही हुआ. पर मैं वर्ष के अंत तक कॉलेज की डिबेट में भाग लेने लगा था. कुछ लड़कियों से बोलचाल का संबंध स्थापित हो गया था.
..और वह मेरा प्रिय बक्सा नष्ट हो गया
नागपुर में घर से मां और जी के पत्र बराबर आते थे. एक पत्र में जी ने लिखा- ‘समझ में नहीं आता, तुम्हें कैसे बताऊं कि तुम्हारे बचपन का वह देवदार का बक्सा जिसमें तुम्हारी संपदा संजोई हुई थी, नष्ट हो गया. वह बक्सा हमने स्टोररूम में रख दिया था. खोलकर देखा तो तुम्हार बक्सा बिलकुल सड़ गया था. और अंदर की चीजें नष्ट हो चुकी थीं. यह सब हमारी गफलत के कारण हुआ है. हमें इसका बहुत दुख है.’
पत्र पढ़कर मुझे ऐसा लगा मानों बहुत सारे सगे-संंबंधियों, संगी-साथियों के एकसाथ मर जाने की मुझे खबर मिली हो. उस दिन में रो-रो दिया. वर्षों तक, जब बक्से की याद आती, दिल में एक टीस-सी उठती थी.
अंगेजी पर जुबान को किया काबू
यहां पुराने साथियों से फिर मुलाकात हुई. अबकी बार कुछ नए लड़के-लड़कियां भी आए थे. मैंने फारसी ले रखी थी इसलिए मेरी मुस्लिम छात्रों से अच्छी दोस्ती थी. भूख लगती तो मुस्लिम मैस में खा लिया करता था. मगर मेरे दोस्त सभी जाति-धर्म के लोग थे- हिंदी भाषी और मराठी भी, क्रिस्तान और फारसी भी, लड़के और लड़कियां भी. जितने क्रिस्तान और एंग्लो इंडियन छात्र थे, सब अंग्रेजी माध्यम से मैट्रिक पास करके कॉलेज में आए थे. स्वाभाविक था अंग्रेजी खूब बोलते थे. मैं मराठी माध्यम वाला था, इसलिए कॉलेज के फर्स्ट ईयर में जब आया तो अंग्रेजी बोलने में जबान लड़खड़ाती थी, पर अंग्रेजी माध्यम वाले छात्रों से दोस्ती और सतत उनके साथ रहने से पहले वर्ष के अंत तक मैं भी अंग्रेजी बोलने लग गया था.
हिमांशु राय के ‘कर्म’ चित्र का भव्य प्रदर्शन
इसी समय पत्र-पत्रिकाओं में ‘कर्म’ फिल्म की जोरदार प्रसिद्धि निकली. हिमांशु राय नामक सभ्य-सुशिक्षित व्यक्ति ने विलायत जाकर इस फिल्म का निर्माण किया था. स्वयं नायक की भूमिका की थी. मुख्य नायिका उनकी पत्नी देविका रानी थीं, जो महान कवि रवींद्रनाथ टैगोर की भांजी थीं. सहनायिका में चित्र ‘वरदान’ की राजकुमारी सुधा देवी थीं. फिल्म का उद्घाटन लंदन में वहां के प्रधानमंत्री के कर कमलों द्वारा हुआ था. फिल्म सराही गई थी. अब वह फिल्म भारत में प्रदर्शित होने जा रही थी.
‘कर्म’ चित्र क्या आ रहा था, भारतीय सिने-इतिहास में यह पहली असाधारण प्रभावशाली विज्ञप्ति थी. दूर-दूर के जिलों से लोग ‘कर्म’ देखने नागपुर आ रहे थे. न जाने क्यों मैं विशेष रूप से उत्तेजित था. फिल्म नागपुर आई और उसका रीजेंट सिनेमाघर में प्रदर्शन हुआ. देविकारानी और हिमांशु राय फिलम के साथ नागपुर पधारे थे. सिनेमाघर के संचालक जगाराव नायडू और मालिक नरसिंहदास डागा ने अतिथियों का राजसी सत्कार किया. थियेटर में ऐसी अपार भीड़ मैंने कभी न देखी थी. पुलिस बैंड बजाया गया और फूलों की बौछार से थियेटर महक उठा.
जागा एक्टर बनने का सपना
पिता जी सदा से मुझे विलायत भेजकर बैरिस्टर बनाने का सोचते थे. अब तक मैं भी बैरिस्टर बनने का सपना देख रहा था. और उसी के लिए अपने को तैयार भी कर रहा था. पर अब कॉलेज के दूसरे साल सहसा मेरा विचार बदल गया. अब मैं बैरिस्टर नहीं, एक्टर बनना चाहता था. और अब मैं इसी लक्ष्य पर सक्रिय हो गया. शहर में जमनादास पोद्दार नामक एक मारवाड़ी सज्जन ने ‘सुदर्शन मूवी टोन’ नामक फिल्म कंपनी खोली हुई थी. शहर के बार इंदोरा गांव के पास उनका एक बंगला था. जहां सुना जाता था चित्र निर्माण की तैयारियां हो रही थीं. दो वर्ष पूर्व जबलपुर के सेठ गोविंद दास और पंडित द्वारिकाप्रसाद मिश्र ने मिलकर एक चित्र प्रस्तुत किया था जिसका नाम था ‘धुआंधार’. उसकी नायिका लीला चिटणिस थीं जिसमें भंडारा निवासी नाना पलसीकर ने पहली बार चरित्र भूमिका की थी. चित्र असफल रहा था और कंपनी बंद हो चुकी थी. पर नागपुर में ‘सुदर्शन मूवी टोन’ खुलने की सनसनी से वातावरण झंकृत हो उठा था. छुट्टी के एक दिन मैं इस कंपनी में जा पहुंचा. बंगले पर ‘सुदर्शन मूवी टोन’ की तख्ती लगी हुई थी. वहां मैंने अपना परिचय देते हुए फिल्म में अपनी दिलचस्पी दिखाई. हालांकि मुझे यह बात समझने में देर न लगी कि इस कंपनी की माली हालत खस्ता थी. कभी बंगले पर एक ही जून खाना बनता था, कभी दो जून चूल्हा न जलता और उधार की मंगाई हुई चाय और भजिए से काम चलता था. जिस आशा से मैं पहली बार ‘सुदर्शन मूवी टोन’ गया था, वह टूट चुकी थी पर फिर भी वहां जाया करता था क्योंकि वहां के प्रमुख स्वामी जी और उनकी वह अनोखी दुनिया मुझे भा गई थी. स्वामी जी का नाम कृष्णानंद सोख्ता था.
स्वामीजी अब हमारे बंगले पर आने-जाने लगे थे. पिताजी से भी उनकी मुलाकात हो गई और वे उनके भी मित्र बन गए थे. हमारे बंगले पर हफ्ते-दो हफ्ते में अक्सर ही बैठकें हुआ करती थीं जिसमें स्वामी जी घंटों अपना गाना सुनाते, अपने लिखे नाटकों का उद्धरण अभिनीत करके दिखाते थे.
स्वामी जी ने बेकारी से खीझकर सहसा शहर में एक नाटक प्रस्तुत करने की ठानी. डी.एल. राय का मशहूर नाटक ‘शाहजहां’ चुना गया. हफ्ते भर के अंदर योजना ने वास्तविक रूप ले लिया. स्वामी जी के एक पोस्टकार्ड पर न जाने कहां-कहां से उनके साथी आ गए.
शहर की एक युवती भी उनके पास आने-जाने लगी. जो सुनने में आया कि शाहजहां की पत्नी की भूमिका करनेवाली थी. मेरे मन भी लहरें उमंगें मारने लगीं. मैंने स्वामीजी से इच्छा प्रकट की. मैंने मुख्य भूमिका- शाहजहां का चरित्र- मांगी जो तुरंत उन्होंने दे दी. और मैं इस प्रकार जुट गया.
महीने भर की लगातार रिहर्सल के बाद नाटक तैयार हो गया. ‘व्यंकटेश थियेटर’ में नाटक प्रस्तुत होने जा रहा था. इसी व्यंकटेश थियेटर में मैंने बैंजामिन को ‘हेमलेट’ खेलते देखा था. और चाहा था कि बड़ा होकर एक दिन इसी मंच पर ‘हेमलेट’ की भूमिका में आऊं. बचपन का वह सपना साकार होने जा रहा था- ‘हेमलेट’ न सही ‘शाहजहां’ ही सही.
आखिर वह शुभ दिन आया. थियेटर खचाखच भरा हुआ था. जोरदार धमाके के साथ परदा उठा और नाटक शुरू हो गया. इसके बाद मेरा इस क्षेत्र में आकर्षण बढ़ गय. बाद में मैंने कॉलेज की गैदरिंग में भी नाटक में हीरो की भूमिका अदा की. सोशल गैदरिंग के बाद मैं तो फिर कॉलेज का हीरो बन गया.
बंबई चला हीरो बनने
बंबई जाकर सिनेमा में अपनी किस्मत आजमाने का इरादा मैंने घरवालों को बताया. घरवाले पिछले दो साल से मेरा रंग-ढंग देख रहे थे. मेरे कमरे में पाठ्यपुस्तकों के साथ देसी-विदेशी सिने पत्र-पत्रिकाओं का ढेर लगा रहताा. विदेशी ‘पिक्चर शो’ और देसी ‘फिल्म इंडिया’ का बहुत चलन था. मां ने तो पहले प्रस्ताव का विरोध किया पर जब पिताजी मान गए तो वे भी मान गर्इं. लेकिन अब ताऊ जी का डर था. वे भी पुराने ख्याल के और रूढ़िवादी थे. उनसे छिपकर मुंबई जाने की तैयारी करने लगा लेकिन जाने से पहले उन्हें पता चल गया. मुझसे पूछने पर मैंने कहा- यूं ही घूमने जा रहा हूं. दस-पंद्रह दिनों में लौट आऊंगा. वे बोले- ‘देखो जी, वे बोले घूमघाम के लौट जाओ. सिनेमा-विनेमा के चक्कर में मत पड़ना.’ दुबक कर मैं उनके बंगले से निकल आया. घर आकर बंबई यात्रा के लिए अपना समान जुटाने-बांधने में लग गया, परीक्षाफल को विलंब था. पर मुझे विश्वास था कि सेकेंड डिवीजन में पास अवश्य ही हो जाऊंगा.
द्वारकादास डागा, प्रो. चोरडया, दिनेश नंदिनी और मैं फर्स्ट क्लास के एक ही डिब्बे में बैठकर नागपुर से मुंबई के लिए मेल से रवाना हो रहे थे. पिताजी, मां, मेरे भाई-बहन और रमेश गुप्ता तथा मित्रमंडली मुझे छोड़ने स्टेशन तक आए थे. मैं घर से पहली बार परदेश जा रहा था- मां-बाप, भाइयों-बहनो से दूर बंबई जो अरब समुद्र के तट पर भारत का बहुत बड़ा शहर है, जहां फिल्में बनती हैं, जहां के लोग बड़े होशियार, चालाक हैं. बड़ा पैसा है जहां, जो शहर मायानगरी कहलाता है, मैं उस नगरी में अपनी किस्मत आजमाने जा रहा था.
स्टेशन से बंबई की ओर जाती हुई ट्रेन के दरवाजे पर खड़ा मैं बहुत देर तक रूमाल हिलाते रहा और हिलते हुए रूमालों को देखते रहा- जो मेरे प्रियजन हिला रहे थे, तब तक देखता रहा जब तक ट्रेन मुड़ न गई.
इस तरह हमारे विदर्भ का यह लाडला पुत्र ‘हीरो’ बनने बंबई चला जाता है. वहां जाकर उसे क्या-क्या करना पड़ता है, अनेक सुखद-दुखद संयोगों का किस तरह सामना करना पड़ता है. आखिरकार सफलता उनके कदम चूमती है. किस तरह से विदर्भ की यह माटी आगे चलकर किस तरह चमकती मूरत बनती है, यह इस किताब में है. आगे के प्रसंग और भी प्रेरणीय, रुचिकर, रोमांचक और अत्यंत मर्मस्पर्शी हैं- यह सब जानने के लिए आपको लगभग 418 पृष्ठीय पूरी किताब ही पढ़नी होगी- ‘मेरी आत्मकथा किशोर साहू’