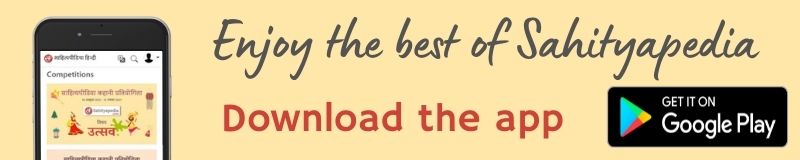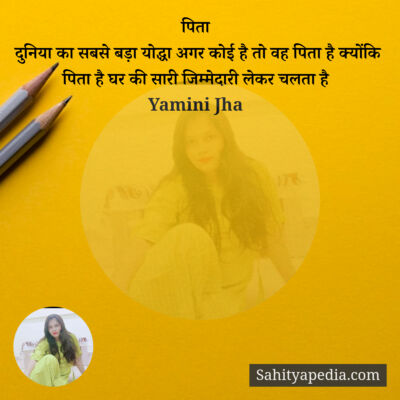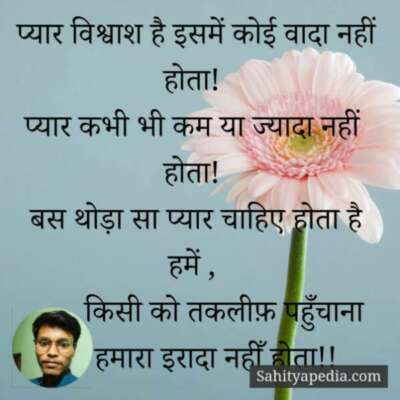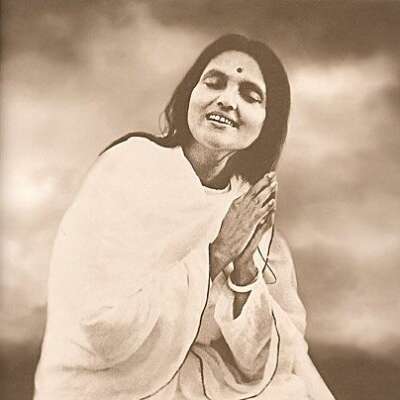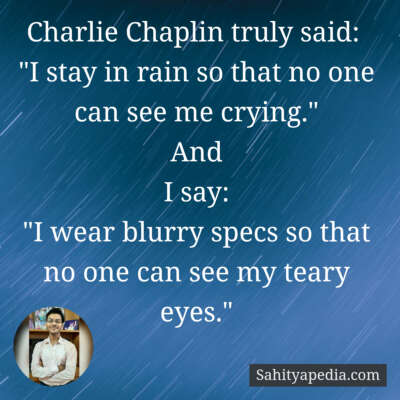*पुस्तक समीक्षा*

पुस्तक समीक्षा
पुस्तक का नाम: ब्रह्मविद्या के मोती
लेखक: उमाशंकर पांडेय (अध्यक्ष उत्तर प्रदेश तथा उत्तराखंड फेडरेशन थियोसोफिकल सोसायटी)
प्रकाशक: इंडियन बुक शॉप, थियोसोफिकल सोसायटी, कमच्छा, वाराणसी 221010
प्रथम संस्करण: 2024
प्रष्ठ संख्या: 433
समीक्षक: रवि प्रकाश
बाजार सर्राफा (निकट मिस्टन गंज), रामपुर, उत्तर प्रदेश 244901
मोबाइल/ व्हाट्सएप 9997615451
——————————–
ब्रह्म विद्या के मोती उमाशंकर पांडेय के ऊंचे दर्जे के विचार-प्रधान लेखों का संग्रह है । इनमें आध्यात्मिक और सांसारिक जीवन के परिप्रेक्ष्य में थियोस्फी की शिक्षाओं के अनुरूप दृष्टिकोण पर चर्चा की गई है। प्रत्येक थियोसॉफिस्ट को यह जिज्ञासा रहती है कि विभिन्न विषयों पर थियोस्फी के प्रामाणिक उच्च स्रोतों से क्या मार्गदर्शन मिला है ? लेकिन जानकारी के अभाव में वह जीवन की दिशा को थिओसफी के पूर्णतः अनुकूल नहीं बना पाता।
उमाशंकर पांडेय ने संसार में जीवन जीने वाले व्यक्ति को संसार से पलायन न करते हुए उच्च आध्यात्मिक चेतना का पात्र बनने के लिए जो लेख उपलब्ध कराए हैं, उनके प्रकाश में थियोस्फी के अनुयायियों को प्रामाणिक पथ सुलभ हो सकेगा।
इक्कीस अध्याय या कहें कि ब्रह्म विद्या पर यह इक्कीस लेख जीवन जीने की कुंजी कहे जा सकते हैं। आइए एक-एक अध्याय पर चर्चा आरंभ करें।
🍃🍃
1) गुप्त विद्या
🍃🍃
पहला लेख ‘गुप्त विद्या’ के संबंध में है। इसमें लेखक ने यह बताया है कि मनुष्य के भीतर एक क्षमता है जो अत्यंत श्रेष्ठ है तथा इसके द्वारा हम श्रेष्ठतर ज्ञानियों से एकता कर सकते हैं, शरीर की इंद्रियों से ऊपर उठ सकते हैं तथा उच्चतर अस्तित्व और दिव्य लोकों के निवासियों की मानवेतर शक्तियों में सहभागी भी बन सकते हैं। (पृष्ठ 12)
इस अवस्था को प्राप्त करने की दृष्टि से लेखक ने समाधि के बारे में प्रकाश डाला है और कहा है कि केवल कुछ ही सिद्ध पुरुष होते हैं जो गहन समाधि में जा सकने में समर्थ होते हैं और परमानंद को प्राप्त कर पाते हैं। ऐसे व्यक्तियों का ‘सर्व’ से एकाकार हो जाता है। अनंत से संपर्क होता है। लेकिन लेखक ने यह भी कहा है कि अन्य सामान्य व्यक्ति इस अवस्था का शब्दों में वर्णन नहीं कर सकते। (पृष्ठ 15)
लेखक ने थियोसोफी को विज्ञानों का विज्ञान बताया है। (प्रष्ठ 16)
उसने कहा है कि थिओसफी सत्य की खोज है। यह ऐसी मशाल है जिसके प्रकाश को केवल जागृत जीवात्मा की आंखों से ही पहचाना जा सकता है। (पृष्ठ 18)
लेखक ने थिओसोफी को ज्ञान, विद्या और हिंदुओं की ब्रह्म विद्या का और हिमालय पार सिद्धों के ज्ञान का पर्याय बताया है। उसने एक ऐसी ‘रहस्य भाषा’ की चर्चा की है, जिसको जाने बगैर गुप्त विद्या के क्षेत्र में बहुत आगे तक कोई व्यक्ति नहीं जा सकता। ‘रहस्य भाषा’ को सीखने के लिए गुरु की आवश्यकता होती है। शिष्य को भी प्रतिभावान होने की आवश्यकता होती है। (पृष्ठ 20,21)
गुप्त विद्या के संदर्भ में ईश्वर पर चर्चा करते हुए लेखक ने बताया है कि मनुष्य के बाहर किसी व्यक्तिगत ईश्वर में विश्वास न करके हम एक परम-तत्व में विश्वास करते हैं। वह ईश्वर न पदार्थ है, न पदार्थ-सार, न ही विचार बल्कि उन सभी चीजों का पात्र या कंटेनर है; परम कंटेनर। ईश्वर के अस्तित्व की भूलभुलैया को रहस्योद्घाटित करते हुए लेखक का मत है कि ईश्वर वह है जो अस्तित्व में नहीं है, लेकिन जो है।( प्रष्ठ 22, 23)
गुप्त विद्या को जानने के लिए व्यक्ति को मनुष्य और मनुष्य के बीच की जा रही क्रूरता को रोकने में काम करना होगा। अपने पड़ोसी से प्रेम करना होगा। स्वयं खाने से पहले जो दूसरा भूखा है; उसे भोजन उपलब्ध कराना होगा। अंत में लेखक कहता है कि जब एक मनुष्य वास्तविक गुप्त-विद्याविद् बनता है, तब वह संसार में अच्छाई के लिए एक बल बन जाता है (पृष्ठ 27, 28)
🍃🍃
2) एक जीवन एक चेतना
🍃🍃
इस लेख में समूचे विश्व में एक जीवन, एक चेतना के अनुभव पर बल दिया गया है। समूचा ब्रह्मांड अविभाज्य बताया गया है। जितने भी विभाजन हैं ,वह कृत्रिम हैं । हालांकि उनके अस्तित्व की एकता के रहस्य को लेखक के अनुसार वे ही जान सकते हैं, जो निर्वाण स्तर को स्पर्श कर चुके हैं।( पृष्ठ 30 )
गीता में श्री कृष्ण के उपदेशों को उद्धृत करते हुए लेखक ने कहा है कि गुप्त विद्या के द्वारा हम सब प्रकार की माया को भेद कर एकत्व का अनुभव कर सकते हैं। इस दृष्टि से लेखक ने गीता के इस कथन को उद्धृत किया है कि “जो मुझे देखता है अर्थात जो एक स्व या आत्मा को देखता है, प्रत्येक चीजों में मुझे और मुझ में प्रत्येक चीजें; वास्तव में वही देखता है।”( प्रष्ठ 36)
अंत में लेखक ने इस बात पर बल दिया है कि गुप्त विद्या के साधकों को एक जीवन, एक चेतना का अनुभव करने के लिए सब प्रकार के अलगावपन को समाप्त करना ही होगा। सृष्टि के हर मनुष्य को अपने साथ जोड़कर ही हम एक जीवन, एक चेतना का अनुभव कर सकते हैं।
🍃🍃
3) ईश्वर और देवगण
🍃🍃
देवताओं के संबंध में कहना कठिन है। ईश्वर के बारे में चर्चा और भी कठिन है। इसलिए इस लेख में उमाशंकर पांडेय ने विभिन्न विद्वानों के कथन उद्धृत किए हैं। न केवल थिओसफी के प्रमाणिक स्रोतों से विचार दिए हैं अपितु स्वामी विवेकानंद आदि के विचारों को भी सामने रखा है।
शुरुआत में ही लेखक ने मैडम ब्लेवेट्स्की को उद्धृत किया है और बताया है कि सवाल यह नहीं है कि हम ईश्वर में विश्वास करते हैं या नहीं, बल्कि सवाल यह है कि हम जिस ईश्वर में विश्वास करते हैं उसका स्वरूप कैसा है ? दि सीक्रेट डॉक्ट्रिन को उद्धृत करते हुए लेखक ने कहा है कि ईश्वर विचार की सीमा और पहुंच से बाहर है। लेखक ने लिखा है कि एक परम तत्व है जिसकी अनुभूति हम केवल अपने हृदय में कर सकते हैं।( प्रष्ठ 42)
मैडम ब्लेवेट्स्की को उद्धृत करते हुए लेखक का कथन है कि मनुष्य-आत्मा ईश्वर-आत्मा को सिद्ध करती है। ईश्वर को मनुष्य की आत्मा के अलावा अन्य किसी तरह प्रदर्शित नहीं किया जा सकता। पानी की एक बूंद ही महासागर को सिद्ध करती है।( पृष्ठ 44)
प्रश्न यह है कि देवता कौन हैं ? लेखक ने इन्हें प्रकृति की अदृश्य शक्तियों की ज्ञात अभिव्यक्ति बताया है। (पृष्ठ 44, 45)
देवताओं के संबंध में लेखक का कथन है कि देवता-गण शुद्ध आत्माएं हैं जो ईश्वर के अधिक निकट हैं। लेख में यह भी बताया गया है कि देवता गण या ध्यान चौहान जीवित लोग हैं। देवता केवल एक उच्चतर प्रकार के मनुष्य हैं। (पृष्ठ 53)
‘की टु थियोस्फी’ पुस्तक को उद्धृत करते हुए लेखक का कहना है कि हमारे देवता न तो किसी स्वर्ग में हैं, न ही किसी विशेष पेड़ भवन या पर्वत में हैं, वह सर्वत्र हैं ।(पृष्ठ 54)
विषय का उपसंहार लेखक ने जीवन को लोक कल्याण के लिए समर्पित करने में बताया है। सब प्रकार के पाखंड का विरोध करें। हृदय में ही ध्यान करें। कर्म को पूजा मानें। सामाजिक वैचारिक सुधार के आंदोलनों में यथा पर्यावरण की रक्षा, जानवरों के प्रति क्रूरता रोकना, बच्चों और वंचित लोगों को अधिकार-संसाधन दिलाना आदि में अधिक से अधिक भागीदारी करें; क्योंकि यह कार्य भी आध्यात्मिक ही हैं ।अंत में लेखक कहता है कि सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हम अपने अंदर के ईश्वर अर्थात प्रेम और सत्य, न्याय और प्रज्ञा, अच्छाई और शक्ति के भाव का अनुसरण करते रहे। (प्रष्ठ 71)
🍃🍃
4) मनुष्य क्या है
🍃🍃
मनुष्य के बारे में तो सब जानते हैं लेकिन उसको परिभाषित करना टेढ़ी खीर है। लेखक ने मनुष्य को घर, परिवार, जाति, धर्म राष्ट्रीयता आदि की सीमाओं में परिभाषित करते हुए उसकी जीव वैज्ञानिक पहचान पर भी चर्चा की है। लेकिन आगे चलकर वह विभिन्न विद्वानों द्वारा मनुष्य के स्वरूप और उसके कार्यों पर चिंतन करने के लिए आगे बढ़ा है। लेखक ने मनु-संहिता का हवाला देते हुए लिखा है कि सभी कर्तव्यों में से प्रमुख कर्तव्य सर्वोच्च आत्मा का ज्ञान प्राप्त करना है। यह सभी विज्ञानों में से पहले है क्योंकि केवल यही मनुष्य को अमरता प्रदान करता है। (पृष्ठ 89)
एक अन्य उद्धरण में लेखक ने बताया है कि मनुष्य कोई विशेष सृजन नहीं है, वह इस धरती पर किसी भी अन्य जीवित इकाई की तरह प्रकृति के क्रमिक सुधार कार्य का उत्पादन है। (पृष्ठ 79)
एक अन्य संदर्भ को उद्धृत करते हुए लेखक का कहना है कि विकास की संपूर्ण योजना में मनुष्य का सबसे महत्वपूर्ण स्थान है। वह वहां खड़ा है, जहां आत्मा और पदार्थ मिलते हैं । वह उच्चतर प्राणियों और नीचे के प्राणियों के बीच की कड़ी है। (पृष्ठ 80)
सत्रहवीं शताब्दी की एक रचना को उद्धृत करते हुए मनुष्य की दयनीयता को लेखक ने अभिव्यक्त कर दिया है। लिखा है-” मनुष्य शरीर को झुकाकर धरती से गंदगी और तिनके उठा रहा है। वह इस दासोचित कार्य में इतना व्यस्त है कि वह अपने सिर के ऊपर मंडरा रहे एक देव- जो उसे एक स्वर्ण मुकुट प्रदान कर रहा है -को देखने में विफल रहता है। (प्रष्ठ 84)
अंत में लेखक ने इन शब्दों के साथ अपनी बात समाप्त की है कि हमें सब समय और सभी स्थानों पर यह याद रखना चाहिए कि हम कौन हैं और हम यहां क्यों हैं। (पृष्ठ 93)
🍃🍃
5) 🕉️ और इसका व्यावहारिक महत्व
🍃🍃
ओम के उच्चारण पर बहुत कुछ कहा गया है। लेखक ने थिओसोफी के मूल स्रोत मैडम ब्लेवेट्स्की द्वारा लिखित लेख को पाठकों तक पहुंचाया है। इससे विषय की प्रमाणिकता उपलब्ध हो पाई है। लेख में अनेक विचारों द्वारा ‘ओम’ की परिभाषा और महत्व पर प्रकाश डाला गया है। इसमें ओम को अत्यंत महत्वपूर्ण माना गया है तथा बताया गया है कि महाराज मनु ने भी वेद पाठ के प्रारंभ और अंत में ओम के उच्चारण की आवश्यकता पर बल दिया था।( पृष्ठ 96)
कठोपनिषद का भी उदाहरण है। जिसमें यह कहा गया है कि जो व्यक्ति ओम को जान लेता है वह जो भी इच्छा करता है, उसे प्राप्त कर लेता है। (पृष्ठ 96,97)
ओम के उच्चारण की प्रक्रिया बताते हुए लेखक ने एक स्थान पर लिखा है कि ओम शब्द नाक के नथुनों द्वारा सॉंस बाहर निकालते समय बोला जाता है। लेखक ने बताया है कि ओम शब्द मृत्यु तथा सांसारिक प्रलोभनों से मनुष्य की रक्षा करता है, पुनर्जन्म से बचाता है।
ओम के उच्चारण से सबसे बड़ा लाभ विद्वान लेखक ने सांस की लंबाई को छोटा करने का बताया है । इसका अभिप्राय यह है कि ओम के उच्चारण से व्यक्ति अद्भुत सफलता प्राप्त कर सकता है । लेखक के अनुसार ओम के उच्चारण से लाभ के लिए एक संयमित और सादा जीवन बहुत जरूरी है। जब व्यक्ति ओम के उच्चारण का अभ्यास करते हुए सफलता की दिशा में आगे बढ़ता है तब उसकी श्वास की लंबाई 9 इंच से घटते-घटते व्यक्ति को परमानंद की प्राप्ति की ओर अग्रसर कर सकती है। श्वास की लंबाई 6.5 इंच की करने से कविता लिखने की शक्ति प्राप्त होती है। छह इंच करने पर भविष्य की घटनाओं का वर्णन करने की शक्ति आ जाती है। 5.25 इंच करने से दिव्य दृष्टि प्राप्त होती है। जैसे-जैसे ओम के अश्राव्य अर्थात बिना शोर किए हुए उच्चारण से जब यह श्वास की लंबाई कम होती जाती है, तब व्यक्ति वायु क्षेत्र में विचरण करने की शक्ति तथा अष्ट सिद्धि और नव निधियां प्राप्त कर लेता है। वह देवलोक को देख पता है। देव-तुल्य हो जाता है (प्रष्ठ 108, 109)
ओम के उच्चारण का व्यवहारिक लाभ जो सिद्धांत रूप में लेखक ने बताया है, उससे आकर्षित होकर पाठक उनके उच्चारण की ओर यदि प्रवृत्त होते हैं तो वह समय आने पर इन सारी उपलब्धियां को अनुभव भी संभवतः कर सकेंगे।
🍃🍃
6) उपनिषद के प्रकाश में आत्मा की प्रकृति में अंतर्दृष्टि
🍃🍃
इस लेख में सर्वप्रथम लेखक ने उपनिषद का अर्थ बताया है। उप अर्थात पास में, नि अर्थात नीचे, षद् अर्थात बैठना। मतलब यह है कि गुरु के पास नीचे बैठकर उपनिषद का ज्ञान प्राप्त किया जाता है।
लेखक का कहना है कि सभी उपनिषदों का निहितार्थ यह है कि हमारे भीतर का आत्मा ठीक वैसा ही है जैसा बाहर का सर्वोच्च ब्रह्म है । सभी देवों को हम अपने अंदर खोज सकते हैं।( पृष्ठ 114, 115)
उपनिषदों के ज्ञान को समझने के लिए लेखक ने वृहदारण्यक उपनिषद की विस्तृत समीक्षा की। उसने अध्याय एक, खंड चार, मंत्र 10 के “अहम् ब्रह्मास्मि” का अर्थ बताया है कि
जो ‘स्व’ का बोध कर लेता है वह ब्रह्म हो जाता है। संपूर्ण अभिव्यक्ति को अपने साथ मानकर उसका विश्व के प्रति आचरण बदल जाता है। यह बात देवी-देवताओं की पूजा से नहीं आती क्योंकि उसमें द्वैत की धारणा बनी रहती है। (प्रष्ठ 118)
आत्मा की प्रकृति को जानने की अंतर्दृष्टि का बोध कराते हुए वृहदारण्यक उपनिषद के अध्याय 2 खंड 4 मंत्र 14 से लेखक ने बताया है कि जिसे जानने से द्वैत समाप्त हो जाता है,वह जानने के योग्य है। तुम भी ब्रह्म बन सकते हो अर्थात बोध कर सकते हो कि तुम ब्रह्म हो। (पृष्ठ 121)
🍃🍃
7) जीवन का अमृत
🍃🍃
‘जीवन का अमृत’ अद्भुत लेख है। संसार में कोई भी व्यक्ति मरना नहीं चाहता। सब अमर होना चाहते हैं। इसीलिए अमृत का विचार बार-बार हर सदी में दार्शनिक करते रहे। वैज्ञानिक मरने से बचने का उपाय खोजते हैं।
लेख में बताया गया है कि जीवन को सैकड़ों वर्ष लंबा किया जा सकता है। मैडम ब्लेवैट्स्की कहती हैं कि जब वह युवा थीं तब भी थियोस्फी के महात्मा युवा ही थे लेकिन अब जब वह वृद्ध हो गई हैं तब भी उन महात्माओं का शरीर पहले जैसा ही युवा है। इसका मतलब यह नहीं है कि उन महात्माओं की आयु एक हजार वर्ष है। लेकिन जीवन का अमृत नामक लेख विचार करता है।
उमाशंकर पांडेय की परिकल्पना यह है कि सिद्ध व्यक्ति अपने शरीर में कुछ ऐसा विकास कर सकते हैं कि जिसके द्वारा जहां एक ओर उन पर वातावरण की मृत्यु का प्रभाव न पड़े और इसके लिए वह सांसारिक परिदृश्य से दूर रहने तक की जीवन साधना को अपना लेते हैं; वहीं दूसरी ओर उनके भीतर अपने शरीर को नियंत्रित करके नया शरीर प्राप्त करने की क्षमता तक विकसित हो सकती है। यह नया शरीर गुप्त-विद्याविदों द्वारा स्वयं का निर्मित हुआ होता है। साधना के द्वारा वह अपने शरीर के सभी पुराने मोटे कणों से धीरे-धीरे छुटकारा पाते हैं और उसकी जगह अधिक महीन और अधिक एथेरियल कणों को रखते हुए आगे के कार्य के लिए उपयुक्त शरीर जो कि स्वयं उनके द्वारा निर्मित होता है बना लेते हैं।
लेख पाठकों को आश्चर्यचकित करने वाला है। विस्मय में डाल देता है। लेख हमारे ज्ञान-चक्षुओं को झकझोरने वाला है।
🍃🍃
8) ध्यान: वैज्ञानिक और व्यावहारिक समझ
🍃🍃
ध्यान पर लेखक ने अच्छा लेख लिखा है। उसने अंग्रेजी के ‘मेडिटेशन’ शब्द को लैटिन से आया हुआ बताया है, जिसका अर्थ है ‘बार-बार ठीक करना’। इसका अभिप्राय यह है कि मेडिटेशन केवल ठीक करना नहीं है बल्कि ‘बार-बार ठीक करना’ है।
ध्यान शब्द को लेखक ने संस्कृत का बताया है। जिसका अर्थ है गति का बंद होना और एकाग्रता।
ध्यान के बारे में लेखक का मत है कि इसमें व्यक्ति को ‘कुछ नहीं करना’ होता है। यह केवल ‘होना है’ जो हम हैं। (प्रष्ठ 169, 171)
ध्यान की प्रक्रिया को समझाने के लिए लेखक ने जे. कृष्णामूर्ति के विचारों को विस्तार से पाठकों के सामने रखा है। इसमें एक विचार यह है कि ध्यान वास्तव में बहुत सरल होता है, लेकिन हम उसे जटिल बना देते हैं।
ध्यान के पंद्रह प्रकार लेखक ने बताए हैं।
ध्यान के वैज्ञानिक अनुसंधान के परिणामों को भी लेखक ने अपने लेख में शामिल किया है। उसका कहना है कि ‘टेलोमेरस’ प्रक्रिया को बढ़ाकर ध्यान बुढ़ापे की प्रक्रिया को धीमा करता है। इसका संबंध क्रोमोसोम और डी.एन.ए.की अवधारणा से है ।
अंत में लेखक का कहना है कि ध्यान व्यक्ति में तांत्रिक-जैविक (न्यूरोबायोलॉजिकल) परिवर्तन लाता है। व्यक्ति को स्वस्थ जीवन जीने में सहायता करता है।
🍃🍃
9) त्याग का नियम
🍃🍃
‘त्याग’ शब्द का अंग्रेजी पर्याय ‘सैक्रिफाइस’ को लेखक ने लेटिन से आया हुआ बताया है। इसका अर्थ है -‘मैं पवित्र बनाता हूं’।
लेखक का कहना है कि जब हम किसी चीज का त्याग करके उसे भगवान को अर्पित करते हैं, तब वह वस्तु पवित्र हो जाती है। हालांकि इसमें कुछ भी त्यागने का विचार त्यागी व्यक्ति के भीतर नहीं होना चाहिए।
थिओसफी में त्याग का विचार एक थियोसॉफिस्ट द्वारा किस प्रकार अमल में लाया जा सकता है, इसके बारे में लेखक का कहना है कि शुद्ध और नि:स्वार्थ जीवन जीते हुए अपने पड़ोसी की सहायता करने में अगर हमें अधिक आनंद मिलता है और हम अपने सुखों का त्याग करने के लिए प्रस्तुत रहते हैं, तो हम सच्चे थियोसॉफिस्ट है। हम सत्य, अच्छाई और प्रज्ञा को उनके गुणों के लिए प्यार करें, न कि उस लाभ के लिए जो इन गुणों को जीवन में धारण करके हमें प्राप्त हो सकते हैं। यही त्याग का असली नियम है।
🍃🍃
10) स्व-निषेध से सुख, शांति और परिपूर्णता
🍃🍃
जीवन में सुख, शांति और परिपूर्णता तभी आ सकती है; जब हम स्व-निषेध को अपनाऍं। लेखक ने स्वनिषेध को सरल और सादगी पूर्ण जीवन जीने से जोड़ते हुए अपरिग्रह के सिद्धांत का उल्लेख किया है। वस्तुओं के संचय को अनुचित बताया है। गीता में वर्णित महाराज जनक के अनासक्त उदाहरण को सामने रखा है। महात्मा गांधी के ट्रस्टीशिप के सिद्धांत का भी उल्लेख किया है, जिसमें व्यक्ति को यह मानकर चलना होता है कि जो धन-संपत्ति उसके पास है; वह उसकी नहीं है अपितु समाज की है।
लेखक ने थियोस्फी के अंतर्गत त्याग को आवश्यक बताया है लेकिन अविवेकपूर्ण त्याग को सही नहीं ठहराया है। लेख इस दृष्टि से अच्छा है कि उपभोग पर नियंत्रण लगाने की अति आवश्यकता है; ताकि व्यक्ति और समाज की आवश्यकताओं के बीच में संतुलन बना रह सके।
🍃🍃
11) गंध और जीव
🍃🍃
‘गंध और जीव’ लेख को प्रोफेसर येगर की खोज के आधार पर तैयार किया गया है। प्रोफेसर येगर ने खोज यह की थी कि पौधों और जानवरों की हर प्रजाति में एक निराला गंध रहता है। यह जानवर के आंतरिक गुण होते हैं। यह संबंधित जानवर के विशिष्ट प्रोटोप्लाज्म से संबंधित होते हैं।
हर प्राणी के शरीर में एक विशिष्ट गंध होती है। इसी के आधार पर दो व्यक्तियों के बीच गंभीर समरसता उत्पन्न होती है, जिसे हम प्रेम कह सकते हैं।
यह गंध क्या है ? लेख के अंत में निष्कर्ष यह है कि डॉक्टर येगर में जिस गंध का उल्लेख किया है, वह स्वयं में जीव नहीं है लेकिन स्थूल शरीर और जीव को जोड़ने वाला कोई पदार्थ प्रतीत होता है।
यह लेख प्रकृति के अनसुलझे रहस्यों को सुलझाने की कोशिशें में से एक है।
🍃🍃
12) चक्रों का सिद्धांत
🍃🍃
चक्रों का सिद्धांत लेख इस बात पर आधारित है कि इतिहास में एक जैसी घटनाएं एक निश्चित समयावधि के बाद बार-बार होती हुई देखी गई हैं ।घटनाओं की बराबर पुनरावृत्ति होती है। एक निश्चित काल-क्रम है। संसार में हर जगह इस कालचक्र की निरंतरता को विद्वानों ने गहन अध्ययन के द्वारा महसूस किया है।
एक विद्वान डॉक्टर जस्से हैं। जर्मनी के हैं। इन्होंने खोज की थी कि कुछ घटनाएं दस वर्षीय चक्र में और कुछ ढाई सौ, पॉंच सौ आदि वर्षों में पुनरावृति करती हैं। खोज चौंका देने वाली है।
जहां तक चक्र का संबंध है, लेख में इस तथ्य को इंगित किया गया है कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर एक वर्ष में चक्कर लगाती है । चौबीस घंटे में पृथ्वी अपनी धुरी पर एक चक्कर लगाती है। इसी तरह बड़े चक्र और बड़े चक्र के भीतर छोटे-छोटे चक्र निरंतर चलते रहते हैं। यह ब्रह्मा के रात और दिन की निरंतरता को दर्शा रहे हैं। लेख दिलचस्प है।
🍃🍃
13) धर्मों का चरित्र, उनका बंधुत्व तथा तुलनात्मक धर्मों का अध्ययन
🍃🍃
यह लेख आज के समय में ही नहीं बल्कि शताब्दियों से एक ज्वलंत विषय रहा है। लेखक ने धर्म के मूलभूत तत्वों को उसके वाह्य आवरण से अलग करके देखा है। उसका कहना है कि विभिन्न धर्मों में जो अनुष्ठान, समारोह, लालच, स्वार्थपरता आदि प्रवेश कर जाते हैं; सारे झगड़े इसी को लेकर होते हैं। जबकि अपने आप में धर्म की आंतरिकता में एकरूपता होती है।
लेखक के अनुसार थियोस्फी का मानना है कि सब धर्मों का दिव्य स्रोत होता है। लेकिन सभी धर्मों में कुछ न कुछ बुराइयां अवश्य हो जाती हैं ।
धर्मों के तुलनात्मक अध्ययन की दृष्टि से एनी बेसेंट ने एक पुस्तक लिखी थी, जिसका नाम सेवेन ग्रेट रिलिजंस (सात महान धर्म) था।
लेखक का कहना है कि तुलनात्मक धर्मों के अध्ययन से विभिन्न धर्मों में जो एकता निहित है, वह समझ में आती है। लेकिन साथ ही साथ उसका यह भी कहना है कि हमें स्वयं ही सत्य का अन्वेषक बनना होगा। किसी अधिकारी के कुछ कह देने को ज्यों का त्यों नहीं मानना है।
🍃🍃
14) सामाजिक सेवा: इसका आध्यात्मिक आयाम
🍃🍃
इस लेख में मैडम ब्लेवैट्सिकी के विचारों को मुख्य रूप से आधार बनाकर थियोस्फी के परिप्रेक्ष्य में सामाजिक सेवा का दर्शन कराया गया है।
एक थियोसॉफिस्ट को परोपकार का अभ्यास होना चाहिए। हर भोजन उसे गरीब के साथ साझा करना चाहिए। साझेदारी में जाति, राष्ट्र और पथ देखना गलत है। हर दुखी की कराह उसके कानों को सुनाई देनी चाहिए। उसे निर्दोष की निंदा नहीं सुनाई चाहिए। यही असली थियोसोफी है।
🍃🍃
15) हम कैसे सोऍं
🍃🍃
इस लेख ने मैडम ब्लेवेट्स्की का यह तथ्य रेखांकित किया है कि पृथ्वी में एक चुंबकीय धारा प्रवाहित होती है। इसी तरह हर व्यक्ति के शरीर में भी एक चुंबकीय धारा प्रवाहित हो रही है। जिस दिशा में पृथ्वी की चुंबकीय धारा प्रवाहित हो रही हो, उस दिशा में पैर करके व्यक्ति को सोना चाहिए ताकि पृथ्वी की चुंबकीय धारा और व्यक्ति के शरीर की चुंबकीय धारा में सामंजस्य स्थापित हो सके।
यह भी बताया है कि आध्यात्मिक साधना से भावना और मन को साम्य में स्थापित करके व्यक्ति उसके बाद किसी भी दिशा में सिर करके सोए, कोई विपरीत प्रभाव नहीं पड़ेगा।
सोने के संबंध में सलाह यह भी दी गई है कि सोते समय व्यक्ति शुरू की सोलह सांसों तक दाहिनी करवट लेटे और फिर बत्तीस सांसों तक बॉंई करवट लेटे, तब उसके बाद वह किसी भी अवस्था में सो सकता है।
🍃🍃
16) प्रेम: अस्तित्व का आधार, सार, स्वभाव और लक्ष्य
🍃🍃
इस लेख में प्रेम को एक दिव्य शक्ति के रूप में व्यापकता के साथ प्रयोग में लाने पर बल दिया गया है। प्रेम से ही सब प्राणियों में देवत्व जगता है। उदाहरण के तौर पर लेखक ने बताया है कि हमें केवल अपनी मॉं से ही प्रेम नहीं करना चाहिए बल्कि संसार की सभी माताओं के प्रति हमारे भीतर प्रेम का भाव उत्पन्न होना चाहिए। तभी यह प्रेम दिव्य प्रेम के रूप में व्यक्त होगा।
वृहदारण्य उपनिषद को उद्धृत करते हुए लेखक ने बताया है कि एक सच्चा व्यक्ति अपने घर, परिवार, पत्नी आदि सभी से प्रेम करता है लेकिन वह यह प्रेम अपनी स्वयं की आत्मा के लिए करता है। खेद का विषय है कि जैसे-जैसे व्यक्ति बड़ा होता जाता है, वह बाहरी दुनिया में अपनी इंद्रियों के साथ आकर्षित होता है और दिव्यता को खो देता है। मनुष्य जीवन का सार नि: स्वार्थ प्रेम में ही निहित है- लेखक का कहना है।
🍃🍃
17) भगवद्गीता की शिक्षाओं में एक अंतर्दृष्टि
🍃🍃
भगवद् गीता की शिक्षाओं पर विचार करने के साथ-साथ इस लेख की विशेषता यह है कि यह थियोसोफिकल दृष्टिकोण से गीता का पक्ष प्रस्तुत कर रहा है। पश्चिम के देशों में गीता किस प्रकार प्रचलित और प्रसारित हुई, इसका भी उल्लेख है।
लेखक ने बताया है कि अंग्रेजी में भगवद् गीता का सर्वप्रथम 1775 ईस्वी में लंदन में अनुवाद किया गया जो चार्ल्स विलकिंस द्वारा प्रकाशित किया गया था। इस अंग्रेजी अनुवाद के परिचय खंड में लिखा गया था कि “मानव समाज के सभी जाने-माने धर्मो में से यही केवल एक अपवाद है जो ईसाई मत के सिद्धांतों से ठीक-ठीक तालमेल रखते हुए मूल सिद्धांत की बड़े शक्तिशाली ढंग से व्याख्या करती है।” (प्रष्ठ 323)
लेख में बताया गया है कि थियोसोफिकल साहित्य में गीता को महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है। मैडम ब्लेवेट्स्की की पुस्तकें आइसिस अनवेल्ड, द सीक्रेट डॉक्ट्रिन, द वॉयस ऑफ़ द साइलेंस तथा थियोसोफिकल ग्लॉसरी में गीता की शिक्षाओं को इंगित किया गया है। (पृष्ठ 321)
थियोस्फी की प्रमुख स्तंभ एनी बेसेंट ने ‘हिंट्स ऑन द स्टडी ऑफ द भगवद् गीता’ पुस्तक लिखी है।
थियोसोफिकल ग्लॉसरी में मैडम ब्लेवेट्स्की का कथन है कि “गीता प्रधानतया उच्चतम आध्यात्मिकता की गुह्य शिक्षा है।” (पृष्ठ 322)
लेखक का मत है कि थियोस्फी के सिद्धांत के अनुसार कौरव भौतिक धारा का तथा पांडव आध्यात्मिक धारा का प्रतिनिधित्व करते हैं ।(प्रष्ठ 336)
लेखक ने गीता का गहरा अध्ययन किया है। जिसके फलस्वरुप उसने बताया है कि कृष्ण ने अर्जुन को स्थान-स्थान पर अलग-अलग नामों से संबोधित किया है और हर नाम का एक अलग वैशिष्ट्य है। लेखक ने उन सब नामों के समुचित अर्थ की व्याख्या भी की है। (पृष्ठ 340, 341, 342)
🍃🍃
18) सात की संख्या
🍃🍃
इसमें सामाजिक, राजनीतिक और धार्मिक दृष्टि से दुनिया भर में सात के अंक को महत्व देते हुए तमाम क्रियाकलापों में जो आदर प्रदान किया गया है, उसका उल्लेख है। स्वयं थियोसोफिकल सोसायटी के प्रतीक चिन्ह में दो त्रिभुजों को एक के ऊपर एक रखकर सात की संख्या को महत्व दिया गया है। लेख अच्छा है। सात के महत्व के पीछे कारण कोई भी हो, लेकिन जानकारी दिलचस्प है।
🍃🍃
19) थिऑसोफी और विज्ञान
🍃🍃
थियोसोफी का ध्येय वाक्य है कि सत्य से बढ़कर कोई धर्म नहीं है। लेखक ने इस कथन को विज्ञान-सम्मत बताते हुए थिओसोफी को सत्य के पथ का अनुयायी बताया है। उसने विभिन्न वैज्ञानिक अवधारणाओं की थियोस्फी के विश्वासों के साथ तुलना की है। अंत में लेखक का यही कहना है कि निरंतर अनुसंधान होते रहने चाहिए तथा वैज्ञानिक और थिओसोफिस्ट दोनों ही इस विचार को साझा कर सकते हैं कि सत्य से बढ़कर कोई धर्म नहीं है।
🍃🍃
20) प्रार्थना
🍃🍃
लेखक ने थियोस्फी की सार्वभौमिक प्रार्थना जिसमें गुप्त जीवन और गुप्त ज्योति से संसार के एकत्व के अनुभव की प्रार्थना की जाती है, सर्वश्रेष्ठ प्रार्थना बताया है। उसका कहना है कि अच्छी प्रार्थना वही है,, जो हमें अपने भीतर के उच्च ईश्वर के साथ एकाकार करती है। ध्यान को भी लेखक ने मौन प्रार्थना बताया है। सांसारिक वस्तुओं के लिए देवी-देवताओं अथवा ईश्वर से की गई किसी भी प्रार्थना को लेखक ने अनुचित माना है। प्रार्थना के संबंध में थियोस्फी के प्रमाणिक कथन लेख में उद्धृत किए गए हैं।
🍃🍃
21) चंद्रमा
🍃🍃
लेख में चंद्रमा की उत्पत्ति पर वैज्ञानिक और आध्यात्मिक दृष्टिकोण प्रस्तुत किए गए हैं। यह तथ्य बताया गया है कि चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता है हमारे सबसे निकट है। चंद्रमा की किरणों से सृष्टि जीवन-शक्ति प्राप्त करती है। यह भी बताया है कि चंद्रमा की किरणें अमावस्या और पूर्णिमा पर कुछ व्यक्तियों को मानसिक विकार उत्पन्न करती हुई देखी गई हैं। अमावस्या पर काला जादू किए जाने का उल्लेख भी है। नीलम पत्थर के प्रभाव को लेखक ने निराधार अंधविश्वास न बता कर कुछ वैज्ञानिक तत्वों पर आधारित भी बताया है।
🍂🍂
निष्कर्ष
🍂🍂
थियोस्फी के साधकों को लेखक उमाशंकर पांडेय ने यह पुस्तक समर्पित की है। विषय जटिल हैं ,लेकिन जैसे-जैसे हमारी साधना और पात्रता बढ़ती जाएगी; यह विषय सरल होते चले जाएंगे। दुर्लभ ज्ञान को अनुवाद के रूप में बहुतायत से प्रस्तुत करने से पुस्तक की उपयोगिता बढ़ गई है। इसके लिए भी लेखक धन्यवाद का विशेष पात्र है।
प्रत्येक जागरुक व्यक्ति के लिए पुस्तक उपयोगी है। लेखक अथवा प्रकाशक के मोबाइल नंबर पुस्तक में उपलब्ध नहीं कराए गए हैं, यह एक भारी चूक है।