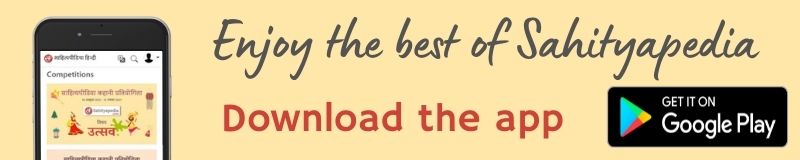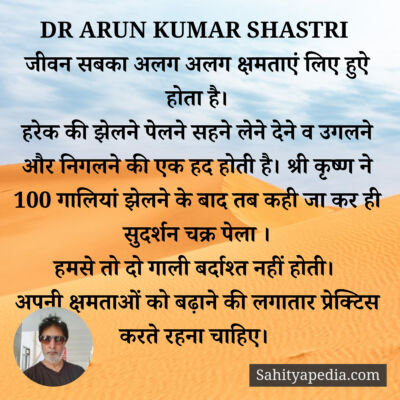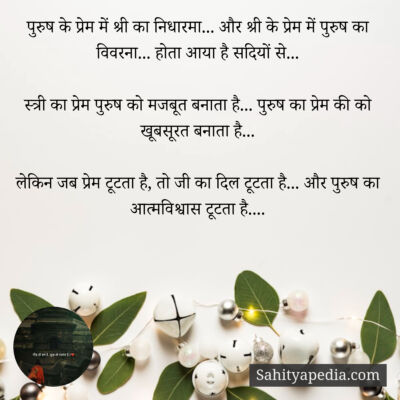“भारतीय संस्कृति और पारंपरिक होली”
मनुष्य समय के सहारे ही जीता चला जाता है, और यही हमारी ताकत है। जब देवी देवताओं ने अपने धर्म को, संस्कृति को संरक्षित रखने को परम हितकारी माना है, तो हम क्यों नहीं! तात्पर्य साफ है कि,उनके द्वारा बताए गए पद चिन्हों का अनुसरण करना, हमारी नैतिक ज़िम्मेदारी है। वसंत ऋतु धरती का सबसे सुंदर चित्रण है, जिसके आने से धरती प्रकृति रंगों से रंग जाती है। अतः वसंत ऋतु प्रकृति का सबसे अनुपम उपहार है। जिसके आगे कामदेव की सुंदरता भी फीकी पड़ जाती है। यह ऐसा दृश्य होता है, जब हमारा मन प्रकृति के छवि को निहार कर संमोहित होने लगता है। इस तरह ऋतुराज के आगमन से लोगों में एक नई उर्जा का संचार होता है। तब हमारे मन की उड़ान बहुत दूर तक विचरण करती हुई देश-प्रदेश रह रहे लोगों के मन की चंचलता को बढ़ा देती है। अर्थात इन नेत्रों को उनके घर आने का बेसब्री से इंतजार रहता है। क्योंकि होली भी वसंत ऋतु में ही आती है।
इस संदर्भ में लेख लिखना मेरे इसलिए जरूरी हो जाता है कि होली हमारे संस्कृत और परांपरा के सुविचारों से जुड़ा हुआ विषय है। होली जैसे जैसे नजदीक आती है मन को ऐसे आनंदित करती है मानों सावन भादो के मंडराते काले बादल लालायित हैं धरती को चूम लेने के लिए। गम्भीरवन की ऐतिहासिक होली यदि कोई एक बार देख लिया तो यह दृश्य उसके मस्तिष्क से विस्मृति नहीं होती। यह सत्य है कि इसे देखकर मानो ऐसा प्रतीत होता है कि दैव लोक की होली आज इस गांव में खेली जा रही है। बचपन से आजतक जो भी मैंने देखा है वास्तव में ये अद्भुत,अलौकिक है। फागुन आते ही हमारे दिलो-दिमाग में होली का प्रतिबिंब ध्रुव तारा की भांति प्रतिबिंबित होने लगता है। यहां की धूम-धाम से मनाएं जाने वाली ऐतिहासिक होली अपनी पारंपरिक पराकाष्ठा के लिए जानी जाती हैं। अपने आदिम काल से लेकर अबतक होली स्वयं संस्कृत व परांपराओ का जीवंत प्रमाण है। यह भी सत्य है कि इस गांव की होली पूरे भारतवर्ष के विरासत के प्रतीक की भांति प्रतित होती है। यह परंपरागत होली का त्योहार हमें प्रेमानंद की अनुभूति कराती है। जहां हर जगह पारंपरिक होली अपने मूल स्वरूप से पथ भ्रमित हो रही है, तो वहीं यहां की सांस्कृतिक और पारंपरिक होली अपने पूरे रंगों (जोश) में फल फुल रही है, तथा लोगों को अपने रंगों में आत्ममुग्ध (सराबोर) कर रही है। आज धीरे-धीरे बहुत कुछ बदल चुका है। यहां तक कि तर-त्योहार मनाने के तौर-तरीके एवं मायने भी बदल चुके हैं। आज के युवा पीढ़ियों को अपना कर्तव्य बोध होना जरूरी है, कि वे अपने इतिहास और संस्कृति को बिसराये बिना पूर्वजों द्वारा चली आ रही परिपाटी को माने तथा उसे संरक्षित करने का भरपूर प्रयास करें। क्योंकि युवा पीढ़ियों के कंधे पर राष्ट्र निर्माण का प्रबल जिम्मेदारी होती हैं, जिसके दशा, दिशा पर देश की दशा और दिशा निर्भर करती है। आज होली मनाते के परंपरा को भूल कर लोग वैकल्पिक तरीके अपना रहे हैं, तो वहीं पर यहां के लोग अपनी परांपरिक होली के त्योहार को धरोहर की भांति संजोकर रखने में कामयाब रहे है। यही हमारी सबसे बड़ी पहचान है, और यही हमारे लिए हर्ष व गर्व का विषय भी है। जिसके लिए हमेशा गम्भीरवन आकषर्ण का केंद्र बना रहता है, वो यहां की होली ही तो है! आज भी यहां चौताल लगते है। ढोल मजीरा के साथ पारंपरिक फगुआ गीत गाए जाते हैं एवं रंग, गुलाल के साथ आपस में प्रेम की होली खेली जाती हैं। जहां हर जगह मैं नागिन तू सपेरा का धुन बजता है, तो वहीं हमारे यहां पारंपरिक फगुआ गीत— पनघट पर, पनघट पर मोहन मोर गागर फोर गयौ,सुनो सुनो जनक की बतिया सखियां सुनो जनक की बतिया, अड़भंगी तुम्हारी कलियां शिव अड़भंगी तुम्हारी कलियां, चुड़िया लेई अईहा छोटी छोट हे सईया नरमी कलईया, गढ़ छोड़ दें लंका रावणा तोर लंका लगे भयावना,और सुमेरहु आज भवानी हे माया सुमरेहू आज भवानी इत्यादि गाए जाते हैं। रात को होलिका दहन के साथ होली की शुरुवात होती है। सुबह सैंकड़ों के संख्या में लोग धुलहड्डी के लिए जाते हैं फिर दोपहर बाद फगुआ गाते बजाते गांव भर घूमते हैं और जगह जगह चौपाल लगाते हैं शाम को देवालयों में अबीर चढ़ाने के उपरांत एक दूसरे को अबीर लगाकर गले लगते हैं और बच्चे आशिर्वाद लेते हैं। फिर तीनों मंडलियां एक साथ दयालापुर तक गाती बजाती हुई जाती है। अनवरत चौबीस घंटे चलने वाली होली मनहर लगती है और उन भूली बिसरी यादों की भी स्मरण कराती है, जो कभी इन त्योहारों में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते थे। वे आज हमारे बीच नहीं हैं फिर भी होली आते ही उनकी यादें हमारे हृदय को स्पर्श करती है कचोटती है। क्योंकि अपने समय में समर्पित भाव से सिद्ध गायक के रूप में इस मंडली का हिस्सा हुआ करते थे। चाहे बाबू संबिहारी सिंह हो, चाहे बाबू अवध बिहारी सिंह हो या अन्य कोई। चैता के साथ होली का समापन तो हो जाता है। लेकिन फिर अगले साल होली आने का इंतजार सुरु हो जाता। यह हमारे पूर्वजों द्वारा विरासत के रूप में हस्तांतरित होती हुई सुव्यवस्था है जो पीढ़ी दर पीढ़ी स्वत: हस्तांतरित होती रही है।
मेरे उत्सुकता को देखते हुए बाबा ने एक बार कहा कि—– हमने आजादी से पहले और बाद की भी होली देखी है और अंग्रेजों का शासत भी। उस समय फागुन लगते ही जगह-जगह चौताल लगने लगते थे और फगुआ के रसिक गीत गाए जाते थे। लोग बहुत प्रेम से फगुआ गीत सुनते थे और त्योंहार मनाते थें। कभी त्यौहारों पर अंग्रेजों का कोई अनुचित प्रभाव नहीं था। तब भारत! भारत था। सब लूटकर ले गए लूटेरे। छोटी सी छोटी गलती के लिए हमें कठोर से कठोर सजा मिलती थी, मुर्गा बनाकर पीठ पर चाकी, पत्थर रख दिये जाते थे। कुछ अपराधों में कोड़ों की भी सज़ा दी जाती थी। जिसे मृत्यु दण्ड की सजा दी जाती थी, उसे गाजीपुर गंगा किनारे श्मशान घाट पर स्थित फांसी घर में फांसी दे दी जाती थी।
जब अंग्रेजों की बात कर ही दी तो एक वाकिया और बताते है, बाबा ने लड़खड़ाते हुए स्वर में बोला- जब यहां से अंग्रेज भगाए जा रहे थे, उसी समय हम लोग बंगाल से होकर समुद्र के रास्ते पाकिस्तान चले गये थे। ठीक उसी समय हिन्दुस्तान-पाकिस्तान बंटवारा का बिगुल बज चुका था। पाकिस्तानी मुसलमान हिंदुओं पर अत्याचार करने लगे। उन्हें मारने पिटने लगे। हम लोग बहुत दहशत में थे। किसी तरह वहां से वापस आ आना चाहते थे, इसलिए वहां काम करने से मना कर दिये। कुछ दिन भय से रात में ड्यूटी करते रहे। लेकिन दिन प्रति दिन विद्रोह बढ़ता देख, हम लोग काम करने से मना दिये और हिंदुस्तान वापस आने का निश्चय कर लिए। तब अंग्रेज सिपाहीयों ने मजबूर होकर हम लोगों को वापस हिन्दुस्तान भेज दिया, उस समय हमारी उम्र तकरीबन 18-29 वर्ष रही होगे गुलाम भारत की तस्वीर उनके आंखों में आज भी दिख रहा था। गांधी जी के लम्बे लम्बे हाथों ने भी हिंदुस्तान-पाकिस्तान बंटवारे को रोकने में असमर्थ रहे। यह बताते हुए उनकी आंखें अर्ध नम हो गई।
लेखक – राकेश चौरसिया