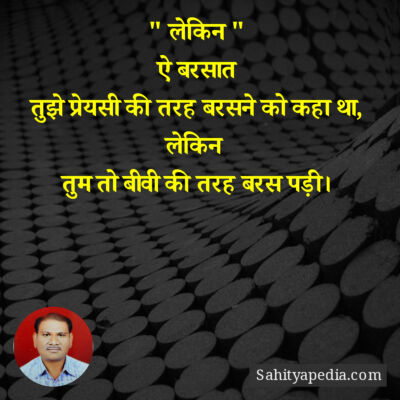देहरीहीन दौर

देहरीहीन दौर
अजीब दौर है, बदलती रीत है,जहाँ पुरानी धरोहरें अब सस्ती पड़ी हैं।
पुश्तैनी देहरियाँ, जो कभी सजीव थीं,अब बिक रही हैं, जैसे कोई यादें अधूरी सी।
वो देहरियाँ, जो सजती थीं संस्कारों से,जहाँ हर कदम पे होता था सम्मान का इज़हार।
झुककर, सिर झुका के, घर में प्रवेश करते थे,पैर धोकर, मानो पवित्रता के संग बंधते थे।
आज के दरवाजों में देहरी का वो भाव नहीं,बस इमारतें खड़ी हैं, पर उनमें कोई चाव नहीं।
दरवाजे तो हैं, पर उनमें अब वो आदर कहाँ,बिना झुके, बेपरवाह, घर में आना, ये कैसा जहाँ।
देहरियाँ तोड़कर, हम क्या पा रहे हैं,संस्कारों की जड़ें उखाड़कर क्या बसा रहे हैं।
जिस मिट्टी में हमारी जड़ें गहराई थीं,उसे छोड़कर, हम किस दिशा में जा रहे हैं।
सिर्फ ईंट-पत्थर का घर अब रह गया है,संस्कारों का आँगन कहीं खो गया है।
जिस देहरी से खुशियाँ बँधा करती थीं,आज वही देहरीहीन दरवाजे हमें बांध रही हैं।
अजीब दौर है, जहां मूल्य बदल गए हैं,पुरखों की धरोहरें अब महज स्मृतियों में बस गए हैं।
देहरीहीन इस दौर में, हम सब बस दौड़ रहे हैं,पर इस दौड़ में हम अपने ही घर की देहरी खो रहे हैं।
यह कविता उस अजीब दौर की बयानी है, जहाँ पुश्तैनी देहरियाँ बेचकर, लोग नए दरवाजे बना रहे हैं, पर वो संस्कारों की खुशबू खोते जा रहे हैं। उम्मीद है कि यह आपके मन के भावों को अभिव्यक्त कर पाई होगी।