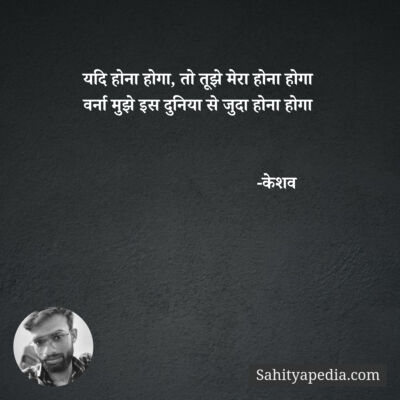कीचड़ से कंचन
फैला कीचड़ सब तरफ
एक-दूसरे पर ही उछालते रहे।
जब सोच बन गई हो कीचड़
तब कौन किसको क्या कहे।।
ये कीचड़ से भरे रास्ते
पार तो करने ही थें जरुर।
कुछ तो मजबूरी थी हमारी
कुछ उजले कपड़ों का था गुरुर।।
लगे हटाने कीचड़ों की कीचड़
कुछ नीलकंठ जैसा काम करने।
खपने लगे अपने रात-दिन
कीचड़ की ही रोकथाम करने।।
खिलाने कमल खुद खाने गरल
बांध पट्टी-कपड़ा आंख-नाक में।
उतर पड़े हम नंगे ही पांव
आज के इस कुंभी पाक में।।
हमको लगा पांव ही फिसले है
पर पूरी जिंदगी ही फिसल गई।
कीचड़ पांवों में खुद पुती थी
पर ये दुनिया चेहरे पे मसल गई।।
एक बार तो लगा हमें
कीचड़ से बचके ही चलना चाहिए।
बस अपना दामन बचा रहे
दुनिया कीचड़ में ही छोड़ना चाहिए।।
सोचा कहां है कीचड़ की जड़
कुछ क्षण तो रह गया मौन।
फिर सोचा दिलों-दुनिया का
कीचड़ साफ फिर करेगा कौन?
किसी को तो जहर पीना होगा
नीलकंठ तो बनना ही होगा।
पंक में पंकज पल्लवित कर
कीचड़ को कंचन करना ही होगा।।
~०~
मौलिक एंव स्वरचित : कविता प्रतियोगिता
रचना संख्या -१२: मई २०२४.©जीवनसवारो