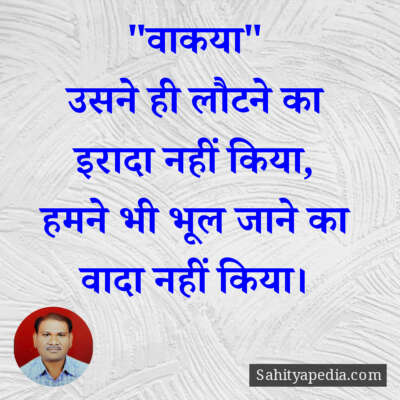काव्य की आत्मा और सात्विक बुद्धि +रमेशराज

आचार्य भोज काव्य के क्षेत्र में आत्मा को अनावश्यक मानते हुए ‘सात्विक बुद्धि की स्थापना करते हैं। सात्विक अर्थात् दूसरों के सुखदुख में प्रविष्ट हो सकने की सामर्थ्य वाली मानव चेतना |’’ [1]
इस प्रकार देखें तो आचार्य भोज काव्य की आत्मा के रूप में ‘सात्विक बुद्धि’ की स्थापना कर एक तरफ जहां रस को ‘गूंगे के गुड़ का स्वाद’ होने से बचाया, वहीं अलंकार ध्वनि, वक्रोक्ति आदि की काव्य में आत्मरूप से प्रतिष्ठित कराये जाने वाली अतिशयता का खुलकर विरोध किया। आचार्य क्षेमेन्द्र के ‘औचित्य सिद्धान्त’ को संशोधित कर आचार्य भोज ‘सात्विक बुद्धि’ को काव्य में जो आत्म प्रतिष्ठा दी, वह हर प्रकार प्रंशसनीय इसलिये है क्योंकि ‘सात्विक बुद्धि’ में ही वह सामर्थ्य होती है, जो सत्-असत्, अंधेरे -उजाले, शोषक-शोषित, अत्याचारी-पीडि़त में मात्र अन्तर ही नहीं करती, वह असत् से सत् की, अंधेरे से उजाले की, शोषक से शोषित और अत्याचारी से पीडि़त की रक्षा करने में हर प्रकार सहायक होती है। लेकिन इसका अर्थ यह भी नहीं है कि ‘काव्य की आत्मा ‘सात्विक बुद्धि’ को ही मान लिया जाये। आचार्य भोज इस बात पर कोई बल भी नहीं देते। दरअसल ‘सात्विक बुद्धि’ को प्राणवत्ता तो सत्योन्मुखी रागात्मक चेतना ही प्रदान करती है। सत्, शोषित, पीडि़त से जब तक हमारे सम्बन्ध रागात्मक नहीं होंगे, तब तक इनके प्रति न तो किसी प्रकार की रमणीयता का उदय होना सम्भव है और न मन के भीतर प्रेम का संचार हो सकता है। अतः यह कहना असंगत न होगा कि दूसरों के सुख-दुःख में प्रविष्ट कराने की सामर्थ्य वाली मानवचेतना, बिना रागात्मक के या तो तटस्थ हो जायेगी या अपनी मूल सामर्थ्य को ही खो बैठेगी।
जिस प्रकार रस का निर्णय अन्ततः अर्थनिर्णय पर निर्भर है,[2] उसी प्रकार रागात्मकता भी हमारे वैचारिक निर्णयों की देन होती है। हम यकायक ही किसी से प्रेम नहीं कर बैठते और न किसी के प्रति विद्रोह। जो वस्तु हमारे आत्म अर्थात् रागात्मक चेतना को तोष प्रदान करती हैं उनके प्रति हम में रमणीयता बढ़ जाती है। जो वस्तुएं हमारे आत्म को असंतोष या असुरक्षा से अनुभूत करती हैं, उनके प्रति हम स्वभाव से विद्रोही हो जाते हैं। इस प्रकार हमारी रागात्मकता का चक्र बुद्धि या चेतना के सहारे आत्मसुरक्षा या आत्मतोष के इर्दगिर्द घूमता हुआ आगे बढ़ता है।
आचार्य भोज रस को अपने तात्विक रूप में अहंकार मानते हैं। और अहंकार के व्यक्त रूप को अभिमान।’’[3] अहंकार अर्थात स्वगत रागात्मक चेतना। स्वगत रागात्मक चेतना जब शेष सृष्टि के साथ रागात्मक सम्बन्ध स्थापित करती है तो उसकी रसात्मकता मात्र रत्यात्मक ही नहीं होती, वह कभी वात्सत्यात्मक बनती है तो कभी ममत्व भरी होती है तो कभी उसका रूप श्रद्धात्मक हो जाता है। इस प्रकार स्व से घनीभूत रागात्मकता ‘पर’ की समाविष्टि बन जाती है। स्व से ‘पर’ की ओर जाने की रागात्मक क्रिया जब अधोमुखी होती है तो मोह, लालासा, लिप्सा, कुंठा, व्यक्तिवाद, दुराचार, व्यभिचार और स्वार्थ को जन्म देती है। स्व से पर की ओर जाने की रागात्मक क्रिया जब सात्विक होती है तो समस्त जगत् से प्रेमपरक सम्बन्ध स्थापित ही नहीं करती, जगत् के प्राणियों पर आये संकट, दुखादि के प्रति करुणाद्र भी होती है। लोक को संकट में डालने वाले कारकों के प्रति विरोध और विद्रोह की रसात्मकता में सघन होती है।
आचार्य भोज कहते हैं कि ‘‘अहंकार या अभिमान को ‘ शृंगार’ भी कहते हैं क्योंकि इसमें मनुष्य को परिष्कृति के उच्चतम शृंग़ पर ले जाने की क्षमता होती है।[4]
इस प्रकार हम देखते हैं कि भोज ने शृंगार को नयी व्यापकता, सार्वभौमिकता ही प्रदान नहीं की, उन्होंने अहंकार को एक नूतन ऊर्जा भी दी, जिसमें दूसरों की रागात्मकता को परिष्कृत रूप में द्रवित कर अपने में समाहित कर लेने की अपार क्षमता अन्तर्निहित रहती है।
अहंकार अर्थात् स्वगत् रागात्मक चेतना, परगत रागात्मक चेतना को किस प्रकार परिष्कृत द्रवित करती है और अन्त में अपने में समाहित कर लेती है, इसको समझाने के लिये यहां एक उदाहरण देना आवश्यक है।
‘‘वह मरा कश्मीर के
हिमशिखर पर जाकर सिपाही
बिस्तरे की लाश तेरा
और उसका साम्य क्या है
पीढि़यों पर पीढि़यां उठ
आज उसका गान करतीं’’
+माखनलाल चतुर्वेदी
कवि ने इस कविता में एक ऐसे सिपाही का वर्णन किया है जिसकी रागात्मकता में समूचे राष्ट्र की रक्षा की कामना रची-बसी है। राष्ट्र की रक्षा करते हुए वह कश्मीर के हिमशिखर पर अपने प्राणों की आहुति दे देता है। सिपाही के इस वीरकर्म को पढ़-सुन या देखकर समूचा राष्ट्र उस पर गौरव अनुभव करता है और उसके प्रति श्रृद्धानत् हो उठता है। कवि ऐसे में बिस्तर पर पड़ी उस लाश को धिक्कारता है, जिसका राष्ट्ररक्षा से कोई वास्ता नहीं रहा है अर्थात् जिसकी रागात्मक चेतना ‘मैं’ से उत्पन्न होकर सिर्फ ‘मैं’ में ही विलीन हो गयी है।
इन पंक्तियों को यदि हम आचार्य भोज की मान्यताओं के संदर्भ में व्याख्यायित करें तो कश्मीर के हिमशिखर पर राष्ट्र के लिये प्राण न्यौछावर करने वाले सिपाही के अहंकार या स्वाभिमान में राष्ट्रीय रागात्मकता इस तरह द्रवित होकर घुलमिल गयी है कि सिपाही अपने आप में एक राष्ट्र बन गया है। कविता में दूसरी स्थिति राष्ट्रीय रागात्मकता से सिक्त उन राष्ट्रवासियों की है, जिनका अहंकार या स्वाभिमान अर्थात् ‘स्व’, सिपाही के रागात्मक उत्सर्ग को अपने भीतर गर्व और श्रृद्धा के साथ द्रवित कर लेता है। कविता में तीसरी स्थिति स्वयं कवि की है जो वीरगति को प्राप्त सिपाही के प्रति श्रद्धानत तो है ही, साथ ही ऐसे व्यक्तियों के अहंकार या स्वाभिमान को दुत्कारता या धिक्कारता है जिनकी रागात्मकता स्वार्थ के वशीभूत होकर भोग- विलास में ही अपनी जीवन-लीला समाप्त कर देती है। इस कविता का सृजन निस्संदेह कवि की ‘सात्विक बुद्धि’ ने किया है, जिसमें सत्योन्मुखी रागात्मक चेतना अन्तर्निहित है।
माखनलाल चतुर्वेदी की इस कविता से एक नया तथ्य और उजागर होता है कि विभाव अनुभाव और संचारी भाव के संयोग से मात्र उसी तारीके की रसोत्पत्ति नहीं होती जैसा कि रसाचार्य अब तक कहते चले आ रहे हैं, बल्कि रसोत्पत्ति का सम्बन्ध सीधे-सीधे हमारे निर्णयों से है। सिपाही की मृत्यु पर स्थायी भाव शोक का निर्माण होना चाहिए, जबकि उक्त कविता में आश्रय श्रृद्धा और गर्व की ऊर्जा से आद्र होकर सिपाही के वीरकर्म का गुणगान कर रहे हैं। मृत्यु का शोक उनसे कोसों दूर है।
बहरहाल ‘स्व’ के भीतर ‘पर’ की समाविष्ट का मतलब ‘पर’ का उदात्त रूप में ‘स्व’ हो जाना भी है। इस प्रसार ‘स्व’ समूची मानव चेतना तक विस्तार पा जाता है। यही काव्य की सात्विक बुद्धि है और सात्विक बुद्धि की सत्योन्मुखी रागात्मक चेतना और इसी का सीधा-सीधा सम्बन्ध काव्य की आत्मा से है।
सन्दर्भ-
1. – रससिद्धांत, डॉ. चतुर्वेदी, पृष्ठ-112
2. कविता के नये प्रतिमान, डॉ. नामवर सिंह
3. रस सिद्धांत, डॉ. ऋषिकुमार चतुर्वेदी, पृष्ठ-121
4. भोज शृंगार प्रकाश, पृष्ठ-465
————————————————————–
रमेशराज, 15/109, ईसानगर, अलीगढ़-202001