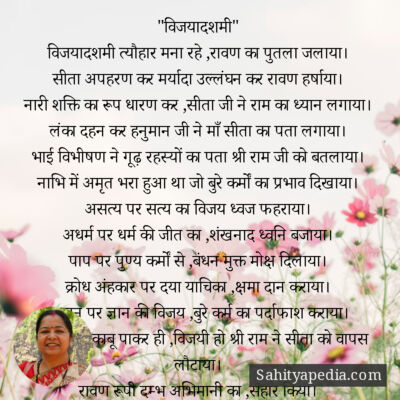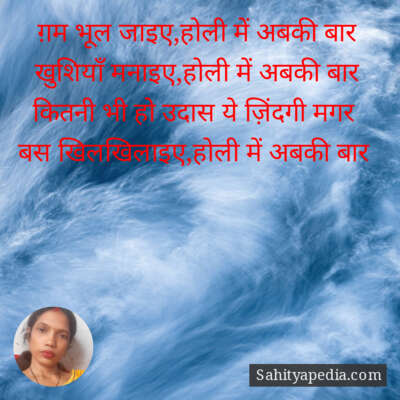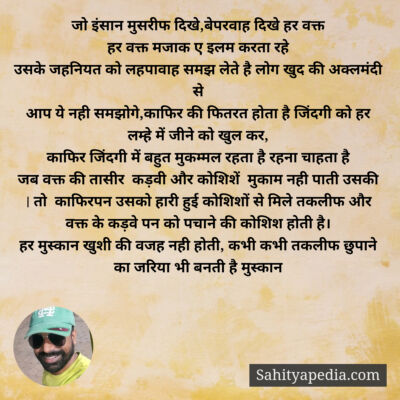कवि की निद्रा
✒
यों भूलकर एक सृजक, अपने तन को,
कुछ नज़्मों को जिंदा किए जा रहा था;
भाल पर नवसृजन, दमक थी छपी यूँ,
लफ़्ज़ों को परिंदा किए जा रहा था।
बनाकर मनस में कुछेक शब्दों को,
दुनिया में लाकर, लिखे जा रहा था;
कोमल हृदय के नाज़ुक स्वभावों से,
रह-रह के सिंचित वह, किए जा रहा था।
सृजन-श्रांति या उम्रभर की थकावट,
भौंहों पर ललचाए टूटे पड़ी थी;
आँखों की विश्रांति मनः झरोंखों से,
अधूरा-सृजनपट्ट रौंदे खड़ी थी।
डाले हुए क्लांत बेलों पर झूले,
पेंगों को, निंद्रा धकेले चली थी;
बेबस किये, शून्य बंधन में बाँधे,
निनिया, कपोलों को चूमे चली थी।
अंतस में जाने को ललचाए अक्षर,
उद्वेलित शब्दों की टोली खड़ी थी;
निकलते ज़ज्बात आरोही होकर,
चतुरंगी महिमा अवर्णित हुई थी।
अलसाया कवि था, थकित सी निगाहें,
हौले-हौले से संग हो चली थीं;
निंदिया-डोली में बैठा सृजनकर,
अनजान राहों में डोली चली थी।
भाँप लिये ‘शब्द’ नन्हें लुभावों को,
चुपके से मन के अंतर में झाँका;
शिखा अंतःकरण प्रज्वलित अनोखी,
आभा निकलती, रौशन खड़ा राका।
तकिये के नीचे से सरक, जुबां से,
बोले लगे शब्द, बोली हमजोली;
निकले रहे सैर मन की ही गंगा,
अदृश्य रंगीन सी रंगत जड़ी थी।
खुश थे बहुत, महाकाव्य से मिलकर,
देखा नहीं जिन्हें, धरती पर आए;
उतावले हो नाद कुलांचे भरें,
कविता की गोदी में दिन बिसराये।
कुछ नन्हे जो अब तक अर्द्ध प्रकट थे,
लेटे पड़े कहीं कोनों में जाये;
कइयों ने देखा जहां का न मुखड़ा,
मुखड़े देख उनके जलज मुरझाये।
स्तब्ध अचंभित थे सबके ही मुखड़े,
चेहरे पर गर्व बहुत ही थे छाए;
सृजनकर मिला एक ऐसा उन्हें जो,
था सत और असत में निर्भय समाए।
गाते चले निज गीतों के बंडल,
धरनी मनुस्मत को रखना बनाये;
जिसने दिया दीप सा हमको जीवन,
दीपशिखा, जीवन की रखना बनाए।
पहुँच दो शब्द, मन की गहराई में,
गोते लगाए ऐसे नैन ललसाए;
कविमन सदा ही निर्मलोपम स्वयं में,
रची आभा ऐसी नयन न समाये।
★(शब्दों ने कवि के अंतर्मन में जो देखा…)
हरियाली फैली तीर तलक,
वसुधा को ढके, रखे छिपाए;
रैन बसेरा करते खगजन,
डैने अपने जरा फुलाए।
ऊपर चाँद चाँदनी लेकर,
झाँक रहा था बरबस नीचे;
स्नेह लिपटकर बैन उचारे,
शब्दों को अपने घर खींचे।
चाँद कहे कुछ कदम बढ़ाओ,
मेरे घर तो शब्दों आओ;
आकर मेरे सुंदर शब्दों,
रूपा हाथ कलेवे खाओ।
निशागेह से आती जाती,
मुस्कानों की रहती आहट;
शोध काम में लगे रहे जब,
नव ऊषा में भी सारे डट।
ताक-झाँक कर नभ, सरवर में,
देख रहा अपनी परछाईं;
चंचल तितली नृत्य रचाकर,
बागों में झट उड़ती आई।
अधर कोष्ठ देख मधुबाला,
रीस रोक बोली सकुचानी;
घर को अपने लौट चलो तुम,
शब्द धनों छोड़ो नादानी।
सफर सुहाना था सबका पर,
मन छाया अचरज था भारी;
कविमन जैसे ही मन सबको,
देना माधव, कृष्ण, मुरारी।
घर को अपने पहुँचे सब मिल,
गिरते पड़े कवित में जाकर;
खुली नींद सोते कवि की ज्यों,
किलकिंचित ध्वनि से टकराकर।
नव तन्मयता जाग उठी थी,
कवि के सुलझे अंतर्मन में;
थे समझ न पाए नैन कवि के,
सच में थे या वे सपनों में।
…“निश्छल”
भावार्थ:-
रूपा – चाँदी (यहाँ चाँदनी से तात्पर्य है)