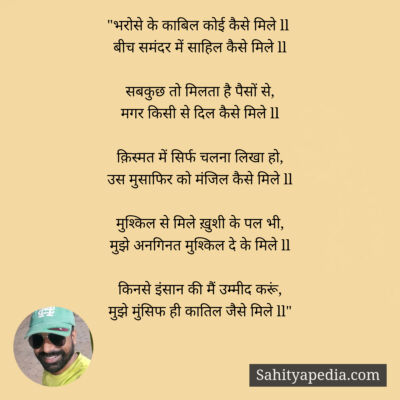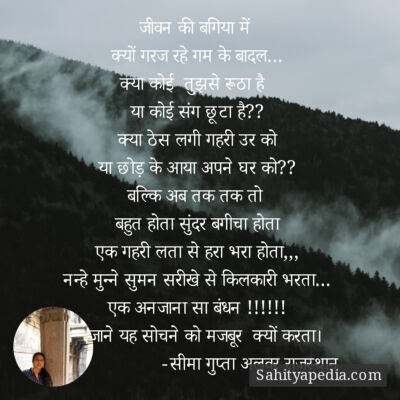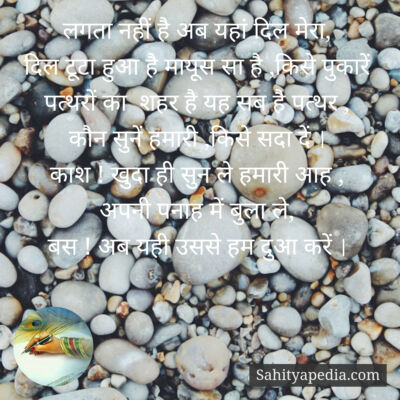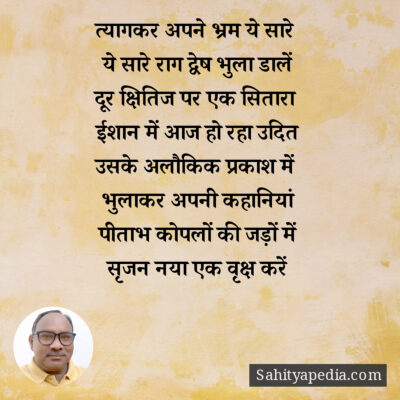कविता

उस दिन, मैं टेक लगाए बैठी थी
और वो, आकर मेरे पैरों से अपना चेहरा सटाकर लेट गया।
उसकी गर्म हथेलियों ने मेरे दोनों पंजों को नर्मी से छुआ
मेरे तलवों पर बारी बारी सटते रहे उसके होंठ।
उसके गालों ने मेरे तलवों से ठीक वैसा ही संवाद किया, जैसे करता है कोई माथा हथेली से।
मैं उसे देख रही थी, एकटक…।
उसे रोकना चाहा,
पर “थरथराते होंठ बागी औरत की तरह होते हैं,” सो “रुक जाओ”, नहीं सुना गया।
और अनजाने,अचानक आँखों से कुछ लुढ़का…,
हां! आँसू ही थे, पर क्यूँ ? ये बाद में सोचूँगी।
उसे देखा… जो आँखें मूँदे अभी भी तलवों से अपने गालों को सुख दे रहा था
तब, उसका चेहरा यूँ लगा,
जैसे “अहम स्वयं बुद्ध के पैरों में गिरकर निर्वाण तलाश रहा हो।”
मन किया उसे उठाकर छाती में समेट लूँ,
मैं बुद्ध नहीं थी, वो अहम/पुरुष नहीं था।
मेरा हृदय मेरे तलवों से, खिसक गया
उसके होठों में, गालों में
सजल हो रही आँखों में।
उस पल लगा जैसे,
उन दो तलवों से सटी, मैं ही हूँ।
मैं ही मुस्कुरा रहीं हूँ।
मैं ही रो रही हूँ।
मेरे ही माथे में चिरशांति स्थापित हो रही है।
लगा, कि वो नहीं हैं।
है, तो बस
छुअन, चुम्बन, आँसू, आलिंगन, शांति, मोक्ष…।
बस!
शिवा अवस्थी