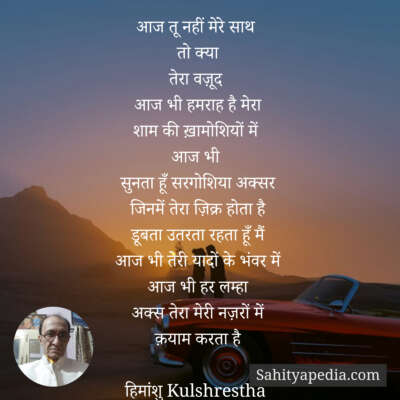एक श्वास पर खुद की भी अपना हक नहीं
एक श्वास पर खुद की भी अपना हक नहीं
चले हम बस्तियों पर हक मगर अपना जताने ।
उपेक्षित होते जब फिर स्वप्न हक के
बिखर जाते है मन के आबदाने ।
न पूँछो टूटता फिर क्या-क्या मन में
उमगती पीर कितनी तन में, मन में,
शिथिल हो जाते सारे गात इतने
लड़खड़ाते पाँव फिर हैं हर कदम में ।
रुधिर सब श्वेत होकर अश्रु का सैलाब बनता
समय की ताप से फिर लावा सा ये तन पिघलता |