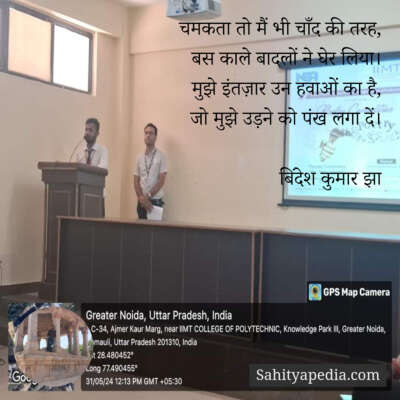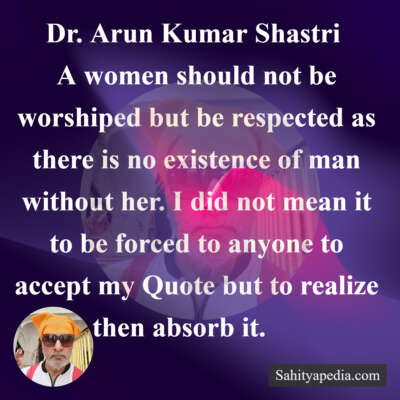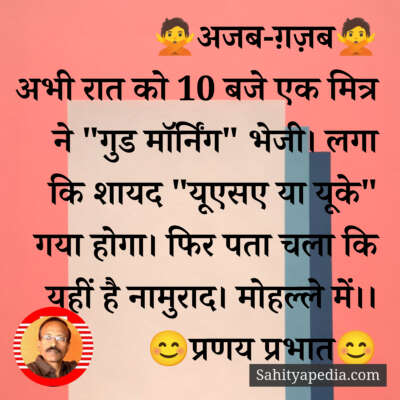साहित्य का बुनियादी सरोकार +रमेशराज

किसी भी देश या काल के साहित्य के उद्देश्यों में पीडि़त जनता की पक्षधरता इस बात में निहित होती है कि यदि तत्कालीन सामाजिक व्यवस्था में किसी भी प्रकार की विसंगतियां, कुरीतियां पनप गई है, तो उनके निर्मूलन हेतु साहित्य का प्रयोग एक गाल पर तमाचा खाने के बाद दूसरा गाल करने या प्रेयसी की जांघें सहलाने, प्रकृति-चित्रण करने के बजाय संस्कृति और सभ्यता के तस्करों की मानसिकता पर चाबुक बरसाने में ही सार्थक होगा।
प्रेयसी के घुटनों पर लेटकर उसकी धड़कनों के ज्वार-भाटों और चेहरे पर प्रेम-प्रसंगों से चढ़ती-उतरती लालामी को ही यदि सूक्ष्म दृष्टि रेखांकित कर सकती है और उसकी अभिव्यक्ति समाज को विकृतियों से दोषमुक्त कर सकती है, तो हमें ‘अफसोस’ के अतिरिक्त कुछ नहीं कहना। साथ ही सामाजिक यथार्थ का तल्ख एहसास कोई बे-बुनियाद, वाहियात और स्थूल वस्तु है, जिसका अनुभव सिर्फ अपने अन्दर के मैले को बाहर फेंकने और अपने दोष दूर करने तक ही होना चाहिए, यानि ‘आप भला तो जग भला’ को चरितार्थ करना है तो यहां यह भी निवेदन करना चाहेंगे कि जब हम शोषण-व्यभिचार या चरित्रहीनता पर व्यक्तिगत दृष्टि के बजाय सामाजिक दृष्टि रखते हैं, तब भी अपने ही दोषों को सर्वप्रथम टटोलते हैं , क्योंकि हम भी उसी समाज के अंग हैं जिस पर हम प्रहार कर रहे होते हैं। इस स्थिति में यह प्रहार क्या हमारे अपने ऊपर भी नहीं होता?
यदि दृष्टि की व्यापकता या सामाजिकता काजीपन या स्वयंभू होने की स्थिति है तो हमें इस समाज में न रहकर गुफाओं-कन्दराओं में धूनी रमाकर अपनी सूक्ष्म दृष्टि के परीक्षण करते रहना चाहिये और अपनी आध्यात्मिकता का दम्भ भरते रहना चाहिये। हमारे देश की विडम्बना यह रही है कि जन-चेतना के लिये जिसने भी पहल की, उसे स्वयंभू, काजी और न जाने किन-किन उपाधियों से विभूषित किया गया।
स्वान्तः हिताय की तथाकथित वांछित साधना, योग और आत्म नियन्त्रण की साधना बनकर जब-जब साहित्य में उतरी, तब-तब उस साहित्य ने समाज को ऐसे ‘सोच’ के गर्त में डाल दिया, जिसमें मलवा तो हर जगह दिखाई दिया लेकिन उसे बाहर फेंकने की हिम्मत कोई नहीं रख सका। लोगों ने नाक पर या तो अकर्म और भाग्य का रूमाल रख लिया या फिर ‘परमानन्द’ की उस स्थिति में पहुंच गये, जिसमें सड़ांध से उठता भभका भी गुलाबों की महक महसूस हुआ।
सामाजिक त्रासदियों के बीच जीवन के सहज आनन्द का ढिंढोरा पीटने वाले अगर देखा जाये तो आज भी वही लोग हैं जिन्हें संटी खाकर बोझा ढोने की गर्दभ परम्पराओं से जुड़े रहकर अपने आचरण से ऐसी परिस्थितियों को जन्म देते रहना है जो युग-युगान्तर आदमी का खून चूसती रहें।
मानव के आचरण की एक-एक इकाई में आमूल-चूड़ परिवर्तन करने या समाज में क्रान्तिकारी संभावनाएं तलाशने के लिये आवश्यक है कि यातनामय, कारुणिक दृश्यों से भयाक्रान्त होकर आंखें मूदने या फोड़ने, चीत्कार के बीच कानों में रुई ठूंसने के बजाय लक्ष्य की प्राप्ति आंखें और कान खोले इसी संसार में रहकर करें। साथ ही साहित्य की प्रासंगिकता उसके यथार्थवादी दृष्टिकोणों से जोड़ें, नहीं तो हम साहित्य की उन्हीं कलात्मक या सौंदर्यवादी रूढि़यों से बंधे रह जाएंगे, जिसमें कबीर की प्रहार क्षमता, आडम्बरों को चुनौती देने की व्यग्रता या ‘पुत्री बेच पिता धन खायो, दिन-दिन मोल सवायो’, मोहि कहा तेरी सीकरी सों काम’, ‘खेती न किसान को, भिखारी को न भीख बलि… कहे एक-एक न सों कहां जाई कहा करी’ ‘एक न को मेवा मिलै एक न को चने भी नाहिं’ ,‘सब जादे मिटि के हरामजादे हो रहे तथा ‘अली-कली ही सों बंध्यौ आगे कौन हवाल’ में हमें कोई तिरोभाव दिखाई नहीं देगा। बिस्मिल, अशफाक, भगतसिंह को साहित्यकार मानता तो दूर, उनका जिक्र करना भी पसन्द नहीं करेंगे। और बेचारे रहीम को गैर साम्प्रदायिक होने के नाते ही काव्य का दूसरा ‘कबीर’ स्वीकार ही नहीं पाएंगे | हम साहित्य के ठेकेदार और पंडित जो ठहरे। धूमिल की कविताओं को हम मात्र गाली-गलौज ही मानेंगे, [जैसा कि अलीगढ़ की एक डिग्री कालिज के एक हिन्दी प्रवक्ता तथा प्रकाशक के मुख से हमें सुनने को मिला, जब हम ‘संसद से सड़क तक’ उनके यहां से खरीदने गये] क्योंकि हमें सौन्दर्यानुभूति उसी साहित्याभिव्यक्ति में होती है जो कोमल, कर्णप्रिय और तिरोभाव से मुक्त होती है। ऐसे तथाकथित साहित्यकारों से हम पूछना चाहेंगे कि दहेज लालचियों द्वारा मिट्टी का तेल छिड़ककर जलाए जाने वाली बहू या बलात्कारियों के बीच छटपटाती नारी की चीत्कार या डकैतों द्वारा एक परिवार पर किये गये लाठी चाकू और कट्टे से प्रहार की करुण-गाथा का वे कौन-से लालित्यपूर्ण, कोमल और सुन्दरतम शब्दों में व्यक्त करना चाहेंगे? तथा ऐसी यातनामय स्थितियों के बीच वे साहित्य का कौन-सा कलापक्ष टटोलेंगे?
यदि कोई साहित्यकार ऐसी स्थितियों में कुव्यवस्था के प्रति सब कुछ कहने का अधिकारी होता है, कलुषता को ललकारता है तो वह वाद, खेमे, विधा का झंडा उठाए, बाल बिखेरे, कफन का उत्तरीय कन्धे पर डाले, कविता और साहित्य को कितना और कैसे नष्ट कर देगा? यह सोचने का विषय है?
वक्त के साथ यदि हमारी रूढि़वादी मान्यताएं न बदलीं और हम मीरा की तरह प्रेम दीवाने होकर जहर पीते रहे, तुलसी की तरह ‘कोऊ नृप होई हमें का हानी’ की रट लगाते रहे तो वह दिन दूर नहीं जब कविता या साहित्य नष्ट हो न हो, रही सही इन्सानियत [यदि है तो] जरूर नष्ट हो जाएगी। तब हमारे सौन्दर्यवादी, अत्याचारी वातावरण के बीच सहज आनन्द को प्राप्त होने वाले रचनाकार साहित्य को कौन से आत्मशुद्धि के दौने में रखकर चाटेंगे? यह तो आने वाला समय ही बताएगा?
साहित्य का बुनियादी सरोकार सामाजिक चरित्र की सार्थक अभिव्यक्ति के साथ-साथ उसे परमार्जित करने में भी होना चाहिए। इसके लिए यह आवश्यक है कि साहित्य समाज के उस हर चरित्र को जिये जो कहीं न कहीं समाज की संवेदना को छूता है। इस संदर्भ में तेवरी ने समाज के उस दलित, शोषित, पीडि़त जन के चरित्र को जीया है जो भीतर ही भीतर सभ्यता को सौदागरों, राजनीति के ठगों, धर्म और समाज के ठेकेदारों के हत्यारे षडयन्त्रों के बीच मुक्त होने के लिए छटपटा रहा है।
जहाँ तक ग़ज़ल का ताल्लुक है तो वह सदियों से खास आदमी के चरित्र जुड़ी रही है, जो तेवरी की मान्यताओं, जीवन-मूल्यों के एकदम विपरीत है। ग़ज़ल के साथ सामाजिक दायित्वों या अभिव्यक्ति का ढिंढोरा पीटने वाले रचनाकार सुषमा, सरिता, सारिका, जाहनवी, धर्मयुग, कादम्बिनी, साप्ताहिक हिन्दुस्तान और समस्त लघु पत्रिकाओं में प्रकाशित लैला-मजून के किस्सों की गौरवगाथाओं का बखान करने वाली ग़ज़लों में कौन-सा सामाजिक दायित्व टटोलेंगे? इमली को आम बताकर, इमली का स्वाद आम की तरह चखने वाले रचनाकारों की पता नहीं कब यह बात समझ में आएगी कि मदिरा से भरे हुए प्याले का जाम कहा जाता है जहर से भरे हुए प्याले को नहीं। यदि ऐसे रचनाकार जहर को जाम की तरह अधरों से लगाने के आदी हो गए हैं तो इनकी बुद्धि पर तरस खाने को जी करता है। वरना स्वतंत्रता आन्दोलन के अगुआ भगत सिंह, चन्द्रशेखर, गांधी और गोखले में, कोठे पर बैठने वाली चम्पाबाई और अंग्रेजों के छक्के छुड़ाने वाली रानी लक्ष्मीबाई, मादाम कामा में तथा प्रधान मन्त्री के रूप में लालबहादुर शास्त्री और नेहरू में, एक शासक के रूप में सम्राट अशोक और हिटलर में कुछ तो अन्तर करना ही पड़ेगा। वे साहित्य और समाज के उस चरित्र को किस आधार पर नकारना चाहते हैं जो प्रवृत्तियों, दायित्वों, कर्तव्यों के आधार पर भिन्नता लिये हुए है?
लिखाई की एक-सी वस्तुओं जैसे-पेन, पेन्सिल और होल्डर, प्यार वासना की तृप्ति के साधन पत्नी, प्रेमिका, रखैल, वैश्या और कॉलगर्ल, सब्जी पकाने के पात्र कढ़ाई, केतली, डेगची, भगौना व कुकर, रोटी सेकने के साधन चूल्हा, अंगीठी, स्टोव, लक्ष्य तक पहुंचाने वाले मार्ग सड़क, पगडन्डी, दगड़ा, परिवहन के साधन ट्रक, टैक्सी, ट्रेन, बस, गाड़ी, रथ, हेलीकाप्टर व हवाई जाहज, सिंचाई के साधन रहट, पुर, ट्यूबबैल व ढैकुली आदि में कोई अन्तर नहीं होता है?
यदि बात मात्र कविता ही कहने से चल जाती तो दोहा, सवैया, घनाक्षरी, गीत, नवगीत, कविता, पद, भजन, ग़ज़ल, हज़ल, कलमा, मर्सिया, नज्म आदि नामों से पुकारने की क्या अवश्यकता थी? और काव्य को प्राचीन, भक्ति कालीन, रीतिकालीन, छायावादी, प्रगतिवादी, प्रयोगवादी, नई कविता आदि खानों में समीक्षकों तथा आलोचकों ने किस आधार पर और क्यों बांटा? दूसरी तरफ कबीर, तुलसी, सूर, विद्यापति बिहारी आदि की कविताओं को उनके नाम से पुकारने के बजाय मात्र ‘कवि की’ कहकर अपना काम नहीं चला सकते?
जिन लोगों को सामाजिक और साहित्यक चरित्र की पहचान नहीं है, ऐसे लोग आदमी, मनुष्य और पुरुष, जल और पानी में कोई अन्तर स्पष्ट कर पाएंगे, संदिग्ध ही नहीं, असम्भव-सा प्रतीत होता है।
यही बात तेवरी और ग़ज़ल में सीमा रेखा खींचते हुए तेवरी के कथ्य पर प्रकाश डालने के उपरान्त तेवरी के शिल्प खासतौर से छन्द पर यहां चर्चा करना आवश्यक है।
तेवरी के किसी भी छन्द की रचना करते समय स्वर और लय की आवश्यकता होती है। जबकि उर्दू में गजल लिखने के लिये लय के साथ वज्न अर्थात बहर पर ध्यान देना जरूरी होता है। उदाहरणार्थ- एक साहब ने दूसरे साहब से नीचे का मिसरा देकर गिरह लगाने के लिए अर्थात इसकी जोड़ का दूसरा मिसरा कहने को कहा-
‘जो बात की खुदा की कसम लाजवाब की’
दूसरे साहब ने तुरन्त ही मजाक में नीचे वाला मिसरा जवाब में कहा-
‘जूते में लगाई है किरन आफताब की’।
दोनों मिसरों में बाईस-वाईस मात्राएं हैं, लय भी एक-सी है, इसलिए हिन्दी कवि दूसरे मिसरे को ठीक बता देगा, परन्तु उर्दू बहरों के हिसाब से पहले मिसरे का वजन ‘मफऊल फाइलात मफाईलु फाइलुन’ तथा दूसरे का ‘मफऊल मफाईलु मफ़ाइलु फाइलुन’ है’’ [संदर्भ-सरल पिंगल प्रवेशिका- श्री प्यारेलाल वृष्णिः]
इस आधार पर तेवरी और ग़ज़ल के छन्द यदि बारीकी से देखा जाये तो किंचित साम्य नहीं रखते। एक तरफ जहां उर्दू में बहरें हैं, ठीक उन्हीं के समान हिन्दी काव्य में छन्द भी है। उदाहरणार्थ-
चैपाई-15 मात्रा की होती है जिसके अन्त में गुरु लघु होता है। वैतालिक [श्री हरगंगा] इसी ध्वनि में गाया जाता है-
कवसों विप्र खड़ौ जिजमान, दानी को धन दें भगवान।’
इसी छन्द में उर्दू की यह बहर है- फाअ फैलुन फाअ फऊल- आज दिखादो दीद हुजूर।
पीयूष छन्द का हर एक चरण 19 मात्रा का होता है तथा अन्त लघु गुरु होता है।- ‘नाक का मोती अधर की क्रांति से, बीज दाडि़म का समझकर भ्रान्ति से।’[‘साकेत’ मैथलीशरण गुप्त]
ठीक इसी तरह फाइलातुन, फाइलातुन, फाइलुन [इब्तिदा-ए-इश्क है रोता है क्या-गालिब] गजल की एक बहर भी है।
इसके अतिरिक्त विजात [मुतदारिक], शक्ति [मुतकारिब-उपभेद], सगुण [मुतकारिब-उपभेद], सुमेरू ‘[हजज महजूफज] , प्रिय [सालिम, बिहारी [हजज मकसूर], दिग्पाल [मजारअ अखरब], गीतिका [रमल महजूफ], हरिगीतिका [रजज], फूलमाला [रमल], विधाता [सालिम], खरारी [मुस्तजाद], झूलना [मुतदारिक] आदि हिन्दी के छन्द अनेक आगे कोष्ठक में लिखी ग़ज़ल की बहरों के [सतही रूप से] समान ही है, अगर अन्तर है तो वजन और स्वर-लय के बीच।
इस आधार पर किसी भी ग़ज़ल की तरफदारी करने वाले रचनाकारों का यह कहना कि तेवरी छन्द के आधार ग़ज़ल ही है, अतार्किक है | कयोंकि तेवरी के छनद अपने हैं और गजल की बहरें उसकी अपनी। लेकिन अफसोस तो इस बात का है कि तेवरी पर अधकचरेपन का लांछन लगाने वाले अधिकांश वे ही तथाकथित ग़ज़लगो हैं जिन्हें न तो गजल लिखने की तमीज या जानकारी है न तेवरी की।
यदि ऐसे लोग मात्रा रदीफ- काफिये [तुकान्तों] के आधार पर तेवरी को ग़ज़ल मानते हें तो हम उनसे पूछना चाहेंगे कि वे कवित्त और पदों को भी ग़ज़ल क्यों नहीं रख लेते? ग़ज़ल के रदीफ, काफियों के समान इनमें भी रदीफ़-काफिये मौजूद हैं, यथा –
पद-
भक्ति का मारग छीना रे।
नहिं अचाह नहीं चाहना, चरनन लौ लीना रे।।
कहैं कबीर मत भक्ति का परगट का दीना रे।।
कवित्त-
शोभा को, सदन, ससि बदन मदन कर
बंदै नरदेव कुवलय वरदाई है।।
पावन पद उदार, लसित हंसक मार
दीपति जलजहार, दिस-दिस धाई है।।
तिलक चिलक चारु, लोचन कमल रुचि
चतुर-चतुर मुख, जग जिब भाई है।।
अमल अंबर नील, लीन पीन पयोधर
केसौदास सारदा कि,सरद सुहाई है।। केशवदास
——————————————————————————
+रमेशराज, 15/109, ईसानगर, अलीगढ़-202001