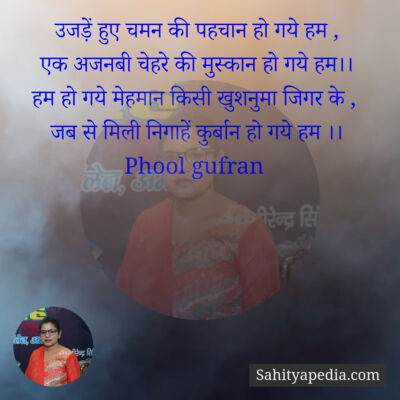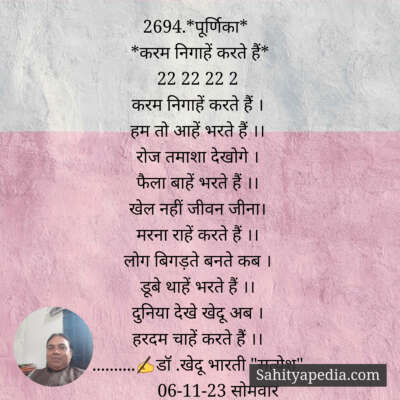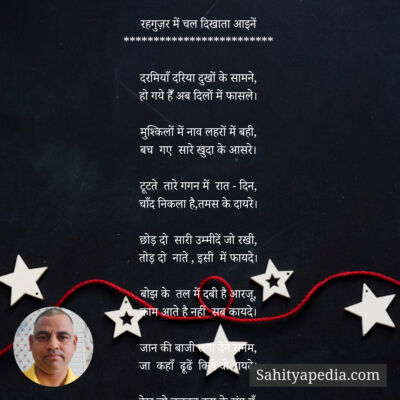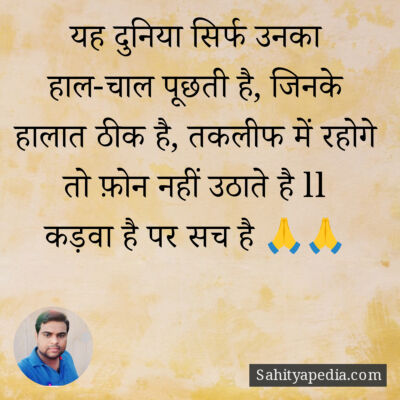शीर्षक – रेल्वे फाटक

ज़िंदगी भर रोज़ की तरह
आज़ की सुबह सुबह
वो सब भी निकल पड़े
हर सुबह शाम की तरह
कुछ अलग नहीं था आज़
हर सुबह की तरह
किसी को जाना था दफ़्तर
तो किसी को जाना था स्कूल
भागदौड़ भरी जिंदगी में
कहां होता है सुकून
चल दिए चलते चलते
भीड़ का हिस्सा होते गए
सफ़र था लम्बा
था काम ये रोज का
थोड़ा सा भी लेट होते
फाटक रेल्वे के रोक लेते
सब का सफ़र
थम गया
कुछ क्षण वक्त
वहीं रुक गया
जो गाड़ियों में थे
वो इंतज़ार करते रह गए वहीं
फाटक खुलने का
सब वहीं थम गए
जो पैदल थे
जान जोख़िम में डाल
निकल गए
उस पार
कुछ फ़ोन उठा लिए
कुछ आपस में बतिआ लिए
कुछ चारों ओर नज़रें दौड़ा लिए
मैं भी उन्हीं में से थी
मैं देख रही थी
किनारें सड़क के पेड़ घनें थे
पेड़ खिलखिला रहे थे
मानो जैसे दुआ दे रहे हों
ठंडी हवाएं
चल रही थी
गर्मी में ठंडी
सांसे दे रहीं थी
पत्तियों की वर्षा
शुभ आशीस दे रहीं थी
मन में ख्याल आया
काश! ये फूल होते
कोई गम नहीं इस बात का
फूल नहीं मिले तो क्या
पत्तियों में ही
खुशियां ढूंढ लिए
देखा चारों तरफ़ मैंने
पीछे एक मुस्कुराता चेहरा
सारे चेहरों में था अकेला
जहां बाहर से सभी मौन थे
अंदर ही अंदर दुनियां समेटे
कुछ अपनी कुछ सपनों की
कुछ अपनी कुछ अपनों की
दुनियां समेटे
मशाल जलाए बैठे
एक युद्ध था होनें को
जो वक्त के विरुद्ध था
लेकिन वक्त तो रुका था
ज़िंदगी के मजे ले रहा था
मुझे कोई जल्दी नहीं थी
में देख रही थी सबको
पढ़ रही थी सबको
आंखें मेरी सबके
चेहरों पर टिकीं थी
चारों ओर नजरें मेरी
दौड़ रहीं थी
चारों ओर शांति छा गईं
ट्रेन के शोर गुल में
शांति कहीं गुम गई
जातें ही ट्रेन के
फाटक खुल गए
हड़बड़ी में ही कुछ लोग
गड़बड़ी कर गए
भागना था सबको
जल्दी थी भीड़ में खोने की
भीड़ का हिस्सा होने की
क्या करें ज़िंदगी है
ज़िंदगी से जुड़े हैं
ज़िंदगी उनसे हैं
जो हमसे जुड़े हैं
इसी लिए सुबह शाम
भाग रहें हैं
क्या थी अपनी ज़िन्दगी
अपने हैं तो
अपनी है ये ज़िंदगी
अपना नहीं तो
मौत भी अपना रस्ता
नहीं पूछती
अपनों से तो बनता घर संसार है
अपनों से होती अपनी पहचान है
_ सोनम पुनीत दुबे