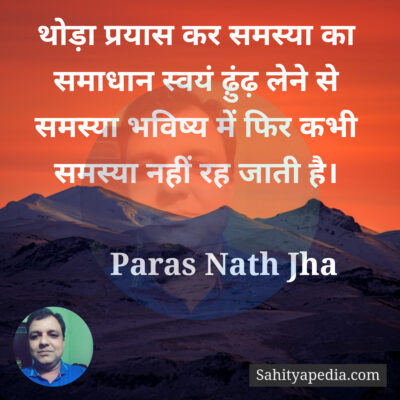‘व्यथित मानवता’

वर्जनाएँ टूटतीँ,
सँयम, सिमटता जा रहा।
कलुषता अरु दम्भ का,
साम्राज्य, बढ़ता जा रहा।।
हो रहे रिश्ते, कलँकित,
घर मेँ भी, अरु सड़क पर।
दिन-ब-दिन, निर्लज्जता का,
ग्राफ, चढ़ता जा रहा।।
अब कहाँ, गरिमा रही,
मिलने मेँ, प्रेमालाप की।
छुद्र अरु भोँडा प्रदर्शन,
सुर्ख़ियां है, पा रहा।।
रह गई शुचिता, सिसकती,
झूठ की दहलीज़ पर।
भरभरा कर सत्य का,पर,
क्यों किला ढहता रहा।।
छद्मता, आडम्बरों का साथ,
निशि-दिन भा रहा।
किन्तु मानवता से क्यों है,
दूर मानव जा रहा।।
कोई तो “आशा” बँधा दे,
व्यथित मन को, अब मेरे।
क्यों चतुर्दिक, धुन्ध सा,
नैराश्य है, गहरा रहा…!
##———-##———-##——