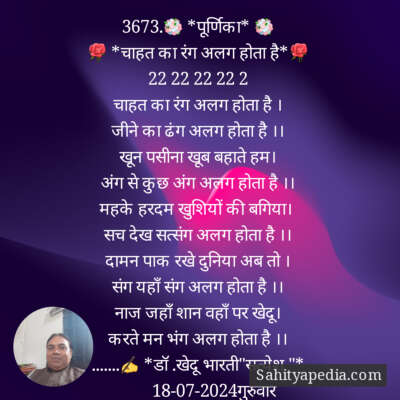रोज़ शाम होते ही
रोज शाम होते ही
समेटने लगती हूँ मैं
दिन भर के अपने आप को
अपने अंदर
चाय के एक अदद प्याले में उड़ेल लेती हूँ
माँ की वो खट्टी-मीठी झिड़कियाँ
पति की झूठी सी तकरार
पापा के रौब के पीछे छुपा हुआ स्नेह
औऱ शक्कर की जगह
घोल देती हूँ ढेर सारी
बच्चों की निश्छल मुस्कान
चेहरे के साथ धोती चली जाती हूँ मैं
दिनभर होती बेमतलब की मीटिंग्स
कुछ पुरुष सहकर्मियों के मन में छिपा मैल
आगे बढ़ता देख अपना कहने वालों की आँखों में उतर आई जलन
घर और नौकरी के बीच सन्तुलन की वो ऊहापोह
कपड़ों की तह के साथ ही संजोकर रखती जाती हूँ
परिवार के साथ बिताये ख़ुशी के वो दो पल
दिनभर में मिले प्रशंसा के कुछ बोल
लोगों के चेहरे पर आई मुस्कुराहट
कुछ पूरे, कुछ अधूरे से सपनें
और कुछ छोटी-छोटी सी आशाएँ भी
भोजन के साथ पकाती चली जाती हूँ
वो अधपके से सास-बहू के रिश्ते
बच्चों का सुनहरा भविष्य
हफ्ते की वो एक अदद छुट्टी का प्लान
जो कई बार अचानक ही हो जाती है निरस्त
और कविता की कुछ अधूरी पंक्तियाँ भी
बर्तन समेटते समेटते
व्यवस्थित कर देना चाहती हूँ मैं
बूढ़े बरगद बाबा के झुके हुए कन्धे
भूखे पेट अन्न उगाते किसान की आँखों से छलकता दर्द
बाजार में खड़ी विक्षिप्त महिला का पागलपन
सिग्नल पर अखबार बेचते बच्चों की उम्मीदें
अखरोट के पीछे भागती गिलहरियों का संघर्ष
और भी ना जाने
कितना कुछ समेटना चाहती हूँ मैं
दिन ख़त्म होने से पहले
पर
हर रोज
कुछ न कुछ रह ही जाता है
शेष
लोधी डॉ. आशा ‘अदिति’