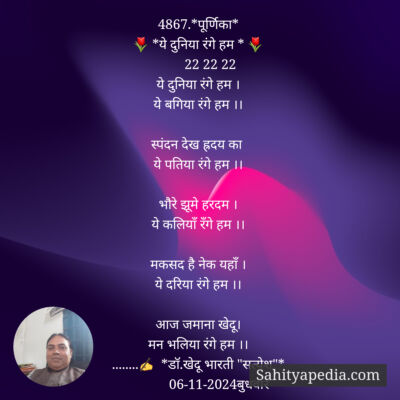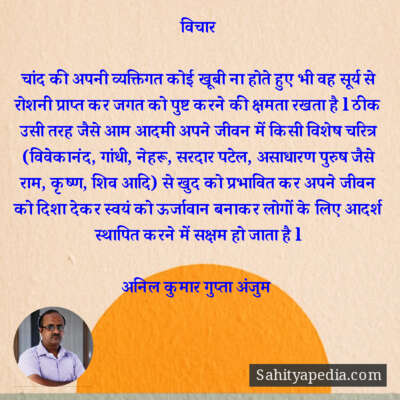बिहार–झारखंड की चुनिंदा दलित कविताएं (सम्पादक डा मुसाफ़िर बैठा & डा कर्मानन्द आर्य)

जिस संग्रह की बहुत दिनों से प्रतीक्षा थी वह दो कर्मठ कवियों- डॉ. मुसाफ़िर बैठा और डॉ. कर्मानन्द आर्य के संपादन में छपकर इस साल प्रकाशित हो गया है। संग्रह का नाम है- ‘बिहार-झारखण्ड की चुनिन्दा दलित कविताएँ’ (बोधि प्रकाशन, जयपुर)।
इस संग्रह में कुल 56 कवियों की 333 कविताएँ हैं। संपादक-द्वय ने बड़े श्रम से कई आयु-वर्ग वाले कवियों की कविताओं को संजोया है। दोनों संपादकों ने अलग-अलग संपादकीय लिखकर इस परियोजना के उद्देश्य और अपनी चिंताओं को शब्द दिए हैं।
‘अज्ञात कुलशील कवियों के अनिवार पदचाप’ शीर्षक से लिखे अपने संपादकीय में डॉ. मुसाफ़िर बैठा ने दलित मुक्ति की शुरुआत का श्रेय अंगरेजी शासन को दिया है। अंगरेजों के शासनकाल में ही दलितों को “अभिव्यक्ति के औजार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अवसर” मिले। अंगरेजी भाषा की शिक्षा ने इस मुक्ति अभियान में केन्द्रीय भूमिका अदा की- “अंग्रेजी शासकों ने भारत में अंग्रेजी शिक्षा का जो दरवाजा खोला वह इन समुदायों के लिए अचरजकारी ’वरदान’ के समान था।” संपादक के अनुसार सर्वाधिक वंदनीय नाम लार्ड मैकाले का है- “अंग्रेजी नौकरशाह एवं भारत शिक्षा मंत्री लॉर्ड मैकाले द्वारा अंग्रेजी शिक्षा का द्वार दलित, शूद्र एवं आम स्त्री तबके के लिए खोला जाना वंदना पाने योग्य काम है।” इस संपादकीय का दूसरा मुद्दा मध्यकाल है। इस काल में तुलसीदास अपनी “बेहूदी कल्पनाओं, कथाओं की जड़ धार्मिक चाल में रह व रम कर अंधविश्वासी विभ्रमों को अपनी रचनाओं के माध्यम से गति दे रहे थे वहीं उनके समकालीन कबीर और रैदास धार्मिक अंधविश्वासों एवं कुरीतियों पर प्रहार करने वाली लक्षणा और व्यंजना में लगभग वैज्ञानिक मिजाज की जनसमस्या-बिद्ध कविताई बाँच रहे थे।” संपादक ने इस विरोधाभास के निराकरण की तरफ ध्यान नहीं दिया है कि जब दलित तबके को दो सौ साल पहले पहली बार अंग्रेजों ने अभिव्यक्ति के औजार और अवसर दिए तो छः सौ साल पूर्व दलित पृष्ठभूमि वाले संत कवि वैज्ञानिक मिजाज की जनसमस्याबिद्ध कविताई किस प्रकार रच रहे थे? अंगरेजों को प्रथम मुक्तिदाता मानने का परिणाम यह निकला कि सन् नब्बे के बाद बहुराष्ट्रीय कंपनियों का जो मकड़जाल पसरा है, उसे विचार के दायरे से बाहर रखा गया है। एक-एक कर तमाम सार्वजनिक/सरकारी उपक्रमों को निजी हाथों में सौंप देने का जो सिलसिला चल निकला है उसका वंचित तबके पर क्या असर हो रहा है उसकी तरफ ध्यान देने की जरूरत संपादक को नहीं महसूस हुई है। लेकिन, इस बात के लिए संपादक की खुले मन से तारीफ करनी चाहिए कि अपनी ‘स्थापनाओं’ को उन्होंने निर्भ्रांत तरीके से रखा है। ऐसी दो स्थापनाएँ बानगी के लिए- 1) “मेरा तो यहाँ तक मानना है कि तुलसी के काव्य में अपनी भक्ति अर्पित करते हुए काव्य सौंदर्य की प्रशंसा में रत होना बलात्कार की घटना में सौंदर्यशास्त्र ढूँढने और उसकी वकालत करने के बराबर है।” 2) “विस्मय तो तब होता है जब कथित वामपंथी खेमे के लेखकों एवं आलोचकों द्वारा मार्क्सवादी माने जाने वाले कवि मुक्तिबोध को सर्वश्रेष्ठ कवि ठहरा दिया जाता है मगर इन मुक्तिबोध के यहाँ एक भी कविता ऐसी नहीं मिलती जो दलित हित को संबोधित हो अथवा ब्राह्मणवाद एवं सवर्णवाद की नब्ज पकड़ती हो।”
संग्रह के दूसरे संपादकीय ‘बिहार क्षेत्र में दलित रचनाशीलता की जमीन’ में डॉ. कर्मानन्द आर्य का ज़ोर स्थिति की विवेचना करने पर अधिक है, ‘स्थापना’ देने पर कम। बिहार के इतिहास का खाका पेश करते हुए कर्मानन्द ने उन पूर्वग्रहों का स्मरण कराया है जिनकी वजह से यह प्रदेश नाइंसाफी का शिकार रहा है। वे बताते हैं कि पिछली सदी के आठवें दशक तक बिहार में तीन बड़े आंदोलन देखने को मिले- वामपंथी, समाजवादी और नक्सल। “तीनों ही आंदोलनों में जो मुद्दा प्रमुखता से सामने आया वह है सामाजिक प्रतिष्ठा, जातीय अपमान और गैर बराबरी के खिलाफ़ लड़ाई। वामपंथी आंदोलन में सबसे अहम भूमिका जिन वर्गों की रही, उनमें सबसे ज्यादा दबे-कुचले वर्ग के लोग हैं।” बिहार के दलित रचनाकारों का परिचय कराते हुए संपादक ने इन्हें तीन पीढ़ियों में रखा है। नवीनतम पीढ़ी भाव-भाषा और सौंदर्यबोधीय आयामों को लेकर खासा सजग है, यह बात आश्वस्तिकारी है। अपने संपादकीय के समापन अंश में डॉ. कर्मानन्द ने लिखा है- “अमूमन यह माना जाता है कि दलित रचनाकारों की रचनाओं में आक्रोश का स्वर अधिक है और यहाँ पर प्रेम, साहचर्य और सहअस्तित्व की रचनाएँ बहुत कम हैं पर इस कविता संग्रह को पढ़ते हुए आपकी यह अवधारणा विखंडित हो सकती है। जहाँ दमन होता है, मुक्ति की शुरुआत वहीं से होती है।” किसी संग्रह की भूमिका लिखने का मुख्य उद्देश्य यह होता है कि नए पाठक बनाए जाएँ और पुराने पाठक समुदाय को सफलतापूर्वक संग्रह की तरफ आकृष्ट किया जाए। कर्मानन्द की ‘भूमिका’ इस चुनौती या दायित्व को बखूबी समझती है।