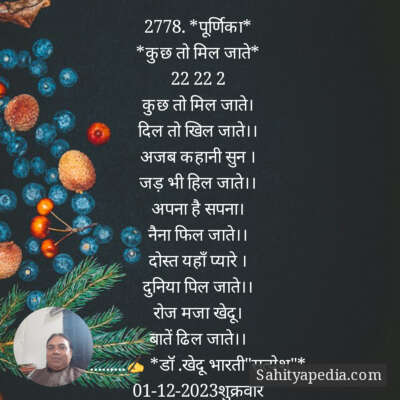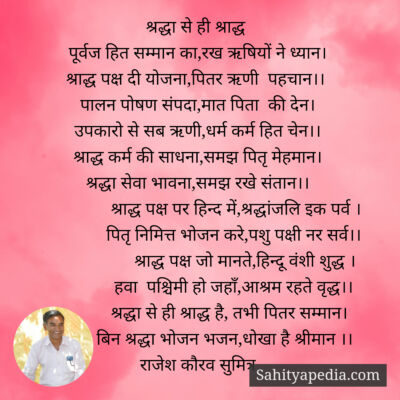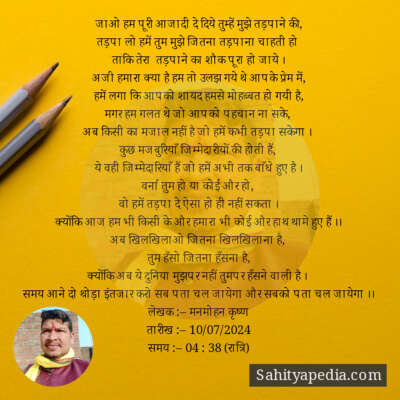पश्चाताप की अग्नि
बन रहे थे तुम उपासक किसलिए..
सह रहे थे कल्प त्रासक किसलिए…
जब वफ़ा की कद्र मैं न कर सका
आंँख में पानी तलक न भर सका।
मैं तुम्हें वीरांगना ही मानता हुंँ
और अपना हर हकीकत जानता हूंँ
जानता हूंँ अपने कृत्य और कर्म को
जानता हूंँ जिंदगी के मर्म को।
जानता हूंँ प्रायश्चित हर पाप का
जानता हूंँ हर सबब संताप का ।
जानता हूंँ था कभी मैं देवता
था तुम्हें देवी की तरहा सेवता।
किंतु मैं भी हूंँ पुरुष अभिशाप हूंँ
भावनाओं में जमा संताप हूंँ।
तुम सती चेतक हृदय से हो सहिष्णु..
और मैं स्नेहिल नयन में पाप हूंँ।
अपराध मुझसे हो गया अब क्या करूंँ…
पश्चाताप के अग्नि में बस जलता रहूंँ..
किंतु इस दाहक ज्वला का मान क्या?
दे सकूंँगा खुद को मैं सम्मान क्या?
प्रश्न है मेरा विचरता चीख में..
कुछ नहीं पाया समय के सीख में।
कौतूहल था पाप निर्मित पल गया था..
मैं वहश कर वहशीपन में जल गया था।
उस ज्वलन की ताप अंतश में समेटे
पीक बहती ज़ख्म पर दीमक लपेटे
मैं चराचर जीव पर अभिशाप बनकर
जा रहा हूंँ बू भरी रक्तों में सनकर।
कर रहा हूंँ कूच स्नेहिल आवरण से
प्रायश्चित करने स्वयं के उर क्षरण से
मैं कभी दीपक था जिसकी बाती तुम थी
आज मैं जीने चला हूंँ दिग मरण से।
मैं किया जो भी उसे तुम भूल जाना
हांँ भले हर स्वप्न में उंगली दिखाना
मैं नहीं काबिल रहा न क्षम्य हूंँ अब
था कभी अवगम्य किंतु गम्य हूंँ अब।।
माफ़ करना मुझको बिन माफ़ी दिए ही।
मैं नहीं काबिल हूंँ कि तुम माफ़ कर दो
बस यही है प्रार्थना गर सुन सको तुम
मुझको आकर दण्ड दो इंसाफ़ कर दो।
दीपक झा रुद्रा