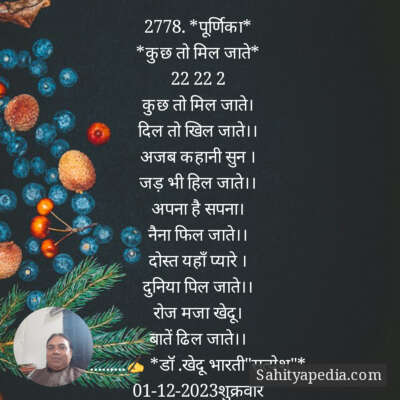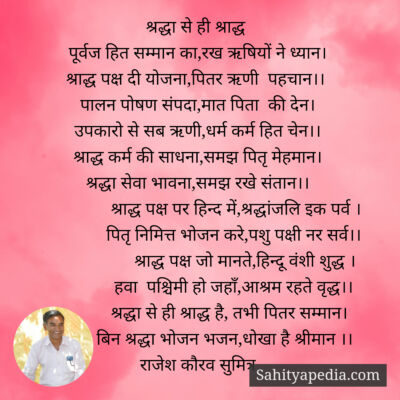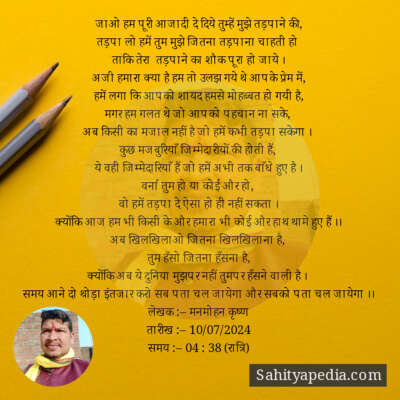ज़िंदगी के माय़ने
न जाने क्यों कभी कोई अजनबी अपना सा लगने लगता है ।
तो कभी-कभी अपना भी बेग़ाना सा नज़र आता है।
कभी-कभी किसी अजनबी शहर की गलियाँ जानी पहचानी सी लगती है।
तो कभी अपने ही शहर की गलियों में हमारी मौज़ूदगी ग़ुम होकर रह जाती हैं।
कभी-कभी ग़ैरों की बेरुख़ी भी हमें उतनी परेश़ान नहीं करती है ।
जितनी अपनों की हम़दर्दी हमें नाग़वार गुजरती है।
जितने स़ितम़ ग़ैरों ने हम पर ढाए हैं ।
उससे ज्यादा फ़रेब हमने अपनों से खाएं हैं।
अब तक इस ब़दग़ुमानी में था कि अपने ही काम आएंगे ।
पर बुरे व़क्त पर ग़ैर ही मेरे काम आए हैं।
शायद मेरी सोच का फ़र्क था या व़क्त का तक़ाज़ा, देर से ही सही ज़िंदगी के क्या माय़ने हैं,
अब समझ आए हैं।