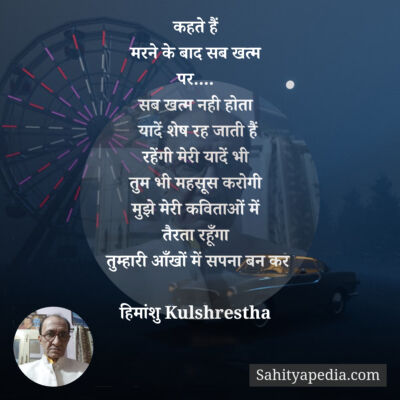ग़ज़ल
नहीं हो बाजुओं में दम वही कायर निकलते हैं।
जिन्हें परवाज़ पर हो नाज़ वो बे-पर निकलते हैं।
रहे भूखे नहीं दो जून की रोटी जुटा पाए
बचा ईमान को अपने यहाँ रहबर निकलते हैं।
इरादों में बुलंदी का जिन्हें अहसास होता है
वही तूफ़ान में कश्ती लिए अक्सर निकलते हैं।
मिटाकर रंज़-ग़म को ज़िंदगी की स्याह रातों से
किया आसान मुश्किल को वही हँसकर निकलते हैं।
दिखाते खौफ़ का आलम दरिंदे देश में घुसकर
लिए बारूद, गोले साथ में खंजर निकलते हैं।
तिरंगा हाथ में लेकर कफ़न बाँधे मुहब्बत का
यहाँ जाँबाज़ सरहद पर कसम खाकर निकलते हैं।
मुहब्बत की फ़िज़ाओं में मिलाके ज़हर क्या होगा
यहाँ साज़िश कुचलते रोज़ बाज़ीगर निकलते हैं।
न जाने ज़िंदगी ‘रजनी’ हमें क्यों आज़माती है
चुनौती को करें स्वीकार हम डटकर निकलते हैं।
डॉ. रजनी अग्रवाल ‘वाग्देवी रत्ना’
महमूरगंज, वाराणसी (उ. प्र.)
संपादिका-साहित्य धरोहर