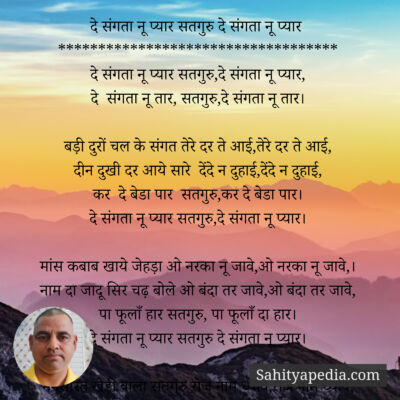ख्वाहिशों में खुद को उलझा के निकलती हूँ
ख्वाहिशों में खुद को उलझा के निकलती हूँ
ज़िंदगी तिरे दर से में मुरझा के निकलती हूँ
होते होते शाम के ये उलझ ही जाती है
रोज़ सवेरे ज़ुल्फ को सुलझा के निकलती हूँ
आज की रात को भी चाहिए रोशनी इसलिए
घर के सारे दीये में बुझा के निकलती हूँ
रक़ीब कोई नहीं सबसे हँस के मिलना है
रोज़ अपने अहम को समझा के निकलती हूँ
फ़िज़ूल की हरकतों से दूर ही रहें इसलिये
बच्चों को उनके काम में उलझा के निकलती हूँ
कोइ और तरीक़ा ढूंढ़ेंगे आज जीने का
रोज़ नया ख़्याल खुद को सुझा के निकलती हूँ
तुमको भी संवारेगी ‘सरु’ जी जान से अपने
घर की दर-ओ-दीवार को समझा के निकलती हूँ