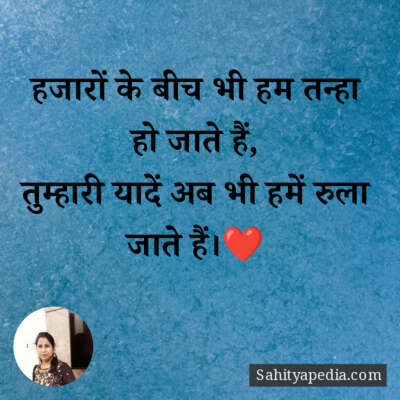काँच और पत्थर

पल्लू में उसके
बंधे रहते हैं
अनगिनत पत्थर,
छोटे-बड़े बेडौल पत्थर
मार देती है किसी को भी
वो ये पत्थर।
उस दिन भी उसके पल्लू में
बंधे हुए थे
ऐसे ही कुछ पत्थर।
कोहराम मचा दिया था
उस दिन उसने
रेलवे-स्टेशन पर।
उन पत्थरों से उसने
अचानक तोड़ दिए थे
चार-पाँच छोटे-बड़े काँच
और फूट गए थे
दो-एक के सिर।
छोड़ो-
जाने दो उसे
‘है वो विक्षिप्त’
कर दिया गया उसे माफ़
यह कहकर,
गुनाह जो उसने किये
आज रेलवे स्टेशन पर।
हट गए थे
उसके रास्ते से
कुछ लोग डरकर,
और कुछ लोग
हँस रहे थे ऐसे
जैसे कोई भैंस रम्भाये
खींसें निपोरकर।
पर नहीं मालूम ये
किसी को भी कि
चुभी हुई है ये काँच
उसके गले में
बनकर एक फाँस,
और चस्पा हैं
अनगिनत सिसकियाँ
अभी भी उसके
विवश, असहाय
घायल मन पर।
काँच से ज्यादा
उसकी फाँस
करती थी घुटन
और होती थी पैदा
इस तरह जो चुभन,
वो जाती थी बाहर
सिसकियों पर चढ़कर।
काँच के टूटने पर
छपाक की आवाज पर
काँच का फ़ैल जाना
बिखरकर,
दे जाता है उसे
दिलासा पल भर।
इसीलिए,
जब वो देखती है
खिड़कियाँ और
उनसे आर-पार
देखने वाले काँच,
तो उसके
पल्लू में समाए पत्थर
बरस पड़ते हैं,
अनायास ही
उस काँच पर-
किसी भी
रेलवे स्टेशन पर।
‘वो है विक्षिप्त’
इसलिए शायद,
लोगों को लगता है एक डर
उसके समीप जाने पर,
और माफ़ कर दिए जाते हैं
अपराध उसके
चाहे वो यदा-कदा
क्यों न फोड़ दे
दो-एक के सिर।
पर वो कैसे माफ़ कर दे?
किसको दे क्षमादान?
उन गुनाहों पर-
जो हुए उसके साथ
चंद रोज़ पहले,
या महीनों या साल पहले
ऐसे ही किसी
रेलवे स्टेशन पर,
जिसकी वजह से वो
कहलाती है आज विक्षिप्त।
क्यों नहीं मचाया था शोर
क्यों नहीं चिल्लाया था ये
क्यों नहीं बोला था ये मूक काँच?
चाहे छोटी सी छनाक ही सही,
तब शायद
उसके पल्लू में
नहीं थे पत्थर, और
वो थी अकेली
किसी रेलवे स्टेशन पर।
(c)@दीपक कुमार श्रीवास्तव “नील पदम्”