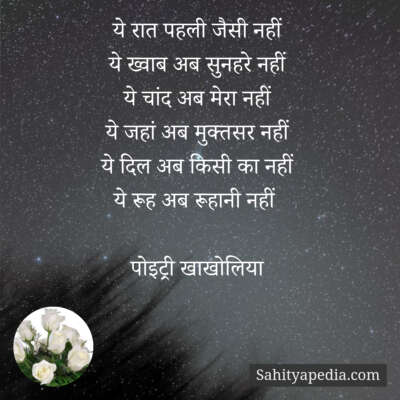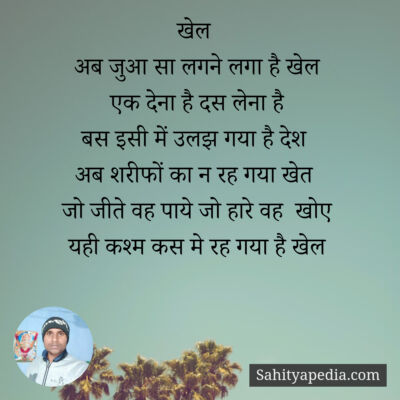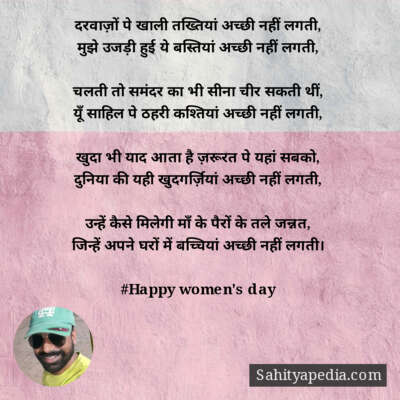इबादत!
बेशक इबादत करने रोज़ हम जाते हैं
फिर भी बेहतर इंसान कहाँ बन पाते हैं
वही रटा रटाया दोहराते हैं रोज़ ही हम
मगर असल मायने कहाँ समझ पाते हैं
रोज़ दुहाई उसी के नाम की देकर हम
उससे ही मोल भाव करने बैठ जाते हैं
दुआ में उठे हाथों का असर कहाँ होगा
जब दिल में नापाक ख़्याल ही आते हैं
खुद से कोई कभी मिला हो देखा नहीं
खुदा से मिलाने के वायदे कर जाते हैं
कई बे-इल्म मज़हबों के पैरोकार यहाँ
मासूमों को ही गुनाहगार बना जाते हैं
अपनी तक़रीरों में जहर उगलने वाले
इंसानियत के हरीफ नफ़रतें फैलाते हैं!












![विचार और रस [ दो ]](https://cdn.sahityapedia.com/images/post/1225a2bc14a5488a66e358ab47e533fe_974d3aa95adcab816b6ca42fbb8ed7f2_400.jpg)