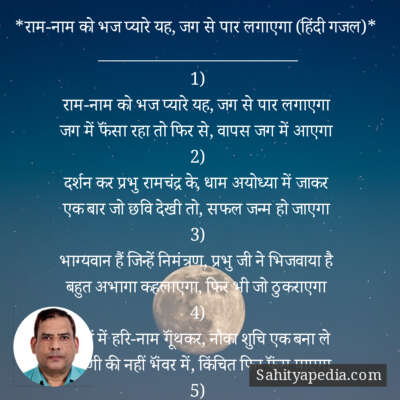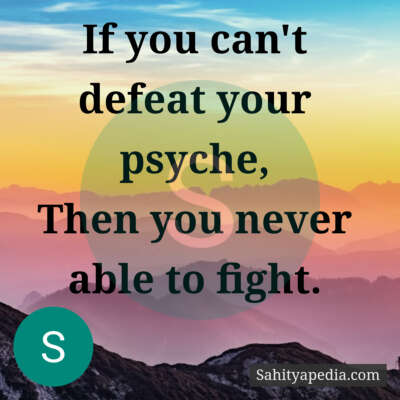अरविंद पासवान की कविताओं में दलित अनुभूति// आनंद प्रवीण

अरविंद पासवान जी का प्रथम काव्य संग्रह ‘मैं रोज लड़ता हूँ’ पिछले डेढ़ वर्षों में कई बार पढ़ा और ठीक से समझने की कोशिश करता रहा। वास्तव में दलित साहित्य को पढ़ना और उसके तह तक समझ पाना कठिन कार्य है, पर मजा भी तो तब ही है जब किसी कठिन कार्य को अन्यों के लिए सरल बना दिया जाए। अरविंद पासवान जी की सारी रचनाएं यही काम करती हैं। उनकी प्रत्येक रचना बड़े ही सहज तरीके से पाठकों से जुड़ कर अपनी बात समझा जाती है। यही कविता की सफलता है और कवि की भी।
‘मैं रोज लड़ता हूँ’ शीर्षक से जो कविता है उसमें कवि ने मोटे तौर पर लड़ाई के तीन स्तर का जिक्र किया है। पहला, स्वयं के भीतर के दो विपरीत भावों के द्वंद्व की लड़ाई है जिसमें कवि ने पाया है कि अक्सर लोभ, ईर्ष्या, घृणा और द्वेष जैसी बुराइयों की ही जीत होती है। इन बुरे मनोभावों के प्रभाव में आकर ही लोग बुरे बनते हैं और अपने ही समाज को कलंकित करते हैं। कवि का मानना है कि भले ही अच्छे मनोभावों की तत्काल हार हो जाए पर बुरे मनोभावों से द्वंद्व जारी रहना चाहिए ताकि हमारी जीवटता बची रहे।
‘ मैं रोज लड़ता हूँ
इसलिए नहीं कि जीतूँ रोज
इसलिए कि लड़ना भूल न जाऊँ।’
दूसरा, समाज में व्याप्त ‘अमानुषिक व्यवस्था’ के खिलाफ। यह अमानुषिक व्यवस्था है जातीय भेदभाव की व्यवस्था, अमीरी- गरीबी की व्यवस्था, रंग और रूप में भेदभाव की व्यवस्था। इस लड़ाई की लंबी शृंखला है। बुद्ध, महावीर से लेकर बाबा साहेब डॉ आंबेडकर तक ने समाज के इस कुरूप चेहरे को खूबसूरत बनाने की कई लड़ाइयाँ लड़ी। यह लड़ाई अभी भी जारी है और आगे भी रहेगी बस हथियार बदलते रहते हैं।
तीसरा स्तर है समाज में प्रेम की स्वीकृति के अभाव के खिलाफ लड़ाई। क़तील शि़फाई अपने एक ग़ज़ल के पहले शेर में लिखते हैं –
‘लिख दिया अपने दर पर किसी ने इस जगह प्यार करना मना है;
प्यार अगर हो भी जाए किसी को, उसका इज़हार करना मना है।’
हमारे सामाज में ऐसी स्थिति से लगभग सारे लोग गुज़रे हैं तो कवि का इस स्थिति से गुजरना कोई नयी बात नहीं है, पर आगे ऐसी स्थिति न आए इसके लिए लड़ने की बात करना नयी बात है। बेहतर समाज बनाने के लिए यह जरूरी है कि हम अपने रूढ़िवादी सोच से मुक्त होकर एक प्रेम पूर्ण समाज का निर्माण करें। इस कविता के जो तीन स्तर हैं सामान्यतः इन्हीं तीनों स्तरों पर संग्रह की अन्य कविताएं भी लिखी गई हैं। इसलिए संग्रह का शीर्षक ‘मैं रोज लड़ता हूँ’ उचित है।
संग्रह की आरंभिक कविताओं में ‘जहाँ मैं पैदा हुआ’ एक गाँव की बनावट को बखूबी दर्शाता है। भारत के प्रत्येक गाँव में टोले- मुहल्ले का निर्माण सामान्यतः जाति के आधार पर हुआ है। शहर भी इससे अछूता नहीं है। पटना शहर में इसके कई उदाहरण मिल जाएंगे – मलाही पकड़ी, दुसाधी पकड़ी, मछुआ टोली आदि। इसीलिए बाबा साहेब डॉ भीमराव अंबेडकर भारतीय गाँव को जातिवाद के जहर का कारखाना कहते थे और शहरों के तीव्र विकास की बात किया करते थे , क्योंकि गाँव की तुलना में शहर जातिवादी जहर से थोड़ा मुक्त है। कविता में सभी जातियों की अपनी विशेषता बताते हुए अंत में कवि कहते हैं-
‘फिर भी टीसता है रह-रह
मन में एक सवाल
कि जहाँ मैं पैदा हुआ
जात ही जी रहे थे
या मनुष्य भी!’
अगर यह सवाल भारतीय गाँव में रह रहे तमाम लोगों से पूछा जाए और वे सभी ईमानदारी से उत्तर दे तो सबका उत्तर एक ही होगा ‘जात ही जी रहे थे।’
‘ताकि अँधेरा कायम रहे’ प्रतिरोध का स्वर है- कमजोर वर्ग के लोगों के ऊपर ताकतवर लोगों द्वारा थोपी जा रही व्यवस्था के खिलाफ।
‘मन मुताबिक अवतार का तिलिस्म गढ़ कर
वे अपनी अमर सत्ता स्थापित करना चाहते हैं
ताकि अँधेरा कायम रहे।’
गौतम बुद्ध को विष्णु के अवतार के रूप में स्थापित करने की कोशिश करना क्या पुरानी व्यवस्था को मजबूत बनाने की कोशिश नहीं है? जिसमें बहुसंख्यक आबादी ज़हालत की जिंदगी जी रहे थे? आज भी उनकी स्थिति सम्मानजनक नहीं है, पर इससे किसी को कुछ फर्क नहीं पड़ता। गाँधी जी ने अछूतों के लिए एक नया शब्द गढ़ा- हरिजन। अछूतों ने तीव्र विरोध किया, बाबा साहेब ने भी इसकी आलोचना की पर फिर भी नाम तो पड़ ही गया। आज यह नाम एक विभत्स गाली से कम नहीं है। यह सही है कि गाँधी जी की ऐसी सोच नहीं रही होगी पर उनके अनुयायियों ने ही इस शब्द को गाली बना दिया और अछूतों पर जबरन थोपा गया।
आजकल जाति के टाइल लगाने से लोग बचते हैं पर उनके भीतर जातिवाद कूट-कूट कर भरा होता है। इसी भाव से प्रेरित एक कविता है ‘फूलमती’। जब फूलमती के नामांकन करवाने के लिए उसके माता-पिता एक सरकारी विद्यालय में जाते हैं तो जातिवादी शिक्षक और उसके पिता की बातचीत की बानगी देखिए-
‘लड़की का नाम?
फूलमती
लड़की के पिता का नाम
हरिचरन
दादा का?
गुरुचरन
परदादा का?
सियाचरन
छड़दादा का?
कलटू मेहतर’
बस बातचीत समाप्त हो गई। यही तो जानना था कि वह किस जाति की है, फिर सीधे तौर पर क्यों नहीं पूछ लेते। शर्म आती होगी शायद या फिर समाज में जो अपना जातिवाद के खिलाफ इमेज बनाया है उसका वास्तविक रूप दिख जाने का भय होगा। पर इससे क्या वास्तविक रूप कभी किसी का छुपा है? हमारे देश के बड़े-बड़े विश्वविद्यालयों में अब तक ऐसे न जाने कितने फूलमती ने जातिवाद का घूंट पिया है और उस जहरीले घूंट को न सह पाने की स्थिति में आत्महत्या भी किया है। यह सिलसिला अभी पूरी तरह खत्म नहीं हुआ है। हैदराबाद विश्वविद्यालय में रोहित वेमुला की आत्महत्या बहुत पुरानी बात नहीं है।
प्रेम का अस्वीकार हमारे सामाज में कई स्तरों पर है। उन्हीं में से एक पर बल्कि दो पर ‘खामोशी’ शीर्षक कविता गढ़ी गई है। एक मुस्लिम लड़की सलमा पड़ोस के ही एक हिंदू और उसमें भी दलित लड़का श्याम से प्रेम कर बैठती है। एक तो अलग धर्म उसमें भी नीच जाति का। जब सलमा के अब्बू को इस प्रेम की भनक लगती है तो पहले वे समझाते हैं-
‘सलमा को बुलाया और कहा:
वह दलित है, अछूत है
बहुत अंतर है उसमें और हममें’
सलमा के नहीं मानने पर उसकी जान ले ली गई, जिसे ऑनर किलिंग कहा जाता है। कविता यहीं खत्म नहीं हो जाती है-
‘श्याम का घर उजाड़ दिया गया
दरिंदगी और हैवानियत की हद पार कर
माँ, पिता और भाई की आँखों के सामने
बीच चौराहे पर
पाश्विकता के नाखूनों से
दबंगों ने
सरेआम
बहन की अस्मत को
नोंचा-खसोटा
माँ की छाती
पिता और भाई के गुप्तांग
घृणा की कुल्हाड़ी से काट कर
मौत की नींद सुला दी
बहन चीखती रही
पुकारती रही
पर लोग अंजान बने रहे
वे सब चर्चा करते रहे:
जाति का मामला है
धर्म का मामला है’
प्रेम जैसा कोमल भाव कैसे इस निकृष्ट स्थिति का कारण बन सकता है? वास्तव में प्रेम इस स्थिति का कारण है भी नहीं। इसका कारण है कमजोर सामाजिक स्थिति, जाति, धर्म और अछूतपन। आज भी कुछ दलित जातियाँ अपने मानव होने का प्रमाणपत्र खोज रही हैं और बाकी जातियाँ अपने शासक होने का प्रमाणपत्र। सबका अपना-अपना स्वार्थ है, अपने-अपने सपने।
‘आखिर
हम किस जहाँ में जीने को मजबूर हैं
जहाँ फूलों के खिलने के मौसम में
फूलों के झरने की खबर मिलती है।’
(‘फूल’ शीर्षक कविता से।)
संग्रह में ‘पेड़’ शीर्षक कविता उन बनावटी वामपंथियों का पर्दाफाश करती है जो यह दंभ भरते हैं कि मजदूरों, किसानों, शोषितों, वंचितों का उद्धार वे ही कर सकते हैं। असल में वे स्वयं अपने उद्धार के लिए वामपंथी बने बैठे हैं ताकि राजनीति में उनका कद बढ़ सके, साहित्यिकों के बीच उनकी इज्जत हो आदि। यह सही भी है कि शोषितों, वंचितों का उद्धार केवल वे ही कर सकते हैं क्योंकि वे ही उनके हिस्से की जमीन पर कुंडली मार कर बैठे हैं, उनके हिस्से की मुस्कान को अपने कब्जे में लेकर स्वयं लाल झंडे के तले मुस्कुरा रहे हैं और राजनीति में अपने कद का गुणगान करवा रहे हैं। ओमप्रकाश वाल्मीकि के शब्दों में- ‘ऐसा नहीं है कि वामपंथियों के यहां दलित नहीं हैं, हैं पर नेता के तौर पर नहीं पिछलग्गू के तौर पर, झंडा ढोने वाले के तौर पर।’
हर तरफ से घेरे इस घनघोर निराशा की स्थिति में भी आशा का दामन थामे रखने की जरूरत है, क्योंकि अब जो सुबह आएगी वह इन्हीं शोषितों, वंचितों के अँधेरे घर को रौशन करेगी।
‘हम लड़े हैं
लड़ेंगे
मरेंगे
पर मिटेंगे नहीं।’
(‘मिटेंगे नहीं’ शीर्षक कविता से।)
आनंद प्रवीण
छात्र, पटना विश्वविद्यालय
सम्पर्क- 6205271834