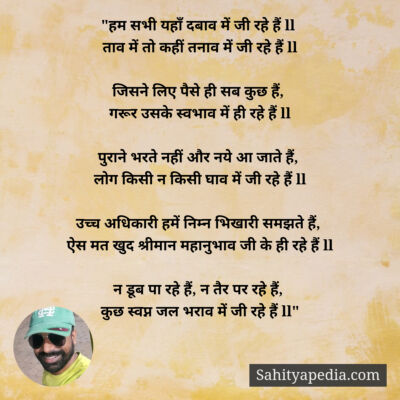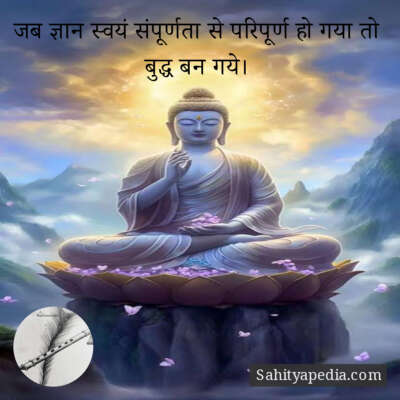डॉ. नामवर सिंह की रसदृष्टि या दृष्टिदोष

‘‘जो केवल अपनी अनुभूति-क्षमता के मिथ्याभिमान के बल पर नयी कविता को समझ लेने तथा समझकर मूल्य-निर्णय का दावा करते हैं, व्यवहार में उनकी अनुभूति की सीमा प्रकट होने के साथ ही यह तथ्य भी स्पष्ट हो जाता है कि काव्य-समीक्षा में सामान्य अनुभूतियों का सहारा लेना भ्रामक है। महाभारत के बाद जिस तरह अर्जुन का गाण्डीव दस्युओं के सम्मुख व्यर्थ हो गया था, उसी प्रकार नयी कविता के समक्ष पुरानी अनुभूतियों से निर्मित सहृदयता को चाहे जितने शब्दों से सुसज्जित किया जाये, किन्तु एक छोटी-सी नयी कविता भी सिद्धांत के गुब्बारे के लिये आलपिन हो जाती है।’’
अपनी पुस्तक-‘कविता के नये प्रतिमान’ के निबंध ‘कविता क्या है’ के अंतर्गत प्रमुख आलोचक डॉ. नामवर सिंह ने उक्त तथ्य मात्र रखे ही नहीं, उन्होंने ‘अज्ञेय’ की ‘सोन-मछरी’ शीर्षक कविता की [‘रस सिद्धांत’ पृष्ठ-56-57] रस-विवेचना की पुनः विवेचना की और लिखा कि-‘‘भाषा-बोध की स्थिति यह है कि हाँफती हुई मछली, थिरकती हुई दिखाई पड़ती है…..ऐसे सिद्धांत [रससिद्धांत] के दायरे में क्या नयी कविता की हालत भी सोन-मछरी की-सी नहीं हो गयी है?’’
इसी पुस्तक के निबंध ‘रस के प्रतिमान की प्रसंगानुकूलता’ के अंतर्गत उन्होंने कविता के नये प्रतिमानों के संदर्भ में रस या रस सिद्धांत से मुक्ति पाते हुए बड़े ही गर्व से कहा कि-‘‘कविता के नये प्रतिमानों की चर्चा के प्रसंग में प्रायः सभी नये लेखक इस बात पर एकमत दिखायी पड़ते हैं कि नये प्रतिमानों का संबंध रस से नहीं हो सकता, क्योंकि कविता से रस का लुप्तीकरण अब विवादास्पद नहीं है।’’
यही नहीं एक गोष्ठी-प्रसंग की चर्चा का इस निबंध में जिक्र करते हुए विजयदेव नारायण साही के चुनौती और व्यंग्य भरे अंदाज में कहे गये इस वक्तव्य को पुनः रसाचार्यों के समक्ष रखा कि-‘‘यह कविता रसीली है, रसाग्रही है, तो हम क्या करें, वह है।’’
डॉ. नामवर सिंह के उक्त कथनों ने जिस तरह आलोचकों को तब चौंकाया होगा, आज भी हम सबको उतना ही चकित और उद्वेलित करते हैं। डॉ. सिंह के उपरोक्त कथन कई ज्वलन्त प्रश्नों को जन्म देते हैं-
1. अगर अनुभूति की क्षमता के आधार पर नयी कविता को जाँचने-परखने का कार्य मिथ्याभिमान है तो क्या इस मिथ्याभिमान के शिकार स्वयं डॉ. नामवर सिंह नहीं है? उन्हें भी तो प्रतिमान के रूप में सामान्य अनुभूतियाँ न सही, अनुभूतियों के नाम पर ‘प्रामणिक और जटिल अनुभूति’ की आवश्यकता पड़ती है। अनुभूति की जटिलता और प्रामाणिकता की ठेकेदारी का दम्भ का आलम भले ही अबाध हो, इस दम्भ को चकनाचूर करने के लिये इसी पुस्तक में उद्धरित श्रीकान्त वर्मा की ‘बुखार’ शीर्षक कविता की यह पंक्तियाँ देखिए-
‘मुझे दुखः नहीं मैं किसी का न हुआ
कि मैंने सारा समय
हरेक का होने की कोशिश की
मेरे साथ
मैंने दगा किया।’
श्रीकांत वर्मा की उक्त कविता में क्या यह दुखः की तीव्रता कथित हृदय से निकली हुई नहीं है? अगर कवि सहृदय न होता तो सारा समय हरेक का होने की कोशिश क्यों करता? ‘हरेक का होने की कोशिश’ सामान्य अनुभूतियों के स्थान पर कौन-सी जटिल और प्रामाणिक अनुभूतियों का अन्तर्जाल है? जिसमें ‘अपने ही साथ दगा करने’ के अपराध-बोध या पश्चाताप को ‘कवि कर्म की परम अभिव्यक्ति’ घोषित किया गया है। ऐसे अपराध-बोध से ग्रस्त कवि यदि कविता के नाम पर पागलपन की हदें पार करने लगे तो कोई आश्चर्य नहीं। श्रीकांत वर्मा की इसी पुस्तक में आलोच्य एक अन्य कविता इसका प्रमाण है-
‘‘मगर खबरदार, मुझे कवि मत कहो
मैं बकता नहीं हूँ कविताएँ
ईजाद करता हूँ गाली
फिर से उसे बुदबुदाता हूँ,
मैं कविताएँ बकता हूँ।’’
[श्रीकांत वर्मा, कविता के नये प्रतिमान पृष्ठ-190]
कवि की इस ‘बुदबुदाहट’ में भले ही गहरा ‘आक्रोश’ अन्तर्निहित है, पर यह नयी कविता है, इसलिए इसकी भावपरक व्याख्या करने का अर्थ बकौल डॉ. नामवर सिंह, मिथ्याभिमान ही होगा। अतः इसके बारे में डॉ. नामवर सिंह क्या कहते हैं, आइए उसे ही समझने का प्रयास करें। इस कविता के बारे में डॉ. सिंह फरमाते हैं-‘‘इसे स्वयं कवि का वक्तव्य न मानकर, कविता के नाम पर ‘मैं’ का ही वक्तव्य मान लिया जाए, तब भी इसकी अति नाटकीयता निश्चित रूप से कविता पर एक धब्बा है।’’
गहरे ‘आक्रोश’ को अतिनाटकीयता कहकर ‘कवि के स्थान पर ‘मैं’ का वक्तव्य’ सुझाकर कुतर्कों के सहारे कोई भी सामान्य अनुभूति किस तरह प्रामाणिक और जटिल हो जाती है और कविता के नाम पर एक धब्बा भी, डॉ. सिंह के उक्त कथन से यह बात आसानी से समझी जा सकती है। लेकिन इस धब्बे को मिटाने के लिये डॉ. नामवर सिंह अपनी आलोचना के डिटरजेंट का इस्तैमाल न करें, भला यह कैसे हो सकता है। इसीलिये वे लिखते हैं कि-‘‘निस्संदेह इस हद की स्वचेतना और आत्मछल को तार-तार करने की ईमानदारी के कारण कविता में अनूठी पारदर्शिता आयी है जो सरल शब्दों के चयन, संक्षिप्त वाक्य-गठन और विरल संरचना में स्पष्ट होती है।’’
अगर इस कविता में स्वचेतना, आत्मछल को तार-तार करने की ईमानदारी, अनूठी पारदर्शिता, विरल संरचना और सरल शब्दों का चयन मौजूद है तो यह कविता, कविता के नाम पर धब्बा कैसे हैं? यदि धब्बा है तो इन सारी खूबियों को गिनाने का औचित्य? इसका सीधा अर्थ तो यही निकलता है कि ‘रिंद के रिंद रहे हाथ से जन्नत न गयी’। ये है डॉ. नामवर सिंह का आलोचना सुकर्म ।
2.‘‘नयी कविता को पुरानी अनुभूतियों से निर्मित ‘सहृदयता’ के सहारे जाँचने-परखने का कार्य कितनी भी युक्तियों से किया जाये, पर यह युक्तियाँ इस प्रकार असफल सिद्ध होंगी, जिस प्रकार महाभारत के बाद दस्युओं के सम्मुख अर्जुन का गाण्डीव व्यर्थ हो गया था।’’
डॉ. नामवर सिंह का यह कथन उनके भीतर छुपे हुए दम्भ को तो प्रकट करता ही है, यह भी सोचने पर विवश करता है कि नयी कविता महाभारत के बाद किसी ऐसे दस्युकर्म का बोध है, जिसमें अर्जुन [सहृदयवादी] के गाण्डीव का व्यर्थ हो जाना है सुनिश्चित है? सहृदयता के बारे में इस तरह की बयानबाजी का अर्थ क्या लगाया जाए? क्या डॉ. साहब इतने हृदयहीन हो गये हैं कि उन्हें दस्युओं की श्रेणी में रखा जाए? सहृदयता को मन के स्थान पर हृदय से जोड़कर जाँचने-परखने के शायद यहीं परिणाम निकलते हैं?
डॉ. नामवर सिंह भले ही इस तथ्य को समझ गये हो कि-‘रस निर्णय अन्ततः अर्थ निर्णय पर निर्भर है,’ लेकिन इस तथ्य की रोशनी में रस को परखने के लिये या उसे नयी कविता के संदर्भ लागू या व्याख्यायित करने का प्रयास बिलकुल नहीं करते। रस के प्रति उनकी यही हृदयहीनता उन्हें यह वक्तव्य देने पर मजबूत करती है कि ‘नये प्रतिमानों का संबंध रस से नहीं है….प्रायः सभी लेखक इस बात पर सहमत है।’’
क्या किसी गलत तथ्य पर सभी लेखकों के एकमत हो जाने से वह तथ्य, सत्य हो जाता है? रस का यदि नये प्रतिमानों से कोई सम्बन्ध नहीं है तो यह भी तय है कि इन प्रतिमानों की संवेदनशीलता मृत या संदिग्ध है, क्योंकि रचनाकर्म की पहली ओर अंतिम शर्त संवेदनशीलता ही है।
3. डॉ. नामवर सिंह का यह कहना कि कविता से रस का लुप्तीकरण अब विवादास्पद नहीं है।’ सोचने पर विवश करता है कि क्या वास्तव में ऐसा है? इस प्रश्न का उत्तर साही की इस चुहलबाजी में अन्तर्निहित है कि-‘कविता रसीली है, रसाग्रही है तो हम क्या करें?’’
रस के प्रतिमान की प्रसंगानुकूलता को खारिज करने का यह दुराग्रहों और ढीठता से भरा हुआ अन्दाज किसी भी समझदार चिन्तक को ‘नासमझी’ के अतिरिक्त कुछ नहीं महसूस होगा। अगर इसी चुनौती और व्यंग्य भरे अंदाज में कोई अन्य यह कहे कि-‘‘ होंगे ये नयी कविता के नये प्रतिमान, जब इनमें रस है ही नही तो इन्हें हम क्यों पढ़ें।’’ इस तरह की बयानबाजी बहरहाल कविता के लिये हर प्रकार हानिकारक ही सिद्ध होगी।
अस्तु, डॉ. नामवर सिंह की रसवादियों से यह शिकायत जायज ही नहीं बेहद सारगर्भित है कि-‘‘माना काव्य में अनुभूति की प्रधानता होती है किन्तु यह काव्यानुभूति यदि गूँगे का गुड़ नहीं है तो उसे विवक्षित करने के लिये शब्दार्थ मीमांसा के बौद्धिक व्यापार के श्रमसाध्य पथ से होकर गुजरना ही पड़ेगा। इसके आत्मपरक व्याख्यता इस कठिन पथ से भय खाते हैं, इसलिए विश्लेषण के औजारों को प्रपंच मानकर अनुभूति के सुकुमार पथों का ही सेवन करना अभीष्ट मानते हैं। यदि यह सुकुमार पथ निजी काव्य-स्वाद तक ही सीमित रहता तो कोई बात न थी। बिडम्बना यह है कि इसी आत्मपरक व्याख्या के द्वारा वे रस को एक सार्वकालिक और सार्वभौमिक काव्य प्रतिमान के रूप में प्रतिष्ठित करने को हौसला रखते हैं। एक ओर मूल्य-निर्णय देने के लिये ऐसा दंभ और दूसरी और अर्थ मीमांसा की पद्यति से नितांत अनभिज्ञता।’’
रस का सम्बंध रागात्मकता, रमणीयता के साथ-साथ भाव, संचारी भाव, अनुभाव और स्थायी भाव से होता है। डॉ. नामवर सिंह के इस कथन को अगर हम सत्य मान लें कि ‘‘रस-निर्णय अन्ततः अर्थ-निर्णय पर निर्भर है।’’ और इसी आधार पर रससिद्धान्त की प्रामाणिकता को सिद्ध करने की कोशिश करें तो यहाँ यह समझ लेना आवश्यक है कि-
[क] विचारों से जन्य ऊर्जा का नाम भाव है। अर्थ यह कि जिस किसी भी वस्तु या काव्य सामग्री से हम जो अर्थ ग्रहण करते हैं, हमारे मन में उसी अर्थ के अनुसार रसात्मकता उद्भाषित होती है। यह तथ्य काव्य के विभावों और आश्रय के साथ-साथ काव्य-सामग्री के आस्वादकों पर भी लागू होता है। सूपनखा का प्रणय निवेदन राम में क्रोधावस्था क्यों जागृत करता है? एक ही काव्यकृति ‘उर्वशी’ पर [कविता के नये प्रतिमान ] रामविलास शर्मा, नैमीचन्द्र जैन, भारत भूषण अग्रवाल, प्रभाकर माचवे और मुक्तिबोध जैसे प्रामाणिक सहृदय आस्वादक एक ही रसबोध के स्थान पर भिन्न-भिन्न रसात्मक दशाओं को क्यों प्राप्त होते हैं, इसका उत्तर रस की अर्थ मीमांसा द्वारा ही सम्भव है।
[ख] संस्कार हमारे वह निर्णीत मूल्य होते हैं, जिनके सहारे हम अपनी रागात्मक दृष्टि का विकास करते हैं, इस नाते कथित सहृदय अर्थात् संवेदनशील मन में सुप्तावस्था में स्थायी भाव नहीं, स्थायी विचार अन्तर्निहित रहते हैं। विचारों का यही निश्चित स्थायित्व हमें निश्चित स्थायी भावों की ओर ले जाता है।
जब तक हम यह निर्णय नहीं कि अमुक व्यक्ति हमारा शत्रु है और हमें किसी भी समय मानसिक और शारीरिक हानि पहुँचा सकता है, तब तक उसके प्रति क्रोध या रौद्रता का क्या औचित्य? ठीक इसी प्रकार जब तक हम यह नहीं विचार लेते कि ‘अमुक व्यक्ति या वस्तु हमें शारीरिक या मानसिक सुख पहुँचाने वाली है,’ तब तक उसके प्रति रमणीयता, रागात्मक और रति का कैसा चरमोत्कर्ष?
[ग] काव्य-सामग्री के आस्वादन के समय आस्वादकों के रसात्मक बोध की दो स्थितियाँ बनती हैं, पहली स्थिति का रसात्मकबोध संवेदनात्मक होता है और दूसरा प्रतिवेदनात्मक। पहली स्थिति में आश्रय लगभग उसी प्रकार के रस-बोध या हर्षादि से सिक्त होता है, जिस प्रकार की रसात्मक स्थिति विभाव की होती है। दूसरी स्थिति में आश्रय विभाव के रसबोध से विपरीत दिशा में रससिक्त होता है। रस की यह सब स्थितियाँ हमारे रागात्मक मूल्यों के अनुसार लिए गये निर्णयों से सम्बद्ध है। ‘रत्नाकर’ के ‘उद्धव शतक’ के शृंगार का संयोग और वियोग पक्ष यदि संवेदनात्मक रसबोध का प्रमाण हैं तो रामचरित मानस में सूपनखा का प्रणय-निवेदन, रस आश्रय राम में क्रोध का संचार करता है, यह रसात्मक बोध का प्रतिवेदनात्मक रूप है।
कविता के नये प्रतिमान के ‘मूल्यों का टकरावः उर्वशी विवाद’ नामक निबंध में रस के ये दोनों संवेदनात्मक और प्रतिवेदनात्मक रूप स्पष्ट देखे जा सकते हैं। अपने विशिष्ट रागात्मक संस्कारों के आधार पर लिये गये निर्णयों में भारत भूषण अग्रवाल यदि संवेदनात्मक रसबोध से सिक्त है तो मुक्तिबोध का रसबोध प्रतिवेदनात्मक है।
रस-सिद्धान का सबसे दुर्भाग्यपूर्ण पक्ष इसी प्रतिवेदनात्मक रसबोध को स्पष्ट न किया जाना है क्योंकि इसे स्पष्ट होते ही ‘साधारणीकरण,’ ‘तादात्म्य’, ‘सहानुभूति’ और कथित ‘रस के ब्रह्मानन्द स्वरूप’ के गुब्बारों में आलपिनें तो चुभेंगी ही, रस को नये सिरे से व्याख्यायित या परिभाषित करने का सवाल भी यक्ष की तरह हम सबके सम्मुख खड़ा हो जाएगा। इसलिये डॉ. नामवर सिंह का यह कहना बेहद सारंगर्भित है कि-‘‘माना काव्य में अनुभूति की प्रधानता होती है, किन्तु यह काव्यानुभूति यदि गूंगे का गुड़ नहीं है तो उसे विवक्षित करने के लिये शब्दार्थ भी मीमांसा के बौद्धिक व्यापार के श्रमसाध्य पथ से होकर गुजरना ही पड़ेगा।’’
सवाल यह है कि क्या डॉ. नामवर सिंह ने ऐसा किया? कविता बनाम नयी कविता के प्रतिमानों को चुन-चुन कर प्रस्तुत करने का व्यापार भले ही बौद्धिक और कथित रूप से जटिल अनुभूतियों का एक सार्वभौमिक और सार्वकालिक कारनामा हो, लेकिन इन प्रतिमानों का संबंध सहृदयता, सामान्य अनुभूति और रस से नहीं , डॉ. नामवर सिंह का यह मानना या मनवाना ही अपने आप में एक बहुत बड़े मिथ्याभिमान का प्रमाण है। उनके इस मिथ्याभिमान को उन्हीं के द्वारा व्याख्यायित कविताओं द्वारा चकनाचूर किया जा सकता है।
पुस्तक-‘कविता के नये प्रतिमान’ के ‘विसंगति और बिडम्बना’ निबंध में व्याख्यारित रघुवीर सहाय की यह पंक्तियां देखिए-
‘‘तुम उसका क्या करती हो मेरी ‘लाडली’
अपनी व्यथा के संकोच से मुक्त होकर
जब मैं तुम्हें प्यार करता हूँ।’’
इस कविता में स्थायी भाव रति मौजूद है। प्रणयात्मकता, प्रेम का घनत्व और रागात्मकता घनीभूत है। प्रेम की यह शुद्ध कविता क्या शृंगार में उद्बोधित नहीं होगी? डॉ. नामवर सिंह इस कविता का विवेचन करते हुये लिखते हैं कि-‘‘छायावादी सखि, सजनि, प्रिये, प्राण, रानी आदि सम्बोधनों के स्थान पर ‘लाडली’ शब्द रखकर रघुवीर सराय ने रूमानी भावुकता को ही नहीं तोड़ा, बल्कि एक मीठी-सी अगम्भीरता के द्वारा प्यार में निहित अकेलेपन की व्यथा को बिजली की कोंध के समान पूरी तीव्रता के साथ उद्भाषित भी कर दिया।’’
छायावादी सखि, सजनि, प्रिये, प्राण, रानी आदि सम्बोधनों के स्थान पर ‘लाडली’ शब्द रख देने भर से रूमानी भाव टूटकर क्या प्रगतिशील भाव बन जाता है? जो नई कविता के प्रतिमानों की चर्चा के प्रसंग में रस से कोई संबंध नहीं रखता? एक मीठी-सी अगम्भीरता के द्वारा प्यार में निहित अकेलेपन की व्यथा का बिजली की कोंध के समान पूरी तीव्रता के साथ उद्भाषित होना अगर रस के अन्तर्गत नहीं आता तो क्या प्रगतिशीलता के अंतर्गत आता है? इसी तरह का एक उदाहरण और प्रस्तुत है-
‘‘जल रहा है
जवान होकर गुलाब
खोलकर होंठ
जैसे आग
गा रहा है फाग।’’
इस कविता में डॉ. नामवर सिंह टटके बिम्ब की ताजगी देखते हुए लिखते हैं कि-‘‘स्पष्टतः इस प्रकार की कविताओं की सीमा है किन्तु भावहीन सपाट वक्तव्यों की अपेक्षा ये भाव चित्र अपने संक्षिप्त रूपाकार में प्रायः एक से अधिक भावों और विचारों की जटिल स्थिति को व्यंजित करता है।’’
डॉ. नामवर सिंह के उक्त विवेचन से इतना तो स्पष्ट है ही यह कविता भावहीन सपाट वक्तव्यों की अपेक्षा अधिक भावों को व्यंजित करती है, तब यह कविता रसात्मकता से रिक्त केसे हो सकती है? इस कविता के भावों को भले ही नामवर सिंह जटिल कहें, लेकिन यह जटिलता कविता में नहीं, उन्हीं के मूल्यांकन में है। इसलिए छायावादी संस्कारों से मुक्त होने की छटपटाहट में रचे गये कविता के नये प्रतिमानों के गाल पर यह कविता रूमानी संस्कारों का जोरदार तमाचा भी है। इस कविता में जब भावों की व्यंजना मौजूद है तो यह कविता रस के सार्वभौमिक, सार्वकालिक प्रतिमान की स्पष्ट और जोरदार उपस्थिति दर्ज करायेगी ही।
पहली कविता में यदि कवि और उसकी प्रेयसि [लाडली] के मन में स्थायी भाव रति का अन्तर्बोध है तो दूसरी कविता में गुलाब के रूप में यौवन का कामदेव स्वरूप है जो कामाग्नि में दहकते हुये फाग के गीत गा रहा है। अतः मानना होगा कि यह दोनों कविताएं रस परम्परा की सहज, सुकोमल और अत्यंत सामान्य अनुभूति से युक्त कविताएं है, जिनमें डॉ. नामवर सिंह जटिलता, विसंगति, बिडम्बना, अहृदयता और न जाने क्या-क्या तलाश करते फिर रहे हैं।
कविता के जिन प्रतिमानों के प्रति डॉ. नामवर सिंह यह घोषणा करते है कि-‘‘ इनसे रस का कोई संबंध नहीं है उनमें रस के प्रतिवेदनात्मक स्वरूप के भी आइये दर्शन करें- रस के प्रतिवेदनात्मक स्वरूप को समझने के लिये आचार्य रामचन्द्र शुक्ल के इस कथन की मार्मिकता को आत्मसात् करना अत्यंत आवश्यक है कि-‘‘ लोक में फैली दुःख की छाया को हटाने में ब्रह्म की आनंदकला जो शक्तिमय स्वरूप घारण करती है, उसकी भीषणता में अद्भुत मनोहरता, कटुता में भी अपूर्व मधुरता, प्रचण्डता में भी गहरी आद्रता साथ लगी रहती है। विरुद्धों का यही सामजस्य कर्मक्षेत्र का सौन्दर्य है, जिसकी और आकर्षित हुये बिना मनुष्य का हृदय नहीं रह सकता।….सौन्दर्य का उद्घाटन असौन्दर्य का आवरण हटाकर ही होता है। धर्म और मंगल की ज्योति, अमंगल की घटा की फाड़ती हुई फूटती है।’’
उक्त कथन के माघ्यम से आचार्य रामचन्द्र शुक्ल रस को मात्र व्यापकता ही प्रदान नहीं करते, रस के सम्बन्ध में ऐसी कई गुत्थियों को भी सुलझा देते हैं, जिन्हें न समझ पाने के कारण अक्सर रसीला और रसाग्रही काव्य ‘रसहीन’ घोषित कर दिया जाता है। लोक में फैली दुःख की छाया निस्संदेह शोषक, साम्राज्यावादी, अहंकारी और व्यक्तिवादी चरित्रों की देन है। ये चरित्र ही लोक को दुःखी याचक और अभावग्रस्त बनाते हैं। इस कारण कवि यदि एक तरफ दुःखी और शोषित वर्ग के प्रति करुणा से आद्र होता है तो दूसरी तरफ इसी करुणा की गति रौद्रता, विरोध और विद्रोह से सिक्त हो उठती है। आताताई व्यवस्था के प्रति कवि में आक्रोश और असंतोष का संचार होने लगता है। इस प्रकार हम पाते हैं कि दुःखी लोक या मानस के प्रति सहानुभूति रखने वाला कवि करुणाद्र होकर अपनी सारी की सारी वैचारिक ऊर्जा को अपचरित्रों के विरूद्ध प्रतिवेदनात्मक रसात्मकता के रूप में विरोध और विद्रोह से सराबोर कर डालता है। कविता का वर्तमान स्वरूप एक तरफ शोषक के भयावह रूप को उजागर करता है तो दूसरी तरफ उसकी अर्थ मीमांसा शोषण विहीन समाज की रसात्मकता में उद्बुद्ध होती है। अतः आचार्य शुक्ल के विचारों की रोशनी में यह रहस्य, रहस्य नहीं रह जाता कि किस प्रकार भीषणता में अद्भुत मनोहरता, कटुता में अपूर्व मधुरता, प्रचण्डता में गहरी आद्रता साथ लगी रहती है।
शोषित के प्रति कवि की करुणामय दृष्टि, शोषक के प्रति किस प्रकार विरोध और विद्रोह को उजागर करती है, इसकी अनुभूति भले ही जटिल हो लेकिन यह रसहीनता की स्थिति नहीं है। यह तो असौन्दर्य का आवरण उठाने का एक सौन्दर्यमय तरीका है, जिसमें धर्म और मंगल की ज्योति, अधर्म और अमंगल की घटा को फोड़ती हुई फूटती है। उदाहरण के लिये इसी पुस्तक की उद्धृरित एक कविता प्रस्तुत है-
‘‘धिक् यह पद-मद, शक्तिमोह! कांग्रेस नेता भी
मुक्त नहीं इससे-कुत्तों से लड़ते कुत्सित
भारतमाता की हड्डी हित! आज राज्य भी
अगर उलट दे जनता, इतर विरोधी दल के
राज इनसे अधिक श्रेष्ठ होंगे-प्रश्नास्पद!
क्योंकि हमारे शोषित शोणित की यह नैतिक
जीर्ण व्याधि है।
डॉ. नामवर सिंह इस कविता के बारे में कहते हैं कि-‘‘सामाजिक भ्रष्टाचार का वर्णन करते हुये ‘पन्तजी’ का यह निष्कर्ष कि इस व्याधि का संबंध हमारे शोषित से है, आकस्मिक नहीं है। सारा विवेक खोकर चरम निराशा में कभी-कभी आम आदमी बोल उठता है कि सारा भ्रष्टाचार तो हमारे खून में है। यही बात ‘पन्त जी’ की कविता की भाषा में है। धिक्कार की मनः स्थिति में स्वभावतः छोटे-छोटे एकाक्षर, द्वयाक्षर शब्दों का प्रयोग किया गया, किन्तु उन्हीं के बीच सहसा प्रश्नास्पद! सामान्यतः भाषा बोलचाल की ही है- यहाँ तक कि कुत्ते भी हैं और हड्डी भी, लेकिन हड्डीहित प्रयोग कैसे? फिर इतर शोणित? भाषा की इतिवृत्तात्मकता की चर्चा छोड़ भी दें तो स्पष्ट है कि परिस्थिति के वर्णन में किसी भी प्रकार की काव्य सुलभ सर्जनात्मकता का प्रयास नहीं है। ‘भ्रष्टाचार हमारे खून में है,’ यह कथ्य जिस स्नायविक स्खलन का सूचक है, अनायास प्रयुक्त निर्जीव भाषा भी उसी मनोदशा को सूचित करती है।’’
सुमित्रानंदन पंत की इस कविता के विवेचन के माध्यम से अगर डॉ. नामवर सिंह को आग्रह और दुराग्रहपूर्वक इस निष्कर्ष पर ही पहुँचना ही है कि-‘‘यह कविता ‘भ्रष्टाचार हमारे खून में है’ कथन के माघ्यम से कवि के सिर्फ स्नायविक स्खलन की सूचना देता है’ तो यह कहना ही पड़ेगा कि यह विवेचन सम्पूर्ण विवेक खोकर चरम निराशा में किया गया है, इसलिये यह कविता के कथ्य का स्नायविक स्खलन नहीं बल्कि आलोचना के स्नायविक स्खलन का सूचक है क्योंकि पंत की इस कविता में भारत माता की दुर्दशा करने वाले भ्रष्ट कांग्रेसी नेताओं के प्रति गहरा ‘आक्रोश’ अन्तर्निहित है, जिसमें वाचिक अनुभावों की सात्विकता ‘धिक्’, ‘कुत्ते’, कुत्सित’ आदि शब्दों के माध्यम से घनीभूत है। आक्रोश का यह केन्द्रीय या स्थायी भाव मात्र कांग्रेसी नेताओं के प्रति ही भीषण, कटु और प्रचंड नहीं है, इसकी व्यंजनात्मक लपटें विपक्षी नेताओं के साथ-साथ उस कथित नैतिक जीर्ण व्याधि को भी जला देने की ओर उन्मुख है, जिसमें ‘भ्रष्टाचार हमारे खून में है’ जैसी मान्यताओं के विषाणु फलीभूत होते हैं। कुल मिलाकर प्रतिवेदनात्मक रसात्मक बोध के रूप में यह कविता कांग्रेसी और विपक्षी नेताओं की कुत्सित मानसिकता के साथ-साथ जन सामान्य के भ्रष्टाचार को सहते रहने की आदत का ‘विरोध’ करती है।
इतनी सारी विशेषताओं के बावजूद अगर डॉ. नामवर सिंह को इस कविता की भाषा या यह कविता निर्जीव लगती है तो यह बताने की आवश्यकता नहीं कि यह निर्जीवता डॉ. नामवर सिंह में है या कविता में? वैसे भी डॉ. नामवर सिंह के लिये यह कविता रसीली या रसाग्रही इसलिये नहीं हो सकती क्योंकि उनके अनुसार कविता से रस का लुप्तीकरण अब विवादास्पद है ही नहीं! लेकिन डॉ. सिंह की इस घोषणा के विपरीत पंत की उपरोक्त कविता में रस के रूप में ‘विरोध’ की स्थापना यदि अनेक विवादों को सम्भावनाओं को जन्म दे सकती है, तो इस संदर्भ में निवेदन यह है कि रस-तालिका पहले भी अपूर्ण थी और आज भी अपूर्ण है। आचार्य भट्टलोल्लट एवं आचार्य भोज रसों की अनन्तता में विश्वास रखते थे। आचार्य भोज ने प्रसिद्ध नवरस के अतिरिक्त प्रेयान्, उदात्त और उद्वत रस का वर्णन अपने ग्रन्थों में किया है। इसलिए रस के रूप में ‘विरोध’ [जिसका स्थायी भाव आक्रोश है] और ‘विद्रोह’ [जिसका स्थायी भाव असंतोष है] क्यों नहीं बढ़ाये जा सकते हैं? सामाजिक भीषणता, कटुता, असमानता, विद्रूपता, शोषण और भेदभाव आदि के प्रति आज की कविता में विरोध और विद्रोह का समावेश जरूरी है। आवश्यकता इसे रस के रूप में जानने-पहचानने और व्याख्यायित करने की है।
डॉ. नामवर सिंह की पुस्तक ‘कविता के नये प्रतिमान’ की ही अगर हम व्याख्यायित कविताओं को देखें तो हम पायेंगे कि इन कविताओं के स्वर सर्वाधिक विरोध और विद्रोह से भरे हुये हैं। गजानन माधव मुक्तिबोध की कविता ‘अंधेरे में’ व्यवस्था की सडाँध भरी भीतर की मोरियों को खोलकर जल की सतह की मलिनता को ही मात्र उजागर नहीं करती, आत्मा के मरे हुये अर्थों से भरी हुई सभ्यता, स्वार्थों की सुख-यात्रा और शोषण की अतिमात्रा का भी ब्यौरा प्रस्तुत करती है। अतः शोषित के प्रति करुणा से आद्र कवि के मस्तिष्क में ऐसे प्रश्नों का कोंधना लाजिमी है-
‘ पुरानी हाय में से किस तरह आग भभकेगी’
डॉ. नामवर सिंह के अुनसार-‘‘यह आग क्रांति है’’। व्यवस्था परिवर्तन के प्रति कवि में गहरा असंतोष और अंतहीन छटपटाहट उसे यह कहने पर मजबूर करती है-
‘ अब अभिव्यक्ति के सारे खतरे उठाने ही होंगे
तोड़ने होंगे ही मठ और गढ़ अब’’।
मुक्तिबोध की उपरोक्त काव्य-पंक्तियों में रस के रूप में ‘विद्रोह’ का अन्तर्बोध घनीभूत है और स्पष्ट है कि यह रसात्मकता स्थायी भाव ‘असंतोष’ के कारण आयी है। लेकिन इन तथ्यों को पकड़े बिना डॉ. नामवर सिंह एक तरफ तो यह कहें कि-‘‘यहाँ अभिव्यक्ति से अभिप्रायः कविता भी है और क्रांति भी’’ और दूसरी तरफ यह घोषणा भी करते हैं कि -‘‘कविता से रस का लुप्तीकरण अब विवादास्पद नहीं है,’ तो सोचने पर विवश होना पड़ता है कि अगर ‘अंधेरे में’ कविता क्रांति का उद्घोष है तो यह क्रांति क्या असंतोष, आक्रोश, विरोध, विक्तोह जैसे संवेग, मनोवेग अर्थात् भावों के योग के बिना सम्भव है? इन सबके योग का ही तो नाम रस है। इसलिये निष्कर्ष यह निकलता है कि रस के प्रति डॉ. नामवर सिंह की दृष्टि दोषपूर्ण तो है ही, उसमें आग्रहों, दुराग्रहों का कालापानी भी उतर आया है। दृष्टि जब ‘कालेपानी’ से ग्रस्त हो तो कविता के प्रश्न को सुलझाने की प्रक्रिया हर प्रकार अधोमुखी हो जाती है।
——————————————————
रमेशराज, 15/109, ईसानगर, निकट-थाना सासनीगेट, अलीगढ़-202001,