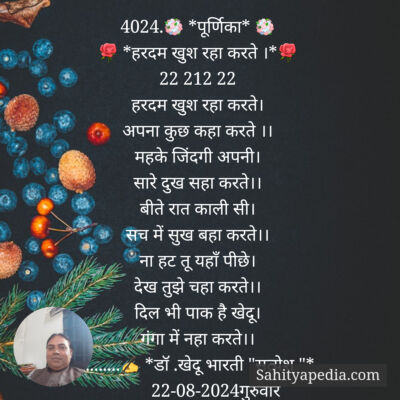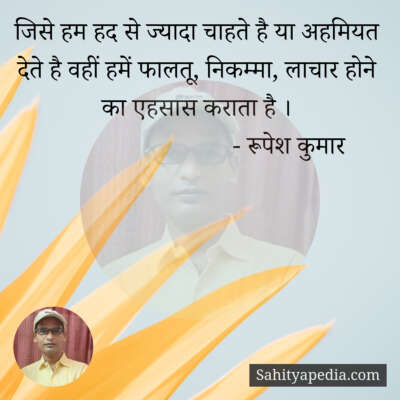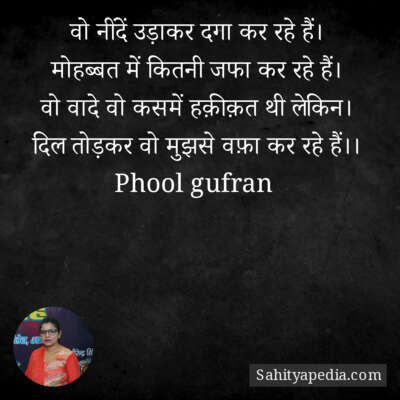■ मेरे अपने संस्मरण

#यादों_का_पिटारा
■ डायनासोर सी लुप्त हुईं “सावन की डोकरियाँ”
◆नई पीढ़ियां अंजान सी◆
◆गाँवों तक सिमटा वजूद◆
【प्रणय प्रभात】
जितना अचरज मुझे और मेरी पूर्ववर्ती पीढ़ियों को डायनासोर की तस्वीर देख कर होता रहा है। उतना ही आश्चर्य शायद मेरे बाद की पीढ़ियों को हो रहा होगा या शायद आने वाले कल में हो। बेहद छोटे मगर ख़ूबसूरत से इस कीट की तस्वीर को देख कर। जो नई पीढ़ियों के लिए लगभग अंजानी सी हैं।
गांवों में बेशक़ इनका वजूद आज भी हो, मगर शहरी क्षेत्र में लुप्त होने की कगार पर है। सुर्ख लाल रंग और विशुद्ध मखमली देह वाला यह एक नन्हा सा जीव है। जिसे देश-दुनिया में तमाम ज्ञात-अज्ञात नामों के बावजूद “सावन की डोकरी” के नाम से जाना जाता रहा। सन 1980 के दशक तक कस्बानुमा श्योपुर के चारों ओर यह बहुतायत में देखी जाती थीं। कच्ची जगहों पर आसानी से दिखाई देने वाले यह कीट खेल के साथ-साथ कौतुहल का विषय भी होते थे।
स्पर्श का आभास होते ही अपने पैरों को समेट लेना इनकी प्रवृत्ति में होता था। ख़ास कर तब जब इन्हें मिट्टी से निकाल कर प्यार से हथेली पर रखा जाता था। मुश्किल से एकाध सेंटीमीटर आकार वाला यह कीट पैर बंद करते ही मखमल के एक छोटे से मोती जैसा दिखाई देने लगता था। ऐसे में बोला जाता था-
“सावन की डोकरी ताला खोल,
नहीं खोले तो चाबी दे।”
कुछ देर में यह कीट अपने सभी पैर बाहर निकाल कर फिर से रेंगने लगता था। हमें लगता था कि यह हमारी मनुहार का असर है।
बिल्कुल “खुल जा सिमसिम” वाली कहानी की तरह। जबकि दोबारा रेंगने की कोशिश यह कीट ख़ुद को सुरक्षित मानने के बाद स्वतः करता था। श्योपुर के विरल आबादी वाले किला क्षेत्र से लेकर पारख जी के बाग़ तक हम इनकी खोज में पहुँचते थे। मामूली सी कोशिश में तमाम “सावन की डोकरियाँ” मिल जाती थीं। कुमेदान के बाग़ और चंबल कॉलोनी में भी। हम माचिस की ख़ाली डिब्बी से लेकर कम्पास (ड्राइंग बॉक्स) तक में भर कर इन्हें घर ले आते। कभी कम्पास बस्ते मैं ही खुल जाता और सब बाहर रेंगती नज़र आने लगतीं। ऐसे में अम्मा (दादी), बुआओं सहित पापा की डांट पड़ती थी। तब इन्हें सकुशल छोड़ कर आने की मजबूरी होती थी। आषाढ़ और श्रावण माह की छुटपुट बारिश में दिखाई देने वाले यह कीट भादों की सतत व तीव्र बरसात में लगभग ग़ायब हो जाते थे।
मुश्किल से एक-डेढ़ माह नज़र आने वाले इन कीटों से हमारा लगाव लगभग एक दशक तक रहा। कस्बे के नगरी में बदलने की प्रक्रिया ने इनकी पैदाइश और परवरिश की जगहों को पहुँच से दूर कर दिया। संभव है कि गाँवों में यह अब भी मिलयी हों। मगर इनको ले कर बाल मन का जो आकर्षण हमारे बचपन मे रहा, वो अब नई पीढ़ी के बच्चों में शायद ही हो। बरसों बाद जानने को मिला कि इनका हिंदी नाम “बीर बहूटी” है। जिसे अंग्रेज़ी में “रेड वेलवेट माइट” के नाम से जाना जाता है। बताते हैं कि प्राचीन काल में इसे इंद्रगोप, इंद्रवधु, बूढ़ी माई भी कहा जाता था। अरबी, फ़ारसी से ले कर तमाम विदेशी भाषाओं में इसके अलग-अलग नाम साबित करते हैं कि इनका बजूद सारी दुनिया में रहा। आयुर्वेदिक और यूनानी चिकित्सा पद्धति में इनके उपयोग की जानकारी अब मिल रही है। जो मानवीय संवेदनाओं के दृष्टिकोण से मानसिकता को कष्ट देने वाली भी है।
माना जा सकता है कि औषधि के रूप में इनके इस्तेमाल ने भी इन्हें लुप्त करने का काम किया है। बहरहाल, अब न पहले जैसी बारिशें बची हैं और ना ही “सावन की डोकरियाँ।” ग्राम्यांचल के मित्रों को दिखें तो वे अपने बच्चों को अवश्य दिखाएं। न दिखें तो इनके बारे में बताएं ताकि वो इन्हें चित्र देख कर तो पहचान ही सकें। साथ ही जीव-दया की पावन भावना के साथ इन्हें व इनके ठिकानों को संरक्षण दे सकें। जो प्रकृति के प्रति मानवीय सरोकार का विषय भी है।
😊😊😊😊😊😊😊😊😊