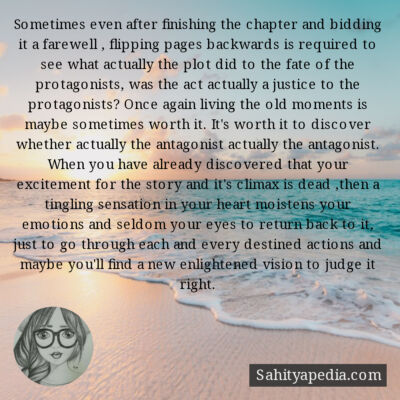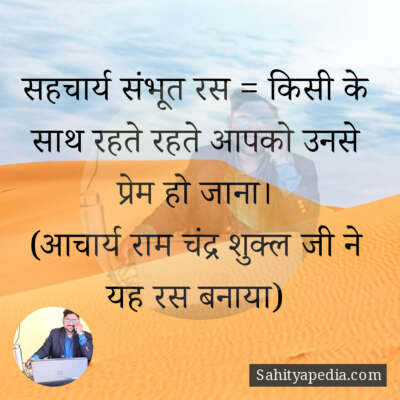ग़ज़ल:- सादगी से अब नही जी पा रहा है आदमी
सादगी से अब नही जी पा रहा है आदमी।
आदमी को आदमी बन खा रहा है आदमी।।
था बुजुर्गों से सुना डायन भी छोड़े एक घर।
साँप बन खुद के सपोले खा रहा है आदमी।।
कल तलक गैरों पे अपना सब लुटाते हम रहे।
अब तो अपनो के लिये तरसा रहा है आदमी।।
वक्त से पहले मिले कब, भाग्य से ज्यादा नही।
क्यों सभी कुछ जान भागा जा रहा है आदमी।।
प्याज़ लहसुन मांस वर्जित, था कभी जो भोज में।
जानवर को गिद्ध जैसा खा रहा है आदमी।
आधुनिकता की ललक में, सब मिटा डाले शज़र।
काट जंगल राज जंगल ला रहा है आदमी।।
अब मशीनों के बिना चल भी न पाये इक़ कदम।
खुद बजूद अपना मिटाता जा रहा है आदमी।।
इस चकाचौंधी के युग में, ग़ैरों को अपना बना।
अपनो से ही दूर खुद को पा रहा है आदमी।।
खो गई इंसानियत अब तो, हर कहीं तांडव मचा।
लोगों को मच्छर समझ निपटा रहा है आदमी।।
चार काँधे अब नही श्मशान जाने के लिए।
अपनी खुद की लाश को ले जा रहा है आदमी।
अब तो लिखना बंद कर, हैं आदमी अपने सभी।
देख शोहरत ‘कल्प’ अब, मुरझा रहा है आदमी।।
✍?? अरविंद राजपूत कल्प?✍?
बह्र- रमल मुसम्मन महज़ूफ़
वज़्न:- फाएलातुन फाएलातुन फाएलातुन फाएलुन
2122. 2122. 2122. 212