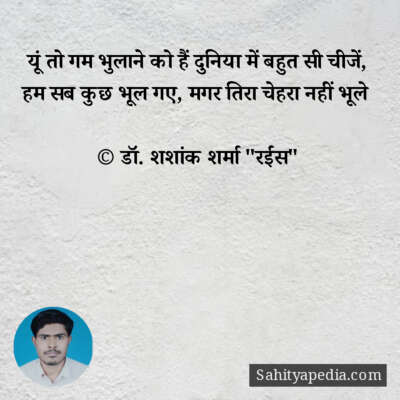हिंदी दलित साहित्यालोचना के एक प्रमुख स्तंभ थे डा. तेज सिंह / MUSAFIR BAITHA

यह हमारे लिए काफी क्लेषदायक है कि हिंदी साहित्य में स्वीकृति एवं चर्चा के मामले में अंडरटोन रह गए दलित साहित्य आलोचना एवं विमर्श के एक प्रमुख स्तंभ रहे डा. तेज सिंह अब स्मृतिशेष हैं। असमय ही उनकी हृदय गति रुक गयी, जबकि दलित साहित्य की बेहतरी के लिए उन्हें अब भी काफी चलना था, बहुत कुछ करना बाकी था। 65 के आसपास की उम्र में ही उनका चला जाना उनकी रचनात्मक एवं चिंतनपरक व अन्यान्य दाय से साहित्य-जगत का बहुत अधिक ही वंचित रह जाना है!
जहाँ 17 नवंबर 2013 को ‘जूठन’ जैसी रचना से यश-अमर हुए ओमप्रकाश वाल्मीकि ने देहरादून में अंतिम सांस ली वहीँ, दिल्ली के रहवासी दलित साहित्य के मान्य आलोचक एवं दलित साहित्य की ‘अपेक्षा’ नामक त्रैमासिक पत्रिका के यशस्वी संपादक डा. तेज सिंह भी इस बीच 15 जुलाई 2014 को हमारे बीच नहीं रहे. यह अजीब संयोग है कि ‘अपेक्षा’ का उनके संपादन में आया संयुक्तांक 46-47 (जनवरी-जून 2014) ओमप्रकाश वाल्मीकि की मृत्यु के बाद का पहला अंक है जिसमें वाल्मीकि पर विशेष सामग्री है. और, दुखद यह कि अंक डा. तेज सिंह के संपादन का आखिरी एवं ऐतिहासिक अंक साबित हुआ है. इस अंक में 12 पृष्ठों का हमेशा की तरह लंबा सम्पादकीय है, पर इस बार खास बात यह है कि इसकी पूरी अंतर्वस्तु ओमप्रकाश वाल्मीकि के व्यक्तित्व एवं कृतित्व पर है और आश्चर्यजनक रूप से घोर नकारात्मक है. डा. तेज सिंह की ‘ओमप्रकाश वाल्मीकि की रचना-प्रक्रिया’ शीर्षक इस सम्पादकीय की शुरुआत वाल्मीकि की मृत्यु की सूचना से होती है और अंत श्रद्धांजलि से. सम्पादकीय बड़ा ही विस्फोटक है. पक्षपातपूर्ण एवं आक्षेपात्मक है. वाल्मीकि के व्यक्तित्व एवं कृतित्व को ख़ारिज करने में डा. तेज सिंह यहाँ इतने आक्रामक एवं आक्रोशित जान पड़ते हैं कि सहसा विश्वास नहीं होता कि ये वहीं मृदुभाषी एवं हरदम अपने होठों पर मधुर मुस्कान रखने वाले शख्स हैं. दलित साहित्य के कुछ धारणात्मक एवं अन्य प्रश्नों पर इन दोनों के आपसी मतभेद इस स्तर तक कटु हो चले थे, संभवतः दलित साहित्य के पाठकों को इसका भान नहीं रहा होगा. कोई गैरदलित अथवा जानी दुश्मन भी क्या इस टक्कर का वाल्मीकि-विरोध अंकित कर सकेगा? अफ़सोस के साथ कहना पड़ता है कि डा. तेज सिंह यहाँ काफी भीरू साबित होते हैं. कारण कि जब वाल्मीकि किसी प्रत्युत्तर अथवा सफाई देने के लिए जीवित नहीं है, तो तेज सिंह ने अपनी भड़ास निकालने का कदाचित इसे सुअवसर माना! ओमप्रकाश वाल्मीकि एवं डा. तेज सिंह के पाठकों एवं चाहने वालों, उभय व्यक्तियों के प्रशंसकों एवं आलोचकों तथा हिंदी दलित साहित्य पर नजर रखने वालों के लिए तो यह भी अब अवसर नहीं रहा कि वे इन दोनों में से किसी से इस भिड़ंत की बाबत कोई सवाल-जवाब कर सके, स्पष्टीकरण ले सके. डा. तेज सिंह ने वाल्मीकि के व्यवहार कुशलता की तो काफी कुछ प्रशंसा अपने इस सम्पादकीय में शुरू में कर दी है पर उनके रचनात्मक अवदान के प्रशंसा-पक्ष में एक भी शब्द नहीं खरचा है, एवं उन्हें ख़ारिज करने में बेहद हमलावर हो आलोचनाओं की झड़ी लगा दी है.
डा. तेज सिंह ने वाल्मीकि को ‘दलित’ शब्द के इतिहास का ज्ञान न होने से लेकर उनके भाजपाई एवं संघी होने जैसे आरोप भी मढे हैं एवं अपने तरीके से उन्हें हिन्दुत्ववादी एवं जातिवादी तक साबित कर दिखाया है! उनका आरोप अन्यान्य रूपों के अलावा इन शब्दों में भी आता है – “वाल्मीकि भाजपा या आर.एस.एस. से अपने राजनीतिक संबंधों को जीवन भर छुपाते रहे लेकिन उनकी मृत्यु के बाद हुए कर्मकांड ने जाहिर कर दिया है.”1 इसी सम्पादकीय में एक जगह तेज सिंह यों टिप्पणी करते हैं – “क्या खुद वाल्मीकि जातिवादी चेतना के ब्राह्मणवादी संस्कारों से मुक्त हो पाए थे? ‘बैल की खाल’, ‘सलाम’, ‘बपतिस्मा’ और ‘अम्मा’ आदि कहानियों में वाल्मीकि के ब्राह्मणवादी संस्कारों की एक झलक मिल जाएगी.” 2 हालांकि अंक में वाल्मीकि पर जो अन्य सामग्रियां दी गयी हैं वे डा. तेज सिंह के सम्पादकीय की तरह विद्वेषपूर्ण न होकर संतुलित विचार रखती प्रतीत होती हैं. यानी पत्रिका की अन्य सामग्रियों के चयन में तेज सिंह ने ओमप्रकाश वाल्मीकि को महज ख़ारिज करने वाली ही चीजें रखने की कोशिश न कर अपने मान की बात कहने दी है, वाल्मीकि की प्रशंसा करते विचारों को भी आने दिया है. यहाँ एक और बात ध्यान देने योग्य है कि जहां ‘दलित साहित्य अथवा साहित्यकार’ शब्द को डा. तेज सिंह ‘अम्बेडकरवादी साहित्य अथवा साहित्यकार’ पद से प्रतिस्थापित करने के पैरोकार रहे हैं, अंक की वाल्मीकि से अलग विषय की सामग्री में भी दलित साहित्य अथवा साहित्यकार जैसे शब्दों से ही काम चलाया गया है. इससे आभास होता है कि ‘अपेक्षा’ के उक्त अंक लेखक भी डा. तेज सिंह की अपनी अम्बेडकरी-जिद्द के साथ होते नहीं दीखते! अबतक का कुल जमा हासिल यही है कि डा. तेज सिंह ‘दलित सहित’ की धारणा को ‘अम्बेडकरवादी’ साहित्य में घटाने अथवा तब्दील करने में नाकाम ही रहे. ‘आत्मकथा’ शब्द को ‘आत्मकथन’ अथवा ‘आत्मवृत्त’ कहने के अपने अभियान को भी डा. तेज सिंह सफल नहीं बना सके. दरअसल, डा. तेज सिंह की ये ‘मौलिक’ धारणाएं उसी तरह स्वीकृति नहीं पा सकीं जैसे कि अभी ‘ओबीसी साहित्य’ की टटका एवं अलबेली धारणा अस्तित्व पाने के लिए संघर्षरत होकर भी उत्तरोत्तर प्राणहीन एवं बेअसर होती जा रही है. प्रसंगवश, डा. तेज सिंह की इन धारणाओं का सबसे मुखर एवं असरदार विरोध किसी गैर दलित हलके से नहीं बल्कि ओमप्रकाश वाल्मीकि की तरफ से आया था. वाल्मीकि कहते हैं – “ हिंदी दलित साहित्य में कुछ ऐसी बहस करते रहने की परंपरा विकसित की जा रही है जिसका कोई औचित्य नहीं रह गया है। ये बहसें मराठी दलित साहित्य में खत्म हो चुकी हैं। लेकिन हिंदी में इसे फिर नए सिरे से उठाया जा रहा है। वह भी मराठी के उन दलित रचनाकारों के संदर्भ से, जो मराठी में अप्रासंगिक हो चुके हैं। जिनकी मान्यताओं को मराठी दलित साहित्य में स्वीकार नहीं किया गया, उन्हें हिंदी में उठाने की जद्दोजहद जारी है। मसलन ‘दलित’ शब्द को लेकर, ‘आत्मकथा’ को लेकर। मराठी के ज्यादातर चर्चित आत्मकथाकार, रचनाकार ‘दलित’, शब्द को आंदोलन से उपजा क्रांतिबोधक शब्द मानते हैं। बाबूराव बागुल, दया पवार, नामदेव ढसाल, शरणकुमार लिंबाले, लोकनाथ यशवंत, गंगाधर पानतावणे, वामनराव निंबालकर, अर्जुन डांगले, राजा ढाले आदि। इसी तरह आत्मकथा के लिए ‘आत्मकथा’ शब्द की ही पैरवी करनेवालों में वे सभी हैं जिनकी आत्मकथाओं ने साहित्य में एक स्थान निर्मित किया है। चाहे शरणकुमार लिंबाले (अक्करमाशी), दयापवार (बलूत), बेबी कांबले (आमच्या जीवन), लक्ष्मण माने (उपरा), लक्ष्मण गायकवाड़ (उचल्या), शांताबाई कांबले (माझी जन्माची चित्रकथा), प्र.ई. सोनकांबले (आठवणीचे पक्षी), ये वे आत्मकथाएँ हैं जिन्होंने दलित आंदोलन को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निर्मित की। इन आत्मकथाकारों को ‘आत्मकथा’ शब्द से कोई दिक्कत नहीं है। लेखकों को कोई परेशानी नही हैं। यही स्थिति हिंदी में भी है। लेकिन हिंदी में ‘अपेक्षा’ पत्रिका के संपादक डा. तेज सिंह को ‘दलित’ शब्द और ‘आत्मकथा’ दोनों शब्दों से एतराज है। उपरोक्त संपादक को दलित आत्मकथाओं में वर्णित प्रसंग भी काल्पनिक लगते हैं। कभी-कभी तो लगता है कि ये संपादक महोदय दलित जीवन से परिचित हैं भी या नहीं? क्योंकि दलित आत्मकथाओं में वर्णित दुख-दर्द, जीवन की विषमताएँ, जातिगत दुराग्रह, उत्पीड़न की पराकाष्ठा, इन महाशय को कल्पनाजन्य लगती है.”3
ऐसा भी नहीं है कि वाल्मीकि की आलोचना नहीं हो सकती. वे एकदम से पाक-धवल नहीं हो सकते, दुनिया में कोई नहीं हो सकता ऐसा. मगर मूल्यांकन का एक तरीका होता है. डा. तेज सिंह ने तो यहाँ बिलकुल डा. धर्मवीर की ही ध्वंसात्मक लाइन पकड़ ली लगती है. हमें पता है कि स्त्री विरोध, प्रेमचंद पर हमले एवं कबीर के द्विज आलोचकों पर एकतरफा प्रहार करके कैसे डा. धर्मवीर ने अपने शोध, श्रम एवं महत्त्व को खुद ही चोट पहुंचाई. धर्मवीर के कबीर पर बड़े काम को भी द्विज हलके में कोई नामलेवा नहीं है, उनकी मोटी आत्मकथा ‘मेरी पत्नी और भेडिये’ को दलित साहित्य में भी बहुत मान-महत्त्व नहीं दिया जाता है तो कारण है उनका अतिरेकी चिंतन, गुड़ को भी गोबर की लपेट से उपेक्षणीय सा बना देना. कबीर एवं प्रेमचंद को दुनिया के सामने प्रस्तुत किये जाने की जिस द्विज-भित्ति पर डा. धर्मवीर ने अपना शोध-कार्य एवं अपनी आलोचना को टिकाया है उसमें प्रेमचंद एवं कबीर पर द्विज आलोचना को सिरे से खारिज करते उनका चलना गलत रास्ते पर चलना है. हाँ, द्विज आलोचकों एवं साहित्यिकों द्वारा डा. धर्मवीर के कबीर संबंधी एवं अन्य आलोचनात्मक कार्यों को महत्व न देना भी कम बड़ा अपराध नहीं है और वह भी बराबर की प्रतिक्रियात्मक कार्रवाई मात्र है. डा. धर्मवीर के लेखन से काफी कुछ काम का बीना जा सकता है. ‘बीसवीं सदी की हिंदी आलोचना’ नामक अपने लेख4 में बिहार मूल के हिंदी आलोचक रेवतीरमण ने 20 वीं सदी के अंत में क्रियाशील आलोचकों का जो जिक्र किया है वहाँ डा. धर्मवीर जैसा जरूरी नाम गायब है. रेवतीरमण जब कहते हैं कि “कबीर से बड़ा आलोचक अभी तक नहीं हुआ है”5, तो बिलकुल सही होते हैं. लेकिन, मुझे यहाँ जोड़ना यह है कि कबीर पर डा. धर्मवीर के आलोचनात्मक कार्य में द्विज आलोचकों के प्रति चाहे पूर्वग्रह भी हैं पर कबीर का डा. धर्मवीर से बड़ा आलोचक अभी तक नहीं हुआ है. कबीर पर डा. कबीर का काम बहुत बड़ा है और सर्वथा मौलिक है. यह भी कि, कबीर के द्विज आलोचकों हजारी प्रसाद द्विवेदी, डा. रामकुमार वर्मा, डा. मैनेजर पाण्डेय, डा. शुकदेव सिंह, डा. पुरुषोत्तम अग्रवाल से उन्होंने जो लट्ठम-लट्ठा किया है वह एकदम से एकतरफा भी नहीं है, दम है उसमें. डा. धर्मवीर की कबीर श्रृंखला की आलोचना पुस्तकें सन 2000 कि शुरुआत में ही आनी शुरू हो गयी थी, वह भी हिंदी के एक बड़े प्रकाशन, वाणी प्रकाशन से. और इससे पहले उनके डा. तेज सिंह से भी वाल्मीकि के प्रति दुराग्रह पालने की भयावह चूक हो गयी है. निश्चय ही वाल्मीकि पर अपनी तोहमतों की इस बौछार के साथ ही तेज सिंह भी तो इस दुनिया से प्रयाण तो नहीं ही करना चाहते रहे होंगे. यदि उनकी मौत अचानक से नहीं होती तो शायद, कभी न कभी अपने इस एकतरफा एवं पक्षपाती अवमूल्यांकन के लिए वे साहित्य जगत एवं वाल्मीकि के समक्ष अपनी खेद, अपनी झेंप प्रकट जरूर करते!
डा तेज सिंह की कलम से वाल्मीकि की मार्क्सवाद की कच्ची-पक्की समझ पर एक रोचक टिप्पणी हम उनके आलेख ‘मार्क्सवाद और दलित साहित्य’ में देखते हैं. वे अनेक दलित साहित्यकार एवं कवि को अम्बेडकरवाद, मार्क्सवाद एवं समाजवाद की कच्ची समझ का साबित करते हुए किंचित ओमप्रकाश वाल्मीकि को भी इस मोर्चे पर घेरते हुए दीखते हैं, मगर कुछ सावधानी बरतते हुए इस तरह, “…दलित साहित्यकार ओमप्रकाश वाल्मीकि भी मार्क्सवादियों की सामाजिक क्रान्ति के नारे को सिर्फ दिखावा मानकर आलोचना करते हैं कि ‘ऊंची-ऊंची अट्टालिकाओं के कहकहे/सफेदपोश नेताओं के भाषण/चौराहे पर गांधी का पुतला/गलियों में/समाजवाद का नारा/मेरा मन बहला रहा है.’ (सदियों का संताप) क्योंकि देश के कम्युनिस्ट सत्तर-अस्सी सालों से समाजवादी क्रान्ति का नारा बुलंद किये जा रहे हैं पर सैकड़ों पार्टियों में बंटा वामपंथी आन्दोलन बिखराव के कगार पर खड़ा है और अपना जनाधार लगातार खोता चला जा रहा है. लेकिन अपने अगले कविता-संग्रह ‘बस्स! बहुत हो चुका’ में ओमप्रकाश वाल्मीकि मार्क्सवादियों को सकारात्मक नज़रों से देखते हैं. जैसा कि लेख के शुरू में डा. अम्बेडकर को उद्धृत करते हुए लिखा कि ‘हिंदू मार्क्सवाद के वर्ग-संघर्ष से बहुत भयभीत रहता है और सबसे ज्यादा विरोध भी वही करता है.’ इसलिए वर्णवादी हिंदू सोवियत संघ के विघटन पर बहुत खुश नजर आता है. उसी सच्चाई की ओर ओमप्रकाश वाल्मीकि इशारा करते हैं कि ‘वर्ण-व्यवस्था को तुम कहते हो आदर्श/खुश हो जाते हो/साम्यवाद की हर पर/जब टूटता है रूस/तो तुम्हारा सीना छत्तीस हो जाता है/क्योंकि मार्क्सवादियों ने/छिनाल बना दिया है/तुम्हारी संस्कृति को.’ (कभी सोचा है)
एक प्रसंग हम प्रेमचंद विरोध का लें, जिससे ओमप्रकाश वाल्मीकि भी प्रकट रूप से जुड़ते हैं. तेज सिंह ‘प्रेमचंद के दलित’6 नामक अपने लेख में कहते हैं कि प्रेमचंद ने ब्राह्मण एवं चमार को एक दूसरे के पक्के विरोधी यानी जानी दुश्मन के रूप में आमने-सामने रखकर विकसित किया है. इसलिए इन दोनों समुदाय के लोगों ने प्रेमचंद पर गंभीर आरोप लगाए हैं कि उन्होंने उनको बुरी नीयत और गलत तरीके से अपने साहित्य में चित्रित किया है. डॉ. तेज सिंह कहते हैं, “यह सब प्रेमचंद के समय में ही उनके सामने शुरू हो गया था. प्रेमचंद ने खुद इस संबंध में कई जगह पर लिखा है.”7 डा. तेज सिंह आगे लिखते हैं जिसमें वाल्मीकि का जिक्र यों आता है, “डा. विमलकीर्ति ने अक्टूबर 1993 में नागपुर शहर में ‘अखिल भारतीय हिंदी दलित लेखक साहित्य-सम्मलेन’ का आयोजन करके दलित लेखकों को विचार-विमर्श का अच्छा अवसर दिया. इस अवसर का लाभ उठाते हुए ओमप्रकाश वाल्मीकि ने खूब सोच-समझकर अपना पहला निशाना प्रेमचंद पर ही साधा और उनकी प्रसिद्ध कहानी ‘कफ़न’ को दलित विरोधी सिद्ध करके गैरदलित साहित्य पर भी अनेक सवाल दागे. इन सवालों पर सबसे तीखी प्रतिक्रिया ‘समकालीन जनमत’ पत्रिका में हुई. ओमप्रकाश वाल्मीकि का आरोप था कि प्रेमचंद ने ‘कफ़न’ कहानी च (चमार) को बदनाम करने के लिए ही लिखी है.” छद्म प्रहार करते डा. तेज सिंह आगे वाल्मीकि पर सीधा निशाना लगाने का मौका भी यूँ ढूंढते हैं, “यह अलग बात है कि प्रेमचंद पर ऐसा आरोप लगाने वाले खुद ओमप्रकाश वाल्मीकि आज च को बदनाम करने वाली ‘शवयात्रा’ जैसी दलित विरोधी कहानी लिख रहे हैं.”8
डा. तेज सिंह ‘शवयात्रा’ पर शुरू से ही अपने आलोचनात्मक स्टैंड पर खड़े रहे हैं. यह बात और है कि इधर वे इस कहानी की सीधे मजम्मत पर ही तूल गए थे. ‘दलित कथा साहित्य का एक वर्ष और बीत गया’ नामक आलेख9 में वे आज से कोई 24 वर्ष पहले ही लिखते हैं कि “ओमप्रकाश वाल्मीकि की ‘शवयात्रा’ (इण्डिया टुडे, 22 जुलाई, 1998) दलित लेखकों में सर्वाधिक चर्चित और विवादास्पद कहानी रही है. ओमप्रकाश वाल्मीकि ने कई वर्ष पहले प्रेमचंद की ‘कफ़न’ कहानी को दलित विरोधी कहकर कटु आलोचना की थी और वे रातों-रात हिंदी साहित्य में चर्चित हो गए. जिस साहित्यिक मानदंड के आधार पर यानी दलित चेतना के आधार पर उन्होंने ‘कफ़न’ को दलित विरोधी कहानी कहा था, क्या उसी मानदंड के आधार पर ‘शवयात्रा’ को दलित चेतना विरोधी कहानी नहीं ठहराया जा सकता है? निश्चित ही यह दलित चेतना विरोधी कहानी मानी जानी चाहिए, क्योंकि वाल्मीकि जी ने इस कहानी की शुरुआत नकारात्मक दृष्टिकोण से की है. मानो अछूतों में अछूत बल्हार जाति का कल्लन ही चमारों का सबसे बड़ा दुश्मन है.” डा. तेज सिंह यहाँ सही प्रतीत होते हैं, और, आगे अपनी शिकायत को इन तर्कों से बलित करते हैं, “यह सही है कि दलित जातिओं में भी जातिगत भेदभाव व्याप्त है पर यह समाज का मुख्य अंतर्विरोध नहीं है बल्कि गौण है, जिसे सामाजिक परिवर्तन की प्रक्रिया में धीरे-धीरे खत्म किया जा सकता है. दलित जातियों का मुख्य दुश्मन उसके अपने समुदाय के लोग नहीं बल्कि ब्राह्मणवाद और सामंतवाद है जिसके खिलाफ ओमप्रकाश वाल्मीकि सहित सभी दलित साहित्यकार एकजुट होकर लड़ रहे हैं.” यहाँ कहानी पर डा. तेज सिंह के मत से अलग एक द्विज टिप्पणी को लेना भी आलोचना के गैर-द्विज ऐंगल से जरूरी साक्षात्कार होना चाहिए. इस आसंग में ‘हिंदी साहित्य में दलित दावे और जनवादी अपेक्षाएं’ नामक लेख में डा. पी. एन. सिंह का रवैया देखें, “…ओमप्रकाश वाल्मीकि की कहानी ‘शवयात्रा’ ने दलित बुद्धिजीवियों को अपनी वास्तविकता से साक्षात्कार कराया है. यह कहानी बताती है कि यांत्रिक अनुभूतियों के स्तर पर भी अपने-अपने दायरों में विवश हैं, विभाजित हैं, संकीर्ण हैं.”10
दलित साहित्यकार का आपसी सिर-फुटौव्वल काफी विचलित करने वाला एवं चिंतनीय है. जयप्रकाश कर्दम ने वर्ष 2012 में जोहान्सबर्ग (दक्षिण अफ्रिका) में हुए विश्व हिंदी सम्मलेन में दलित लेखक डा. श्योराज सिंह बेचैन द्वारा जहाँ-तहां लिख-बोलकर उनपर उपेक्षा का इल्जाम लगाने की बाबत अपना मत रखते हुए अपनी निराशा एवं अपना कंसर्न वृहतर सन्दर्भों में यूँ आक्रोशमय अभिव्यक्ति की है, “….आज कई स्थापित दलित रचनाकार सार्थक लेखन से कहीं अधिक रुचि एक-दूसरे पर कीचड़ उछलने और नीचा दिखाने में ले रहे हैं या कहिये, एक-दूसरे पर लांछन लगा रहे हैं. यह दलित साहित्य में लांछनवाद का प्रतिवादन या नई धारा का उदय है.” 11
अब डा. तेज सिंह से निजी परिचय एवं बातचीत पर कुछ टिप्पणियाँ. उनसे मेरा प्रथम परिचय कोई दस वर्ष पुराना है, वह भी महज खतोकिताबत की मार्फ़त, आमने-सामने की मुलाकात से नहीं. और, यह परिचय बहुत सहज भी नहीं रहा! बल्कि कहें तो अजीबोगरीब रहा. हुआ यों कि मैं तब भी ‘हंस’ का नियमित ग्राहक व पाठक था और भाई तेज सिंह द्वारा सम्पादित मूलनिवासियों की एकता एवं चेतना को लक्ष्य कर निकलती टेबलॉयड पाक्षिक पत्रिका ‘अहवाल-ए-मिशन’ को भी अपने कार्यालय के पते से पटना मंगवा कर पढ़ता था. बताऊँ कि इस पत्रिका को उलट-पुलट मेरे स्त्री-पुरुष सवर्ण सहकर्मी खासा चिढ़ा एवं कुढ़ा करते थे, एवं मेरे पीठ-पीछे कहते थे कि कैसी-कैसी वाहयात चीजें छपती हैं और ये महाशय पढ़ते हैं? द्विजों को सीधे-सीधे वाट लगाती वह पत्रिका ‘शुद्ध’ सवर्णों को कैसे हजम होती भला? बहरहाल, बिना बहके प्रसंग पर सीधे रुख करें तो दरअसल, ‘हंस’ के किसी पन्ने पर मैंने डा. तेज सिंह की पत्रिका ‘अपेक्षा’ का विज्ञापन देखा था. मैंने डा. तेज सिंह एवं भाई तेज सिंह के अंतर पर ध्यान नहीं दिया एवं डा. तेज सिंह को एक पोस्टकार्ड लिख दिया कि मैं आपकी पत्रिका ‘अहवाल-ए-मिशन’ पढ़ता रहा हूँ, ‘अपेक्षा’ की भी ग्राहकी चाहता हूँ. डा. तेज सिंह ने अलग से कोई पत्रोत्तर तो नहीं दिया और न ही भाई तेज सिंह से अलग अपनी पहचान ही बताई पर मेरे पास ‘अपेक्षा’ पत्रिका के किसी अंक की दस प्रति का बंडल भेज दिया था. बण्डल में एक कागज पर उनका सन्देश था जिसमें मुझसे आग्रह किया गया था कि पत्रिका की बिक्री करवा कर पत्रिका के अंकित मूल्य में 20% बाद कर शेष राशि मुझे मनीऑर्डर कर दिया करें. जबतक वे पत्रिका भेजते रहे तबतक मैं इसी हिसाब से उन्हें पैसे भेजते रहा, हालांकि पत्रिका की पूरी कॉपी कभी नहीं निकल पाती थी. कुछ प्रतियाँ मुफ्त में दो-तीन जनों को दे देता था अथवा अपने घर ही रह जाती थी. हमारे संबंध जब घनिष्ठ हो चले तब भी ‘भाई’ एवं ‘डा.’ के द्वैध एवं अलग अलग व्यक्तियों के होने का जिक्र न मैंने उनसे कभी किया न ही उनने मुझसे! लंबी अवधि में फैले अपने परिचय के दौरान तेज सिंह जी से कई पत्रों के आदानप्रदान भी हुए. कम से कम उनके लिखे नौ-दस पोस्टकार्ड एवं अंतर्देशीय पत्र मेरे पास सुरक्षित होंगे. फोन संवाद भी हमारे खूब हुए पर मेरी तरह और लोग भी इस अनुभव के होंगे कि बातचीत के दरम्यान उनकी कुछ बातें अस्पष्ट सी उच्चरित रह जाती थीं.
डा. तेज सिंह और मेरे बीच कुछ समय तक संवादहीनता की स्थिति रही और यह गफलत में हुई. फेसबुक पर कॉमेंट करने के मामले में मुझे अपने कार्यालय ने सन 2011 में निलंबित कर दिया था जो संयोग से लम्बा चला. इस बीच मैं आर्थिक एवं मानसिक रूप से काफी परेशान रहा. और, फोन पर उनसे बातचीत की बारम्बारता घट गयी, जबकि मेरे एक कार्यालय सहकर्मी, जिनका परिचय मेरी मार्फ़त ही तेज सिंह से हुआ था, उनसे लगातार बतियाते रहे. ऐसे में तेज सिंह को लगा कि मैं उनसे नाराज चल रहा हूँ अथवा उन्हें कम भाव देने लगा हूँ. मुझे उस सहकर्मी ने यह बात बताई भी. जब फोन से एक बार तेज सिंह से बात की तो लगभग उलाहना देते हुए उन्होंने कहा कि तुम तो अब बात भी नहीं करते, जबकि वह (मेरे उक्त सहकर्मी का नाम लिया उन्होंने) हमेशा फोन करते रहता है. मैंने निलम्बन जनित अपनी परेशानी का उन्हें ध्यान दिलाकर कहा कि अभी काफी अव्यवस्थित हो चला हूँ इसलिए यह संवाद गैप हुआ है. इस बीच उनने पत्रिका का एक पैकेट मुझे भेजा पर मुझे मिला नहीं. वे मुझे ‘अपेक्षा’ की दस प्रतियाँ भेजा करते थे और मैं उन्हें उनके निदेशानुसार, पत्रिका के कुल कवर प्राइस की अस्सी प्रतिशत राशि मनीआर्डर कर देता था. मैंने समझा कि उनने आक्रोश में आकर पत्रिका भेजना बंद कर दिया है, दूसरी तरफ. उनने समझा कि मैं नाराज हूँ अतः न तो उस पैकेट के मैंने पैसे भेजे और न ही कोई संवाद किया. उभय ओर से गलतफहमी के चलते हमारी संवादहीनता लंबी खिंच गयी. इसके बाद क्या देखता हूँ कि पत्रिका का एक पैकेट मेरे उस मित्र के नाम आता है, पहली बार आता है. मैं उनसे एक प्रति खरीद लेता हूँ जिसमें ओमप्रकाश वाल्मीकि पर ही लगभग पूरा लंबा सम्पादकीय केंद्रित होता है. इस सम्पादकीय के गुण दोष की चर्चा इस आलेख के शुरू में ही हो चुकी है. मैं उत्सुकता से पत्रिका के उस पन्ने को झट उलटाता हूँ जिसमें संपादक का नाम, पत्रिका का पता-ठिकाना आदि दिया होता है. देखता हूँ कि पत्रिका के तीन बिहार प्रतिनिधियों में मेरा नाम यथावत है.
अबतक मेरा निलम्बन भी खत्म हो चुका था और तेज सिंह से संपर्क में न रहना मुझमें बेचैनी और एकतरह से अपराधबोध भी भर रहा था. मैंने इस अंक के मिलने की बात उनसे फोन पर की. वे जैसे मेरे फोन का लगातार इंतज़ार कर रहे हों! कोई शिकायत नहीं, बल्कि पहले मेरे निलम्बन के मामले का हांल लिया और, मेरी स्थिति सकारात्मक व सहज पाकर काफी प्रसन्न हुए. कहा कि इस अंक को पढ़कर प्रतिक्रिया देना और अगले अंक के लिए अपनी कुछ रचनाएँ जरूर भेजना. काफी लंबी बात चली. लेकिन, सब धरा का धरा रह गया. विडंबना देखिये, उनसे संवाद शुरू तो हुआ था पर अंत लिए हुए! वे सदा सदा के लिए संबंध-विच्छेद कर संवाद की लड़ी तोड़ कर न लौटने के लिए चले गए!
दिल्ली उनके घर दो बार जाना हुआ. दोनों बार कृष्णानगर के घोंडली गाँव में स्थित उनके पैतृक निवास पर गया. बड़ी आत्मीय मुलाकातें. वे प्रथम मंजिल पर स्थित अपने अध्ययन कक्ष में बड़ी सादगी से रहते थे. दीवारों के साथ लगी उनकी छोटी छोटी मंजिलों में तह पर तह लगा रखी किताबें, पत्र-पत्रिकाएँ एवं अन्य पठान-सामग्री एवं बीच कमरे में एक ओर बिछावन बिछी हुई थे एवं कमरे में कुर्सी टेबल भी लगे थे, जहाँ वे सुविधा अनुसार कभी लेटकर तो कभी बैठकर लिखते पढ़ते थे. कोई फोकस नहीं, नयनाभिराम अथवा भडकदार सजावट की कोई कोशिश नहीं. सादगी एवं बुद्धिजीविता का एक वातावरण एवं सहज आकर्षण वहां व्याप्त था. पहली बार मैं जब उनके यहाँ गया था तब मैंने पटना विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग में पीएचडी के लिए अपना रजिस्ट्रेशन ही करवाया था. तब उन्होंने मेरे पीएचडी के लिए अनिवार्य प्राथमिक स्रोत सामग्री का एक जरूरी हिस्सा समझ के. नाथ की आत्मकथा, ‘तिरस्कार’ भी अपनी निजी लाइब्रेरी से दी थी. हालांकि इस आत्मकथा को मैंने अपने शोधकार्य का हिस्सा नहीं बनाया था, इस वजह से कि पुस्तक ही उपलब्ध नहीं पा रही थी. कई अन्य जरूरी पुस्तकें एवं अपेक्षा के पुराने अंक भी उन्होंने मुझे दिए. एक बार तो उनसे मिलने दिल्ली विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग में पहुंचा था मैं, जहाँ उनसे मुलाकात नहीं हो सकी थी, पूर्व परिचित एवं पटना विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग में रहे बिहार मूल के आलोचक गोपेश्वर सिंह से वहां जरूर मुलाकात हुई जिनने वहां उपस्थित कुछ और लोगों से मिलवाया. तब सुधीश पचौरी वहां विभागाध्यक्ष थे एवं युवा आलोचक विनोद तिवारी भी बीएचयू में कुछ काल तक सहायक प्रोफेसरी कर पहुँच चुके थे जिनसे एक क्षणिक भेंट ही हो पायी थी, वे क्लास लेने निकल रहे थे.
पटना में भी दो-तीन मुलाकातें हुईं उनसे. अंतिम मुलाकात 2010 में हिंदी विभाग, पटना विश्वविद्यालय एवं साहित्य अकादेमी, नई दिल्ली के संयुक्त तत्वावधान में 28-29 नवंबर, 2010 को आयोजित ‘दलित साहित्य के सौंदर्यशास्त्र और इतिहास लेखन की समस्याएं’ विषयक राष्ट्रीय संगोष्ठी के दौरान हुई थी, इससे करीब दो वर्ष पहले हुई पटना में उनसे भेंट तो खैर काफी लंबी एवं मेरे शैक्षणिक कैरियर का अनिवार्य हिस्सा ही बन गयी. सन 2008 में हुए मेरे पीएचडी साक्षात्कार में वे वाह्य परीक्षक बनकर आये थे. (बता दूँ कि मेरी यह पीएचडी ‘हिंदी दलित आत्मकथाओं में अभिव्यक्त क्रूर यथार्थ का संसार’ शीर्षक से है. संभवतः बिहार क्षेत्र के किसी भी विश्वविद्यालय से हिंदी साहित्य में दलित विषयक यह प्रथम पीएचडी-शोधकार्य है.) इस समय तक तो उनसे मेरे प्रगाढ़ संबंध बन ही चुके थे, इस अवसर ने उसे और पक्का कर दिया था. उनके संपादन में निकलती हिंदी दलित आलोचना की महत्वपूर्ण त्रैमासिक पत्रिका ‘अपेक्षा’ का मैं बिहार प्रतिनिधि तो था ही, साथ ही उसमें गाहे ब गाहे मेरी रचनाएँ छपा भी करती थीं. वे इसबार सपत्नीक पटना आये थे और पत्नी संग गौतम बुद्ध से जुड़े बिहार के दो प्रख्यात स्थलों, राजगीर एवं बोधगया भ्रमण का एजेंडा भी लेकर आये थे. पटना विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग के वर्तमान अध्यक्ष एवं तत्कालीन प्रोफ़ेसर कवि-उपन्यासकार डा. सुरेन्द्र स्निग्ध के डा. तेज सिंह गहरे मित्र थे. और इधर, मेरे पीएचडी करने में प्रो. स्निग्ध का बड़ा हाथ रहा. वे नहीं होते, उनकी जोरदार मदद मुझे न मिली होती तो मेरी पीएचडी निर्विघ्न पूरी नहीं हो पाती. यहाँ तक कि मेरा रिसर्च-सिनोप्सिस (शोध प्रस्ताव) ही मंजूर नहीं हो पाता. यहाँ बहुत विस्तार में जाने का मौका नहीं है, और यह करने से विषयान्तर भी हो जाएगा. अन्यथा पूरे रिसर्च काल में एक से एक रोचक मोड़ एवं प्रसंग आये जो काबिलेजिक्र हैं.
पीएचडी के मेरे इस साक्षात्कार में एक अलग बात यह रही कि मुझे ऐसा कुछ महसूस ही नहीं हुआ कि मैं इस वक्त छात्र हूँ और परीक्षा के दौर से गुजर रहा हूँ. छात्र का यानी मेरा जो परिचय वहां उपस्थित मुझसे अनभिज्ञ लोगों को दिया गया उसमें एक सरकारी संस्था में मेरे कार्यरत होने एवं एक दलित कवि एवं साहित्यकार के रूप में दिया गया. सवाल-जवाब का दौर संपन्न हुआ और मेरे इंटरव्यू के सफल होने की घोषणा कर मुझे पटना विश्वविद्यालय के हिंदी संकाय के विभागाध्यक्ष डा. दिनेश प्रसाद सिंह ने मेरी ओर हाथ बढ़ाते हुए बधाई दी. उस वक्त जब मैं हाथ मिलाने में सकुचा रहा था तो सुरेन्द्र स्निग्ध सर ने कहा, “मुसाफ़िर जी, संकोच नहीं करें, आप विद्यार्थी थोड़े ही हैं”! यह कहते कहते उन्होंने भी अपना हाथ बढा दिया था. और, फिर, डा. तेज सिंह समेत वहां उपस्थित मेरे गाइड डा. शरदेंदू कुमार एवं कुछ अन्य शिक्षकों-छात्रों एवं मित्रों ने बधाई दी एवं हाथ मिलाया. इंटरव्यू के बाद नाश्ता आदि चला जिसका एक हिस्सा पान का चलना भी था. पान भी मुझे ऑफर किया गया पर इस बार मैं शिक्षकों के मध्य बिलकुल विद्यार्थी बने रहने पर अडिग रहा!
साक्षात्कार के अगले दिन सुबह हम राजगीर एवं बोधगया भ्रमण पर निकले. बोधगया में गर्म जलकुंड एवं प्रसिद्ध बौद्ध स्तूप के दर्शन किये एवं प्रसिद्ध रज्जूमार्ग के सहारे चढ़कर पहाड़ी पर पहुंचे जहाँ बौद्धस्तूप स्थित है. तेज सिंह सर डिजिटल कैमरा भी साथ लाये थे जिससे बौद्धस्तूप पर एवं कई स्थलों पर हमने तस्वीरें लीं. अक्सर मैं उन दोनों दम्पती की साथ साथ की अथवा अकेले-अकेले की फोटो खींचता तो कभी वे मेरी तस्वीर उतारते. कुछ तस्वीरें तो मेरी मैडम के साथ की सर ने ही हमें खड़ा कर खींची. जब तीनों जने की साथ की तस्वीर की बात होती तो हम किसी पर्यटक से ही फोटो खींच देने का अनुरोध करते. राजगीर पहुँचने से पहले रास्ते में पड़ने वाले मशहूर नालंदा विश्वविद्यालय के अवशेष स्थल का भी हमने भ्रमण किया था एवं स्वभावतः वहां भी फोटोग्राफी की थी. जाहिर है कि तस्वीरों का यह सिलसिला आगे की यात्रा के पड़ाव बोधगया में भी चला. बोधगया के लिए हमारी कार सूरज ढलने से पहले ही चल पड़ी थी. पटना में यात्रा शुरू करने से पहले बिहार से एकमात्र हिंदी दलित आत्मकथाकार (‘घुटन’) एवं वीर कुँवरसिंह सिंह विश्वविद्यालय के पूर्व उपकुलपति एवं वर्तमान में पटना विश्वविद्यालय में दर्शनशास्त्र के प्रोफ़ेसर रमाशंकर आर्या ने कुछ इस तरह बताया था, “राजगीर-बोधगया सड़क मार्ग से करीब दो घंटे में तय होता है. अँधेरा होने से पहले ही आप लोग यह रास्ता तय कर लें तो बेहतर, क्योंकि इन इलाकों में ‘हमारे भाईलोगों’ (नक्सलाईट) का प्रभाव है. हालाँकि उनसे हमें डर नहीं है, वे ‘उनलोगों’ को खोजते हैं! ‘वसूली’ केवल उन्हीं से करते हैं! आमना-सामना हो भी जाये तो हमारा परिचय लेकर वे हमारा रास्ता छोड़ देते हैं.”
रात्रि-विश्राम हमने बोधगया के एक साधारण होटल में किया. मैंने देखा कि हमारे किराये की कार के ड्राइवर की फ़िक्र तेज सिंह सर की यात्रा के दौरान बराबर रही. उनने बलपूर्वक एवं ध्यान देकर ड्राइवर को हर जगह नाश्ता-पानी, भोजन हमारे साथ करवाया, जबकि वह सकुचाता रहा, क्योंकि भाड़े की शर्त में ड्राईवर का कोई व्यय हमारे जिम्मे न था, पर व्यय हमने ही किया. यहाँ तक कि ड्राईवर को सर के सुझाव पर हमने होटल में ठहराया. सर ने मुझसे पूछा था, “दो बेड का दो कमरा हम ले लेते हैं, तुम्हें अपने कमरे में ड्राईवर को ठहराने में कोई आपत्ति तो नहीं होगी?” मैंने भी फ़ौरन कहा था, “नहीं सर, कोई दिक्कत की बात नहीं”.
बोधगया में महाबोधि मंदिर देखने में हमने सर्वाधिक समय खर्च किया. इस कैम्पस में कुछ विचार-खुराक भी मुझे मिली थी! देखा कि बौद्ध धम्म से अधिक प्रभाव तो इस कैम्पस में हिंदू धर्म का है. कैम्पस में स्थित तालाब के आसपास पिंडदान का कार्यक्रम चलता है, और, महाबोधि मंदिर के अंदरूनी मुख्य द्वार से पहले मंदिर परिसर के दक्षिण हिस्से में अलग से एक छोटे एकमंजिले गेरुआ/भगवा रंग के मंदिर में कुछ हिंदू देवता भी स्थापित हैं जिनकी हिंदू श्रद्धालु पूजा करते हैं. मुख्य मंदिर (महाबोधि) के भी पश्च भाग में चबूतरे पर हिंदू साधुओं का कब्ज़ा है जहाँ भजन कीर्त्तन होते रहता है. मंदिर के परिसर के पश्चिम-उत्तर हिस्से में बौद्ध-विपश्यना के लिए चबूतरे, चौके आदि बने हुए थे जहाँ कुछ भंते साधना रत भी थे. एक बात मुझे यह भी खटकी कि एक बौद्ध साधु भी हिंदू पुजारियों छोकी तरह श्रद्धालु को अधिक से अधिक दान करने पर जोर दे रहा था. एक बौद्ध साधु के पास जाकर जब सर की पत्नी ने एक बोधिसत्व की मूर्ति के समीप जाकर अपनी श्रद्धा निवेदित करनी चाही तो साधु ने कम से कम एक निश्चित राशि देने का दवाब डाला. तेज सर ने इशारे से मैडम को उसके दवाब में आने से मना किया पर मैडम ने पुनर्विचार करते हुए दान की राशि उचकाकर (बढ़ाकर) साधु का मान और मन रख दिया! महाबोधि मंदिर से निकलने के बाद हम विदेशी बौद्ध मठों, जैसे तिब्बती, जापानी में घूमे तथा बोधिसत्व की विशालकाय पद्मासन मुद्रा में ध्यानस्थ मूर्ति स्थल का भी हमने अवलोकन किया.
एक बात यहाँ मैं फिर से पीएचडी शोध की करूँगा. ऐसे शोध-कार्यक्रमों का एक ढर्रा निर्धारित होता है. यह काल, स्थान के भेद से कुछ अलग हो सकता है पर कुछ मोटी मोटी बातें हर जगह एक सी चलती हैं. मसलन, वाह्य परीक्षक के आने-जाने, खाने-पीने, भ्रमण से लेकर कई अन्य खर्चे शोधार्थी के परम कर्तव्यों में बलात शामिल कर दिया गया होता है. कुछ खर्च एवं शिष्य-कर्तव्य वहन तो ब्राह्मणी-गुरु-दक्षिणा की तर्ज़ पर गाइड (शोध-निर्देशक) के प्रति भी करना होता है! पर मेरा मामला सर्वथा अलग रहा. मैंने ही जिद्द करके एवं सुरेन्द्र स्निग्ध सर के माध्यम से तेज सिंह सर को इस बात के लिए मनवाया कि कार भाड़े का खर्च मेरा रहेगा, मैं तो एक लेखे से विद्यार्थी हूँ भी नहीं, और नौकरी में हूँ. आत्मीयता एवं रागात्मक संबंध भी काफी पहले से ही है हमारा. आखिर, मेरा भी अधिकार एवं कर्तव्य तो कुछ बनता है! और तो और, मैं तो तेज सिंह सर को अपनी पीएचडी मौखिकी से पहले ‘भैया’ ही संबोधित करते आया था. बावजूद, बड़ी ही कठिनाई से उन्हें इसबात के लिए राजी किया जा सका था.
हार्ट अटैक से उनकी आकस्मिक मृत्यु की खबर फेसबुक पर थी. दिल्लीवासी जय प्रकाश कर्दम, अजय नावरिया, कैलाश चन्द्र चौहान, रजनी अनुरागी जैसे सक्रिय दलित साहित्यिक फेसबुकियों की 15 जुलाई 2014 की सर्वप्रमुख फेसबुक स्टेटस इसी दुखद समाचार को साझा करते लगी थी. खबर पढ़ते ही मैंने झट जयप्रकाश कर्दम को फोन लगाया. वे गाजियाबाद, वसुंधरा स्थित डा. तेज सिंह के घर पहुँच ही रहे थे. उन्होंने फेसबुक की दुखद खबर पर मुहर लगाते हुए कहा कि अभी-अभी उनके फ़्लैट पर पहुंचा हूँ. तबतक उनके अंतिम संस्कार का फैसला नहीं हुआ था कि कहाँ और कब होगा? उनकी हृदयगति रुके बहुत समय नहीं बीता था. कर्दम जी से बात करने के बाद मैंने बिहार-झारखण्ड के कुछ प्रमुख दलित साहित्यकारों, बुद्धशरण हंस, विपिन बिहारी, रमाशंकर आर्य एवं अजय यतीश को फोन से शोक-सूचना दी कि हिंदी दलित साहित्य आलोचना के एक जरूरी एवं प्रमुख स्तंभ, डा. तेज सिंह अब हमारे बीच नहीं रहे.
पाद-टिप्पणियाँ
1. ‘अपेक्षा’, संयुक्तांक 46-47 (जनवरी-जून 2014), (डा. तेज सिंह के महापरिनिर्वाण के चलते यह उनके संपादन में पत्रिका का अंतिम अंक साबित हुआ है.)
2. वही
3. वही
4. बीसवीं सदी का हिंदी साहित्य, पृष्ठ संख्या 182-206, संपादक, डा. विश्वनाथ प्रसाद तिवारी, भारतीय ज्ञानपीठ, प्रथम संस्करण 2005
5. वही
6. पहल – 80, अंक जुलाई-अगस्त 2005, संपादक ज्ञानरंजन
7. वही
8. वही
9. दलित साहित्य 1999, संपादक जयप्रकाश कर्दम
10. तद्भव, अंक 4, सन 2000, संपादक अखिलेश
11. दलित साहित्य (वार्षिकी) 2013 का सम्पादकीय लिखते हुए
आलेख : डा. मुसाफ़िर बैठा
पता : बसंती निवास, प्रेम भवन के पीछे, दुर्गा आश्रम गली, शेखपुरा, पटना-800014
इमेल : musafirpatna@gmail.com
मोबाइल : 9835045947