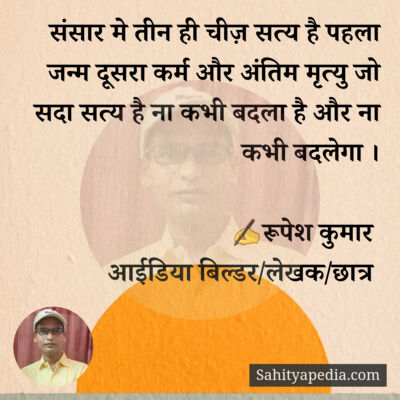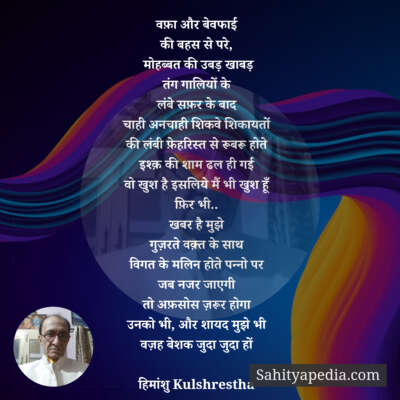सज़दा
इश्क़ में ख़ुदा माना था तुम्हें
और इबादत में तेरी, मन को मंदिर बनाया था
पूजा था तुम्हें कुछ इस तरह
कि साँसों की बाती संग तन का दिया जलाया था
तुम्हारी कही हर इक बात को
आयत की तरह माना था कभी
तुम्हारी गोद में सर रख लेती थी
बस इसी को सज़दा जाना था कभी
तुम मुस्काते तो वही बहार थी मेरे लिए
तुम्हारी एक नज़र ही करार थी मेरे लिए
तुम्हारे बिना ये सारी दुनिया बेमानी लगती थी
तुम साथ न हो तो मैं ख़ुद को ही बेगानी लगती थी
कितनी नासमझ थी मैं, और तुम कितने समझदार
मैं हज़ारों बार बिखरी, पर तुमने न समेटा इक बार
तुम सिर्फ़ ये बाज़ी जीतने आये थे
और मैंने तो इसे खेल जाना ही नहीं
मेरा हारना तो सदियों से तय था
जब किसी भी जन्म तुम्हें पहचाना ही नहीं
ख़ुदा से इश्क़ होना था,
मैं इश्क़ को ही ख़ुदा जान बैठी
तुम तो कभी थे ही नहीं इस रिश्ते में
मैं किस बुत को मसीहा मान बैठी
लो साँसों की इस डोरी के संग
बँधा था जो तुमसे, वो नाता तोड़ दिया
आज जन्नत में ख़ुदा भी पूछ बैठा मुझसे
क्या उसके दर पर सज़दा करना छोड़ दिया?
सुरेखा कादियान ‘सृजना’