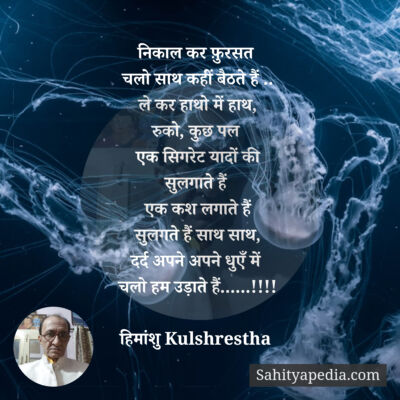स्वीकार्य
व्योम में दिखता विकृति नेत्र से गिरता लहू है
चांँद की मोहक छवि से तुम भले बादल हुए हो।
उत्सवों की रश्मियों से है प्रकाशित यह नगर, पर
मेरे मन में है अंधेरा जब से तुम ओझल हुए हो।
मैं कदाचित पीर में अब उम्रभर रोता रहूंँगा।
और आहत अक्षरों के व्यूह से होता रहूंँगा।
रिक्तियों से भर चुका है प्रेम का सूखा समन्दर
गूंँजता है कर्ण में क्षण क्षण तुम्हारे स्नेह का स्वर।।
है नहीं सामर्थ्य मुझमें जो तुम्हें पाकर दिखाऊंँ
डर रहा हूं कैसे घायल यह हृदय आकर दिखाऊंँ
भोग के सीमा से ऊपर प्रेम में आसक्त हूंँ मैं।
नेह के चितवन से बहता पीत वर्णी रक्त हूंँ मैं।
पीर है मेरे हृदय में,कैसे यह स्वीकार कर लूंँ।
मैंने चाहा सिर्फ़ तुमको ,तो किसे अवधार कर लूंँ।
हांँ कोई बंदिश नहीं है जिससे चाहो प्यार कर लो..
तुम विजय हो जिंदगी में,मुझको अपनी हार कर लो।
भाग्य में ठोकर लिखा है मैं इसे कब जान पाया
एक निर्भय मन के बल से प्रेम ही तुझपर लुटाया।
जानकर अनजान हूंँ बस लोभ है कुछ सांँस भर की।
कुछ बरस जीने की खातिर झूठ को सच मान पाया।
अब अगर स्वीकार कर लूंँ,तुम मेरी कुछ भी नहीं हो
तो कोई शंका नहीं है ,आयु का प्रतिकार कर दूंँ।
तुम हमारे आत्मा की रंध में बसती रहो या
तुम कहो तो मैं स्वयं को काल का आहार कर दूंँ।
दीपक झा रुद्रा