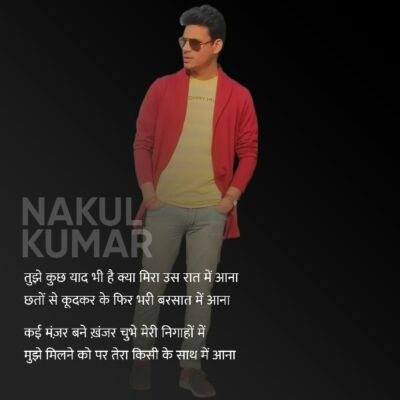सुबह-सुबह
सुबह-सुबह
किसी अजनबी से
मैं मिल लेता हूं
कभी-कभी
उसका भी चेहरा
पढ़ लेता हूं
उसके चेहरे पर
चांदनी सी फैली हुई
अपार खुशियों से
थोड़ी सी मैं ले लेता हूं
फिर मिलने वाले
हर अजनबी को
थोड़ी-थोड़ी ही सही
सबको कुछ न कुछ
मैं बांट देता हूं
और मैं पूरा का पूरा
रिक्त हो लेता हूं
सुबह मिले हुए ऋण से
खुद को शाम तक
मुक्त कर लेता हूं
पर जब भी अपनों के
मध्य मैं होता हूं
शून्य से शून्य को
गुणा कर लेता हूं
वो हो गए न्यूनतम
मैं भी हो लेता हूं
उनके चेहरों पर
फैली विषैली मुस्कानों से
अतिक्रमित संक्रमित
मैं भी हो लेता हूं
अगली सुबह को फिर
किसी अजनबी की तलाश
मैं निकल लेता हूं
कहीं न कहीं से
मैं उसे ढ़ूढ़ लेता हूं
और फिर से थोड़ी ही सही
मैं खुशी पा लेता हूं
और पुनः अजनबियों को
मैं बांट देता हूं
यह चक्र है जिसमें
मैं चक्रित हो लेता हूं
थोड़ी -थोड़ी ही सही
पा लेता हूं बांट देता हूं
इसी तरह से तो
इस जीवन के चक्र को
पूरा करने की कोशिशें
मैं हो लेता हूं
सुबह-सुबह
किसी अजनबी से
मैं मिल लेता हूं
***
-रामचन्द्र दीक्षित ‘अशोक’