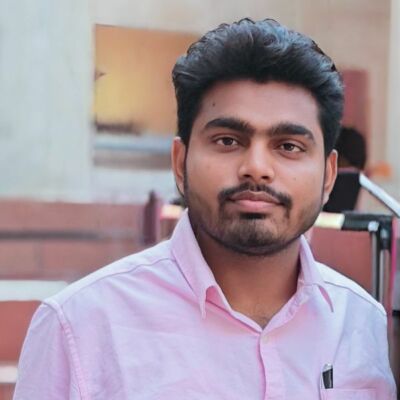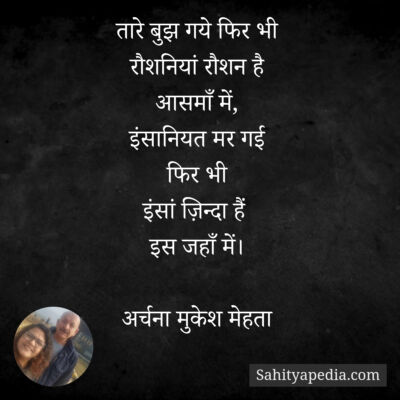साए

साए, कहीं से भी निकलकर,
पल भर के लिए
सामने से गुज़रकर
खो जाते हैं,
धुंध में,
यूँ ही बारबार
प्रकट हो-हो कर,
निरंतर लगातार।
साये में छिपे
चेहरों को
पहचानने का हुनर
सीख रहा हूँ
आजकल;
या शायद ज़िंदगी
सिखा रही है आजकल।
शायद अब
अंदाज़ लग जाता है
इन नक़ाब के अन्दर
है कोई और
और ये कि
मुझसे मुख़ातिब
साया है कोई।
कोई साया अब
गायब नहीं होता
धुंध में,
तब तक-
जब तक न गुज़र जाये
उतारकर अपना नक़ाब
वो
सामने से होकर
पलभर।
(C)@ दीपक कुमार श्रीवास्तव “नील पदम्”