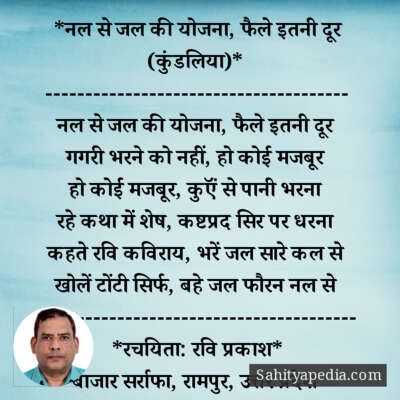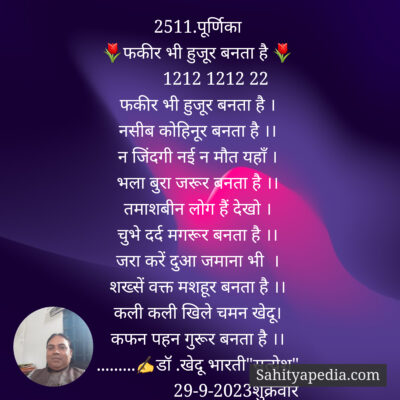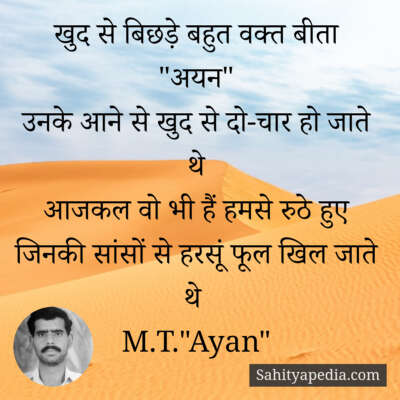सभ्यों की ‘सभ्यता’ का सर्कस / मुसाफिर बैठा
गालियों का एक अपना मनोविज्ञान है। और इस मनोविज्ञान के अभिव्यक्त होने के कई-कई संस्तर और रूप हैं। इन्हें और विधियों के अलावा सभ्यों के तथाकथित सभ्य आचार-सर्कस में भी देखा-तलाशा जा सकता है। मनुष्य की चेतना के स्तर पर असंतुष्ट असामाजिक, अनैतिक इच्छाएं अचेतन में दब जाती हैं। परंतु, ये दमित होकर चुप नहीं बैठतीं। जैसे ही ‘सुपर ईगो’ की पकड़ ढीली होती है, ये इच्छाएं स्वयं को गालियों, छोटी-मोटी मनोवैज्ञानिक भूलों व अन्य रूपों में प्रकट कर लेती हैं। एडलर के अनुसार, जीवन की दो आधारभूत प्रवृत्तियां होती हैं- श्रेष्ठता की भावना और हीनता की भावना। हीनताजन्य ग्रंथि पर विजय पाने के लिए व्यक्ति कुछ ऐसा काम करना चाहता है जो उसे समाज के ‘अन्य लोगों से अलग करे। अपने को दूसरों के मुकाबले बेहतर साबित करने के क्रम में वह गालियों का सहारा लेता है।
फिर, अपशब्द वृत्ति का यह मनोवैज्ञानिक व्यापार लोक और आभिजात्य संस्कृतियों के द्वंद्वात्मक रिश्ते को भी अभिव्यक्त करता है। ‘जिस वर्ग, जाति या सांस्कृतिक समुदाय (आभिजात्य संस्कृति) का समाज में वर्चस्व होता है वह निचले और दबे समुदाय (लोक संस्कृति) की भाषा, मुहावरों, जाति या आदतों को ‘गाली’ (अपशब्द) बना देता है। आपस में जब एक ‘सुसंस्कृत’ समुदाय एक-दूसरे को ‘भंगी’ या ‘चमार’ कहता है तो उसे गाली दे रहा होता है, यानी उसे ‘असभ्य’ और ‘असंस्कृत’ कहता है। इसके पीछे उस वर्ग-
साक्ष्य । ३०१
जाति के लिए खौलती घृणा की उसकी पूर्वग्रंथि होती है।’ (‘कांटे की बात’/ राजेन्द्र यादव) क्या करें, हमारे बिहार की लोक संस्कृति भी सभ्यों की आभिजात्य संस्कृति के विपर्यय में है, विरोध में है।
‘आज वी.पी. सिंह एक गाली है। उत्तर भारतीय ‘प्रबुद्ध’ मध्यवर्ग के लिए उससे ज्यादा घृणित, कुत्सित और नाम लेते ही ‘पापशांत’ वाला शायद ही कोई दूसरा नेता हो।’ (‘कांटे की बात’/ राजेन्द्र यादव)। उसी तरह, ‘भारतीय सोच-निर्माता’ इस मध्यवर्ग के लिए लालू प्रसाद यादव ज्यादा से ज्यादा एक जाहिल, विनोदी विदूषक है या फिर, निकृष्ट छवि में, भ्रष्टाचार, अक्षमता तथा उन सब का पर्याय/संकेतक, जो भारत में बुरा है।’ (स्मिता गुप्ता/टाइम्स ऑफ इंडिया/फरवरी १९९८)
और रहा ‘बिहार’ और ‘बिहारी’ शब्द, तो इन्हें बिहार ‘प्रेमियों’ ने अपनी अभिधा-सत्ता से उचकाकर इनके लिए अतिशय, पिछड़ापन, अबाध भ्रष्टाचार, नंगी हिंसा व अव्यवस्था प्रभृति तमाम गजालतों को संबोधित एक ‘निर्विशेष’ मुहावरापरक नाम- ‘बिहार सिंड्रोम’- ही दे डाला है। यह मुहावरा बिहार के राज्यतंत्र, राजनैतिक नेतृत्व की कथित विफलता और बिहारी समाज मात्र के लिए चल निकला है। गोया, बिहार के अलावा यह सब देश के इतर प्रदेशों में है ही नहीं, होता ही नहीं।
आश नारायण (हिन्दुस्तान टाइम्स/१७ अक्तूबर, १९९८) कहते हैं कि ‘लंबे समय से बिहार कृषिजन्य हिंसा, सामाजिक विघटन व प्रशासनिक क्षय का समरूप रहा है। अभी तो यह एक ‘निषिद्ध भूमि’ व ‘भयावह स्थल’ बन गया है। यहां ज्यादा से ज्यादा लोग कानून अपने हाथ में लेने लगे हैं; नक्सल और जाति ‘सेनाएं’ राज्य का स्थानापन्न बनाने का प्रयत्न करती रहती हैं। यदि १९५० के दशक को छोड़ दे-जिस कालखंड को एपलबी रिपोर्ट में बिहार को ‘सर्वोत्कृष्ट शासित प्रदेश’ का
तमगा दिया गया था तो शेष काल में बिहार ‘अव्यवस्था’ का मुहावरा बनकर रह गया है।
बिहार की अधःयात्रा १९६० से आरंभ होती है। सन् १९७० के दशक में मशहूर अंग्रेजी उपन्यासकार वी.एस. नायपाल ने बिहार को ‘द एण्ड ऑफ अर्थ’ (The End of Earth) कहकर खारिज किया था।’ प्रेमपाल शर्मा (समयांतर जनवरी-फरवरी, २००१) यहां तक कहते हैं कि ‘जो उत्तर प्रदेश-बिहार को जानते हैं, वे तो इन राज्यों की कुव्यवस्था को देखकर इनकी तरफ जाने की तो छोड़ें, देश से ही अलग होने को तैयार है। याद कीजिए, ‘मंदिर-मस्जिद’ और ‘मंडल’ के दिनों की भयानक त्रासदियां। दक्षिण के कुछ राज्यों के नेताओं और बुद्धिजीवियों ने आवाज उठायी थी कि इसके असर से हम तभी बच पाएंगे जब हिन्दी-भाषी क्षेत्र से बिलकुल अलग ही हो जाएं। … जो राज्य सबसे ज्यादा ‘आई.ए.एस’ पैदा कर रहे हैं वे अपने राज्यों को ही सुव्यवस्थित नहीं कर पाते। कारण साफ है, नौकरियों के लिए प्रतियोगिता में आगे आना एक बात है, समाज में परिवर्तन के लिए आगे आना दूसरी बात।’
दरअसल, हम कुछ है ही ऐसे कि हमारी पहचान बिहारेतर भारत में एक नकरात्मक ‘सिंड्रोम’ से करायी जा सक रही है। बिहार की वर्तमान धरती कहीं से भी महात्मा बुद्ध, महावीर औ’ महात्मा गांधी की वो धरा नहीं लगती जो कभी उनकी कांतिमय कर्मस्थली रही थी। हिंसा, अव्यवस्था, अंधविश्वास,
३०२ । साक्ष्य
जाति और धर्म की जंजीरों में जकड़ा हमारा औपनिवेशिक, सामंती, बंद बिहारी समाज इन कर्मवीरों की तौहीन करता प्रतीत होता है।
बिहार के शिक्षा-संसार की दुर्गति देखते हुए भी नालंदा विश्वविद्यालय की आहत थाती पर कैसे गर्व करें हम ! गांधी की सत्य-अहिंसा की भारत में प्रथम प्रयोग की भूमि रही है बिहार, यह हम किस मुंह से कहे! क्या यही है गांधियों के सपनों का बिहार! बुद्ध-महावीर के हिंसारहित वैज्ञानिक, समरस समाज की चाहना के बरअक्स विरुद्धधार्मिता जनित काहिली-कारस्तानियों में डूबे-पगे अपने सांप्रतिक बिहार पर कैसे इतराएं-इठलाएं हम ! हम तो उर्वर अतीत की विरासतों को न संजो-संभाल पाने वाले, खो देने वाले वो मरा समाज हैं, चुके हुए लोग है, जो फिर से किसी आमूलचूल परिवर्तन की बाट जोहता है।
सो, कोई बिहार के समृद्ध अतीत की स्मृतियों से भले ही खुश हो ले, पर मेरे मन में यह (स्मृति) कचोट ही पैदा करती है। हम इसके नपुंसक उत्तराधिकारी (वारिस) से लगते हैं। संपन्न कल के बीतयौवना गौरव गाथा गाने-बांचने से हमारा कोई हित सद्यः नहीं सधने वाला। बेशक उससे प्रेरणा ली जा सकती है, अपनी नादानियों-नाकामियों पर शर्मसार हुआ जा सकता है। एक समर्थ उत्तराधिकारी में स्वस्थ विरासत की हिफाजत का माद्दा भी होना चाहिए। हम बिहारियों की एक बड़ी क्षति/कमी खुद में छायी आत्मविस्मृति ही है। और यह आत्मविस्मृति आत्मविकास और आत्मविश्वास का सबसे बड़ा शत्रु है।
एक संगठन, समाज के रूप में गाली खाने की बेचारगी गाली परोसने वाले का प्रतिकार न कर पाने की बेबसी अपनी नुक्ताचीनी, हेठी के प्रति सम्यक्-सबल-एकाग्र प्रतिरोध न कर पा सकने की दयनीयता का ही द्योतक होती है। एक स्वस्थ, स्वाभिमानी प्रदेश का तमगा हासिल करने के लिए हमें अपनी मलामतों-मलिनताओं से छुटकारा पाना होगा और भी दूसरी चीजें सीखनी होंगी। हमें बंगालियों, पंजाबियों की तरह प्रतिरोध की संस्कृति विकसित करनी होगी। अपने में एक ‘किलर इंस्टिंक्ट’ – हर हालत में सफल होने की इच्छा-शक्ति पैदा करनी होगी। हममें यह सब नहीं है, इस कारण ही हमारे हिंदी-भाषी क्षेत्र को ‘गोबर पट्टी’ या ‘काउ बेल्ट’ जैसा उपहासात्मक लक्षणात्मक नाम दिया जाता है। ‘बिमारु’ (BIMARU- बिहार, मध्यप्रदेश, राजस्थान, यूपी) प्रदेशों यानी हिंदी भाषा-भाषी राज्यों को ‘बीमार’ कर दिया जाता है और ‘बिहार’ को ‘बिहार सिंड्रोम’। मानो, यह बिहार द्वारा पैदा की गई कैसर-एड्स जैसी कोई गंभीर, लाइलाज व्याधि हो। है भी, जो समाज खुद ही जाति-संप्रदाय, ऊंच-नीच के विकृत खांचे में नाभिनाल बद्ध हो, जहां का पढ़ा-लिखा, सभ्य- सुसंस्कृत और बुद्धिजीवी कहा जाने वाला तबका तक कूदमग्ज और इस वैज्ञानिक-तार्किक युग में भी मनुरचित व्यवस्था-विधानों में जीने का आग्रही हो, वह क्योंकर किसी ‘सिंड्रोम’ का पात्र नहीं बनेगा और कैसे अपनी हकमारी, वाजिब अधिकार से मुतल्लिक जंग लड़ने की खातिर सामने आने का ‘साहस’ कर सकेगा। हम बिहारियों की ऐसी ‘कारयित्री प्रतिभा’ ‘सभ्यता’ के मुंह पर तमाचा है। पेश है कुछ बानगी।
साक्ष्य । ३०३
बात कुछेक दिन पहले की है। दरभंगा स्थित ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के एक दलित उच्चाधिकारी के अपने पद से हटने के बाद नवागत ‘श्रेष्ठ कुल जात’ अधिकारी ने अपना पदग्रहण करने से पूर्व अपने कुर्सी-टेबुल का ‘शुद्धिकरण’ करवाया (कुछ उसी तर्ज पर, जैसे काशी में कभी दलित बाबू जगजीवन राम द्वारा किसी देवता की मूर्ति छूने भर से देव अपवित्र हो गया था और किसी पवित्रता के ठेकेदार, पुजारी, द्वारा उसे पुनः पवित्र करना पड़ा था!) इस सोच की ‘उर्वरता’ को क्या कहिएगा। जब ये पढ़े-लिखे और सुसंस्कृत लोग हैं तो अपढ़ कबीर के ‘ढाई आखर प्रेम’ और ‘मनुष्यता’ पढ़ने को क्या कहिएगा!
कुछ प्रबुद्ध जनों द्वारा मेरे दलित संकेतक नाम (टाइटिल) ‘बैठा’ के साथ शाब्दिक व्यंग्य-व्यभिचार किया जाना या फिर उन्हीं में से एक जातिगत श्रेष्ठता दंभ से पीड़ित सज्जन का भारतीय संविधान निर्माता डा. भीम राव आम्बेडकर का सुबह-सुबह नाम मात्र लिये जाते सुनकर मुंह का जायका बिगड़ जाना, दिन खराब हो जाना, ‘बिहार सिंड्रोम’ को न्योतना नहीं या कि हम बिहारियों का ही कोई गलित सिंड्रोम नहीं? जब अपनी ही काया गंदी हो तो दूसरों की मलिनता भला क्या देखेंगे आप ! दूसरों की कुत्सित दृष्टि का प्रतिकार-प्रक्षालन हम कैसे कर पायेंगे भला! कहावत भी है-अपनी पगड़ी अपने हाथ। अपनों की कमियों को छुपाना अपनी विचारधारा और समाज के साथ तो विश्वासघात है ही, नैतिकता के लिहाज से भी उचित नहीं।
बहरहाल, अब हम कुछ ‘बिहार-विरोधी सिंड्रोमों’ की चर्चा करना चाहेंगे ताकि ‘बिहार सिंड्रोम’ का राग अलापने वालों का अंतस् चक्षु भी खुले और वे सिंड्रोम का व्यापक-सम्यक् अर्थ भी गह सकें। शब्दकोशों से इस शब्द का सम्यक् बोध उनके ‘भेजे’ में नहीं जाने-अटने वाला।
हाल ही में राजस्थान सरकार ने प्रदेश के इंजीनियरी संस्थानों में दाखिला हेतु जो प्रतियोगिता आयोजित की थी, उसमें वैसे छात्रों को ‘प्रवेश पत्र’ निर्गत ही नहीं किए गए जिनके पास ‘बिहार इंटरमीडिएट शिक्षा परिषद्’ की डिग्री थी।
एक-दो मौकों पर मैंने भी एक बिहारी होने की सिंड्रोमी सजा पायी है। एक घटना वर्ष १९९४ की है। मुंबई के एक लब्धप्रतिष्ठ निजी प्रबंधन संस्थान-टाटा समाज विज्ञान संस्थान (टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज) के प्रबंधन कोर्स में प्रवेश हेतु प्रतियोगी के रूप में मैं वहां गया था। मैंने संस्थान द्वारा आयोजित लिखित और ‘ग्रुप डिस्कशन’ चरण की परीक्षा पास कर ली पर मुझे अंतिम चरण की परीक्षा-अंतर्वीक्षा में शामिल नहीं होने दिया गया। ‘इंटरव्यू’ से पूर्व मुझसे स्नातक उपाधि के तीनों वर्ष के अलग-अलग अंक पत्र मांगे गए। मेरे पास तृतीय वर्ष (स्नातक उपाधि) का अंक पत्र था, – प्रथम, द्वितीय वर्ष का अंक पत्र नहीं था जिसमें प्रथम एवं द्वितीय वर्ष के परिणामी अंक भी अंकित थे और मुझे अंतिम रूप से स्नातक उत्तीर्ण घोषित किया गया था। पर संबद्ध परीक्षा-अधिकारियों ने मेरी एक न मानी और एक ने टिप्पणी की कि बिहार में डिग्रियां तो यो भी बंटती हैं। क्या भरोसा, आप उक्त (प्रथम, द्वितीय खंड की) परीक्षाएं उत्तीर्ण किए बगैर तृतीय वर्ष की डिग्री ले आए हों। उन्होंने मेरे अनुरोध (शायद अधिकार भी) को भी नकार दिया कि आप स्नातक ‘अपीयरिंग कैंडिडेट’
३०४ ।
को भी बाद में प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने की मोहलत देते हैं, फिर मुझे महज तीन-चार दिनों का ही समय दे दें ताकि मैं पटना जाकर इसे ले आऊं। पर वे क्योंकर मानने लगे। बिहारी होने के नाते मैं इसी सलूक का अधिकारी जो था!
दूसरा वाक्या पिछले साल का है। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय (इग्नू) में ‘सहायक निदेशक’ पद हेतु आयोजित साक्षात्कार में मुझे दिल्ली बुलाया गया था। ‘इंटरव्यू’ के दौरान साक्षात्कारकर्ताओं से बातचीत के क्रम में मेरे यह बताने पर कि मैं बिहार विधान परिषद् में नौकरी करता हूं और मेरे पद-दायित्वों में प्रकाशन के अलावे रिपोर्टिंग से सबद्ध कार्य भी आते हैं, एक महोदय ने फौरन एक सवाल दागा अच्छा! तो आप ‘लल्लू के यहां’ काम करते हो! अजी, फिर तो बड़े तकदीर वाले हो! दूसरे का प्रश्न था- ‘भई, आप ये बताओ कि वहां ‘हाउस’ में जो धक्का- मुक्की, मारपीट होती है (इस अवसर पर उन्होंने अपनी मुट्ठियों को बांधकर आपस में भिड़ाने का संकेत किया), उसकी भी रिपोर्टिंग करते हो आप!’ इन दोनों मौको पर साक्षात्कार बोर्ड में उपस्थित कई सदस्यों ने ठहाके लगाने, हीं-हीं, हो-हो करने से गुरेज नहीं किया जबकि कुछ के होठों पर महज फीकी, मंद-मंद कुटिल मुसकान तैर रही थी। ध्यातव्य है कि इस ‘चयन मंडली’ में ‘इग्नू’ के निदेशक, वरिष्ठ अधिकारी व अन्य ख्यात संस्थानों-विश्वविद्यालयों के अधिकारी विद्वान भी शामिल थे। यहां पहले सवाल की ‘कॅरालरी’ (Corollary) शायद यह कि फिर यहां क्यों आना चाहते हैं आप। यह भी कि आप यहां की नौकरी के लायक नहीं। दूसरे प्रश्न के निहितार्थ की व्यंजना यह कि केवल बिहार के विधानमंडल में ही यह सब होता है, अन्यत्र नहीं। कहना न होगा कि इन दोनों प्रश्नों की काया में कुछ अन्य गुप्त-सुप्त बिहार सिंड्रोमी सोच भी तो उनके काम कर ही रहे होंगे।
एक प्रसंग बिहार के विवादित राष्ट्रभाषा पुरस्कार का। पंकज विष्ट (समयांतर । मई २००१) ने बिहारी साहित्यकारों-नचिकेता, मधुकर सिंह, प्रेम कुमार मणि आदि द्वारा राष्ट्रभाषा पुरस्कार लौटा दिए जाने (हालांकि पुरस्कार देने की विवादित घोषणा भर हुई थी, दिया नहीं गया था।) की तारीफ की, पर सबसे पहले पुरस्कार न लेने की घोषणा करने वाले व सर्वाधिक मुखर प्रतिरोध करने वाले जाबिर हुसेन का नामोल्लेख करना तक उन्होंने उचित नहीं समझा। क्या ऐसा भूलवश हुआ होगा? गालिबन, पंकज विष्ट जाबिर हुसेन को साहित्यकारों की कोटि में शुमार करना ही नहीं चाहते या कि खालिस राजनेता ही मानते हैं। अब इसे क्या कहिएगा, कोई लेखकीय-बौद्धिक सिंड्रोम…! प्रसंगवश, विष्ट जी का यह संपादकीय वक्तव्य ‘हम विरोध करना कब सीखेंगे!’ शीर्षक से आया है। और हां, यह जरूर है कि उनका यह वक्तव्य इन पुरस्कार-उदासीन बिहारी लेखकों के ‘स्टैण्ड’ का समर्थन ही करता है।
ऐसा क्यों है कि ‘बिहार सिंड्रोम’ का नकारात्मक सिंड्रोम गढ़नेवाले किरीट रावलों, सिंड्रोम रचयिताओं को बिहार की खासियतों पर कोई सकारात्मक सिंड्रोम रचने को नहीं सूझता? ये खासियतें उनका ध्यानाकर्षण क्यों नहीं कर पातीं?
देश की शीर्ष-नामचीन सिविल, प्रावैधिक, प्रबंधकीय व अन्य संस्थाओं-आई आई.टी., आई.आई.एम..
साक्ष्य । ३०५
जे.एन.यू. आदि-की प्रवेश परीक्षाओं में सफल छात्रों की भारी व प्रभावी संख्या किस तथ्य की ओर इशारा करती है? फिर, प्रतिष्ठित सरकारी और गैरसरकारी सेवाओं-नौकरियों में भी बिहारी प्रतियोगियों का प्रभूत संख्या में चयन इनकी विशिष्ट प्रतिभा व दमखम का परिचायक नहीं? जबकि गौरतलब यह है कि इनमें चयन के लिए आयोजित साक्षात्कारों में बिहारी प्रतिभागियों के प्रति प्रायः उपेक्षा भाव या नकारात्मक रवैया अपनाया जाता है। यानी, ‘इंटरव्यू’ स्तर पर सम्यक् मूल्यांकन न होने, कमतर होने के बावजूद लिखित परीक्षाओं में अपने उच्च व प्रखर मेधा प्रदर्शन के बलबूते ये अंतिम चयन सूची में अपना नाम दर्ज करवा लेते हैं। बुलंद इरादों से हार खाकर असफलता भी पनाह मांगती है!
अब कुछ ‘अवांतर’ (यहां अवांतर = बिहार से बाहर की) कथाएं-जो किसी ‘सिंड्रोम’ का रूपाकार लेने का दम रखती हैं और एतदर्थ सिंड्रोम-सर्जकों की मुखापेक्षी हैं। सिंड्रोम-सर्जकों का काम आसान करने के लिए उनका संभावित नामकरण भी किए देता हूं।
कुछ न्यायिक सिंड्रोम : समाज सेविका (साथिन) भंवरी बाई बलात्कार कांड में राजस्थान के एक न्यायालय में विद्वान न्यायाधीश ने एक दूरदर्शी फैसला सुनाया कि एक सवर्ण पुरुष दलित महिला से
बलात्कार कर ही नहीं सकता।
भारत सदृश एक समाजवादी-स्वतंत्र राष्ट्र (वैसे, १९९१ के उदारीकरण, निजीकरण और भूमंडलीकरण के बाद अपना देश कितना समाजवादी और स्वतंत्र रह पाया है, आपसे छुपा नहीं है) की न्याय- व्यवस्था ‘छोटे-बड़े’ का कितना ख्याल रखती है! राव, जयललिता और हर्षद तीनों के भिन्न-भिन्न प्रकृति के भ्रष्टाचार के मुकदमे अलग-अलग कोर्ट में हुए, मगर सजा (!) सबको एक जैसी मिली (भारतेन्दु की ‘अंधेर नगरी’ – टके सेर भाजी, टके सेर खाजा)। मजा तो यह कि किसी को जेल जाना ही नहीं पड़ा। दूसरी तरफ ‘यूपी’ के एक श्यामसुंदर मिश्रा का उदाहरण देखिए, उसे ३६ वर्षों तक जेल में सड़ना पड़ा, बिना कोई मुकदमा चले। पश्चिम बंगाल के अजय घोष ने ३७ वर्षों तक बिना मुकदमा, जेल की चक्की पीसी। दिल्ली के बग्गा सिंह को १२ वर्ष जेल की हवा खानी पड़ी, महज इस अपराध में कि एक ट्रक से उसने लिफ्ट मांग ली थी, आगे चलकर ट्रक चालक के साथ उसका भी चालान कर दिया गया और १७१वीं तारीख पर सुनवाई के बाद बिना कोई आरोप के वह ‘बाइज्जत’ रिहा किया गया। (राष्ट्रीय सहारा के एक समाचार पर आधारित)
उच्चतम न्यायालय ने माना है कि हिन्दू देवी-देवता, उनकी मूर्तियां भी वैध व्यक्ति (legal person) हैं। इस न्याय-निर्णय का संदर्भ यह है कि पटना हाईकोर्ट के एक भूमि विवाद के ‘वाद’ में किन्हीं जज का मत था कि अमुक देव छद्य/नकली था। ‘केस’ दिल्ली पहुंचा और यहां देश की शीर्ष न्यायिक संस्था, सुप्रीम कोर्ट के एक विद्वान न्यायाधीश का उलट फैसला आया कि हिन्दू कानून के मुताबिक ‘झूठा/नकली’ देव हो ही नहीं सकता। शास्त्रों एवं अन्यान्य संदर्भ ग्रंथों के हवाले सुधी न्यायवेत्ता ने बताया कि मूर्तियों के ‘पवित्रीकरण’ व ‘प्राण-प्रतिष्ठा’ के पश्चात् देव झूठा/नकली/मूर्तिमात्र रह कहाँ जाता है, वह जीवंत-साक्षात् हो जाता है और फिर मनुष्य की भांति किसी जमीन-जायदाद के स्वामित्व
३०६ / साक्ष्य
का अधिकारी बन जाता है, यानी दिव्य भूस्वामी’ बन जाता है। यहां एक जबरदस्त सवाल की तरफ इशारा हो सकता है कि मूर्तियों को जीवंत देवता का बाना पहना व भूपति बनाकर अभी के बाहीच वर मानसिकता के जो जज जमीदारों का संरक्षण कर रहे हैं, गर उनकी जगह कोई ऐसा जज आए जो पवित्र बाह्यणिक अनुष्ठानों, तंत्रों-मंत्रों को सुनना भी गवारा नहीं करे- तब क्या होगा इन दैव भूस्वामियो का, इनके नाम पर कब्जाई गई अपार धन-संपत्तियों का, उनके भोक्ताओं का! (‘दि हिन्दू /जून ९, १९९९)
हमारे न्यायालयों में औपनिवेशिक अतीत के कई अभिसंकेत और आचार अब भी किसी ‘सिंड्रोम’ की मानिंद न्यायिक बहसों-कार्यकलापों में ढोये जा रहे हैं। औपनिवेशिक ‘माई-बाप’ वाली सरकार की अदालती बहसों में प्रयुक्त होने वाले आचार-संबोधन ‘माई लॉर्ड’, ‘योर हाइनेस’, ‘ऑर्डर-ऑर्डर’ जैसे जुमले-जो गुलाम मानसिकता के द्योतक है-अब भी प्रयुक्त होते हैं।
बंद पवित्र-पावन सिंड्रोम ः १९९८ के हरिद्वार कुंभ मेले में शाही स्नान के दौरान ‘कौन पहले डुबकी लगाएगा’ के प्रश्न पर विभिन्न साधु गुटो/अखाड़ों के बीच हुए द्वंद्व के फलस्वरूप जूतमपैजार हो गयी। इन ‘पवित्र’ साधुओं ने ‘अपवित्र’ मुठभेड़ें कीं, एक-दूसरे को आतंकित-अपमानित-प्रताड़ित किया, लूटा, पीटा और जलाया। दरअसल, ये साधु-संन्यासी भी जाति आधारित भेदपरक संगठनों में बटे है। कोई ४८ साल पहले कुंभ मेले में ही जब नागा साधुओं के उम्र जत्थे ने स्नान की उतावली में निहत्थे निर्दोष तीर्थयात्रियों-दर्शनार्थियों को अपने त्रिशूलों से कोंचना शुरू किया तो भगदड़ मच गई। दर्जनों लोग कुचलकर या डूबकर ‘स्वर्ग-सिधार’ गए। कुछ वर्ष पूर्व ‘सिंहस्थ’ (उज्जैन) के कुंभ के अवसर पर ऐसी जानलेवा भगदड़ का दुखद दुहराव हो चुका है। फिर भी हम है कि ईश्वर की शक्ति-सत्ता लौट आने की आशा नहीं छोड़ रहे!
बिहार से भी अधिक मजबूत सामंती ढांचा वाला प्रदेश है राजस्थान। ‘राष्ट्रीय सहारा’ (१५ जून, २००१) की एक खबर के अनुसार वहां के एक गांव में देवी मंदिर में प्रवेश का साहस करने वाले दलित समुदाय के एक व्यक्ति को कुछ खास जाति के लोगों ने पीट-पीट कर मार डाला। मृतक का अपराध यह था कि उसने वहां की प्रभु जाति-गुर्जर व राजपूत की कुलदेवी के मंदिर में पूजा-अर्चना (जबकि देवी अवकाश पर थीं!) का ‘दुस्साहस’ किया था।
इसी राजस्थान की ‘वीर-धरा’ पर १९८५ में देवराला में एक लोमहर्षक-दिल दहलाने वाली घटना घटती है। एक युवा महिला (रूपकंवर) को किसी विशिष्ट जातीय आन-बान औ’ शान की रक्षा में पति की चिता की धधकती अग्नि में बर्बरतापूर्ण ढंग से जिन्दा झोंक दिया जाता है (रक्षा में हत्या!) और चिता के पास इकट्ठा उन्मत्त, वीभत्स, निर्दयी, नपुंसक समाज ‘सती माता की जय’ का खूनी उद्घोष करता है। ‘सती’ का महिमामंडन कर ‘चिता’ पर मेले का विद्रूप आयोजन किया जाता है। हद दरजे की दरिंदगी, यह नीचता की पराकाष्ठा भी कोई ‘सिंड्रोम’ चिपकने-चिपकाने के लायक नहीं?
साक्ष्य ।
३०७
एकाच मीडियार्ड सिंड्रोम : हिन्दी मीडिया ने एक दौर में युवक-युवतियों के दिमागों को गलत व भ्रमपूर्ण सूचनाओं, विद्वेष और घृणा से इतना लबालब भर दिया था कि ‘रामरथ’ भले ही आज भारत की सड़कों को-सोमनाथ से अयोध्या तक-रौंद नहीं रहा है, मगर वह लोगों के दिमाग को आज भी रौद रहा है।
लोकतंत्र के इस चौथे खंभे, मीडिया, का एक अवयव पत्रकार बिरादरी का कुछ हिस्सा मंडल कमीशन लागू होने और आडवाणी की रथयात्रा के बाद प्रगतिशीलता का लबादा उतारकर ‘दक्षिणपंथी कर्म’ में लग जाता है। बुद्धिजीवियों के खास वर्ग का ध्यान रखकर सांप्रदायिक पार्टियों के पक्ष में लिखना और तर्क जुटाना शुरू कर देता है। ‘प्रगतिशील’ नामवर अंग्रेजी पत्रकार रामचंद्र गुहा कह बैठते हैं कि मुसलमानों से अधिक प्रगतिशील तो राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ है।
एक वैज्ञानिक सिंड्रोम : केन्द्रीय मंत्री मुरली मनोहर जोशी ने ज्योतिषशास्त्र को एक विज्ञान-विषय के रूप में विश्वविद्यालयीय पाठ्यक्रमों में शामिल करने का नायाब निर्णय किया है। कुछ ऐसा ही इरादा राजस्थान सरकार का भी लगता है। ‘आउटलुक’ (जून ११, २००१) के अनुसार, प्रदेश की विदुषी महिला मंत्री ने विधानसभा में एक बहस के दौरान संस्कृत को एक वैज्ञानिक भाषा (जाने क्यों देवभाषा के सिंहासन से उतारकर, दैव यह क्या हो रहा है!) घोषित किया है। उन्होंने केन्द्रीय सरकार की तर्ज पर हस्तरेखा ज्ञान और ज्योतिषशास्त्र को भी विज्ञान करार दिया। मजा तो यह कि जुदा-जुदा विचारों वाले विपक्षी दल भी इस मुद्दे का विस्मयकारी रूप से समर्थन करते पाए गए।
और अंतिम सिंड्रोम प्रधानमंत्री के नाम जो प्रधानमंत्री कभी अपने ग्रामीण व १९४२ के ‘भारत छोड़ो’ आंदोलन के क्रांतिकारी लीलाधर वाजपेयी को अंग्रेजी हुकूमत से सजा दिलवाने में सहयोग करता है और खुद आंदोलन का सक्रिय हिस्सा नहीं बनता (फ्रंटलाइन, २० फरवरी, १९९८), बाबरी मस्जिद ध्वंस को राष्ट्रीय भावना का प्रकटीकरण बताता है, चंद्रास्वामियों, साई बाबाओं का ‘पालागन’ कर अंधश्रद्धा निवेदित करता है, वह बुद्धिजीवियों का कोई ‘सिंड्रोम’ नहीं बनकर, गले का हार बनता है।
बिहार का जीवन और समाज जड़ और थमका हुआ नहीं है, प्रत्युत् कई अर्थों में परिवर्तित हो रहा है। परिवर्तन की इस बयार की ताजा मिसाल लें। हालिया संपन्न बिहार पंचायत चुनावों में बिना किसी आरक्षण के सामान्य सीटों पर भी अपने संघर्ष के बूते १२४ दलितों ने जीत हासिल की है। हालांकि १५ प्रतिशत की उनकी आबादी की तुलना में महज १.५७ प्रतिशत सीटों पर ही उनकी जीत हुई है, पर इस छोटी संख्या में भी यह ‘बड़ी जीत’ इस मायने में है कि इसे एक नए सामाजिक उभार और सामाजिक हलचल के रूप में देखा जा सकता है। समाज ने इस वर्ग की स्वाभाविक नेतृत्वकारी भूमिका स्वीकारना शुरू किया है। कहते हैं, क्रांति अपने ही शिशु का भक्षण कर लेती है, को लील जाती है, पर यहां बिहार में यही क्रांति अपने शिशु का उर्वर पोषण-सिंचन करती है। बिहार का सांप्रतिक उथल-पुथल इसी मायने में गहराते जाते प्रजातंत्र का द्योतक है। कभी संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में ’सिविल वार’ ने ऐसे ही प्रजातंत्र की नींव को मजबूती प्रदान की थी। ख्यात समाजशाली प्रो. सामिन्यदानंद काफी महत्वपूर्ण तथ्य रेखांकित करते हुए कहते हैं कि बिहार का यह परिवर्तन गांव के “बौशल एनॉटोमी’ आपसी भाईचारे, सामाजिक-आर्थिक संबंध (विभिन्न जाति समूहों के), शक्ति- संरचना और उत्पादन-संबंध में टूटन-बदलाव, महत्वकांक्षा के स्तर, जातिगत-वर्गगत तनाव में बढ़ोतरी आदि – में परिलक्षित होते हैं। जिन्हें अपना भाग्य स्वयं निर्मित करने की मनाही थी, उन्होंने अपना वजूद दिखाना शुरू किया है। ‘मौन की संस्कृति’ का प्रतिस्थापन ‘मुखर प्रतिरोध’ से हो रहा है।
बहरहाल, बिहार की दयनीयता की पड़ताल करें तो इसे मलिन चित्रित करने वालों, गरियाने वालों में दिल्ली के मीडिया, प्रशासन, राजनीति तथा बौद्धिक जगत में अटे-बंटे बिहारी ही सर्वाधिक आगे पाए जाएंगे। ये दरअसल, ‘बिहारीपन’ से ऊपर उठे वो बिहारी हैं जिनकी सोच की ‘प्रगतिशीलता’ केवल इसी (सिंड्रोमी) रूप में मुखर-प्रकट हो सकती है। इन विभीषणों की पांत, फिलवक्त, अंतहीन है। ये अनिवासी, प्रवासी व स्वयंभू प्रगतिशील बिहारी या ‘बिहार सिंड्रोम सर्जक’ अन्य लोग बिहार पर व्यंग्य कर भले ही क्षणिक संतोष पा लें, प्रसन्नता महसूस कर लें, पर ये दरअसल, आगत- अनागत भय से व्याकुल होकर चीखने वाले वे लोग हैं जो शायद बिहार में हो रहे सकारात्मक परिवर्तनों से या तो परिचित ही नहीं या फिर गहरे डरे-सहमे हैं।
वैसे भी, बिहार की अस्वस्थता जितनी बाह्य कारणों से है, उतनी भीतरी कारणों से नहीं। बिहार को चाहिए एक ऐसा प्रखर सामाजिक-बौद्धिक नेतृत्व, जो हमारी अन्दरूनी ताकत को जगाकर भीतर- बाहर की व्याधियों से लड़ लेने का सामर्थ्य बनाए, जज्बा पैदा करे। और फिर, कालिदासी कुल्हाड़ी चलाने वाले बिहारियों को अब बस भी करना चाहिए। फिर देखिए, बिहार के अतीत का गौरव वापस पुनः कैसे लौट नहीं आता है।