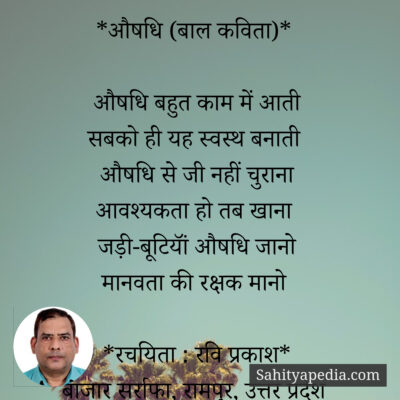संवेदनाएँ सस्ती हो गईं!
चौखट पर टिकी आँखें
गली से गुजरते डाकिया से लपककर पूछ ही लेतीं थीं!
मेरे नाम की चिट्टी तो नहीं आई कहीं से?
कड़ी दोपहर में नंगे पैर दौड़कर
कुल्फी लाने में न शर्म थी
न बीमार होने का डर। कोई भी तीन लकड़ियाँ ,कपडे़ की गेंद
और मुहल्ले की किसी भी गली में
वनडे डन्डे के सहारे शुरू हो जाता था।
शाम से गाँव में अलाव
धीरे-धीरे घेरा बडा़ होता
जगह सबको मिल जाती थी
ठिठुरती ठंड में तापने को।
शहर भी तब गाँव हुआ करते थे
पंक्षियों के झुंड यहीं से गुजरते थे
अकेली टिटहरी रात में शोर करती थी
हवा ,कहीं दूर होती भक्तों की ढोलकी
की आवाज से ,आधी रात और सुबह
होने में अभी देर है ,संदेश लाती थी।
अभी भी सब कुछ शेष है
मगर यूं जैसे सुगंध !कहीं
अब धीरे-धीरे सब ,दो नीले सही के निशानों की परिधि के मध्य सिकुड़ता जाता है- – -!
आप समझ ही गये होगें! आपका अगूंठा क्यों थम गया
यूं लगता है,संवेदनाएँ सस्ती हो गयीं हैं?
हवाएँ दूषित और खुशबुएँ यांत्रिक हो गयीं हैं!
मुकेश कुमार बड़गैयाँ ,कृष्णधर द्विवेदी