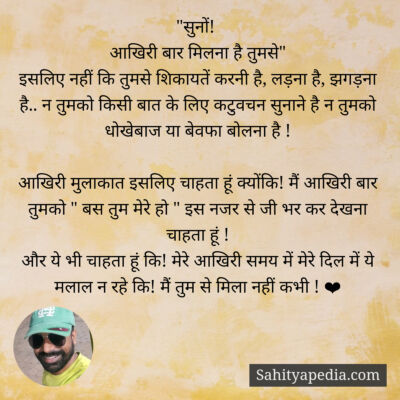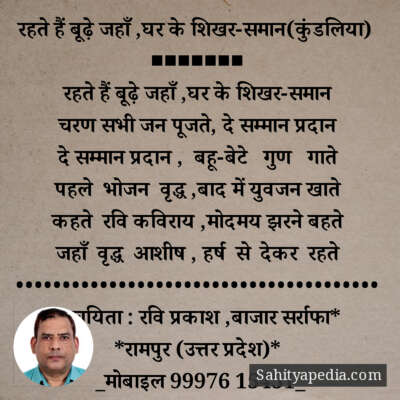वो रोज़ निकल पड़ती है
वो निकल पड़ती है
भोर होते ही मुंह अंधेरे
अलसाई देह को झकझोरती
अपनी उनींदी आंखों में
ढेर से श्वेत श्याम स्वप्न लिए
रास नहीं आते उसे रंग भरे स्वप्न
क्योंकि
जानती है वो अपनी सीमाएं
जो उसे दूर ही रखती है
रंगीन मायाजाल से
जिसकी वो कभी
हकदार भी नहीं हो सकती ।
कांधे पर बड़ा – सा
बोरानुमा थैला लटकाए
जो दो – तीन थैलियों से
जोड़कर बनाया लगता है ।
भटकती है कचरे की तलाश में
इधर – उधर
और खोजती है उसमें
अपनी जिजीविषा
मेरे – तुम्हारे इसके – उसके द्वारा
व्यर्थ समझ फेके गए
पुरानी बोतल , गत्ते के टुकड़े
प्लास्टिक टूटे फूटे
पन्नियां , धातु के टुकड़े
और न जाने क्या- क्या
सब बेकार फालतू
पर उसके लिए
आधार रोटी का
आधार वस्त्र का
आधार सर छुपाने की जरूरत का
आधार मैले कुचैले कपड़ों में ढंके
बच्चों के भविष्य संवारने का
आंखों में स्वप्न संजोए
वो रोज़ निकल पड़ती है ।
अशोक सोनी
भिलाई ।