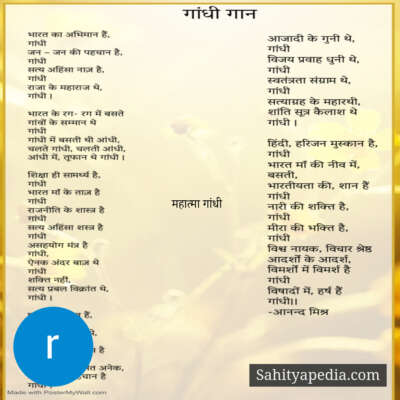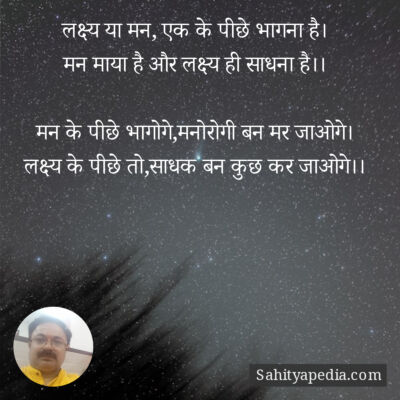विश्व रंगमंच दिवस
विश्व रंगमंच दिवस पर विशेष
#पंडित पी के तिवारी (लेख़क एवं पत्रकार)
#बदलता बक्त और रंगमंच
आज विश्व रंगमंच दिवस है ,जीवन के रंगमंच पे रंगमंच की मूल विधाओ का सीधा नाता है ,वे आईने की रूप में समाज की अभिव्यक्तियों को व्यक्त करती है ,सभ्यता के विकास से रंगमंच की मूल विधाओ में परिवर्तन स्वभाविक है किन्तु लोकरंग व लोकजीवन की वास्तविकता से दूर इनदिनों आधुनिक माध्यमो यथा टीवी सिनेमा और वेब्मंच ने सांस्कृतिक गिरावट व व्यसायिकता को मूल मंत्र बना लिया है जिससे मूल विधाए और उनके प्रस्तुतिकारो को वह प्रतिसाद नहीं मिल पाया है जिसके वो हक़दार है|
हिन्दी रंगमंच-नाटक का जो रूप स्वरूप, विधान आज हमारे सामने है, वह समय समय पर हुये परिवर्तन और प्रयोगधर्मिता का ही परिणाम है. रंगमंच के नाटक ने नये आयाम स्थापित कर नये धरातलों को छुआ है, इसमें दो राय नहीं है. किन्तु साथ ही साथ आधुनिक रंगमंच ने कई प्रश्नों को भी जन्म दिया है. विचार नाटक की रीढ की हड्डी की तरह होता है. किन्तु प्रयोग के नाम पर हो रहे अधिकतर नाटकों में पिछले वर्षों से विचार ही लुप्त होता जा रहा है. विचार के स्थान पर आज शरीर और उसके संचालन को अधिक महत्त्व दिया जा रहा है. इसका परिणाम यह हो रहा है कि नाटक एकायामी न होकर जटिल और बहुआयामी होता जा रहा है. लगता है आज का नाटककार एक साथ ही बहुत कुछ देना चाहता है और निर्देशक प्रयोग के नाम पर कुछ भी नया कर दिखाने की ललक में एक बिन्दु पर नहीं ठहर पा रहा है.
जहाँ तक नाटकों में प्रयोगधर्मिता का प्रश्न है, परम्परा और प्रयोगधर्मिता के अन्तःसंघर्ष ने ही नाटक को नया रूप दिया है. संवेदन और शिल्प ने ही नाटक को बहुरंगी बनाया है. नाटकों के क्रमिक विकास की बात करते हुए यदि हम वैदिककाल की बात करें तो संस्कृत नाटकों में भी प्रयोगधर्मिता के दर्शन होते हैं. वेदों में यम-यमी, पुरुरवा-उर्वशी, अगस्त्य-लोपामुद्रा आदि के जो संवाद सूक्त हैं उसमें नाटकीय कथोपकथन के गुण विद्यमान हैं. नाटकीय प्रयोग से सम्बन्ध रखने वाली अनेक धार्मिक क्रियाओं का उद्भव वैदिक कर्मकाण्डों से हुआ है.
नाटक की उत्पत्ति भले ही वैदिक संवाद सूक्तों से हुई हो, किन्तु नाटक ने शरीर पुराणों से पाया है. पौराणिक नाटकों की रचनाओं के मुख्य आधार कहीं धर्म प्रतिपादन, कहीं खेल, कहीं युद्ध, कहीं वध तो कहीं काम का वर्णन रहे हैं. उस समय के नाटककार चाहे अश्वघोष हों चाहे भास, शूद्रक, भवभूति या कालिदास. उनकी रचनाओं का मुख्य आधार महाभारत की घटनाएँ रही हैं. भास के तेरह नाटकों में से नौ नाटकों का आधार महाभारत अथवा रामायण रहा है. संस्कृत के सर्वश्रेष्ठ माने जाने वाले कालिदास का नाटक अभिज्ञान शाकुन्तलम् हो चाहे, भवभूति का उत्तर रामचरित, उनमें अधिकतर रामायण-महाभारत की घटनाओं का नाट्य-रूपान्तर ही किया गया है. समय-समय पर प्रयोग भी किये गये हैं और नाटक के सभी तत्त्व उनमें मौजूद भी रहे हैं. समय के अन्तराल के साथ एक परिवर्तन यह हुआ कि इन नाटकों की स्वाभाविकता लोप होने लगी और इनमें रूढवादिता उभरकर सामने आने लगी. नाटकों के संवादों की भाषा पांडित्यपूर्ण होने लगी. दैनिक जीवन की भाषा और नाटक की भाषा की खाई निरन्तर बढने लगी. नाटक आम आदमी से कटकर विशिष्ट वर्ग के लिए रह गया. परिणाम यह हुआ कि संस्कृत नाटकों के रंगमंच का पतन प्रारम्भ हो गया किन्तु संस्कृत के नाटकों ने नाटक की जिन परम्पराओं को जन्म दिया, एक लम्बे समय तक वे परम्पराएँ हिन्दी नाटक को प्रभावित करती रहीं.
पौराणिकता काल स्वरूप और प्रासंगिकता भरत-वाक्य व पूर्व-रंग आदि परम्पराएँ हमारे इन शास्त्रीय नाटकों की ही देन है. ये परम्पराएँ एक लम्बे समय तक चलन में रही हैं और हमारे लीला व लोकनाट्यों में तो यह आज भी विद्यमान है. हमारे लीला नाटकों के प्रसंग महाकाव्यों से लिए गये हैं और हमारी लोकनाट्य शैलियों ने उन महाकाव्यों के उप-प्रसंगों को अपनाया है. इन प्रसंगों के पात्रें की अलौकिकता और उनमें आस्था ही दर्शक का प्रयोजन रहा है. सम्प्रेषण इनका मूल उद्देश्य नहीं रहा है. हमारे लीला नाटकों की तुलना में लोकनाट्य शैलियों में सार्थक प्रयोग किये गये हैं. इनकी प्रस्तुतियों की अगर बात करें तो सम्पूर्ण प्रस्तुति आँगिक अभिनय गायन और संवादों पर आधारित होती है. मंच सज्जा तो होती ही नहीं है. क्योंकि इनका प्रदर्शन किसी भी खुले स्थान पर होता आया है. हाँ, रंगभूषा और रूप सज्जा इनके प्रदर्शन के सहायक तत्त्व ज़रूर होते हैं. एक बात और कि इनके आलेख और प्रस्तुति में बडा अन्तर होता है. आलेख बहुत छोटा होता है और प्रस्तुति उससे दस गुना अधिक होती है. क्योंकि इन नाट्यों में उप-प्रसंग बहुत जोड दिये जाते हैं. जो हमारे शास्त्रीय नाटकों के पूर्व-रंग की तरह होते हैं. प्रायः सभी स्थानों के लोकनाट्यों में यह प्रयोग किये जाते हैं. जैसे गुजरात का भवाई, महाराष्ट्र विदर्भ का खडी गम्मत, बंगाल की जात्र या हमारे राजस्स्थान की लोकनाट्य शैली गवरी या लोकनाट्य खयाल. इन सभी में पूर्व रंग के रूप में वेश या स्वांग लाने की परम्परा रही है. मूल नाटक की प्रस्तुति से पहले नाई का वेश, सेठ का वेश, मालिन का वेश या महाराष्ट्र के लोकनायक खडी गम्मत में ग्वालिन का वेश. इसी तरह आदिवासी नाट्य शैली गवरी में विभिन्न स्वांग वाले पात्र.
ऐसा भी नहीं है कि इस परम्परा का प्रयोग केवल हमारे देश में ही होता है. पश्चिमी देशों व यूनान में भी यह प्रथा प्रचलन में रही है. पश्चिम में इसे करटेन रेजर के रूप में जाना जाता है तो यूनान में कोरस के रूप में. हमारे नाटकों में जो भूमिका सूत्रधार द्वारा अदा की जाती है वही भूमिका यूनान में कोरस के द्वारा अदा की जाती रही है. हमारे यहाँ सूत्रधार एक या दो होते हैं तो यूनान में कोरस में पूरा नृतकों और गायकों का समूह होता है. यूनानी नाटकों की एक विशेषता यह भी होती है कि उनका दृश्य-विभाजन नहीं होता. अनवरत नाट्य-व्यवहार चलता रहता हैं ऐसा नहीं है कि पूर्व रंग के इस एक प्रकार का प्रचलन नाटक के प्रारम्भ में होता हो-यूरोप में नाटक की अवधि बढाने के लिए नाटक के अंत में आफ्टर-पीसेज जोडने की प्रथा भी रही है.
संसार भर में प्रथम महायुद्ध के पश्चात् सभी सृजनात्मक और रचनात्मक विधाओं और मानवीय संवेदनाओं में बहुत बडा परिवर्तन हुआ. 1890 के आसपास के इस समय को हम प्रयोगधर्मी संक्रमण काल भी कह सकते हैं. इसी दौर में परम्पराओं से हटकर आधुनिक रंगमंच के नाटक की नींव रखी गई. यही दौर हमारे प्रयोगधर्मी नाटककार भारतेन्दु जी का काल रहा. इसी काल में हिन्दी के साहित्यिक रंगमंच की स्थापना हुई. यह दौर व्यवसायिक पारसी रंगमंच के उत्कर्ष का भी दौर था. भारतेन्दु हरिश्चन्द्र ने व्यवसायिक रंगमंच के भडकीले-रोमांचक प्रदर्शनों के स्थान पर रंगमंच की नई परम्पराओं की शुरुआत की. ना केवल प्रदर्शनों के स्तर पर बल्कि नाटक लिखने की नई परम्पराओं को भी जन्म दिया. उन्होंने अकेले भाषा साहित्य के माध्यम से समाज और राष्ट्र को नई दिशा दी. सदियों से चली आ रही नाटकों की पुरानी परम्पराओं पूर्व रंग, सूत्रधार, यम-यमी, नंदी आदि की प्रथाओं को तोडा. उन्होंने नाटकों की भाषा को सहज और अर्थपूर्ण बनाया. उन्होंने अपने नाटकों व कविताओं में दो भाषाओं का प्रयोग किया-खडी बोली और ब्रजभाषा. वे बहुत अच्छे कवि और व्यंग्यकार भी थे. उनके पिता जी गिरधरदास भी लेखक थे. उन्होंने एक नाटक भी लिखा था नहुष. शीर्षक से स्पष्ट है कि अवश्य ही यह नाटक किसी पौराणिक प्रसंग पर आधारित होगा. भारतेन्दु जी ने नाटकों में आम व्यक्ति की त्रसदियों का समावेश किया. लिहाजा आम आदमी नाटकों से जुडता चला गया. वह निर्विवाद सत्य है कि भारतेन्दु जी ने आधुनिक नाटक की नींव रखी.
भारतेन्दु युग के बाद द्विवेदी युग नाटक के विकास की दृष्टि से महत्त्वहीन रहा. इस दौर में कुछ नाटकों के अनुवाद अवश्य हुये और फिर आया प्रसाद युग. जयशंकर प्रसाद जी ने ऐसे नाटकों का सृजन किया, जिनका रंगमंच पर प्रदर्शन सम्भव नहीं था. प्रसाद जी ने अपने नाटकों में बडी सुन्दर भाषा शैली का प्रयोग किया. लेकिन उनके नाटक गूढ और गम्भीर थे. उनकी गम्भीरता को देखकर उस समय एक प्रश्न उठा था कि नाटक और रंगमंच में कौन श्रेष्ठ है? स्पष्ट है कि रंगमंच के प्रयोग उन नाटकों में नहीं के बराबर थे. उनके नाटक ऐतिहासिक और पौराणिक थे.
किन्तु प्रसाद जी के पश्चात् उपेन्द्रनाथ अश्क ने अपने नाटकों को रंगमंच से जोडने का प्रशंसनीय प्रयास किया. उन्होंने अपने नाटकों में मध्यमवर्गीय जीवन की विसंगतियाँ दर्शाते हुए नाटक को आम आदमी तक पहुँचाने का प्रयोग किया. उन्होंने अनेक एकांकी नाटक लिखे जिनका प्रदर्शन सफलतापूर्वक रंगमंच पर किया गया. उनके कुछ नाटकों में वैवाहिक उलझनों का यथार्थवादी मनोवैज्ञानिक चित्र्ण बडा सुन्दर है.
लेखकीय स्तर पर प्रयोगधर्मिता का एक अनूठा उदाहरण हमको धर्मवीर भारती जी के काव्य-नाटक अन्धायुग के रूप में मिलता हैं. क्योंकि यहाँ से नाट्य लेखन को एक नया मोड मिलता है. अन्धायुग ने पहली बार हिन्दी नाटक में यह स्थापित किया कि काव्य और नाटक का परस्पर घनिष्ठ सम्बन्ध है और एक श्रेष्ठ नाट्यकृति काव्य का ही एक प्रकार है.
यहाँ मैं थोडा रंगमंच से हटकर रेडियो की बात करना चाहूँगा. सन् 1936 में रेडियो अपने अस्तित्व में आया. रेडियो ने नाट्य प्रस्तुति और लेखकीय स्तर पर बहुत प्रयोग किये हैं. रेडियो का ज़िक्र करना यहाँ इसलिए भी आवश्यक है क्योंकि जिस अन्धायुग नाटक की हम बात कर रहे हैं वह मूलतः रेडियो के लिए ही लिखा गया था. और इसका प्रसारण सर्वप्रथम आकाशवाणी के इलाहाबाद केन्द्र से किया गया. यही नहीं सुप्रसिद्ध नाटककार मोहन राकेश का बहुचर्चित नाटक आषाढ का दिन भी मूलतः आकाशवाणी के लिए लिखा गया नाटक है जिसका सर्वप्रथम प्रसारण जालन्धर से किया गया. इसी तरह जगदीशचन्द्र माथुर का क्लासिक नाटक कोणार्क भी मूलतः रेडियो के लिए लिखा गया नाटक है. रंगमंच के कई प्रतिष्ठित नाटककार रेडियो की ही देन हैं. रेडियो ने उन श्रेष्ठ नाटकों का प्रसारण किया जिनका प्रदर्शन रंगमंच पर संभव नहीं था. उनमें जयशंकर प्रसाद, सेठ गोविन्ददास, डॉ. रामकुमार वर्मा, उदयशंकर भट्ट जैसे प्रसिद्ध नाटककारों के नाटक जैसे अजातशत्रु, स्कन्दगुप्त, जनमेजय का नाग-यज्ञ, ध्रुवस्वामिनी, राज्यश्री जैसी रचनाएँ शामिल हैं.
इसी दौर में नेशनल स्कूल ऑफ़ ड्रामा की स्थापना हुई. संगीत नाटक अकादमी अस्तित्व में आई. इप्टा, पृथ्वी थियेटर यूनिट आदि भी अस्तित्व में आये. इन्होंने हिन्दी रंगमंच के आधुनिक स्वरूप निर्माण व विकास में महत्त्वपूर्ण योगदान दिया. यह प्रयोगधर्मिता का प्रमुख दौर रहा और इसी दौर ने कई सुप्रसिद्ध आधुनिक नाट्यकारों को दिया. जैसे डॉ. लक्ष्मीनारायण लाल, सुरेन्द्र वर्मा, रमेश बक्षी, सुशील कुमार सिंह, मुद्राराक्षस, शंकर शेष, ज्ञानदेव अग्निहोत्री, सर्वेश्वर दयाल, नरेन्द्र कोहली, बृजमोहन शाह, असगर वजाहत आदि.
राष्ट्रीय स्तर पर चर्चित-इन नाटककारों ने जर्जर विगलित रूढयों पर प्रहार कर यथार्थवादी अभिव्यक्ति के नाटकों की रचना की. प्रयोगधर्मी नाटककार डॉ. लाल के नाटक एक सत्य हरिश्चन्द्र, मादा कैक्टस, कफ्र्यू, व्यक्तिगत आदि. सुरेन्द्र वर्मा के नाटक द्रौपदी, सूर्य की अन्तिम किरण से सूर्य की पहली किरण तक आदि इसके उदाहरण हैं. इसी प्रकार रमेश बक्षी का देवयानी कहना हैं. मुद्राराक्षस का मरजीवा-यौर्स फ़ेथफुली. शंकर शेष के एक और द्रोणाचार्य, कोमल गांधी, फंदी. हमीदुल्ला के दरिन्दे, उलझी-आकृतियाँ समय सन्दर्भ. सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का बकरी. ज्ञानदेव अग्निहोत्री का शुतुरमुर्ग. मणि मधुकर के रस गंधर्व और बुलबुल सराय आदि. बृजमोहन शाह का त्र्शिंकु-ये सभी नाटक प्रयोगधर्मिता के उदाहरण हैं. कुछ नाटक एब्सर्ड शैली की तर्ज़ पर भी लिखे गये जिनमें लक्ष्मीकान्त वर्मा का रोशनी एक नदी, सत्यव्रत सिन्हा का अमृत-पुत्र् शामिल हैं. एब्सर्ड शैली रंगजगत् में बडे विवाद का कारण रही है. इसके जनक जर्मनी के नाटककार यूगन बेर्थाल्ड फ्रेडरिक ब्रेख्त हैं. 1898 में उनका जन्म हुआ और स्थापित आदर्शों की धज्जियाँ उडाने वाला उनका पहला नाटक ड्रम्स इन द नाइट उन्होंने 1922 में लिखा.
एब्सर्ड शैली अलगाव की तकनीक है, जो एलिएनेशन कहलाती है. यह मंच पर संगीत के साथ सूचना देकर केवल नाटक के कार्यव्यवहार को यथार्थ दृश्य के रूप में प्रस्तुत करती है. संवादों को गीतों से अलग कर पाठक के विषय का खरा प्रस्तुतीकरण कर दर्शकों को भावनात्मक बहाव से रोकती है.पाश्चात्य देशों में एब्सर्ड शैली के नाटक भले ही सफल रहे हों किन्तु भावनाप्रधान हमारे देश में विचार एवं भावहीन नाटक दर्शकों को प्रभावित कर पायेंगे, इसमें संदेह है.आज के पलपल परिवर्तित होते वैज्ञानिकयुग में समयानुकूल परिवर्तन और प्रयोग नाटकों की माँग और आवश्यकता है. किन्तु प्रयोग के नाम पर कुछ भी कर दिखाना बेमानी है. प्रयोग की एक सीमा होनी चाहिए. क्योंकि हर वर्ग का दर्शक नाटक के साथ जुडा रहता है. उसे यह कहने का अवसर नहीं देना चाहिए –
मानवता की सेवा में रंगमंचकी असीम क्षमता समाज का सच्चा प्रतिबिम्बन है। रंगमंच शान्ति और सामंजस्य की स्थापना में एक ताकतवर औज़ार है लोगों की आत्म-छवि की पुर्नरचना अनुभव प्रस्तुत करता है,सामूहिक विचारों की प्रसरण में ,समज की शान्ति और सामंजस्य का माध्यम है ,यह स्वतः स्फूर्त मानवीय, कम खर्चीला और अधिक सशक्त विकल्प है व समाज का वह आईना है जिसमें सच कहने का साहस है। वह मनोरंजन के साथ शिक्षा भी देता है।
भारत में भारतेन्दु हरिश्चन्द्र के नाटकों व मंडली से देश प्रेम तथा नवजागरण की चेतना ने तत्कालीन समाज में उद्भूत की जो आज नही अविरल है अन्धेर नगरी जैसा नाटक कई बार मंचित होने के बाद भी उतना ही उत्साह देता है .कालिदास रचित अभिज्ञान शार्कुंतलम् राकेश का आषाढ का एक दिन मोलियर का माइजर धर्मवीर भारती का अंधायुग विजय तेंदुलकर का घासीराम कोतवाल श्रेष्ठ नाटकों की श्रेणी में हैं।भारत में नाटकों की शुरुवात नील दर्पण ,चाकर दर्पण , गायकवाड और गजानंद एण्ड द प्रिंस नाटकों के साथ इस विधा ने रंग पकड़ा ।
समय के गर्भ में २०१० -२०१५ ईसा पर्व मिश्र के सम्राट सिसोस्ट्रियम के काल में संभवतः पहला नाटक लिखा गया,पाश्चात्य विधाए आपेरा से रंगमंच हेपनिंग्ज , चेम्बर थियेटर , कैफे थियेटर , टैरेस थियेटर की शैली में के रूप में मंचित हो रहे हैं।शैक्सपीयर लिखित ओथेलो , मैकबैथ , हेमलेट , किंगलियर यूनिवर्सल थीम पर आधारित उनके सर्वश्रेष्ठ नाटक हैवी सोफोक्लीज के त्रासदी पर आधारित नाटक एंटीगनी , इडिपस अलग पहचान रखते हैं।
लेकिन वास्तविक तौर पर आज हिन्दी रंगमंच की स्थिति दयनीय है, अच्छे लेखन और नाट्यकर्मी का अभाव है। शौकीया नाटक करने से हिन्दी रंगमंच विकसित नहीं हो सकता। रंगमंच की सबसे बडी कमजोरी स्थायी जीविकोपार्जन का पूरक न बन पाना है रंगमंच एवं कला की संस्थाओं का विकास सृजन दृष्टि पर निर्भर है, उसमें पुरस्कार, अनुदान अथवा सम्मान की नींव पर रंगमंच के विकास की कल्पना बेमानी है।
साहित्य, कला और संस्कृति की त्रिवेणी माने जाने वाले बिलासपुर में रंगमंच की पहचान को लोकाक्षर ,बिलासा कला मंच ,काव्य भारती ,मड़ई,छत्तीसगढ़ मूय्जिक थेरेपी सहित स्कूल ,महाविद्यालयों ,प्रशासन से लेकर विभिन्न संघटनो ने बनाये रखने का सजग प्रयास किया तथापि कला को मंच दिलाने और उसे अनिरंतर बनाये रखने मे जागरूक प्रयास अभी बाक़ी है ,पिछले दिनों “अग्रज नाट्य दल” ने मंगल से महात्मा की अभिनव प्रस्तुति दी उनकी प्रस्तुति “हरेली से होली तक ” सही मायनो छत्तीसगढ़ के लोकजीवन की गाथा बताती है लेकिन इन् प्रयासों को आम नागरिको की रूचि ,सहभागिता के बिना वर्तमान समाज जो की न सिर्फ टीवी संस्कृति का अनुसरणकर्ता है उसे रंगमंच की मूल विधाओ से कोई सरोकार नही है ,
अपना कहा गर आप ही समझे तो क्या समझे
मजा तब है जब एक कहे और दूसरा समझे.