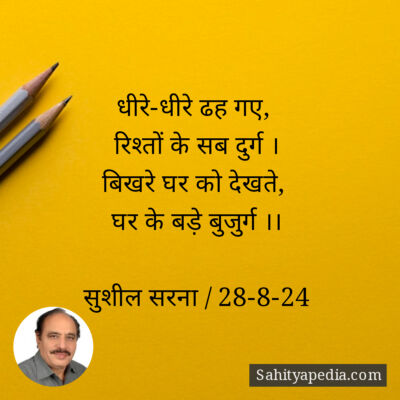पिताश्री रामभक्त शिव (जीवनी)
कहने को कवि मैं हूँ और दोहों को मात्राओं में पिरोने का काम मैंने किया है, मगर इसकी प्रेरणा और मुख्य स्रोत पिताश्री और उनकी राम भक्ति है। यदि वे रामभक्त न होते तो ये किताब भी न होती। 24 जुलाई 1971 ई. में जब मेरा जन्म हुआ, पिताश्री तैंतीस-चौंतीस वर्ष के थे और जब 7 फरवरी 2005 ई. में पिताश्री ने संसार छोड़ा, मैं तैंतीस-चौंतीस वर्ष का था। यहाँ विडंबना देखिये। सन 1938 ई. में शिवरात्रि के दिन पिताश्री पैदा हुए। वह वर्ष 1938 ई. की 28 फरवरी का अन्तिम सोमवार था। और जब 7 फरवरी 2005 ई. में पिताश्री ने सुबह के वक़्त राम-राम कहते हुए शरीर त्याग किया तो यह 2005 ई. में फरवरी का प्रथम सोमवार था। शिव नाम होते हुए भी पिताश्री राम जी के परम भक्त रहे। सनातनी होने के कारण बाक़ी सभी देवी-देवताओं में भी उनकी श्रद्धा थी, मगर राम नाम का उन पर न जाने क्या प्रभाव था? पिताश्री का जन्म: शिवरात्रि के दिन सन 1938 ई. में, ग्राम: काण्डी मल्ली, नैनीडांडा, पौड़ी गढ़वाल, उत्तर प्रदेश (जो कि 2002 ई. से अब उत्तराखण्ड राज्य) में हुआ था। उनकी कर्मस्थली दिल्ली रही और यहीं उनका राम जी के लोक में गमन हुआ।
पिताश्री परम रामभक्त थे। ये बात कई मौक़ों और घटनाओं से भी सामने आई है। पिताश्री को जानने वाले चाहे उनके मित्र, परिचित-अपरिचित व्यक्ति, घर-बाहर, दफ़्तर तक में वह अपने वास्तविक नाम ‘शिव’ की जगह ‘भगत जी’ के नाम से विख्यात थे। उनके दफ़्तर के थैले में भी शंख, घण्टी व भजन की किताबें। रामायण (छोटा संस्करण) हरदम मौजूद रहते थे। दफ़्तर में एक बार थैला बाहर खुली पार्किंग में उनकी साइकिल में ही टंगा रह गया। वो राम धुन गाते हुए दफ़्तर में जब अपनी कुर्सी पर बैठे तो ज्ञात हुआ थैला बाहर रह गया है। थैला लेने वापिस आये तो उन्हें नहीं मिला। पिताश्री वहीँ बोले, जो राम इच्छा। ख़ाली हाथ वापिस दफ़्तर में ही चले गए। शाम को छुट्टी होने पर वापिस पहुँचे तो देखते हैं, थैला साइकिल पर ही टंगा है। उसमे एक काग़ज़ का पुर्ज़ा था। जिस पर ले जाने वाले व्यक्ति ने लिखा था—”क्षमा करें, मैं थैला ले गया था, पर जब दूर जाकर मैंने थैला खोला तो धार्मिक पुस्तकें, रामायण, शंख, घण्टी मिली। मैं आत्मगिलानी से भर गया। और इसी अपराधबोध के चलते मैं संकल्प करता हूँ कि आगे से कभी ऐसा नहीं करूँगा।”
शुरू-शुरू में कई जगह पिताश्री और ताऊजी संयुक्त रूप से किराये के मकानों में ही रहे। पिताश्री रामायण पाठ करते हुए सबकुछ भूल जाया करते थे। उन्हें रामायण से इतना रस मिलता था कि, क्या कहें? ताऊजी ने एक बार मुझे बताया था कि, “तुम्हारे पिताजी कई बार रामायण पढ़ते-पढ़ते रोने लगते थे।”
“ऐसा क्यों ताऊजी?” मैंने जिज्ञासावश पूछा।
“रामायण में दशरथ मरण का जो वर्णन तुलसीदास जी ने किया है। पुत्र वियोग में राजा दशरथ, राम के वन गमन के उपरान्त तड़पते हैं। और ‘राम-राम’ चिल्लाते हुए मूर्छित हो जाते हैं। इसके पश्चात जब दशरथ मरण के उपरांत उनके शव को तेल में डुबोकर रखा है। इसका बड़ा ही मार्मिक वर्णन बाबा तुलसीदास ने ‘रामचरितमानस’ में किया है। इन सब विषयों को पढ़कर तुम्हारे पिता भी विलाप करने लगते हैं। उनकी आँखों से आँसू ऐसे ही बहने लगते हैं, जैसे राम वियोग में राजा दशरथ कोई और नहीं वह स्वयं हों।”
“ताऊजी तो आप उनको रोकते नहीं थे क्या?” मैं फिर और जिज्ञासु होकर पूछता।
“भाई हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूँ मैं—ऐसे हृदयविदारक प्रसंग मत पढ़ा करो।” ताऊजी मेरी जिज्ञासा शांत करते, “कई बार तो अड़ोस-पड़ोस के लोगों का मजमा लग जाता था। तब उन्हें समझाना पड़ता था कि ये सब रामायण में दशरथ मरण के प्रसंग की वजह से है।”
“तो क्या जब सीता स्वयंवर और अन्य ख़ुशी के प्रसंग रामायण में आते हैं तो पिताश्री की क्या मनोस्थिति होती थी?” अपने बाल मन की जिज्ञासा को शान्त करने की दृष्टि से मैं बातों का क्रम आगे बढ़ता।
“इन प्रसंगों को तुम्हारे पिता ख़ुशी-ख़ुशी पढ़ते और अत्यधिक प्रसन्न होते। रामायण में चारों भाइयों की शादी, जब दशरथ बारात लेकर जनकपुरी जाते हैं। यहाँ तुम्हारे पिताश्री अपने जीवनकाल में दिखी हुई यार-रिश्तेदारों की शादियों का ज़िक्र करते थे! जिसे कक्ष में उपस्थित, सभी लोग आनन्द–मग्न होकर सुनते, उन घटनाओं को तुम्हारे पिता के द्वारा पुनः जीते थे।” तब ताऊजी के शब्दों से मुझे ज्ञात हुआ कि पिताश्री और रामायण से जुड़ी ऐसी अनेक घटनाएँ हैं। कई लोग ये मानते हैं उनके सम्पर्क आये व्यक्तियों को पिताश्री में अजीब-सी आध्यात्मिक ऊर्जा महसूस होती थी! सामने वाले के नकारात्मक विचार उनको देखते ही लुप्त हो जाते थे। अतः अधिकांश व्यक्ति उन्हें ‘भगत जी’ कहा करते थे।
शुरू में पिताजी भंडारपाल व भंडार रक्षक (Store Keeper) थे, सरकारी दफ़्तर में, जो कि वेस्ट ब्लॉक नंबर 7, आर.के. पुरम, सेक्टर-1, नई दिल्ली में स्थित था। यह विकास आयुक्त (हस्तशिल्प), कपड़ा मंत्रालय, भारत सरकार के अन्तर्गत आता है। बाद में पिताश्री पदोन्नति होकर मुख्य लिपिक (Head Clerk) बनकर खान और इस्पात मंत्रालय, शास्त्री भवन, दिल्ली में आ गए थे। जहाँ वह रिटायरमैंट तक रहे। अंत में वे सहायक अधिकारी (Assistant Officer) के पद पर रिटायर हुए। ख़ैर, जहाँ पिताजी भंडारपाल (Store Keeper) थे, उस दफ़्तर में मैंने गरमी की छुट्टियों में वाटरमैन (कूलर में पानी डालने वाले के तौर पे 2 महीने काम किया था) क्योंकि दसवीं में फेल हो जाने के उपरान्त मेरा मन उन दिनों पढाई में नहीं लगता था। तब माताश्री ने कहा कि इसको कहीं लगा दो।
दफ़्तर में भी सब कहते, ‘ये भगत जी का लड़का है।’ तब मैं खुद भी उनसे मिलने आये लोगों को देखता था। हर कोई ‘भगत जी’ कह कर ही उन्हें नमस्ते करता था। कई तो पिताजी के चरणस्पर्श भी करते थे। तो पिताश्री चरण छूने से लोगों को मना करते थे। तब कुछ लोग ये कहते थे, “इसी बहाने रामायण का कुछ पुण्य हमें भी प्राप्त हो जायेगा ‘भगत जी’।”
अकेले में दफ़्तर के कुछ लोग मुझसे कहते थे। यार तुम्हारे पिता जी बड़े ही ईमानदार स्टोरकीपर हैं। दफ़्तर का सारा सामान, स्टेशनरी, फ़ाइल्स, पैन-पेन्सिल, स्याही, रबर आदि सब कुछ उनके हाथ में है। काश! एक दिन के लिए वे हमें स्टोरकीपर बना दें तो दफ़्तर का आधे से ज़ियादा सामान अपने घर में पहुँचा दें। ‘भगत जी’ न खुद कुछ लेते हैं, न हमें लेने देते हैं।
जब मैं उन्हें बताता कि “पिताश्री हमारे लिए भी कभी दफ़्तर से एक पैन तक नहीं लाये। हमेशा बाज़ार से ख़रीद कर लाते हैं।” तो वे हँसने लगते, लेकिन मन ही मन वो पिताश्री की ईमानदारी का लोहा मानते थे। शायद ये सब ईमानदारी उनकी रामभक्ति के कारण सम्भव हो पाई। उन दो महीने दफ़्तर के कुलरों में पानी डालते-डालते मैंने समझ लिया कि ज़िंदगी जीना इतना सहल व सहज नहीं है। उच्च शिक्षा से ही बात बनेगी और मैंने दसवीं, बारहवीं ही नहीं बल्कि दिल्ली यूनिवर्सिटी से वर्ष 1994 ई. में अपनी बी.ए. की डिग्री प्राप्त की। सरकारी नौकरी तो नहीं मिली, मगर आज तक कई कम्पनियों में सम्मानजनक नौकरी की है। इतने वर्षों बाद मैं आज समझता हूँ अगर वो दो महीने “वाटरमैन” डेलीवेजर्स की कठिन ड्यूटी नहीं करवाई गई होती तो जीविका चलने के लिए आज मुझे मेहनत मज़दूरी के कठिन श्रम में न जाने क्या-क्या पापड़ बेलने पड़ते?
‘वाटरमैन’ के काम में मेरा सहयोगी हर्षवर्धन नामका लड़का था। जो मुझसे सात-आठ साल बड़ा था। वो मुझसे अक़्सर कहता था, “मेरा तो बाप मर गया है। तब जाकर मैं मज़बूरी में ये काम कर रहा हूँ।”
“मेरा पढाई से मन उचाट हो गया है, इसलिए मैं शौक़िया ये काम कर रहा हूँ।” जवाब सुन, वो मुस्कुराता। मेरे अन्दर लेखकीय कीड़ा होने के कारण हाज़िर-जवाबी की आदत शुरू से ही रही है। दफ़्तर में आज भी मनोरंजन करने का दायित्व मेरे कन्धों पर ही होता है। उन दिनों काव्यात्मक तुकबन्दियों की शुरुआत हो रही थी और दफ़्तर में पिताश्री के अभिन्न मित्र सरदार रणजीत सिंह जी मज़ाक़ में पूछते, “आज क्या लिखा कक्का?” और मैं नई तुकबन्दी सुना देता। तब खुश होकर सरदारजी कहते, “अपनी आगे की पढाई-लिखाई ज़ारी रखो। तुम्हारे अन्दर साहित्यकार बनने के गुण हैं।” मैं मुस्कुरा देता।
शुरू से ही पान, बीड़ी, सिगरेट, तम्बाकू, गुटका इन सब से पिताश्री को परहेज़ था। शायद रामभक्ति इसका बड़ा कारण थी। इसी कारण हमारे भाइयों में भी इन चीज़ों के प्रति विरक्ति सी रही। पिताश्री को गुज़रे आज पन्द्रह वर्ष हो गए हैं। कभी-कभार शादी-ब्याह, पार्टी के मौक़ों पर हम अब मदिरा सेवन और धूम्रपान भी कर लेते हैं। मगर इन वस्तुओं के आदि हम कभी न हो सके। ये पिताश्री की रामभक्ति के कारण ही सम्भव हो सका। एक लेखक के रूप में, मैं कई बार नास्तिक भी हो जाता हूँ, लेकिन पूजा-पाठ में रमे हुए पिताजी को महसूस करता हूँ तो नास्तिकता का भ्रम टूटने लगता है और राम के प्रति हृदय आस्था-विश्वास से भर उठता है।
सतसंग और धार्मिक कार्यों में पिताश्री बढ़-चढ़कर हिस्सा लेते थे। परिवार को बताये बिना अपनी श्रद्धा से दान-पुण्य भी किया करते थे। सामाजिक, पारिवारिक दायित्व भी वह कुशलता से निभाते रहे। अवैध कालोनी होने के कारण खोड़ा, ग़ाज़ियाबाद, उत्तर प्रदेश का बहुत बड़ी जनसंख्या वाला इलाक़ा है। जहाँ सरकारी सुविधाओं के नाम पर आज तक शून्य पसरा पड़ा है। एक बार मई में काफ़ी गरमी पड़ी और लोग बार-बार घण्टों तक लाइट कटने से दुखी थे। सेक्टर 62 में स्थित उत्तर प्रदेश बिजली दफ़्तर का खोड़ावासियों ने घेराव किया और नारे लगाने लगे। बलवा होने की आशंका से बिजली विभाग वालों ने पुलिस बुला ली। लाठी चार्ज हुआ प्रदर्शनकारी इधर-उधर भागने लगे। पिताश्री अपनी जगह डटे रहे और भीड़ का उत्साहवर्धन करते रहे। एक पुलिस वाले ने उनके पैर पर ज़ोरदार प्रहार किया, तो उनके मुख से स्वतः ही निकला, “जय श्री राम।” उस पुलिस वाले को आभास हुआ कि, किसी ‘भगत टाइप’ व्यक्ति पर उसने प्रहार कर दिया है। इसके बाद उस पुलिसवाले ने माफ़ी मांगते हुए कहा—”गुरु जी आप कहाँ इस भीड़ में आ गए? आप पूजा-पाठ करने वाले कोई भगत हैं, घर जाइये।” इसके बाद पुलिस ने किसी पर लाठी नहीं चलाई और हाथ जोड़कर सबसे चले जाने को कहा। तब खोड़ा में बिजली आने और कटने का एक सुनिश्चित आश्वासन बिजली विभाग के अधिकारियों ने लोगों को दिया और भीड़ घर चली गई। ख़ैर बिजली का तो वही हाल रहा। पिताश्री के पैर को ठीक होने में लगभग दो सप्ताह लगे। कहने की आवश्यकता नहीं कि आज भी उत्तर प्रदेश में आधारभूत सुविधाओं के प्रति सरकार आज़ादी के बाद से ही उदासीन है।
गाँव में दादाजी का बड़ा परिवार, पाँच पुत्र और तीन पुत्रियाँ होने के कारण दोनों बड़े भाइयों पिता शिव सिंह जी और ताऊ चन्दन सिंह जी पर छोटी उम्र में ही कमाने का दायित्व आ खड़ा हुआ था। दादा भूर सिंह किसान थे और दादी दयोंथी देवी एक साधारण गृहणी थी। दादाजी ने परिवार चलाने के लिए किसानी के अलावा राज मिस्त्री का काम भी किया। कांडी गाँव में बनी बैठक दादा जी के कर कमलों द्वारा ही निर्मित है। जो आज जर्जर हालत में है। छोटी उम्र में ही रोज़गार की दृष्टि से पिताश्री नौ-दस साल की उम्र में अपने बड़े भाईसाहब चन्दन सिंह जी के पीछे-पीछे दिल्ली आ गए थे। साउथ एक्स में सर्वेन्ट क्वाटर में दोनों भाई रहने लगे और काम के साथ-साथ पिताश्री ने पढ़ना-लिखना नहीं छोड़ा। शायद रामायण पढ़ने की वृति ने ऐसा करवाया और उन्होंने उच्च शिक्षा, श्रीनगर, गढ़वाल से पास की। हमें पिताश्री अक्सर कहते थे—’तुम लोग ट्यूब लाइट की रौशनी में घर के अन्दर नहीं पढ़ पा रहे हो। हमने बाहर फुटपाथ पर सड़क की रौशनी में रातभर पढ़कर इम्तेहान की तैयारी की है।’
पिताश्री से छोटे तीन भाइयों में बड़े चाचा श्री कल्याण सिंह जी सीमा सुरक्षा बल से सेवानिवृत हुए। मंझले चाचा श्री कुंवर सिंह जी आर्मी से कैप्टन के पद पर सेवानिवृत हुए। जबकि छोटे चाचा श्री मनोहर सिंह जी स्वेच्छा से गाँव में रहे। बड़े चाचाजी ने बी.एस.एफ. में रहते हुए ही पढाई की। जबकि मंझले और छोटे चाचा जी ने दिल्ली से ही 10वीं—12वीं तक की शिक्षा अर्जित की। काकाओं से जुड़े कुछेक रोचक क़िस्से हैं जो मैं यहाँ पाठकों से बाँटना चाहूँगा।
बात शायद सन 1985–86 की है, उन दिनों हम मदनगीर में रहते थे। गरमियों के दिन थे। दिन में हमारा परिवार भोजन कर रहा था कि पड़ोस की सरदारनी आंटी घबराई हुई आई। हमारे घर के सामने एक सिख परिवार रहता था। दरवाज़े से ही आंटी जी पिताश्री से मुख़ातिब होकर ज़ोर से बोली, “भाईसाहब तुसी गल सुनो! एक पुलिस वाला आपका नाम लेकर सबको पूछ रहा है। गली के बाहर खड़ा है। मैंने उनको कुछ नहीं बताया, सीधा आपको बता रही हूँ। भाईसाहब, आप कहीं छिप जाएँ?” हम सब चौंक गए।
“बहन, हम रामभक्त आदमी हैं। हो सकता है पुलिस वाला कुछ जानकारी चाहता हो। मैं मिलके आता हूँ।” पिताश्री ने इतना कहकर घर से बाहर क़दम निकाला ही था कि, सामने बड़े चाचा जी बी.एस.एफ. की वर्दी में हमारा पता ढूंढते-ढूंढते गली के अन्दर तक आ चुके थे और दोनों भाई बड़ी आत्मियता से गले मिले। ये देख सरदारनी आंटी चौंक गई और बग़ल में खड़ी माताश्री पार्वती देवी जी ने उन्हें बताया, “ये मेरे बड़े देवर हैं।” इस तरह सब हंसते-हंसते लोटपोट हो गए। बाद में इस घटना का ज़िक्र चाचाजी से किया तो वो भी ठहाके लगा कर हंसने लगे।
मंझले काकाश्री कुंवर सिंह जी कहते थे, “मुझे पूजा-पाठ की आवश्यकता नहीं, क्योंकि मेरे लिए तो जीते-जी भगवान भाईसाहब और भाभी जी (शिव-पार्वती) हैं।”
सन 1971 में लालक़िले में जब फौज के लिए भर्तियाँ खुली तो मंझले काकाश्री का चयन उसमें हो गया। जब घर जाकर ये बात उन्होंने बड़े भाइयों को बताई तो किसी को यक़ीन नहीं हुआ। अगली सुबह जब काकाश्री चलने की अनुमति लेने लगे तो सबको यक़ीन आया। उसी साल पाकिस्तान ने हिन्दुस्तान पर दुबारा हमला किया था। तेरह दिन चले इस युद्ध में सिपाही की हैसियत से काकाश्री को भी पूर्वी पाकिस्तान (अब बांग्लादेश) जाना पड़ा। जिस दिन काकाश्री वहाँ पहुँचे युद्ध विराम हो गया। उनके युद्ध लड़ रहे अन्य फौजी साथियों ने कहा, “यार कुंवर सिंह आप पहले आ जाते, तो ये युद्ध तभी ख़त्म हो जाता।” काकाश्री बताते थे उन्होंने युद्ध के दौरान बांग्लादेश में काफ़ी नारियल खाये। काकाश्री अत्यन्त हँसमुख और मज़ाक़िया स्वभाव के व्यक्ति थे। पुरानी फ़िल्मों और पुराने गीतों के शौक़ीन थे। ख़ासकर रफ़ी साहब की आवाज़ जितनी मुझे पसन्द थी उतनी काकाश्री को भी। क्रिकेट को काकाश्री मूर्खों का खेल कहते थे। लेकिन क्रिकेट के शौक़ीन हम सभी थे। जिस दिन 1983 का विश्वकप फाइनल था मेरे पिताश्री और ताऊजी आश्वश्त थे कि विजयश्री भारत को ही मिलेगी। ट्रांजिस्टर रेडिओ कानों में लगाए ताऊजी और चाचाजी क्रिकेट का ताज़ा हाल सुनने को हमेशा लालायित रहते थे। ये सब उस वक़्त की घटनाएँ हैं जो लोग रिश्ते निभाया करते थे। रिश्तों को जीते थे। आपस में खूब प्यार-प्रेम-सदभाव से रहते थे।
हमारे पितृ पण्डित जी, व्योम (पहाड़ी में उच्चारण ब्योम किया जाता है।) प्रसाद जी (ग्राम: नैखणा) जिन्होंने हमारे ताऊ, पापा, चाचाओं, भाइयों, बहनों की शादियाँ करवाईं आज भी ग्राम कांडी मल्ली में तमाम संस्कार, पूजा-पाठ वही करवाते हैं तथा उनके छोटे भाई स्वर्गीय मथुरा प्रसाद जी, हमेशा ही पिताश्री को भगत जी कहकर ही उच्चारित करते थे। जब पिछली बार जागर (पूजा की पहाड़ी प्रथा, जिसमें देवी-देवताओं से लेकर, भूत-प्रेत और पूर्वजों की मृत आत्माएँ नाचती हैं।) में परिवार सहित मैं गया था। तब भी पण्डित जी पिताश्री को याद कर रहे थे। मेरे ईश्वर स्वरुप यजमान तो ‘भगत जी’ ही थे। उनके बराबर तपस्वी, पूजा-पाठ करने वाला कोई व्यक्ति मैंने ब्राह्मणों में भी नहीं देखा।
हमारी ग्राम बेलम की बुआ जी का नाम ‘शिवी देवी’ है। वह पिता जी के बाद ही धरा में अवतरित हुई। उन्होंने पारिवारिक शादी-ब्याह के मौक़ों पर कई बातें परिजनों से साँझा की। एक बार वो बोलीं, “दादा (बड़े भाई को गढ़वाली में दादा भी कहते हैं।) तो जन्म से ही भगवान के बड़े भगत थे। पूजा-पाठ में ही रहते थे। वो तो सन्यासी होने जा रहे थे। दादा कहते थे कि, ‘मेरे ताऊ–चाचाओं के सात बच्चे और खुद मेरे चार भाई और हैं। कुल मिलाकर दर्ज़नभर। यदि मैं सन्यासी हो जाऊँ, तो क्या फ़र्क़ पड़ेगा?'”
“अच्छा फिर क्या हुआ दीदी? (पहाड़ में बुआजी को दीदी भी कहा जाता है)” मैंने कौतुहलवश पूछा।
“सन्यास की बात सुनकर सब रोने लगे। तुम्हारे बड़े दादाजी रत्न सिंह बोले, नहीं ऐसा नहीं होगा। तू क़सम खा सन्यास नहीं लेगा। बाक़ी सब ने भी दबाव डाला तो दादा की जन्मपत्री कई जगह भेजी गई, मगर संयोग देखिये पन्द्रह–बीस जगह मिली ही नहीं। अंत में तुम्हारी माता जी से जन्मपत्री मिली। दोनों का नाम भगवानों (शिव–पार्वती) का हैं।” आदर में छोटी होने के कारण बुआ जी मम्मी-पापा का नाम नहीं लेती।
“अच्छा, बड़ी दिलचस्प कहानी है!” मैंने कहा।
“इस तरह दादा को ज़बरदस्ती अँगूठी पहनाई गई। ओहो, अब तुम लोगों ने मुझे गृहस्थ में बाँध ही दिया।” इतना कहकर सब ठहाका लगाने लगे और बुआ जी अपनी यादों की पोटली से कुछ और क़िस्से सुनाने लगी।
पिताश्री हिन्दी, संस्कृत, गढ़वाली और अंग्रेज़ी अच्छी तरह बोल, लिख, पढ़ व समझ लेते थे। सादा सात्विक खान-पान, और समस्त व्यसनों से दूर, पठन-पाठन में अभिरूचि थी। हम चार भाई—विक्रम, महावीर, सोबन व ओमस्वरूप तथा बहन वीरा। सबने पिताश्री का ही अनुशरण किया और सादा जीवन उच्च विचार के सिद्धान्त पर ही चले और अमल किया। बड़े भाईसाहब विक्रम को लेकर एक क़िस्सा में यहाँ सबसे बाँटना चाहूँगा। बड़े भाईसाहब सातवें महीने में जन्में और पैदा होते ही उन्हें निमोनिया हो गया। जिससे उनका मानसिक विकास उस गति से न हो सका जिस तरह एक सामान्य बालक का होता है। तरह-तरह के सब जतन करके देख लिए, जिसने जहाँ, जैसा कहा, वहाँ दिखाया, मगर मानसिक रूप से कमज़ोर रह गए। हालांकि घर के सारे काम-काज, डेयरी से दूध या दुकान से सौदा लाना, और इधर-उधर घूमना भी वे अब सुचारु रूप से कर लेते हैं। हम सभी की शादियां और बच्चे भी हो गए हैं मगर बड़े भाईसाहब अविवाहित ही हैं। ख़ैर एक बार पिताश्री उनको अपने साथ दफ़्तर ले गए। ये बात शायद 1982-83 की है। उस दिन दोपहर में दफ़्तर की बिजली गुल हो गयी। स्टोरकीपर होने के कारण पिताश्री दफ़्तर के काम से बाहर गए हुए थे। बिजली गुल होने सब बाहर आ गए थे और विक्रम भाई जो दफ़्तर में अकेले बैठे थे। उन्होंने समझा दफ़्तर की छुट्टी हो गयी है और पापा मुझे दफ़्तर में ही छोड़कर चले गए हैं। ये सोचकर वो बाहर निकल आये और घर की तलाश में पैदल ही अकेले पता नहीं कहाँ को निकल गए? उन्हें घर का पता तो था नहीं! अंतर्मुखी थे। किसी अपरिचित से बातचीत में खुद को सहज महसूस नहीं करते थे। ऊपर से थोड़ा हकलाते भी थे। इस कारण कोई कुछ पूछे भी तो भाईसाहब कुछ बताने में असमर्थ। फ़िलहाल उस रोज़ दफ़्तर में भी हड़कम्प मच गया।
चारों तरफ़ खोज हुई भगत जी का लड़का कहाँ गायब हो गया? सब पिताश्री से इस पर दुःख प्रकट करते रहे। ख़ैर पिताश्री घर पहुँचें तो गली में भी हड़कम्प मच गया। विक्रम कहाँ गायब हो गया। माताश्री का रो-रोके बुरा हाल। अड़ोसी-पड़ोसी के बाद, रिश्तेदार भी घर पर पहुँचकर वही सवाल पूछने लगे। जिसका जवाब किसी के पास नहीं था? करें तो क्या करें? खोजें तो कहाँ खोजें? सब सान्त्वना ही दिए जाते थे बस।
पड़ोस में ही एक गजेन्द्र (शम्मी, बुलबुल के नाना) नाम के बुज़ुर्ग रहते थे। वे अपने इर्द-गिर्द ज़मा लोगों से कह रहे थे— “भगत जी जानबूझकर छोड़ आये होंगे अपने पगले लड़के को। उनके और भी तीन बेटे हैं।”
“क्यों ऐसी उलटी बात कर रहे हो? क्या अपनी किसी औलाद को माँ-बाप, वो भी भगत जी जैसे देवता आदमी! अपने बेटे को खुद ही छोड़ देंगे। जिसे चौदह-पन्द्रह सालों से पाल रहे हैं।” बगल के ही किसी पहाड़ी पड़ोसी ने ऐसा कहा तो शम्मी के नाना जी लज्जित हुए।
लगभग दस दिन बीत गए थे। भाईसाहब का कहीं अता-पता नहीं चल पाया। रिश्तेदार भी आते-जाते रहे। हौंसला बढ़ाते रहे। सारे मामा, चाचा, जितने दिल्ली व आस-पास के इलाक़ों में रहते थे, सब ने कहा–हिम्मत से काम लो। भगत जी की भक्ति उनके लड़के को वापिस ले लाएगी। पिताजी ने दूरदर्शन के गुमशुदा तलाश केन्द्र से भी दूरदर्शन पर विक्रम भाई का फोटो ज़ारी करवाया। जिसे बलवन्त भैजी की श्याम-श्वेत टीवी पर हमने देखा था। पूछयरों (पहाड़ों में जिन पर देवी-देवता आता है। उन लोगों से भी पूछने गए विक्रम भाई के नाम के चावल लेकर।) पर कुछ फ़ायदा नहीं, वो भी सान्त्वना ही दे रहे थे। पिताश्री ने अपनी दृष्टि पूजा-पाठ में और ज़ियादा केन्द्रित कर दी थी। उनका विश्वास था–भाई को राम जी खुद रास्ता देंगे। इस बीच दिन-रात रो-रोकर माताजी की आँखों के आँसू भी सूख गए थे। ठीक दसवें दिन की शाम को विक्रम भाई घर पहुँचे। जिसको भी भाई के आने का पता चला। वही खुश था। पिताजी भी दफ़्तर से आये तो हैरान रह गए। हमें खुद यक़ीन नहीं हो रहा था कि विक्रम भाई वापिस आ गए। सबकी आँखों में ख़ुशी के आंसू छलक आये। जब दो-चार दिन में विक्रम भाई नॉर्मल हो गए तो उन्होंने जो बताया कुछ यूँ था—’वो दिल्ली से चलते-चलते हरियाणा पहुँच गए थे। उनके चमड़े के जूते पूरी तरह घिस चुके थे। कीलें उनके पैरों को लहूलुहान किये दे रहीं थी। जिस दिन वो आये थे सबसे पहले उनके जूते उतरवाए। देखके सब दंग थे भाई कैसे इन जूतों से चल रहे थे? विक्रम भाई ने बताया—’मैं रात को रास्ते के ढ़ाबे में सो जाता था और दिन में घर को तलाश करता था।’ हरियाणे में वे घर का पता केवल खानपुर (जो हमारे निवास मदनगीर के बग़ल में था।) बता पाते थे। लेकिन लोग नहीं समझ पाते थे ये कहाँ है? हरियाणे के लोग काफ़ी अच्छे और मिलनसार थे। वे भाई के प्रति दयालू थे। उनमें से एक आदमी को पता था कि खानपुर कहाँ है? उसने ही प्रयास करके भाई को दिल्ली की बस में बिठाया और कंडेक्टर से आग्रह किया कि इसको खानपुर में ही छोड़ना। भाई कई दिन से घर से लापता है। मैंने भी राम जी का आभार व्यक्त किया। आज कहाँ ऐसे मिलते हैं? पहले रिश्तेदारों के घर लोग पूरे परिवार के साथ जाते थे तो मेहमान भी उनका स्वागत दिलो-जान से करते थे। अब तो एक आदमी भी आ जाये तो मेजबान को बेचैनी होने लगती है—ये बला कब टलेगी? कहीं रात को तो नहीं रुकेगा? रुकेगा तो कितने दिन के लिए रुकेगा? मेजबान अब ये सोच ही रहा होता है कि मेहमान कहता है, अच्छा मैं अब चलता हूँ। आपने पानी पिला दिया, इतना ही काफ़ी है।
‘खाना खाते जाइये।’ एक फार्मेलिटी की तरह इस शब्द को उछाला जाता है मेजबान की तरफ़। मगर वो हृदयगत भावों को समझकर ‘शुक्रिया’ कहकर निकल जाना ही पसन्द करता है। हावी होते अर्थतन्त्र में मानवीय संवेदनाएँ अब निन्यानवे प्रतिशत खो चुकी हैं।
अस्सी के दौर में मदनगीर में उत्तराखण्ड कमेटी वालों की तरफ से रामलीला खेली जाती थी। हमारे पिताश्री भी उसके सदस्य थे। ऐसी भीड़ होती थी कि अतिरिक्त पुलिस बल तैनात करना पड़ता था। रावण गली नम्बर 33 के नेगी जी बनते थे। जिनकी आवाज़ बिना माइक के काफ़ी दूर तक गूंजती थी। देखने वाले पागल हो उठते थे। हर कलाकार अपने चरित्र में गहरे रमा रहता था। एक गौतम नाम का आदमी था जो दशरथ मरण के दृश्य को इतना जीवन्त कर देता था कि अगले दिन उसके हाथ में पलस्तर चढ़ा होता था। राम-सीता-लक्ष्मण के वियोग में गौतम भाई सीधा स्टेज़ पर हाथों के बल ‘आह सीते’, ‘आह राम’ कहते गिर पड़ते और अपने हाथों की चोट की परवाह न करते।
एक बार शिव का रोल करने वाला पात्र गाँव चला गया तो पिताश्री को ही ‘शिवजी’ का रोल करने को कहा गया। जो की छोटा सा रोल था। जिसमें रावण कैलाश परवत उठाने की ज़िद्द करता है मगर शिव के पैरों के भार तले दब जाता है और त्राहिमाम! त्राहिमाम!! कहकर भाग खड़ा होता है। ये दृश्य गम्भीर होने की जगह हास्य का दृश्य बन गया। पिताश्री शिव के रूप में और पड़ोस के जोशी भैजी का मंझला लड़का पप्पू पार्वती बन गया। रावण के रूप में उस दिन दमदार रावण नेगी जी उपलब्ध नहीं हो पाए। एक मरियल-सा आदमी रावण की वेशभूषा में खड़ा कर दिया गया। वह नया था और अपना सम्वाद याद कर-करके उसने अपना गला बैठा लिया था। जब स्टेज पर लाइव सीन शुरू हुआ तो पप्पू भाई जो पार्वती बना हुआ था बोला, ‘नाथ ये अभिमानी रावण कैलाश परवत को उठाना चाहता है। इसका घमण्ड तोड़िये। पिताश्री ने त्रिशूल का निचला भाग मंच पर ज़ोर से पटका तो मरियल रावण के पैर पर उसका तेज प्रहार लगा और त्राहिमाम चिल्लाता हुआ। वह मंच पर भोलेनाथ के चरणों में गिर पड़ा। बैठे हुए गले से रावण के पात्र का ‘त्राहिमाम’ का स्वर लोगों को बकरे के मिमियाने जैसा लगा। जिसे वह बार-बार दोहरा रहा था। ये देखकर किसी की हँसी नहीं रुक रही थी। खुद पिताश्री भी हँस पड़े और पर्दा जल्दी गिरना पड़ा। इसके बाद फिर कभी पिताश्री को कोई रोल नहीं दिया गया। हालाँकि रामलीला की अन्य व्यवस्थाएँ वे करते रहे।
मेरे ऊपर पिताश्री की असीम कृपा रही और मेरे तीनों बच्चों पर भी। मृत्यु से एक दिन पहले 6 फरवरी 2005 को रविवार की शाम अभिषेक रो रहा था। जो कि एक माह का था। पिताश्री ने उसे अपने हाथों में उठाया तो वो शान्त हो गया। मैं सामने ही बैठा था। मुझसे कहने लगे, “अपनी ज़िम्मेदारियाँ अब तुम ही उठाओ। मैं काफ़ी थक चुका हूँ।” मैं समझ नहीं पाया, उन्होंने ऐसा क्यों कहा? शायद उन्हें अपनी मृत्यु का पूर्वाभास हो गया था। अगली सुबह वह हमेशा की तरह ब्रह्ममुर्त में उठे। नित्यक्रियाओं को अंज़ाम दिया। मोटर चलाकर पानी की टैंकी भी भरी। फिर अपने स्थान पर बैठकर राम नाम का जाप करने लगे। मूर्छित होकर गिर पड़े। उन्हें दिल का दौरा पड़ा था। हम डाक्टर डोभाल को भी बुलाकर लाये मगर तब तक देर हो चुकी थी। पिताश्री जा चुके थे। मैंने आँसुओं को रोक रखा था। कई रिश्तेदारों को मोबाइल द्वारा सूचित किया। पिताश्री नहीं रहे। सोमवार की उस सुबह भी काफ़ी लोग जमा हो गए थे। मैं समझ नहीं पा रहा था कि अचानक ये सब क्या हो गया? पिछली गली से देवराणी पण्डित जी को बुलाया गया। रिश्तेदारों का आने का सिलसिला शुरू था। विलाप ज़ारी था। माताश्री और ताई जी ऊँचे सुर में रो रहे थे। पण्डित जी ने अन्तिम संस्कार की विधियाँ करवानी शुरू कर दी। मुझसे पिंड बनाने को कहा गया। पिण्ड बनाते वक़्त मेरी आँखों में आँसू आये। पृष्टभूमि में मेरे कानों में पिताश्री के स्वर गूँज रहे थे। शरीर नाशवान है। विद्वान इसका शोक नहीं करते और मेरे मनोमस्तिष्क पर वे सभी दृश्य चित्रपट की भाँति घूम रहे थे। जो पिताश्री के साथ पूजा-पाठ, धार्मिक बहस, चिन्तन और मनन में बीते थे। भले ही उनका शरीर हमारे साथ नहीं है। मगर उनकी आत्मा के होने का अहसास मुझे हमेशा होता रहा है।
पिताश्री के सामने ही कॉलेज के ज़माने से मेरा साहित्य सृजन आरम्भ हो चुका था। ‘दहेज दानव’ पक्षिक, लखनऊ; में पहली बार कविता छपी। बदलाव का संघर्षपथ मासिक (इटावा); मोदिनी, मासिक (नई दिल्ली) आदि कुछ अख़बारों मेरी कई छन्दमुक्त रचनाएँ 1991 ई. से निरन्तर छपती रही। पहली लघुकथा बदलाव का संघर्षपथ के लघुकथा विशेषांक में छपी थी। बड़ी कहानियों की एक “किताब नस्लें तथा अन्य कहानियाँ” नवराज प्रकाशन से सन 2003 ई. में ही प्रकाशित हो चुकी थी। जिसे पिताश्री ने भी अपना आशीर्वाद दिया था। 1996 ई. में प्रथम बार मेरे रामनामी दोहे बदलाव का संघर्षपथ में ही प्रकाशित हुए थे। जिन्हें देखकर पिताश्री अत्यन्त प्रसन्न हुए क्योंकि उनके विचारों को मैंने छन्दों में पिरोना शुरू कर दिया था। वे मेरी नौकरी को लेकर भी चिन्तित रहते थे। चाहते थे कहीं सरकारी नौकरी में ही मेरा इंतज़ाम हो जाता। एक बार उन्होंने मुझसे कहा भी था कि यदि नौकरी के दौरान ही मेरा भी निधन हो जाता तो तुम्हें सरकारी नौकरी मिल जाती। मैं हँस दिया। यदि वाटर मैन की वो नौकरी मैंने निरन्तर की होती शायद सरकारी में जुगाड़ हो जाता। आज मेरे साथ काम करने वाला हर्षवर्धन बी.ए. करने के बाद कलर्क हो गया। पिताश्री को एक बार पुराने दफ़्तर के साथी सरदार रणजीत सिंह जी ने मिलने पर बताया था। 1994 ई. में बी.ए. करने के तीन साल बेकार रहने के बाद मैं भी 1997ई. में इनोडाटा, नोएडा में कम्प्यूटर ऑपरेटर के पद पर लग गया था।
बेरोजगारी मेरे लिए मन्थन और चिन्तन के बड़ी काम आयी। उस काल को मैंने साहित्य सृजन में लगाया। अपने भीतर के साहित्यिक स्केल को विकसित किया। नामचीन उस्तादों से मिला और साहित्यिक बारीकियाँ सीखी। और सिखने का ये सिलसिला बदस्तूर ज़ारी है। पिताश्री की मृत्यु के बाद 2005 ई. में लफ़्ज़ के सम्पादक श्री तुफ़ैल चतुर्वेदी जी से मिला और ग़ज़ल का पहला सबक सीखा। सुरंजन जी से मेरी मुलाक़ात भी 2005 ई. ही हुई थी। उनके लक्ष्मी नगर, दिल्ली स्थित कार्यालय में, जो कि चौराहे के पास एक शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में स्थित था। बाद में सुरंजन जी के साथ कहानियों पर कई महत्वपूर्ण काम हुए। पत्रिका सम्पादन की बारीक़ियाँ सीखी। सुरजन जी मगध प्रकाशन के अधिपति थे। ख़ैर सुरंजन जी के साथ ग़ाज़ियाबाद में सुप्रसिद्ध साहित्यकार व कवियत्री लीलावती बंसल जी के घर में एक काव्य गोष्ठी में आदरणीय मंगल नसीम साहब मिल गए। सुरंजन जी अपनी पत्रिका कथासंसार का एक अंक लीलावती बंसल जी पर निकालना चाहते थे। यहीं आदरणीय डॉ. कुंवर बेचैन साहब को भी मैंने पहली बार आमने-सामने सुना। बहुत पसन्द आये। गोष्ठी में मैंने और सुरंजन जी ने अपनी छन्द मुक्त कवितायेँ भी पढ़ी। उस्ताद नसीम साहब के ग़ज़ल कहने के अंदाज़ से मैं अत्यन्त प्रभावित हुआ और उन्हें अपना उस्ताद बना लिया। 2009 ई. में मेरा पहला ग़ज़ल संग्रह ‘आग का दरिया’ आया। जिसे मैंने पिताश्री को समर्पित किया। बाद में इस संकलन की आठ ग़ज़लें राजेन्द्र तलवार जी ने अपनी संगीत एल्बम “फिर वही आवारगी” सोनोटेक म्यूजिक कम्पनी हेतु ली। इस एल्बम में मशहूर गायिका साधना सरगम जी ने भी गाया है।
इस बीच सुरंजन जी के कारण ही आदरणीय गुरुदेव रमेश प्रसून जी व डॉ. अनूप सिंह जी से भी मेरी भेट हुई। प्रसून जी ने दोहा और जनक छन्द से मुझे अवगत कराया। साथ ही ग़ज़ल पर भी मेरी पकड़ मज़बूत हुई। एक के बाद एक कई लोग मिलते गए और मेरे भीतर भी कुछ बेहतर रचने का जोश बढ़ने लगा। शायद पिताश्री ही साहित्य के इस सन्मार्ग में मुझे लगाना चाहते थे। भले ही मैंने ज़िन्दगी में ज़ियादा दौलत नहीं कमाई लेकिन लेखन वो हथियार और असली कमाई है जो पीढ़ी-दर-पीढ़ी हमें जीवित रखेगी। साहित्यिक यात्रा का ज़िक्र करने का अभिप्राय सिर्फ़ इतना है कि कहीं न कहीं मेरे बाल मन पर पिताश्री की राम भक्ति ने वो असर छोड़ा—शा’इर, कवि व कथाकार बनने में मुझे सहायक सिद्ध हुआ। आने वाली पीढ़ियों में जब इस पुस्तिका को पढ़ा जायेगा। तो मेरे पिताश्री पर लोग गर्व करेंगे।
आडवाणी जी ने जब राम मन्दिर के समर्थन में 25 सितंबर, 1990 ई. को गुजरात के सोमनाथ से अयोध्या तक की कारसेवा यात्रा (जो विभिन्न राज्यों से जानी तय थी।) निकली थी। तब पिताश्री ने भी उसका समर्थन किया था। सरकारी नौकरी में होते हुए वह खुलकर तो आगे नहीं आये पर उनकी बड़ी इच्छा थी कि उनकी आँखों के आगे ही राममन्दिर का निर्माण हो जाये। लालू जी ने जब बिहार में यात्रा रोकी और आडवाणी को गिरफ़्तार किया तब तक आन्दोलन का मक़सद पूरा हो चुका था। आगामी चुनाव में इसके परिणाम भी दिखे। हिन्दी भाषी प्रदेशों में भाजपा सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी। इस यात्रा की पृष्ठ्भूमि पर जाएँ तो एक चीज़ उभर के आती है। 1949—1986 ई. (करीब 37 वर्षों तक) राम जन्मभूमि का मामला जस का तस था। वहाँ परिन्दा भी पर नहीं मार सकता था। वो महज तीन–चार वर्षों में शिलान्यास तक पहुंच गया। आंदोलन की कमान संभाल रहे संघ परिवार के प्रमुख संगठन विश्व हिन्दू परिसद (माननीय अशोक सिंघल जी) का आत्मविश्वास सातवें आसमान पे था। सबको लगने लगा था कि अब तो राम मंदिर निर्माण निकट भविष्य में कभी भी साकार हो सकता है। जनता-जनार्दन ने भी इसे स्वीकार कर लिया था। साधु-संतों का आशीर्वाद भी था। अतः तमाम तैयारियाँ व कोशिशें ज़ोर पकड़ने लगीं।
पिताश्री भी पूजा-पाठ में अति उत्साह से जय-जय श्री राम बोलने लगे थे। वे अक्सर कहते थे—”मैं रहूँ न रहूँ, निकट भविष्य में राम मंदिर निर्माण हमारी आने वाली पीढ़ियाँ अवश्य देखेंगी!” बाद में घटनाक्रम बदले। एक यादव मुख्यमंत्री ने बिहार के समस्तीपुर में आडवाणी का रथ रोक कर उन्हें गिरफ़्तार कर लिया। और दूसरे यादव मुख्यमंत्री ने उत्तर प्रदेश के अयोध्या में असंख्य निहत्थे कार सेवकों पर गोलियाँ चलवाकर उन्हें मौत के घाट उतार दिया। इस तरह आंदोलन की बीच में ही हत्या कर दी गई। 30 अक्टबूर, 1990 ई. को पहली बार कारसेवकों पर चली गोलियों में 5 लोगों की मृत्यु हुई। इस घटना को लेकर पूरे देश में आक्रोश था। इस गोलीकांड के मात्र दो दिन बाद ही, 2 नवंबर को हजारों कारसेवक फिर से हनुमान गढ़ी के करीब पहुंच गए, जो विवादास्पद बाबरी मस्जिद के करीब था। सुबह का वक्त था, हनुमान गढ़ी (अयोध्या) के सामने लाल कोठी के सकरी गली में कारसेवकों का हज़ूम बढ़ा आता है। मुल्ला मुलायम की पुलिस ने सामने से आ रहे निर्दोष-निहत्थे कारसेवकों पर फायरिंग कर दी। सैकड़ों कार सेवक मारे गए। मगर सरकारी आंकडे में सिर्फ़ ढेड़ दर्जन लोगों की मौत बताई गई। इसमें कोलकाता से आए कोठारी बंधुओं की भी मौत हुई थी। जिन्होंने बाबरी मस्जिद पर भगवा ध्वज फहराया था। मैंने पहली बार इस घटना में क्षुब्ध पिताश्री को क्रोधित अवस्था में देखा, “रामभक्तों का लहू व्यर्थ नहीं जायेगा। ये मुल्ला मुलायम का ऐसा जघन्य अपराध है, जिनके लिए इतिहास इसको कभी क्षमा नहीं करेगा। हे राम! अपने भक्तों को मुक्ति देना। जिन्होंने आपके मन्दिर निर्माण के लिए प्राण गंवाये।”
वैसे पिताश्री हिन्दू-मुस्लिम एकता के भी पक्षधर थे। मेरा एक दोहा जो उन्हीं के विचारों की पुष्टि करता है:—
सबका खेवनहार है, एक वही मल्लाह।
हिन्दी में भगवान है, अरबी में अल्लाह।।
बात यूँ हैं कि मुझे गुरुदेव रफ़ी साहब की आवाज़, जबसे होश सम्भाला है, प्रभावित करती रही है। कॉलेज के ज़माने में जब घर में टेपरिकॉर्डर आया, तो मैं हरिओम शरण, अनूप जलोटा और रफ़ी साहब के भजनों की ऑडियो कैसेट ले आया था। सभी ने भजन अच्छे गाये हैं लेकिन मुझे रफ़ी साहब के फ़िल्मी भजन ज़ियादा पसन्द थे तो पिताश्री भी कई बार उन्हें सुनते थे। उसमें राजेंद्र कृष्ण का रचा ये भजन, ‘सुख के सब साथी, दुःख में न कोई। मेरे राम, मेरे राम, तेरा नाम एक साँचा, दूजा न कोई।’ इस भजन के बारे में पिताश्री कहते थे, “रफ़ी जी ने इस भजन में अपनी आत्मा डाल दी है। बड़े मनोयोग से गाया है।” मैं रफ़ी साहब का पोस्टर ले आया था। जिसे कक्ष में लगा दिया था। घरवालों ने इसका विरोध नहीं किया। ये प्रमाण है, हमारे धर्मनिरपेक्ष ढांचे का। पिताश्री कई बार बोलते भी थे, “भविष्य में जब कभी राम मन्दिर बने तो उसकी नींव पर पहली ईंट कोई मुस्लिम भाई रखे।” भाईचारे की जो मिसाल पिताश्री ने रामायण से पाई थी, उसे व्यवहारिक जीवन में भी जीते थे।
लगभग पाँच–छह वर्ष की अवस्था में जब मुझमे कुछ समझ पैदा हुई तो पिताश्री मुझे रामायण के दोहे और चौपाइयों का ज्ञान भावार्थ सहित समझाते रहे। कुछ अपने अनुभव भी वो इन दोहों और चौपाइयों में डाल देते थे। इस तरह मेरे भीतर छिपे कवि और कथाकार का कैनवस विकसित हुआ। इसलिए इन 108 दोहों में पिताश्री के अनुभव व विचार भी शामिल हैं। मैंने तो उनके विचारों को दोहा छन्द में पिरोने भर की चेष्टा मात्र की है। पिताश्री का मूल आधार तुलसीदास रचित साहित्य था। अतः उनके विचार तुलसी बाबा से प्रेरित रहे। पिताश्री ने अपने जीवनकाल में इतने अधिक धर्मग्रन्थ ख़रीदे थे कि यदि उन सबको संभाल के रखा जाता तो एक दस बाई दस का कमरा उन किताबों से भर जाये। अधिकांश साहित्य गीताप्रेस गोरखपुर का था। सन्तों की लिखी किताबें भी पिताश्री रूचि के साथ पढ़ते थे। श्री राम किंकर जी महाराज द्वारा रची पुस्तक ‘धर्मसार भरत’… पढ़ते-पढ़ते पिताश्री अत्यंतभावुक हो जाते थे। मेरे सामने अनेक बार उन्होंने भरत के चरित्र को भगवान श्रीराम के समान महान बताया था। उन्हें डायरी लिखने का भी शौक था, जिसमें उनके धर्म के प्रति विचार झलकते हैं।
वे कोई लेखक तो थे नहीं, मगर चाहते थे कुछ लिखना, जो हो न सका। लिखने की ये बीमारी प्रभु राम ने मेरे सुपुर्द कर रखी है। मैंने धीरे-धीरे उनके विचारों और भक्ति भावना को लिपिवद्ध करना शुरू किया। जो कि अब पुस्तक रूप में सम्भव हो सका। लगभग चालीस वर्षों में जितना हो सका और जितना मैं रामजी की भक्ति को पिताश्री के माध्यम से समझ सका वह दोहों की शक्ल में उपस्थित है। बड़ा दुर्भाग्य यह रहा कि पिताश्री की मृत्यु के उपरान्त उनकी साहित्यिक और धार्मिक विरासत को कोई संभल न सका। अतः उनकी अधिकांश वस्तुएँ आज अप्राप्य है। उनके विचारों की डायरी अब उपलब्ध नहीं है मगर मेरे दिमाग़ में कई बातें थी जो पिताश्री की इस संक्षिप्त जीवनी के रूप में आप सबसे साँझा की। रामभक्ति ने पिताश्री को आशावान, सकारात्मक ऊर्जावान और अत्यन्त विवेकशील बना दिया था। उन्हीं भगवान श्री राम के चरणों में ये पुस्तक अर्पित है।
—महावीर उत्तरांचली
9 जून 2020 ई.