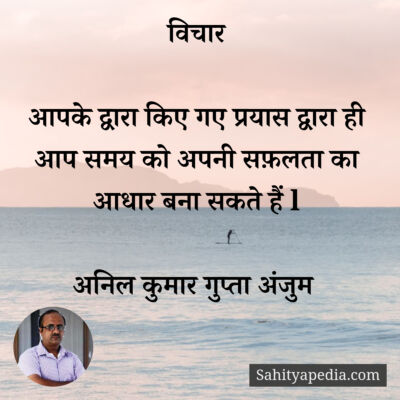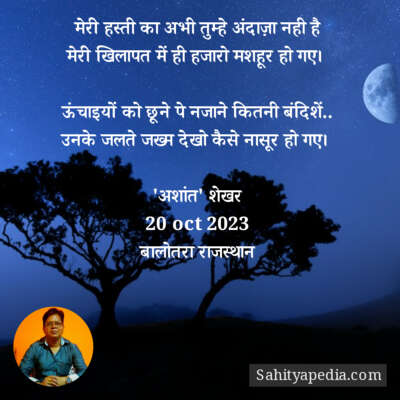रमेशराज की पिता विषयक मुक्तछंद कविताएँ

-मुक्तछंद-
।। ओ पिता ।।
मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ ओ पिता
ओ पिता मैं तुमसे पूछना चाहता हूं
मेरे इन निष्कंलक हाथों में
अहिंसा का हनुमान चालीसा थमाकर
इस तरह मुझे एक झूठे तप की आग से
गुजरने के लिए क्यों छोड़ गये हो?
मेरे साथ ये कैसा
अभिशाप जोड़ गये हो।
अहिंसा की बौनी दलीलें देते हुए
क्या कभी तुमने सोचा था
कि अत्याचार के विरोध में
जुबां न खोलना
सबसे बड़ी हिंसा होती है
जिसके तल्ख अहसास को
आगे आने वाली हर पीढ़ी
अपने सीने और पीठ पर
पड़े चाबुक की तरह ढोती है।
मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ ओ पिता
ओ पिता मैं तुमसे पूछना चाहता हूं
कि तुम्हारे तीन बन्दरों के आचरण पर
अमल करने वाले हमारे सोच
यूं ही कब तक किये रखेंगे
हमारी बन्द आंख,
जबकि किसी चोर दरबाजे से
इस व्यवस्था की हिंसक बिल्ली आती है
और हमारे सुख के कबूतरों को
चट कर जाती है।
मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ ओ पिता
ओ पिता, मैं तुमसे पूछना चाहता हूं
कि कब तक न सुनें हम
कानों में थोथे आदशों की
अंगुलियां डाले
सीता का करुण चीत्कार,
जबकि हमारे भीतर का जटायु
हमें धिक्कार रहा है,
हमारा थोथा अहं
हमें मार रहा है।
मैं तुमसे पूछना चाहता हूं ओ पिता
ओ पिता मैं तुमसे पूछना चाहता हूं
कि तुम ये कैसा पढ़ा गये
आजादी का पाठ
जिसे पढ़कर हम गुलामी को
स्वतंत्रता मान बैठे हैं
नैतिकता के खिलाफ
अहिंसा का चाकू तान बैठे हैं ।
मैं तुमसे पूछना चाहता हूं ओ पिता
ओ पिता मैं तुमसे पूछना चाहता हूं
कि सत्य की जीत का ढिंढोरा
पीटने के पहले
क्या तुमने कभी सोचा था
कि यहां सत्य की जीत कभी नहीं होती
जो जीतता है वही सत्य बन जाता है।
मैं तुमसे पूछना चाहता हूं ओ पिता
ओ पिता मैं तुमसे पूछना चाहता हूं
अपनी इस घुनी हुई लाठी के सहारे
कब तक सहता रहू
अपने पुरुषत्व पर
असभ्यता के वार
कब तक दर्शाऊं अपने ही दुश्मन से
एक नाठकीय प्यार।
जबकि समूचा जिस्म
उत्तेजना और आक्रोश का
व्याकरण बन चुका है
असत्य से लड़ना
मेरा आचरण बन चुका है।
-रमेशराज
————————————————
-मुक्तछंद-
।। कहां गये वो आदमी?।।
कहां गये वो आदमी
वो आदमी कहां गये
जिनके बारे में
बतलाया करते थे मेरे पिता?
वे आदमी
जिनकी रंगों में खून नहीं
देशप्रेम हिलौरे मारता था
जिन्हें उनका सकंल्प
अग्निसुरंगों से
हंसा-हंसा कर गुजारता था।
कहां गये वो आदमी
वो आदमी कहां गये
जिनके बारे में
बतलाया करते थे मेरे पिता?
वो आदमी
जिनकी अमानुषिक यातना का तहत
गूंगी न हो सकी ज़बान
जिन्होंने दहशत-भरी आवाजों से
फोड़े की तरह पका दिये
गोरी नस्लों के कान।
कहां गये वो आदमी
वो आदमी कहां गये
जिनके बारे में
बतलाया करते थे मेरे पिता?
वे आदमी नहीं
पिघली बर्फ के कतरे थे
जो नदी बन कर
इस देश की बंजर आत्मा में बहे थे
किन्तु मेरे बच्चे
आजादी मिलते मिलते
उस नदी का पानी
बस कीचड़ होकर रह गया
और आजादी का अर्थ
पूंजीपति की तिजोरी
और खादी की लंगोटी के बीच
कहीं खोकर रह गया |
उन लोगों के साथ
ये कितना बड़ा धोखा था
मेरे पिता ने यह भी कहा था।
कहां गये वो आदमी
वो आदमी कहां गये
जिनके बारें में
बतलाया करते थे मेरे पिता।
-रमेशराज
——————————————–
।। शायद मैं भी।।
जब भी मेरे और पिताजी के बीच
कोई दुख-भरी शाम पसरी होती है
पारिवारिक दायित्वों के
बोझीले अर्थो से लदी हुई,
मैं पिताजी के सामने बैठा होता हूं
गुमुसम-सा।
मैं पिताजी के चेहरे पर
तिरती हुई झुर्रियां का
इतिहास पढ़ने लगता हूं,
जिस पर अकिंत हैं
पिताजी के अन्तहीन संघर्ष
गहरे विषाद के क्षण
जीने के अप्रत्याशित हादसे
पपड़ाई सूखी झील-सी आखों में
मरी हुई सोन-मछलियों में
सड़े गले अवशेष।
उस वक्त मुझे लगता है
कि पिताजी के चेहरे की
अनगिनत झुर्रियां
एक-एक कर मेरे चेहरे पर
उतर रही हैं : लगातार।
पिताजी होते हैं
निर्विकार, एकदम शांत
हुक्का गुड़गुड़ाते हुए
पहलवान छाप बीड़ी
कश-दर-कश खींचते हुए।
फिर भी मुझे लगता है
कि पिताजी के अन्दर कुछ है
ज्वालामुखी-सा सुलगता हुआ
नागफनी-सा कसकता हुआ।
पिताजी के होठों पर
दही जैसी जमी हुई चुप्पियां
संदर्भ हैं दमाग्रस्त मां के
बिना दवा के दम तोड़ते हुए
मेरे जवान बेरोजगार भाई के,
बिना दहेज
आत्महत्या करती हुई मेरी बहन के।
पांच साल से मुझे
कतरा-कतरा चूसती हुई
बेरोजगारी की जोंक के।
मन होने लगता है
और भी ज्यादा उदास
मेरे चेहरे पर उतर आती है
पिताजी के चेहरे की
सारी की सारी झुर्रिया।
मैं महसूसता हूं
जैसे कि अब मुझे भी
ग़म ग़लत करने के लिए
एक काठ के हुक्के की जरूरत है
मुझे भी चाहिए
कुछ पहलवान छाप बीडि़यां।
शायद मैं भी अब
पिताजी की तरह
बूढ़ा और अशक्त
हो चला हूं।
-रमेशराज
———————————————-
रमेशराज, 15/109, ईसानगर, अलीगढ़-२०२००१