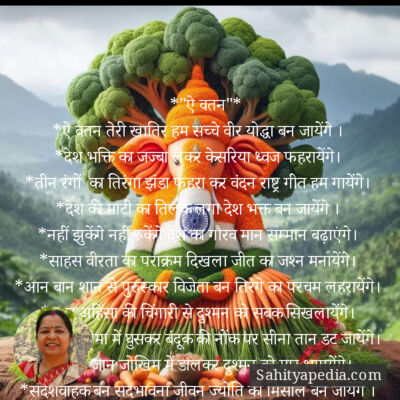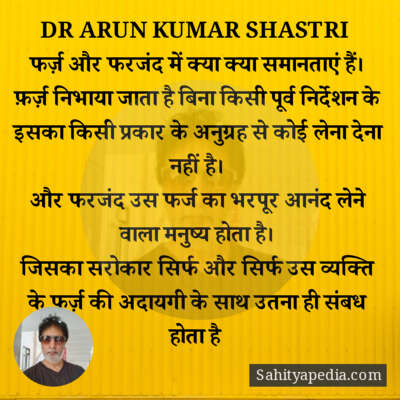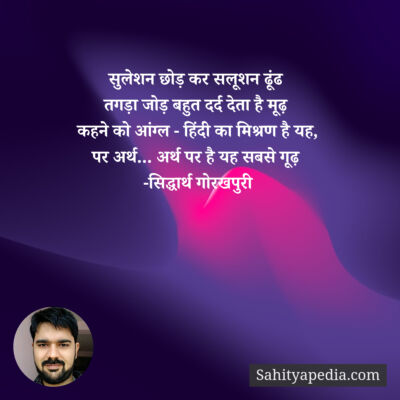मेरे विह्वल परिताप लिये
✒
सतरंगी परिधान लपेटे,
वनदेवी तुम बन जाती हो;
गिरती बिजली मेरे मन, औ’,
मंद-मंद तुम मुस्काती हो।
मुख प्रसन्न, पर शील झलकता
शीतलता, जैसे परिपाटी,
विचरण करती हो, देवि तुमहिं,
रहती बन, निशि-दिन मदमाती।
हवा बसंती, फागुन की तुम
रंगें, मेरे वीरानों की;
कोटि-कोटि जीवन वारूँ, कर
दर्शन तेरे मुस्कानों की।
प्यासे मन का अहसास, कली,
तुम मेरे मन की ज्वाला हो;
नित सेंक रहा हूँ मन को मैं,
जीवनसाथी तुम हाला हो।
अंबर में छा जातीं निशि में,
पूनम बन नवल चाँदनी सी;
अनुभूति प्रिये होती निशि में,
रानी तुम धवल दामिनी सी;
तन की हर आहट तुमी सुमुखि,
चेतन की तुम्हीं दुशाला हो;
जब होती ना अंबर में तुम,
जीवन प्रचंड विष प्याला हो।
भ्रमित खड़ा नभ, चाँद दृगों से
ताक रहा है भूधर का सर;
आखिर यह कैसा चमत्कार
आभामंडित सारा भूधर;
जगन्निगाहें भाँप रहीं हैं,
निश्चल प्रतिमान, अमी मंडल;
रुख़ करो जिधर, हे देवि, परम,
बन जाता है सुंदर कुंडल;
विद्युत मेरे मन में उठती,
महसूस करूँ मैं प्राणों की;
है नाम गूँजता यह मेरा,
भीने तेरे अहसानों की;
भौहें टेढ़ी, तिरछी निगाह,
नित मुस्कानों की साख लिये;
कह दो प्रिय तुम विचरण करती,
मेरे विह्वल परिताप लिये।
…“निश्छल”