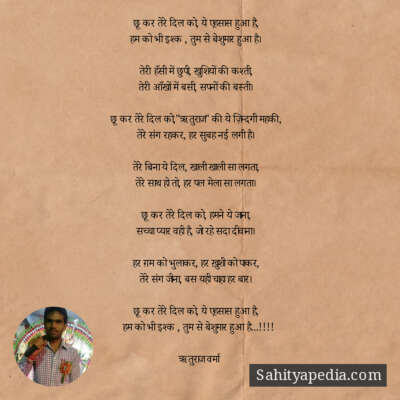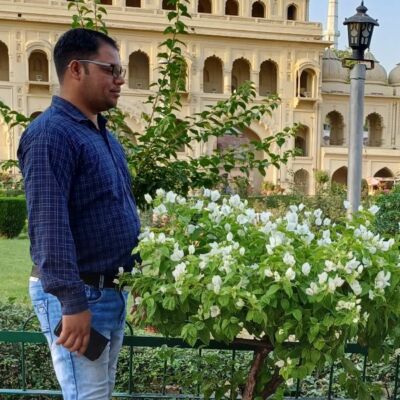*मुक्त-ग़ज़ल : दिल लगाने चल पड़ा हूँ मैं ॥
हथेली पर ही सरसों को जमाने चल पड़ा हूँ मैं ॥
कि बिन पिघलाए पत्थर को बहाने चल पड़ा हूँ मैं ॥
नहीं हैं आँखें जिसकी और न जिसके कान भी उसको ,
गले को फाड़कर अपने बुलाने चल पड़ा हूँ मैं ॥
जड़ें अपनी जमाने में जहाँ पे नागफणियाँ भी
उखड़ जाएँ , वहाँ तुलसी उगाने चल पड़ा हूँ मैं ॥
कहाँ तक हुस्न से उसके बचाऊँ अपनी आँखों को ,
कि आख़िरकार उससे दिल लगाने चल पड़ा हूँ मैं ॥
जो सुलगा दे नदी को वो उसे ही अपना दिल देगी ,
यही सुनकर समंदर को जलाने चल पड़ा हूँ मैं ॥
हमेशा आँख में आँसू भरे वो घूमता रहता ,
उसे कर मसख़री थोड़ा हँसाने चल पड़ा हूँ मैं ॥
दमे आख़िर ज़माने से जो दिल में दफ़्न है इक राज़ ,
उसे इक राज़दाँ को अब बताने चल पड़ा हूँ मैं ॥
न रेगिस्तान में पीने को भी पानी मयस्सर था ,
हुई बरसात तो प्यासा नहाने चल पड़ा हूँ मैं ॥
बहुत फूलों को सिर ढोया , उठाए नाज़ हसीनों के ,
अब उकताकर पहाड़ों को उठाने चल पड़ा हूँ मैं ॥
-डॉ. हीरालाल प्रजापति