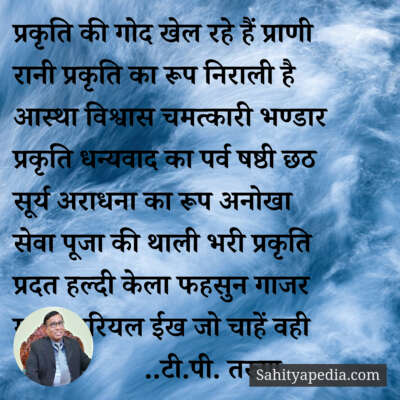मज़दूर
सच कहा आपने
मैं
मज़दूर हूँ
पर मजबूर नहीं
बहुत मज़बूत हैं
मेरे कंधे
सँभाल सकते हैं दर्द का भारी बोझ
तभी तो
ढोती हूँ दिन-रात शब्दों की ईंटें
उन्हें सलीके से रख
उन पर लगाती हूँ
भावों का सीमेंट
और करती हूँ
अपनी रचना की इमारत को पक्का
फिर सजाती हूँ उसे
अलंकारों के रंगों से
तब कहीं बन पाती है
मेरी कविता/ कहानी की कुटिया
फिर मैं उसमें जलाती हूँ स्वर के दीपक
तब खिल जाता है एक
गीत प्रसून
सब को लुभाने वाला
और मैं
फिर चल देती हूँ
किसी नई इमारत को बनाने
क्योंकि मैं सचमुच मज़दूर हूँ