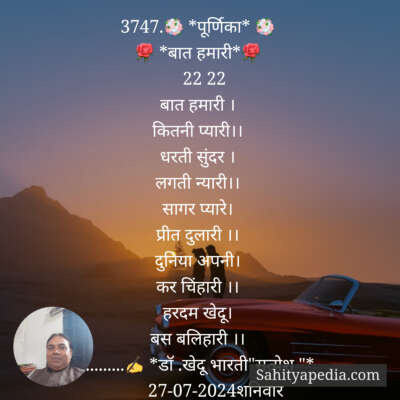मजदूर की अंतर्व्यथा

मैं उस बेबस लाचार मजदूर को देखता हूं,
जो रोज सुबह सवेरे चौराहे पर इकट्ठी दिहाड़ी मजदूरों की भीड़ का हिस्सा बनता है,
अपनी बारी आने का इंतज़ार करता है ,
उसके चेहरे पर अनिश्चितता की चिंता के भाव उसकी अंतर्वेदना प्रकट करते हैं,
दिहाड़ी न मिलने पर व्यवस्था के विकट प्रश्न उसे चिंतित करते है ,
कभी- कभी सोचता है, क्या-क्या सपने संजोकर वह शहर आया था ,
शहर आकर हकीकत से दो चार होकर वह अपनी करनी पर पछताया था,
सोचा था शहर में गांव से अच्छी मजदूरी मिलेगी,
तब उसकी जिंदगी बीवी बच्चों के साथ हँसी -खुशी गुज़रेगी,
अब वह समझ गया था , कि दूर के ढोल सुहावने होते हैं,
लोग बातों में आकर नाहक शहर की तरफ भागते हैं,
गांव में खुद की पहचान को छोड़कर शहर की भीड़ का हिस्सा बनते हैं,
गांव की मजदूरी में दो जून रोटी तो हासिल हो जाती थी, कभी भूखे पेट तो नहीं सोते थे ,
शहर में तो आए दिन फाके पड़ जाते हैं ,
दो रोटी के भी लाले पड़ते हैं ,
शहर में तो आए दिन काम की तलाश में
भटकते फिरते हैं ,
गांव में तो काम होने की सूचना लोग घर पर
ही भेज देते है,
शहर में तो लोग अपने-अपने सुख की चिंता करते हैं,
गांव में कम से कम एक दूसरे के दुःख को
तो लोग समझते हैं,