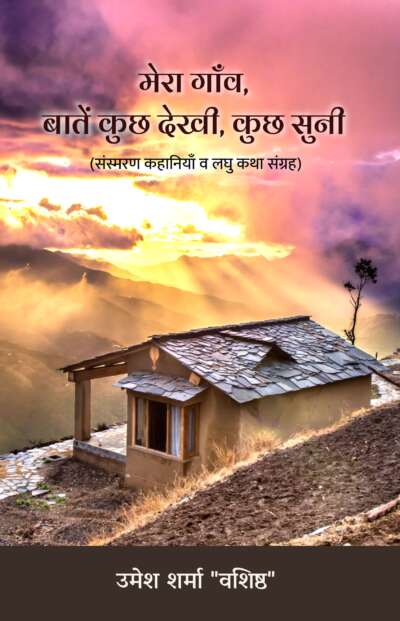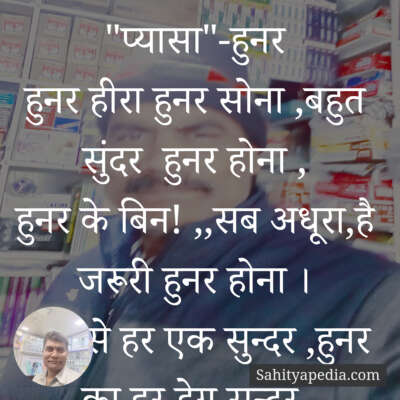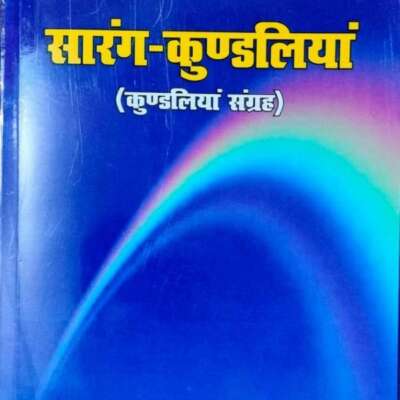फिल्मों का वो दौर
सत्तर और अस्सी के वो दशक जो गांव में गुज़रे थे, उसमें फिल्में जिंदगी का एक महत्वपूर्ण हिस्सा थीं। टेलिविजन उस समय न के बराबर थे और शुरू शरू में जब आये भी तो सिर्फ दूरदर्शन हुआ करता था , जिसमें हिंदी फिल्में सप्ताह में एक बार ही देखने को मिलती थी।
बाहरी दुनिया से जुड़े रहने का रेडियो के अलावा फिल्में ही माध्यम थीं, जिन्होंने उस दौर के मनोरंजन की भी जिम्मेदारी उठा रखी थी।
गांव के राधा टॉकीज की भी क्या शान थी उस वक़्त। प्रथम , द्वितीय और तृतीय श्रेणी की टिकटों के अलावा महिलाओं की
अलग टिकट खिड़की, प्रवेश और बैठने की व्यवस्था थी।
बिजली विभाग के रहमो करम पर चलने वाला यह सिनेमाघर अपने तीनों शो के समय नियमित करने में असफल था। खैर , उससे हमें क्या फर्क पड़ने वाला था, समय की कोई कमी नहीं थीं, घड़ियाँ भी धीरे धीरे चलती थीं उस वक़्त।
सिनेमाघर के पंखे केवल सांत्वना देते थे, कहते रहते थे कि कुछ हम हिल रहे हैं कुछ आप भी हिलते रहिए, तीन घंटे यूँ ही निकल जाएंगे। गर्मियों के दिनों में मध्यांतर के समय हॉल से बाहर निकलने पर एयरकंडीशनर का सा आनंद मिलता था।
हॉल की सीटें दर्शकों की कृपा से जितनी उधड़ सकती थीं , उतनी जगह जगह से उधड़कर , उनकी ये छेड़खानी बयान करने से नहीं चूकतीं थी,
उन्होंने भी अपनी रक्षा के लिए खटमलों को बसा रखा था। उँगलियाँ बार बार तशरीफ़ के किसी न किसी हिस्से को ढाँढस बंधाने दौड़ती ही रहती थी। सीट के साथ ये जंग , फ़िल्म का ही हिस्सा थी।
बहरहाल, इन छोटी मोटी परेशानियों से फ़िल्म देखने का आकर्षण , कहाँ कम होने वाला था भला?
शो शुरू होने के पंदरह बीस मिनट पहले हॉल की टीन की छत पर लगा माइक ये कह कर बजना शुरू कर देता कि,
“बेदर्दी बालमा तुझको मेरा मन याद करता है”
गाँव के सारे लोग यही समझते थे कि ये गाना उनके लिए ही बज रहा है , उनके हॉल की तरफ बढ़ते कदम तेज होने लगते।
इस गाने के खत्म होते ही, ये उलाहना देता गीत भी बजने लगता
“जा रे जा ओ हरजाई, देखी तेरी दिलदारी”
कदम थोड़े और तेज हो जाते, साथ चल रहे दोस्त को गालियां भी पड़ती कि कमबख्त आज तेरे कारण ” प्रेमजीत लाल का टेनिस वाला विज्ञापन छूटेगा, क्या चमकते सफेद तौलिए से अपना चेहरा साफ करता नज़र आता है।
साथ में, आनी वाली फिल्मों के ट्रेलर छूटने का जघन्य अपराध भी आज तेरे सर पर ही होगा, टूटी हुई चप्पल को हाथ में लेकर अब जल्दी चलो, अभी तो पिक्चर की टिकट लेने की दंगल भी जीतनी है।
कोई अग्रिम टिकट लेने की व्यवस्था नहीं थी। दमखम है तो टिकट कटा लो। टिकट कटाने वाले शूरवीर अलग ही होते थे। ५ इंच लंबे और उतने ही चौड़े एक सुराख में ५ हाथ किस तरह घुस जाते थे, ये अब आश्चर्य का विषय लगता है। टिकट मिल जाने पर शरीर का सारा जोर लगाने के बाद,उस सुराख से वो हाथ सही सलामत निकल कर अपनी वीरगाथा खुद बयान कर देता।
इन जाँबाजों के हाथों पर बने खरोंच के निशान, कई किस्से भी बयान करते नज़र आते, कि ये वाला निशान तब पैदा हुआ, जब अमुक फ़िल्म देखते वक़्त टाटानगर की नटराज सिनेमा में वो
किस तरह एक योद्धा की तरह भीड़ को चीर कर टिकट लेके आया था, पुलिस के एक दो डंडे भी हंसते हंसते झेल गया था।
इनका रुतबा अलग ही होता था, इंटरवल में फिर साथ आये दोस्त ही झालमुड़ी और मूंगफली से , इनका ये कर्ज उतारने की कोशिश करते, सिवाय उस दोस्त के जिसने इसको पीछे से पकड़ कर टिकट खिड़की की भीड़ से निकाला था।
कुछ बेचारे अपनी जान पहचान की महिलाओं को तलाशते फिरते और दिखने पर महिलाओं की अपेक्षाकृत थोड़ी कम भीड़ वाली टिकट खिड़की से टिकट लेने का आग्रह करके अपनी नामर्दगी का सबूत भी देते।
जान पहचान वाली महिला की यदा कदा कुटिल मुस्कान ,ये जताने से नहीं चूकती कि मर्द बनने की सारी हवा निकल गयी तो आज?
आज के इस युग में ऑनलाइन टिकट बुक करके या सभ्य तरीके से कतार में खड़े होकर टिकट लेने वाले लोग उस वीरता को शायद ही समझ पाएं।
हॉल के अंदर जाने से पहले गलियारे में खड़े होकर आने वाली फिल्मों के पोस्टर देखने का आनंद भी अलग था। दूसरी घंटी बजते ही हॉल की लाइट बुझा दी जाती, अब हॉल में टॉर्चलाइट पकड़े उस महानुभाव को तलाशने का काम शुरू होता जो खाली सीट दिखाने में मदद करता, टिकट पर कोई नंबर नहीं होता था। स्कूल से भाग कर फ़िल्म देखने आए छात्र इसी अंधेरे की बाट जोहते रहते कि अब हॉल के अंदर जाने का मुनासिब वक़्त आ चुका था।
बीड़ी ,सिगरेट और तंबाकू की गंध से भरा हॉल, एक अलग ही तरह का नशा पैदा करता था, जिसको झेल पाने के फेफड़े भी अलग ही होते थे, आज कल इनका उत्पादन बंद हो चुका है।
फ़िल्म की रील १५ -१६ गोलाकार लोहे के डब्बों में आती थी। उस जमाने के फ़िल्म के पर्दों की भी इज्जत थी, आज के मल्टीप्लेक्स के पर्दों की तरह मुँह उघाड़ के नहीं रहते थे, नाटक के मंच की तरह दो रंगीन पर्दे ,पहले धीरे धीरे सरक कर कोने
में खिसकते , तब जाकर फ़िल्म का सफेद पर्दा हाज़िर होता।
हॉल की लाइट बुझने पर, दर्शकों के पीठ पीछे बनी दीवार पर बने ऊँचे सुराख से जब फोकस पर्दे पर पड़ता, तो अचानक दर्शकों का शोर शांत होने लगता।
पिक्चर शुरू होने के पांच सात मिनट बाद, कुछ लेट लतीफ भी पहुंचते ,अपनी सीट ढूंढते हुए एक दो के पांव पर अपना पांव धरते और बैठ कर बगल वाले से ये प्रश्न करते,
भाई कितनी पिक्चर निकल गयी? और ये आशा भी करते कि अभी तक जो आंखों से देखी है जरा उनके कानों तक भी पहुंचा दें।
कुछ ,एक ही फ़िल्म को बार बार देखने वाले शोधकर्ता, फ़िल्म का हर एक डायलॉग याद करके, धीमे स्वरों में उसको दोहराकर, चल रहे सीन की प्रतिध्वनि पेश करने में अपनी शान समझते।
कुछ के हाथ , फिल्मी मारपीट के समय, हीरो के हाथ के साथ साथ ही चलने लगते।
बिंदु और हेलेन के डांस पर न जाने कितने सिक्के पर्दे की ओर फेंके जाते, वो सिक्के मिलने तो इन कलाकारों को चाहिए थे, पर हॉल के मालिक और कर्मचारियों ने आज तक उनको नहीं भेजे।
एक और किंवदंती भी थी, कि प्रोजेक्टर की जो लाइट पर्दे पर पड़ रही है अगर सिक्के उछल कर उसे छू गए तो पर्दा जल जाएगा!!!
बहुत से शहरों में जल चुका था, इसके चश्मदीद गवाह भी थे, मेरे गाँव का पर्दा इससे अछूता रहा।
किसी ने तबियत से उछाला ही नहीं !!!
बेचारे दुष्यंत कुमार साहब कहते ही रह गये और यहाँ हमारे गाँव वालों से एक सिक्का भी ढंग से न उछल पाया!!!
एक गाने पर जब हेलेन ये कह रही थी कि,
“पिया तू अब तो आजा”
एक दर्शक इतना भाव विभोर हो उठा, कि उसके मुँह से बरबस ही निकल पड़ा, “आएं क्या”?
वैसे तो गाँव के सिनेमा प्रेमी शांत ही थे, बस रील बदलते वक्त या बिजली चले जाने के बाद फिर आने पर चल रहा दृश्य , अगर थोडा आगे खिसक के शुरू होता , तब हो हल्ला करने से नहीं चूकते, कि फ़िल्म वहीं से शुरू करो, कभी कभी दर्शकों की मांग मान भी ली जाती, और कभी शोर में ज्यादा दम नहीं होने पर फ़िल्म वैसे ही जारी रहती, उस समय दर्शक फिर ये कहते हुए ही निकलते,कि कमबख्तों ने आज फ़िल्म काट ली, पूरे पैसे वसूल नहीं हुए।
उस जमाने में, राजेश खन्ना को फिल्मी पर्दे पर मरने का इतना शौक था, कि दर्शकों का तो दिल ही टूट जाता , हॉल से निकल कर यही उद्गार व्यक्त करते, धत, एक दम मूड खराब कर दिया मरकर,
नायक भी कभी मर सकता है क्या?
संवेदनशील महिलायें भी कहाँ पीछे रहने वाली थी, वो भी रोते बिलखते ही निकलती जैसे कि राजेश खन्ना तो सचमुच में मर गये हों।
कुछ थोड़ी बहादुर किस्म की भी थीं, जिनकी आंख सिर्फ भर आयी थी टपकी नहीं, वो छुपा जाती और कह उठती, अरे ये तो फ़िल्म है, इसे देख कर कोई रोता है क्या?
फ़िल्म “हाथी मेरे साथी” में राजेश खन्ना तो सही सलामत रहे , पर रामू हाथी को गोली मार दी गयी, इस हादसे से एक दर्शक इस कदर आहत हुआ कि उसने दीवार पर लगे पोस्टर में, के. एन.सिंह साहब की फ़ोटो पर गोबर मल दिया, तब जाके उसके कलेजे में थोड़ी ठंडक पड़ी।
जिन बेचारों को फ़िल्म देखने का मौका नहीं मिलता, वो कहानी सुनकर ही संतोष कर लेते या फिर हॉल के आस पास बनी पान की दुकानों में लटके फ़िल्म के दृश्यों को देख कर मन बहलाते। पान वाला भी इन फोकटियों को देख कर बोल पड़ता,कि कुछ चाहिए तो बोलो, नहीं तो अपना रास्ता नापो।
फ़िल्म के कुछ कहानी वाचक भी अलग सी शान रखते थे, तीन घंटे की फ़िल्म, ये लगभग तीन घंटों में ही सुनाते थे, पार्श्व संगीत और गानों के साथ। साथ ही अपनी विशेष राय भी देते रहते थे।लोग बड़ी श्रद्धा से इन कथाओं का उपभोग करते थे।
एक बेचारे को कहानी सुनते वक़्त ही लघु शंका के लिए जाना पड़ा, तो बोल पड़ा , असलम भाई ,थोड़ा रुकिए , मैं अभी गया और अभी आया। दूसरों को ये गुजारिश नागवार गुजरी, वे भी बोल पड़े, ये सब काम तो मध्यांतर में ही करने के हैं।
एक बार ननिहाल में, बिहार टॉकीज में “अमर प्रेम”देखने गया था, घर के दस बारह लोग साथ में थे, फ़िल्म हम बच्चों के पल्ले क्या पड़नी थी, हमें तो मध्यांतर का बेसब्री से इंतजार था, फांटा और चिप्स की पैकेट जो मिलने वाली थी। हमारे लिए तो फ़िल्म में ये दो चीजें ही सबसे विशेष थीं।
फिर जैसे ही, बोतल और चिप्स की पैकेट खाली हुई,
दिमाग में, ये गीत गूंजने लगा,
“ये क्या हुआ, कैसे हुआ, कब हुआ, क्यूँ हुआ”
“मेरा नाम जोकर” से, इसलिए भी ज्यादा प्रभावित हुए थे कि इसमें दो मध्यांतर थे!!!
मुग़ले आज़म और शोले के डायलॉग न जाने कितनी बार बैठ के सुने होंगे, “संगतराश” शब्द जिंदगी में पहली और आखिरी बार यहीं सुना था। उसके बाद इस शब्द ने फिर खुदकुशी ही कर ली। लंबू जी, टिंकू जी और सरकाइलो खटिया के साथ इसका गुज़ारा वैसे भी मुश्किल ही था।अब तो माशाअल्लाह, गालियाँ भी पर्दो पर अभिव्यक्ति के नाम पर उतर आई हैं। फिल्में इतनी तो बिकाऊ नहीं हुई थीं उस दौर में!!!!
खैर, इसमें निरीह फिल्मवालों का क्या दोष, इन्होंने कोई समाज सुधार का बीड़ा थोड़े ही उठाया हुआ है। ये तो दर्शक जो चाहते हैं, वही परोस देते हैं आजकल। धंधे में वैसे भी लाज शरम का क्या काम जी?
मेरा बचपन में,अपना मत था कि कालिया भले ही नमक का कर्ज अदा नहीं कर पाया हो, बसंती के डांस तक तो जिंदा रहना चाहिए था, सांभा ने भी कौन सा तीर मार लिया था? बस पहाड़ी पर बैठा ही तो रहता था। पर सलीम जावेद साहब को मैं मशवरा देने वाला कौन था भला?
बचपन में हमारे नसीब में अच्छी सामाजिक फिल्में ही थीं, जो राजश्री प्रोडक्शन वाले बनाते थे।
बॉबी और जूली जैसी फिल्मों को बंडल फ़िल्म कहते थे, जो वयस्कों के लिए थी।
हम भी फिर बददुआएँ ही देते थे, कि सचमुच ही चाबी खो जाए , रहो एक कमरे में बंद और भूखे मरो!!
धीरे धीरे ये समझ भी आ गयी, फिल्मों का आनंद लेते वक्त, अपने दिमाग का कम से कम इस्तेमाल करना है। तेज दिमाग मजे को किरकिरा करके ही छोड़ता है।
अब भी कभी कभी फ़िल्म तो देख आते हैं, पर वो दीवानगी और जुनून उस दौर के साथ ही कहीं रह गया।
यदा कदा ,भूले बिसरे ये अनुस्मरण लौट ही आतें हैं, उस अहसास को ताजा करने!!!!