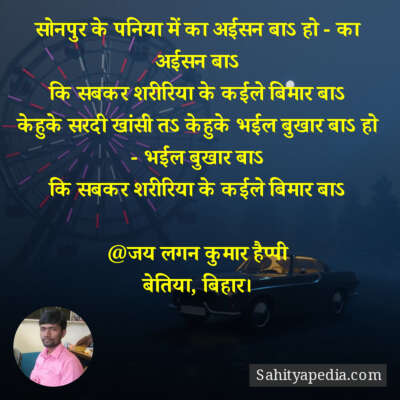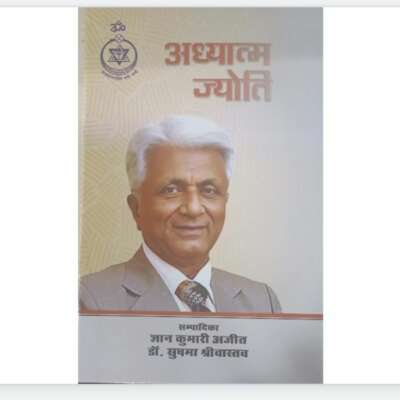प्रेम पर्दे के जाने “””””””””””””””””””””””'”””””””””””””””””””””””””””””””””

मैं, मेरे ख़त के मुसाफ़िर
क्या ये प्रेम पर्दे के जाने को ?
रहती कहती ये पड़ी यहीं हैं
जानती मगर अब ये भी नहीं
जवानी, यौवन रही कामुक काम
तड़प – तड़प उठी कहर मन में
ये कसर बाकी है पर न जानें ये
तन सौंदर्य थी पर भोग नहीं कोई
ये सफ़र में कौन रहा किस रन्ध्र में
बता दूं कह नहीं पाता मैं करूण को
रह-रह यह देती किसे पन्थ के महफ़िल
महक नहीं मेरे प्रिय/प्रियतमा तो ही नहीं
हर एक में ढूंढू पर राह नहीं हल नहीं
कुदरत के लिए कुदरत को पाने को
तुझे पाने की तमन्ना पहले, बस अब नहीं
तेरे यौवन बदन किसके भोग के सज रही
ख्वाब बंजारे-सी रहती हृदय तो और पाने को
समा जाता हूं खुद में, बहा देता, दहलीज़ पे नहीं
न कोई अपनत्व, न ही बदन को कोई भोग पाने
किस कदर सृजन महकेंगे, मेरे सफ़र के लिए
तेरे स्पर्श की अनुभूति कल्पनीय है पर तू नहीं
मुखरे कमल खिलती पंक जैसे मानो नव कण
करंट उर में रहती नस नस में झुनझुन सी तड़प
तुझे पाता हूं अपने ऊपर कभी तेरे ऊपर खुद को
किस कसमसाई से चुम्बन अहा-अहा भर देता
तुझे बांह में जकड़ जोर से पकड़ असंतुष्ट – सा
टूट पड़ता तुझपे तेरे समर्पण के समंदर के भव में
मसल-मसल के जन्नत की खुशामद आनन्द भरता
निचोड़-निचोड़ के केवल तुझे पाता, पाने को है
परिणय बंधन में एक हमसफ़र हैं ये अर्द्गागिनी हैं
मेरे साथ चलने को, सिने से लगाने को मुझको
खड़े हैं मेरी नैया के खैवया हैं शुरू हैं जाने को