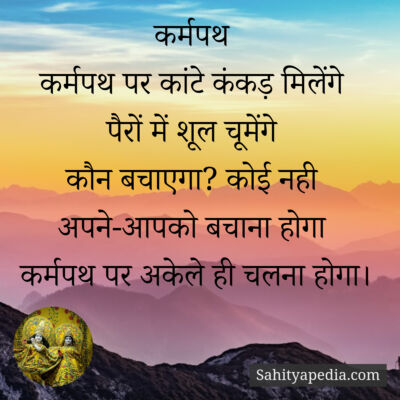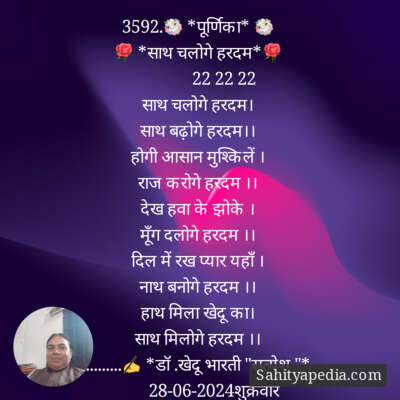प्रेमचंद के उपन्यासों में दलित विमर्श / MUSAFIR BAITHA

हिंदी साहित्य में संगठित एवं सुनियोजित चेतनापरक दलित विमर्श बहुत इधर की बात है. सन 1960 के दशक में अम्बेडकरवादी चेतना से उपजे मराठी दलित साहित्य आंदोलन के प्रभाव में यह यहाँ आया. हिंदी में दलित साहित्यकारों की खेप बीसवीं शताब्दी के अंतिम दशक में आकार सक्रिय होती है जहाँ दलित साहित्यकार मोहनदास नैमिशराय की आत्मकथा ‘अपने-अपने पिंजड़े’ 1995 में प्रकाशित होकर पहली हिंदी दलित आत्मकथा बनती है. इसी समय आत्मकथाओं के अलावा कविता, कहानी, नाटक, आलोचना सहित तमाम विधाओं में दलित लेखक की हस्तक्षेपकारी भूमिका की शुरुआत होती है. गौरतलब है कि हिंदी ही नहीं मराठी में दलित विमर्श की शुरुआत होने के पर्याप्त पहले सन 1905 से 1936 के बीच प्रेमचंद ने दलितों से सम्बधित प्रश्नों एवं समस्याओं को गहरे पैठ कर अपनी कहानियों, उपन्यासों, हंस पत्रिका के अपने संपादकीयों एवं अन्य वैचारिक लेखों के जरिये बड़ी संजीदगी से उठाया.
‘प्रेमचंद के उपन्यासों में दलित विमर्श’ विषय पर बात करने के क्रम में यह नोट करना भी आवश्यक है कि कोई जरूरी नहीं कि किसी के दलित चिंतन में दलित चेतना हो ही, जबकि दलित साहित्य को आवश्यक रूप से अम्बेडकरवादी, व्यवस्थाविरोधी, वर्णवाद-ब्राह्मणवाद-सामंतवाद विरोधी होकर चेतनापरक होना है, सरोकारी होना है. इसलिए, महज दलित चिंतन एवं दलित विमर्श दलित साहित्य का अभीष्ट अथवा प्राप्य नहीं हो सकता. स्वानुभूत अथवा सहानुभूत के साथ यहाँ चेतना का तत्व समाहित होना जरूरी है. दलित चेतना से रहित रचना दलित साहित्य का अंग नहीं बन सकती, किसी दलित रचनाकार की भी नहीं. मुख्यधारा कहे जाने वाले पारंपरिक हिंदी साहित्य का जो प्रगतिवाद अथवा वामपंथ है उसमें आये दलित संदर्भों में प्रायः दलित चेतना नहीं है. दलितों पर पर्याप्त सरोकारी रचनात्मक लेखन कर भी प्रेमचंद हिंदी में दलित चेतना के पुरस्कर्ता नहीं है, क्योंकि उनकी चेतना में न तो निरंतरता है न ही स्थिरता. गोदान जैसे ‘सेलेब्रिटी’ उपन्यास तक में गांधीवाद, दलित चेतना एवं वामपंथ तीनों गड्डमड्ड हो एक साथ आता है. बहरहाल, दलित विमर्श की स्वागतयोग्य एवं दूरदर्शी शुरुआत उनसे जरूर होती है.
सन 1910 से 1940 के बीच लगभग तीन दशकों का हिंदी साहित्य गाँधी के गहरे प्रभाव में लिखा गया. दलित चेतना के एक्का-दुक्का पुट को छोड़ दें तो इसी अवधि के लेखक प्रेमचंद के यहाँ भी प्रायः गांधीवादी नजरिये से स्त्री एवं दलित प्रश्नों को उठाया गया है जिनमें अस्पृश्यता, मद्यनिषेध, अहिंसा आदि के आदर्श को ही नैतिक उपदेश की छौंक के साथ प्रस्तुत किया गया है. जबकि सम्यक दलित चेतना गोदान, सद्गति, ठाकुर का कुआँ, कफ़न जैसी अग्रगण्य मान्य उत्तरवर्ती रचनाओं में भी नहीं है. गांधी की तरह ही वर्णभेद के खांचे में ही छुआछूत एवं अन्य विभेद व समस्याओं के निवारण की पैरवी तथा ब्राह्मणी एवं सामंती तत्वों की मुखालफत प्रेमचंद के यहाँ है. तथापि यह रेखांकित करने योग्य है कि हिंदी में अबतक दलित प्रश्नों पर दलित लेखकों के अलावा सबसे ज्यादा प्रेमचंद ने ही रचनात्मक साहित्य लिखा है.
प्रेमचंद ने अपनी रचनाशीलता के आरंभिक चरण में जहाँ सामंत वर्ग को केन्द्र में रखा था, वहीं आगे चलकर उनके कथा साहित्य के केन्द्र में मध्य वर्ग और और अंतिम चरण में समाज के सर्वाधिक दबे-कुचले लोग हैं. सन 1910 से 1936 के बीच उनकी लगभग 300 प्रकाशित कहानियों में से कोई 40 कहानियां दलित, वंचित एवं विपन्न तथा कमजोर वर्गों से संबंधित हैं, जिनमें से एक दर्जन से अधिक कहानियां तो सीधे दलित जीवन को संबोधित हैं. यह रोचक तथ्य है कि ‘दोनों तरफ से’ नामक प्रेमचंद की पहली प्रकाशित कहानी ही दलित सरोकार वाली है.
प्रेमचंद के उपन्यासों को दलित विमर्श के संदर्भ में मूल्यांकन करने से पूर्व उनके लेखन काल की दलित समस्याओं पर भी राजनीतिज्ञों की सोच, सामाजिक मान्यताओं, बुद्धिजीवियों, लेखकों की धारणाओं, विचारों आदि को भी ध्यान में रखना आवश्यक है, क्योंकि इसी दौर में स्वतंत्रता आंदोलन, हिंदू महासभा, गाँधी, अम्बेडकर आदि के दृष्टिकोण एवं आंदोलन समाज में अपनी अपनी तरह से प्रभावकारी भूमिका में थे. दलितों के लिए अम्बेडकर द्वारा पृथक निर्वाचन क्षेत्र की मांग के विरुद्ध थे गाँधी और प्रेमचंद भी गाँधी की इस दृष्टि को राष्ट्रीय भावना करार दे रहे थे. प्रेमचंद अपने प्रारंभिक रचनाकार जीवन में जहाँ आर्य समाज से प्रभावित दिखाई पड़ते हैं, फ़िर गाँधीवादी, वहीँ अंतिम दौर में वे खंडित प्रगतिशीलता एवं वामपंथ के साथ हैं. एक ओर वे अपनी रचनाओं में हृदय-परिवर्तन, रामराज्य, ट्रस्टीशिप जैसे अव्यवहारिक गांधीवादी आदर्श रखते हैं तो दूसरी ओर दलितों को शराब न पीने, मरे जानवरों का मांस न खाने की नसीहतें भी देते हैं. ये गाँधीवादी मूल्य उनके दलित अन्तर्कथाओं वाले कर्मभूमि, रंगभूमि एवं गोदान जैसे अंतिम उपन्यास में भी अनुस्यूत हैं. गोदान में हालांकि कुछ दलित चरित्रों में क्रांतिकारिता एवं विद्रोह का भी समावेश है. कर्मभूमि के पात्रों में से बूढ़ी सलोनी भी है जिसे हाकिम जब लगान वसूल करने के दरम्यान हंटर मारता है तो वह सरेआम उसके मुंह पर थूक देती है. हालाँकि ‘कर्मभूमि’ में एक आत्मलोची दलित पात्र को सुधारवादी चरित्र में प्रस्तुत किये जाने की बहुतेरे दलित लेखकगण आलोचना करते हैं. रंगभूमि का नायकत्व प्रेमचंद सूरदास नामक दलित को सौंपते हैं जो विद्रोही तेवर का है. हालांकि प्रेमचंद की एक सौ पचीसवीं जयंती के मौके पर दलित साहित्यकारों के एक गुट ने अपनी आपत्ति दर्ज़ कराई कि प्रेमचंद एक खास दलित जाति को इस उपन्यास और कफ़न कहानी में अपमानजनक ढंग से बरतते हैं. उनका आरोप था कि प्रेमचंद मानते हैं कि दलितों में गन्दी आदतें होती हैं और वे आदतन गन्दा काम करते हैं. उन्हीं दिनों वामपंथी चिंतक मुद्राराक्षस ने प्रेमचन्द के कथा साहित्य के बहुजन दृष्टि से पुनर्पाठ की मांग उठाते हुए ‘कफन’ कहानी के ब्याज से सवाल उठाया कि क्या स्थिति बनती अगर कफ़न के पैसे से दारू और पूड़ी जीमने वाले व्यक्ति दलित नहीं बल्कि ब्राह्मण बाप-बेटे होते?
‘गोदान’ को कुछ वामपंथी आलोचक प्रेमचंद के गांधीवाद से मोहभंग का उपन्यास कहते हैं, क्योंकि वे यह सिद्ध करना चाहते हैं कि प्रेमचंद की गांधी निष्ठा बाद में जाकर तिरोहित हो गयी. गोदान के बहुप्रशंसित दलित सिलिया और पंडित मातादीन के प्रेम प्रसंग में चमारों द्वारा मातादीन के मुंह में हड्डी डलवाकर प्रेमचंद उसके पंडितपन को तोड़ते हैं एवं चमारों की ओर से यह भी कहलवाते हैं कि मुदा हम तो ब्राह्मण नहीं बन सकते पर पंडित को उसकी जात से च्युत कर सकते हैं. प्रेमचंद द्वारा चमारों से यह कथित क्रांतिकारिता करवाना उच्च जातीय ग्रंथि तोड़वाने में समर्थ नहीं हो सकती. यह संदेहास्पद है कि किसी ब्राह्मण द्वारा मांस खा लेने मात्र से उसकी जात चली जाएगी. क्या प्रेमचंद के जमाने में ही मांस खाने वाले ब्राह्मण नहीं रहे होंगे?
दलित हलके से प्रेमचंद की आलोचना पुरजोर हुई है. कबीर विषयक अपनी आलोचना श्रृंखला की पुस्तकों से प्रसिद्ध हुए दलित लेखक डा. धर्मवीर ने भी प्रेमचंद के यथार्थवादी लेखन और दलित उत्पीड़न से सम्बंधित आधारभूत स्थापनाओं पर गहरे प्रश्नचिन्ह लगाए हैं. ‘सामंत का मुंशी’ एवं ‘प्रेमचंद की नीली आँखें’ नामक अपनी धुर आलोचना पुस्तकों को तो डा. धर्मवीर ने प्रेमचंद की आलोचना में भी एकाग्र किया है. हालांकि प्रेमचंद पर उनकी आलोचना लगभग एकतरफा एवं एकांगी है. जो हो, प्रेमचंद ही नहीं हिंदी जगत की सर्वश्रेष्ठ कहानी में शुमार ‘कफ़न’ एवं उनका कीर्ति-स्तंभ साबित उपन्यास ‘गोदान’ खास विवादों के घेरे में आए. जबकि दलित आलोचक कँवल भारती तक का मानना है कि हिंदी साहित्य के 1936 तक के कालखंड में प्रेमचंद अकेले लेखक हैं जिनसे साहित्य में दलित विमर्श की शुरुआत होती है.
अपनी वार्ता का समाहार करते हुए कहना चाहूँगा कि तमाम सहमतियों-असहमतियों के बावजूद प्रेमचंद अपने समय के एक ऐसे दृष्टिपूर्ण एवं समाज-सजग अप्रतिम रचनाकार हैं जिन्होंने गल्प एवं आदर्श में गोता लगाते हिंदी साहित्य में यथार्थ को स्वीकार्य बनाया, पाठकों की रुचि संस्कारित एवं मर्यादित की तथा साहित्य को अधिक जमीनी और जीवंत बनाकर सीधे समाज के प्रश्नों से जोड़ा. किसान, मजदूर, दलित, वंचित, विकलांग, स्त्री, छोटे कामगार, बच्चों आदि के हित एवं समस्याओं को अपने लेखन में वाणी दी. कहें कि हिंदी उपन्यास को स्तरीयता और सही आकार देने का युगान्तकारी कार्य प्रेमचंद ने किया. प्रेमचंद के समकालीन लेखकों के साथ जब हम प्रेमचंद की तुलना और मूल्यांकन करते हैं तो फरक दिखाई पड़ता है. प्रेमचंद साफ़ अलग विराट व्यक्तित्व के रचनाकार के रूप में सामने आते हैं. उनके यहाँ समकालीन छायावादी युग का अमूर्त स्वप्निल आदर्श भरसक ही दिखाई देता है. बांग्ला के प्रसिद्ध साहित्यकार बंकिमचन्द्र चटोपाध्याय द्वारा हिंदी-उर्दू के अप्रतिम कथाशिल्पी प्रेमचंद को उपन्यास सम्राट की संज्ञा दिया जाना यों ही नहीं है.
प्रेमचंद जीवन के लेखक है, जिजीविषा के कलमकार हैं अतः दलित लेखक-पाठक समाज भी प्रेमचंद को अपने करीब पाता है. दलितों-वंचितों के प्रति प्रेमचंद की रचनागत पक्षधरता एवं सहानुभूति निर्विवाद है. प्रेमचंद साहित्य का अध्ययन करना दलित समेत, हर उस व्यक्ति के लिए उपादेय है, काम का है जो साहित्य को मनुष्य की चिंताओं के लिए जरूरी मानता है. देश को स्वाधीन हुए लगभग सत्तर साल होने को हैं, बावजूद, लोकतंत्र में समाज का जो चिंताजनक हाल है, उसके हिसाब से प्रेमचंद के उपन्यासों एवं तमाम अन्य विधा की रचनाओं में आये विचार उनके अपने समय में जितने प्रासंगिक थे उससे कहीं ज्यादा आज मौजूं हैं. दलित समाज के संबंध में तो यह बात और लागू होती है. प्रेमचंद के दलित ‘कंसर्न’ की महत्ता इस बात से भी परिलक्षित है कि आज भी दलित समाज की दयनीयता जारी है जबकि प्रेमचंद के पराधीन भारत से अब हम स्वाधीन देश के नागरिक में तब्दील हैं. दलित साहित्यकारों का स्वानुभूत लेखन जोरों पर है लेकिन आज भी दलित प्रश्नों पर ईमानदार कलम चलाने गैरदलित लेखकों का टोटा ही है. और, जबतक ऐसा है, साहित्य में प्रेमचंदधर्मी लेखकों की जरूरत लगातार बनी रहेगी.
*********************