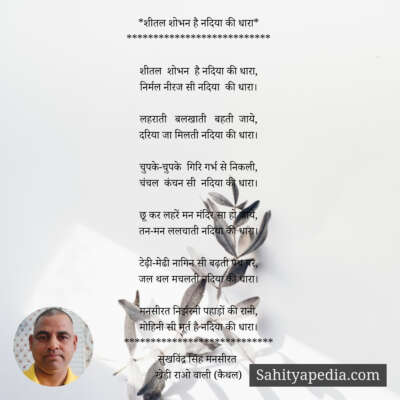प्रारंभ से भय
समाज की रूढ़ीवादी मान्यताएं
तीरों सी चुभती हैं फिर भी
रोकर – चिल्लाकर – छटपटाकर सहते हैं
क्योंकि हमें भी यही मान्यताएं
बचपन में घुट्टी में
घोलकर पिलाई गयीं हैं
इसीलिये हम
गूंगें – बहरे – अंधे बनकर
पड़े रहते हैं और सोचते हैं
कि कोई तो
बोलने वाला – सुनने वाला – देखने वाला हो
जो शुरुआत करे
इन मान्यताओं के विरूद्ध
आवाज उठाने की
यूँ हीं पड़े सोचते
सड़ – गल – मर जायेगें
परन्तु अपनी कमजोरियों का
इलाज न करेगें
अगर किया
तो कही इनके विरूद्ध
हमें ही ना करनी पड़े
अपनी आत्मा शुद्ध ।
स्वरचित एवं मौलिक
( ममता सिंह देवा , 20/05/87 )