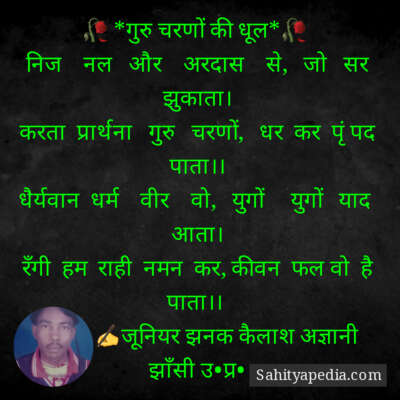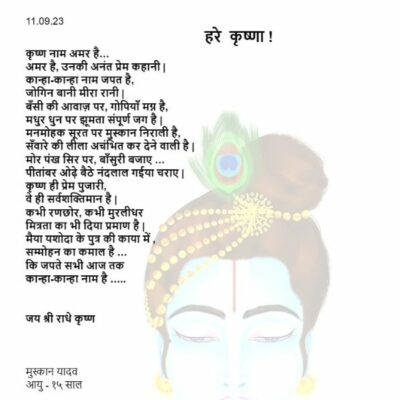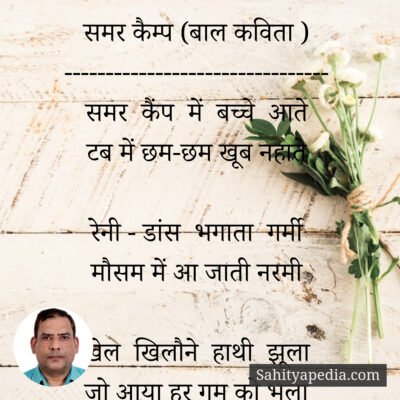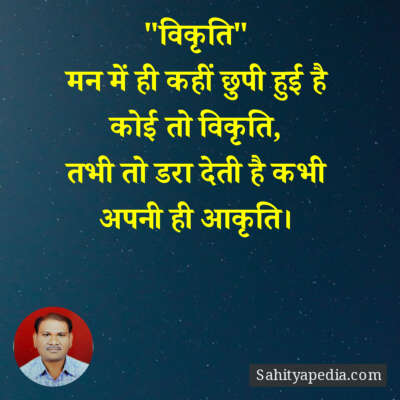#प्रसंगवश

#प्रसंगवश
■ आख़िर क्या दोष था प्रतापभानु, अरिमर्दन, धरमरुचि का…?
★ प्रश्न अस्पृश्यता नहीं पवित्रता का।
【प्रणय प्रभात】
छोटी-छोटी बातों पर बड़े-बड़े विवाद आज हमारे देश की पहचान बन चुके हैं। इस अनापेक्षित व असहनीय परिवेश के निर्माण का कारण क्षुद्र सोच, अमानवीय कृत्य व ध्रुवीकरण पर निर्भर कुत्सित राजनीति है या टीआरपी के लिए हर “चिंगारी” को “दावानल” बना डालने के प्रयास में दिन-रात जुटी बिकाऊ व बेशर्म मीडिया, यह एक अलग शोध का विषय है। तथापि जो परिदृश्य सामने हैं, वो चिंतन करने और मुखर होने के लिए आए दिन उत्प्रेरित करते हैं।
विशेष कर उन्हें, जिनके पास अपना अध्ययन, समयोचित चिंतन व तर्क प्रकटीकरण की थोड़ी सी भी सामर्थ्य है। उन्हें भी, जो धर्म-संस्कृति व राष्ट्र के प्रति निष्ठावान हैं और अपनी जागृत चेतना का पक्ष साहस के साथ रख पाने में समर्थ हैं। ईश्वरीय अनुकम्पा व गुरुजनों की अनंत कृपा से। मेरा सौभाग्य है कि मैं इस विचारशील समुदाय की एक इकाई हूँ। सम्भवतः इसीलिए अपनी बात आपकी सोच के सुपुर्द करता आया हूँ। आज भी कर रहा हूँ। बिना किसी भय, संकोच, आग्रह, दुराग्रह या पूर्वाग्रह के। एक सामयिक व ज्वलंत विषय के परिप्रेक्ष्य में। अपने जीवन के मार्गदर्शी महाग्रंथ श्री रामचरित मानस जी के पावन आलोक में।
जो सनातनी व मानसपाठी हैं, वो मेरी बात सहजयता से समझ पाएंगे। जो किसी भी कारणवश मानस जी की विषय-वस्तु से अनभिज्ञ हैं, उनके लिए बात को सरल बनाना मेरा दायित्व है। सर्वविदित है कि सात सौपानों में समाहित श्री रामचरित मानस का प्रथम सौपान “बाल-कांड” है। जिसमें प्रभु श्री राम के अवतरण व बाल्यकाल का आद्योपांत वर्णन है। इसी सौपान में प्रभु श्री के प्राकट्य के पांच प्रमुख कारणों का उल्लेख संक्षेप में गोस्वामी तुलसी दास जी द्वारा किया गया है। इन पांच कारणों में चार आसानी से समझ में आते हैं और स्वीकार्य होते हैं। तथापि एक कारण ऐसा है, जो यक्ष-प्रश्न बन कर मानसिक व बौद्धिक चेतना को झकझोरता है। इस कारण के केंद्र में है “राजा प्रतापभानु।” जो परम्-प्रतापी, प्रजापालक व धर्मनिष्ठ होने के बाद भी न केवल शापित हुआ, वरन अपने अनुज व मंत्री के साथ अगले जन्म में राक्षस योनि में उत्पन्न हुआ। जिसे “रावण” के रूप में जाना गया। यही नहीं, धर्म-पथ पर चलने वाले उसके छोटे भाई “अरिमर्दन” को “कुंभकर्ण” व मंत्री “धर्मरुचि” को “विभीषण” के रूप में जन्म लेना पड़ा। जिनके उद्धार हेतु प्रभु श्री नारायण को “नर-रूप” में धरा-धाम पर आना और विविध लीलाएं करना पड़ा।
उक्त प्रसंग का दुःखद पक्ष यह है कि तीनों ने उस अपराध का दंड पाया, जो उनके कर्म तो दूर कल्पना तक में नहीं था। तीनों शिकार बने एक छल के, जो पूर्णतः सुनियोजित व प्रायोजित था।
कथा प्रसंग के अनुसार युद्ध में परास्त व राज्य से विमुख एक शत्रु ने एक साधु का छद्म वेश धारण कर राजा प्रतापभानु को अपनी कुटिल चाल में फंसा लिया और उसे भाई व सचिव सहित घोर पाप व ब्रह्म-अपराध का भागी (धर्म-भ्रष्ट) बना दिया। छल का शिकार प्रतापभानु निरपराध हो कर भी न केवल अधर्म कर बैठा, वरन संत-समाज का कोप-भाजन भी बन गया। जबकि सत्य यह है कि उसने अधर्म किया नहीं था, छलपूर्वक उससे कराया गया था। उससे बदला लेने और उसे पथभ्रष्ट करने के उद्देश्य से। एक पूर्वाग्रही व कुंठाग्रस्त शत्रु द्वारा।
अब आप स्वयं विचार करें कि इस में प्रतापभानु का दोष क्या था? मेरे विचार से उसका दोष मात्र इतना सा था कि वो अपने शत्रु को पहचान पाने में असमर्थ रहा और उसके छलावे में आ गया। ऐसे में प्रश्न खड़ा होता है कि “क्या उसका बैरी उसे अपना मूल स्वरूप छुपाए बिना छल सकता था?” सोचेंगे तो उत्तर पाएंगे कि “कदापि नहीं।” स्पष्ट है कि सारा षड्यंत्र छद्म-नाम, छद्म-वेश और कपट-नीति के कारण सफल हुआ। यदि प्रतापभानु तत्समय उसकी वास्तविकता को जान पाता, तो उसके साथ वो सब न हुआ होता, जो दुर्योग से हुआ। न वो मायावी के वशीभूत अनुष्ठान कर देव-तुल्य विप्रजनों को भोजन में अभक्ष (मांसाहार) परोसता, न शापित होकर अपना इहलोक व परलोक बिगाड़ता। स्मरण रहे कि यह प्रकरण हज़ार दो हज़ार नहीं, लाखों वर्ष पहले का है। जो सिद्ध करता है कि सनातन के विरुद्ध कुचक्र तब भी था, जब कोई विधर्म अस्तित्व में नहीं था। पता चलता है कि धर्म के पराभव के लिए अधर्म अनादिकाल से प्रयासरत रहा है। जो आज भी विकराल रूप में विद्यमान है। मानव-रूप धारण किए बैठी “दानवी सोच” में। जो “आपदा में अवसर” तलाशती रही है। तमाम बार सफल भी हुई है। प्रमाण बीते कुछ वर्षों के संक्रमण काल ने दिए। जब फलों पर थूकने व सब्ज़ियों पर मूत्र-विसर्जन करने की घटनाएं देश के कोने-कोने से प्रकाश में आईं। क्या कोई दावा कर सकता है कि इस “घृणित सोच” पर अब पूर्ण-विराम लग चुका है। चंद सिरफ़िरों के इस कृत्य ने जहां सम्पूर्ण मानवता को लज्जित किया, वहीं अपनी बिरादरी को भी कलंकित किया, जिसके अधिकांश लोगों की इसमें न कोई भागीदारी थी, न सहमति। लगभग इसी तरह के कुकृत्य उन “अधर्मियों” ने भी किए, जिन्हें चुनावी जीत के लिए विकृत सोच वाली भीड़ चाहिए थी। अंतर इतना सा था कि उनके निशाने पर फल या सब्ज़ी नहीं, अपने ही ग्रन्थ व देव-चरित्र थे। जिस पर उन्होंने अपने मुख से “मल-मूत्र विसर्जन” का पाप किया। दुर्भाग्य की बात है कि ऐसे कुकर्मी आज भी समाज में सक्रिय हैं। सत्ता के संरक्षण में, कड़ी सुरक्षा व बड़ी भूमिका के साथ।
शर्मनाक बात तो यह है कि मानवीय समुदाय में एक ओर दिन-प्रतिदिन बढ़ते वैमनस्य को हवा-पानी देने का काम खद्दर-धारियों द्वारा किया जा रहा है। वहीं दूसरी ओर पारस्परिक अविश्वास को समाप्त करने के समयोचित प्रयासों पर बलात् प्रश्न-चिह्न लगाए जा रहे हैं। जिनका उद्देश्य या तो मात्र विरोध के लिए विरोध करना है, या फिर सुर्खी में रह कर भीड़ का सिरमौर बने रहना। कोई धर्म के नाम पर पाखंड की दुकान सलामत रखने के प्रयास में जुटा है, तो कोई विरासत में हाथ आई सियासत की भद्दी सूरत को चमकाने में। उकसाने का मंसूबा रखने वालों को न दीन से मतलब है, न दुनिया से। उनका काम बस उन्माद की आँधी का साथ देना है। बहुमत को भांप कर भीड़ के पक्ष में माहौल बनाना है। नाम व दाम की भूखी मीडिया की तरह।
आज की विडम्बना यह है कि “लोकतंत्र” व “संविधान” के नाम पर “अधिकारों का अरण्य-रोदन” हर कोई कर रहा है। बस “कर्तव्यों के अनुपालन” को लेकर “याददाश्त” दिव्यांग बनी हुई है। हम अपने हित व हक़ के लिए मरने-मारने पर आमादा हैं, पर औरों के हित के साथ खिलवाड़ के शाही शौक़ से मुक्त नहीं हो पा रहे। हम अपने सुधार से जुड़ी हर प्रक्रिया के विरोधी हो कर दूसरों के दृष्टिकोण में सुधार की आस रखते हैं। यही नहीं, हरसम्भव कोशिश करते हैं। बेतुके व बेहूदे तर्क दे कर। पूरे कुतर्क के साथ।
ऐसे में एक उदार धर्म का वर्तमान अत्यधिक विकृत व विषाक्त परिवेश में सुरक्षित कैसे माना जा सकता है? वो भी तब, जब “विधर्म” से अधिक संक्रमण “अधर्म” फैला रहा है। रही-सही कसर स्वयं को प्रगतिशील बताने वाले “कूप-मण्डूक” पूरी कर रहे हैं। जो “समष्टि” के बूते “व्यष्टि” पर प्रहार किए जा रहे हैं। मर्म तक पहुंचे बिना धर्म की मनमानी व्याख्या का रोग महामारी बनता जा रहा है। “विश्व-बंधुता” की संवाहक एक विराट संस्कृति अपनी ही धरा पर शरणार्थी बनने की कगार तक आ पहुंची है। इस माहौल में सवाल और सुधार से बचने की चेष्टा क्यों? यदि मन में चोर और ठग नहीं है तो। उजाले में आने से उजाला नहीं, केवल अंधेरा फ्लडरता है। यह सच तो याद होगा ही।
प्रश्न है कि क्या इस देश काल और वातावरण में एक “सहिष्णु सनातनी” को इतना भी अधिकार अपनी मातृभूमि पर क्यों नहीं, कि वो सामने वाले अपरिचित के सच से परिचित हो? क्या उसे यह भी अधिकार नहीं कि वो अपनी परंपरा व मान्यता के अनुसार उचित-अनुचित का विचार कर धर्म-सम्मत निर्णय अपने हित में ले सके? अतीत के की शिक्षाओं और वर्तमान के अनुभवों के आधार पर भला-बुरा तय करने का अधिकार हर बार एक सहिष्णु से ही क्यों छिने? वो भी तब, जब “लंका” जैसे परिवेश में “राम-राज्य” का ढिंढोरा पीटा जा रहा हो। “अरण्य” को “अवध” बना डालने का दम्भ भरा जा रहा हो। धर्म की रक्षा के नाम पर राजनीति की चालें चली जा रही हों।
निस्संदेह, अस्पृश्यता (छुआछूत) एक अपराध है। मानवता के मुख पर “कलंक की कालिख” के समान है। तथापि इसका अभिप्राय यह नहीं, कि “शुद्धि” को “अशुद्धि” के साथ विवाह के बंधन में बांध दिया जाए। प्रत्येक मानव अपने उदर में भोजन से निर्मित “मल” ले कर घूमता है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि वो उसे भोजन की मान्यता दे डाले। पूजा करती एक मां भी अपने गंदे बच्चे से कुछ देर के लिए दूरी बनाती है। उसी बच्चे से, जिसे साफ-सुथरा रखने के लिए वो सब कुछ सहज भाव से करती है। इबादत के लिए तैयार होता एक बाप भी चाहता है कि कुछ पलों के लिए मल-मूत्र से दूषित उसके अपने बच्चे उससे दूर रहें। चाहे वे उसे कितने ही प्यारे क्यों न हों। मां-बाप के इस समयानुकूल बर्ताव को क्या हम घृणा, वैमनस्य अथवा छुआछूत का नाम दे सकते हैं? पूछा जाए तो एक ही उत्तर होगा कि “बिल्कुल नहीं।” फिर चाहे सवाल पूछने व जवाब देने वाले का धर्म या संप्रदाय कोई सा भी हो। वस्तुतः मामला अस्पृश्यता नहीं, पवित्रता का है। जो हरेक का मौलिक अधिकार है। इसे सम्मान की दृष्टि से देखें जाने की आवश्यकता है। न कि अकारण तूल दे कर विवाद का विषय बनाए जाने की।
जहां तक बात नीति और न्याय की है, उसके कुछ अपने निहितार्थ हैं। तमाम तथ्य हैं, जिन्हें थोथे आदर्शवाद के नाम पर झुठलाना कतई उचित नहीं कहा जा सकता। कटु सत्य यह है कि “विरोधाभास” के अंधड़ में “समरसता” का दीप नहीं जलता। रीति-नीति में परस्पर विरोध जो दूरी पैदा करता है, उस पर सामंजस्य का पुल बनाया जा सकता है। जिसे अक्षुण्ण रख पाना न किसी एक पक्ष के लिए आसान है, न संभव। याद रखा जाना चाहिए कि विश्वास का एक पौधा बरसों में वृक्ष बन पाता है। जिसे अविश्वास की आंधी पल भर में धराशायी कर देती है। विश्वास बनाए रखने के लिए पहली शर्त है पारदर्शिता। जो आज “चील के घोंसले में चंदन” सी हो गई है। निश्छलता दूसरी शर्त है, जो “गूलर के फूल” की तरह दुर्लभ है। ऐसे में “गंगा-जमुनी तहज़ीब” शायद एक जुमले और मुग़ालते से अधिक कुछ नहीं। सच यह है कि अब धर्म की दो धाराएं स्वयं को एक चुम्बक की तरह मानें, जो एक हो कर भी दो ध्रुवों के प्रति समर्पित हैं।
जहां तक बात दुराव-छुपाव की है, वो किसी भी तरह ठीक नहीं। रंगे सियार के हश्र की कथा हम और आप बचपन में पढ़ ही चुके हैं। नहीं पढ़ी हो तो “पंचतंत्र” अभी भी बाज़ार में सुलभ है। आज दुनिया को “धर्म-निरपेक्षता” जैसे शब्द से अधिक आवश्यकता “छद्म-निरपेक्षता” की है। मन में कपट न हो तो न रावण की तरह भिक्षुक बनना भाए, न कालनेमि की तरह साधु बनना सुहाए। “मारीच” मायावी हो कर भी लंबे समय तक “स्वर्ण-मृग” कहाँ बना रह पाया। एक तीर ने असली रूप सामने ला दिया। “काग” बन कर आए इंद्र के पुत्र “जयंत” की भांति। छद्म-वेश अघासुर, बकासुर, धेनुकासुर, शकटासुर जैसे दैत्यों को नहीं फला साहब! आप-हम किस खेत की मूली, गाजर, शलगम या चुकंदर हैं? इसी छद्म-वेश के चक्कर में तो “पूतना” ने प्राण गंवाए और “शूर्पणखा” ने नाक-कान। भलाई इसी में है कि हम जो हैं, वही बने रहें। नहीं भूलना चाहिए कि पहचान बदल कर हम दस-बीस दिन या महीने सौ-पचास मूर्खों (बोलों) को झांसा दे सकते हैं, दुनिया और दुनिया बनाने व चलाने वाले को नहीं।
मेरा अपना मत है कि सभी को अपनी मूल पहचान पर गर्व होना चाहिएं। एक छल के लिए मां-बाप, जात-औक़ात, धर्म-मज़हब क्या छुपाना और क्यों? वो भी तब, जब अपने दीन को सब से बड़ा व महान बताना भाता हो। ईमान से दूर या पास का कोई नाता हो। बाप मालदार हो तो उसका नाम “फ़क़ीर चंद” से बदल कर “अमीर दास” नहीं किया जाता। यह बात जितनी जल्दी समझ आ जाए, उतना अच्छा। मरने के बाद स्वर्ग की चाह से बेहतर है अपने जीते-जी धरती को जन्नत बनाना। जो आपकी, हमारी, सब की पालक भी है, पोषक भी। संसार के सारे धर्म भी इस सच का उद्घोष करते आए हैं।
आवश्यकता अब इस सच को आत्मसात व अंगीकार करने की भी है कि सबके लिए सब उपयुक्त व यानुकूल नहीं होते। खाई खोदने और दूरी बढाने के बाद समय-समय पर कच्ची-पक्की पुलिया बनाने व ढहाने वाली धूर्त राजनीति के भरोसे मत रहना भूल से भी। फिर चाहे वो जिस भी दल या नेता की हो। स्वार्थ के ग़ुसलखाने में सब एक हैं। घड़ी भर में तोला, घड़ी भर में माशा। ये “भाईचारे” की बात करते-करते किस भाई को चारा और बेचारा बना डालें, इन्हें ख़ुद नहीं पता। अपने-अपने खोल में रहें और जीवन का आनंद लें। चैन से जिएं और सुक़ून से जीने दें। भगवान के लिए, ख़ुदा के वास्ते।
दिल से कुछ कर पाएं तो ही करें। वो भी दिमाग़ को एक तरफ रख कर। दिखावे का दौर लगभग बीत चुका है। थोथे दिखावे की दुकान नेताओं को चलाने दें। जो अपने बाप-दादा के नहीं हुए, तुम्हारे-हमारे कै से होंगे। पहचान बदलने और छिपाने से परहेज़ करें, कर पाएं तो। न कर पाएं तो मान लें कि न आप नेक हैं और न आपके इरादे। फिर चाहे आप जिस कुल या खानदान के हों। उपासना पद्धति व जीवन शैली सहित अनेक अंतर हैं, जो अंतर्मन की शुद्धि के बिना न आज तक समाप्त हुआ, न कल होने वाला है। भलाई इसी में है कि शाहों की बिसात के मोहरे न आप बनें न हम। प्रयास करें कि पुरखों की विरासत बनी रहे। ताकि न कोई तनाव हो, न तनातनी रहे। अंततः साधुवाद सभी वर्ग-समुदाय के उन देशवासियों को, जो उकसावे और बहकावे के बीच तनिक भी विचलित नहीं हैं तथा समय की मांग के अनुसार सही-ग़लत को समझ व परख रहे हैं। लानत उन पर, जो “वितंडावाद का पौधरोपण” करने से बाज़ नहीं आ रहे। उनका उपचार वक़्त के साथ करने को ऊपर वाला है। जिसे हम ईश्वर, अल्लाह, जीसस, वाहे-गुरु जैसे नामों से जानते और मानते हैं।
जय हिंद, जय हिंदुस्तान।।
◆सम्पादक◆
न्यूज़ & वयूज़
श्योपुर (मप्र)Y