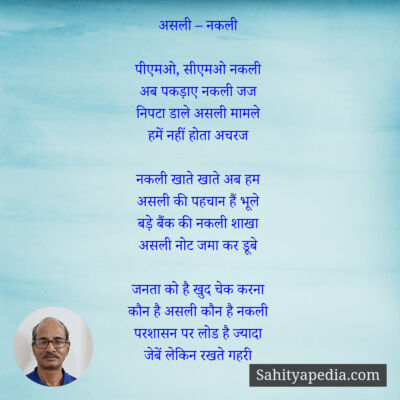पुरखों का घर – दीपक नीलपदम्

पता पिता से पाया था
मैं पुरखों के घर आया था
एक गाँव के बीच बसा पर
उसे अकेला पाया था ।
माँ बाबू से हम सुनते थे
उस घर के कितने किस्से थे
भूले नहीं कभी भी पापा
क्यों नहीं भूले पाया था ।
जर्जर एक इमारत थी वो
पुरखों की विरासत थी वो
कितने मौसम बीत चुके थे,
पर उसे अकड़ता पाया था ।
दरवाजे हठ कर बैठे थे
कितने ऐंठे कितने रूठे थे
चीख चीख कर करें शिकायत
क्यों तुमने बिसराया था ।
द्वार खुले तो मिला बरोठा,
मुझे लगा वो भी था रूठा,
मुख्य द्वार पर बड़ा सा कोठा,
वो रोने को हो आया था ।
दीवारों पर लगे थे जाले
हठ करके न हटने वाले
जैसे धक्का देके भगाएँ
कितनी मुश्किल से मनाया था ।
कभी पिताजी ने बतलाया
इस कमरे में रहते थे ताया,
गजब रसूख था, गजब नाम था
पर अब वो मुरझाया था ।
उसके आगे एक बरामदा
उससे आगे था फिर आँगन
आँगन के आगे कुछ कमरे
वक़्त वहीँ ठहराया था ।
तभी वहाँ कुछ खनक गया था
शंखनाद भी समझ गया था
देखा वहाँ एक मंदिर था
मैं कितना हर्षाया था ।
उस आँगन के कितने चर्चे
सुने हुए काका के मुख से
कितनी रौनक होती थी ये
काका ने बतलाया था ।
तभी वहां कुछ हमने देखा
दीवालों पर बचपन देखा
पापा के हाथों की छापों पे
अपनी हथेलियाँ रख आया था ।
न थी लकड़ी धुआं कोयला
न चूल्हे की ठण्डी राख़
उस रसोई में प्यार पका था
जो था अब भी पर सकुचाया था ।
मोटी थी मिटटी की दीवारें
पर पक्के रिश्ते बसते थे
छूट गया था घर आँगन वो
बाबू ने भूल न पाया था ।
ड्राइंग रूम नहीं होते थे
एक हॉल में सब सोते थे
चिट्ठी के चट्टे अब तक थे
मैं कुछ को पढ़ आया था ।
उसी हॉल की दीवालों पर
पुरखों के कुछ चित्र लगे थे
मेरी आँखों से नीर वहा तब
मैं उन सबको ले आया था ।
पता पिता से पाया था
मैं पुरखों के घर आया था
एक गाँव के बीच बसा पर
उसे अकेला पाया था ।
(c)@दीपक कुमार श्रीवास्तव “नील पदम् “